दरवाजे खोलती कहानियाँ
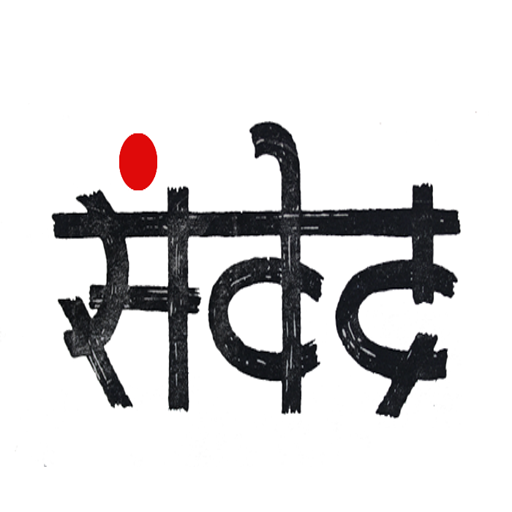
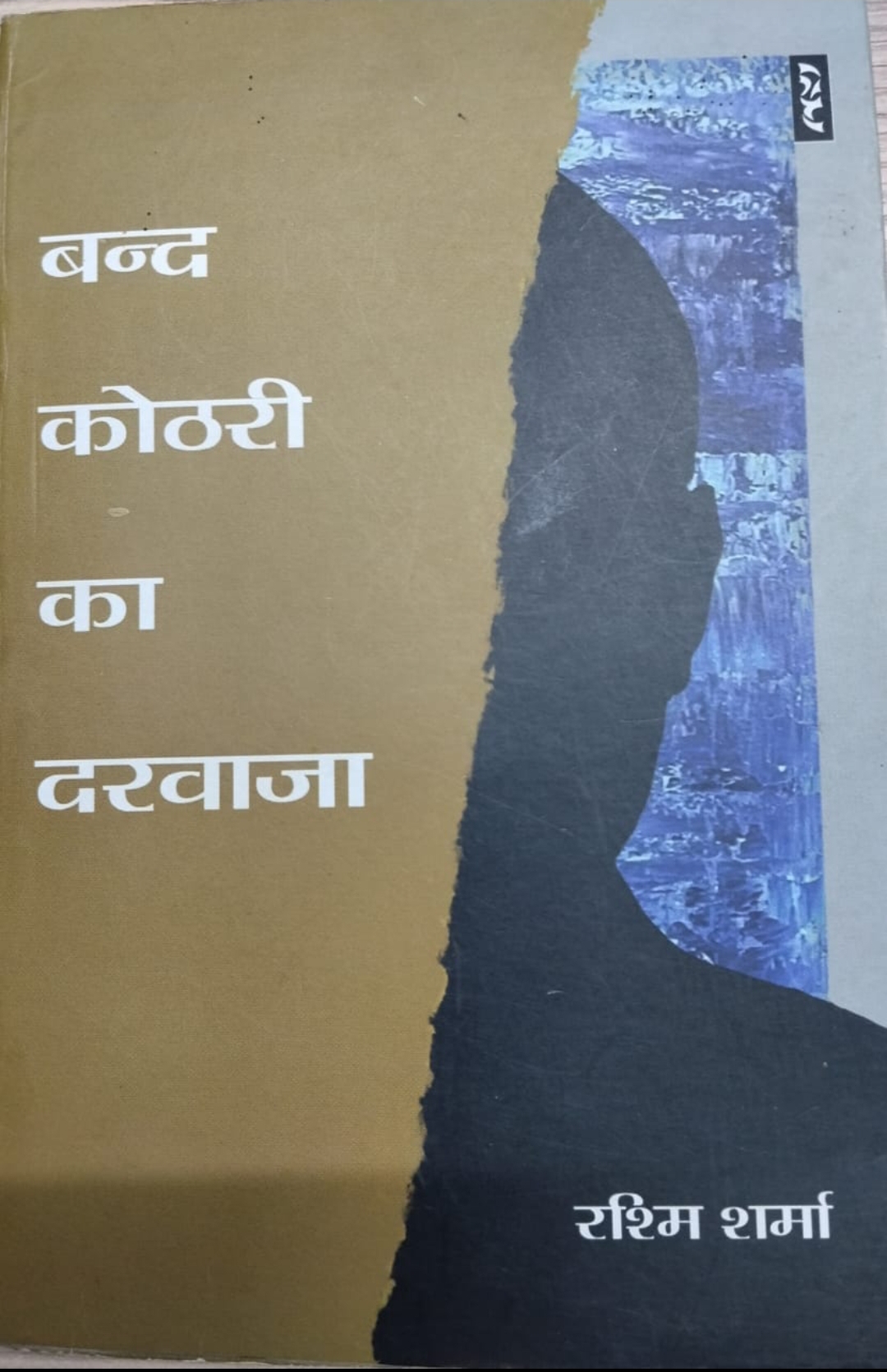
प्रकाश देवकुलिश
आज हम जिस समय से गुजर रहे हैं, उसमें रचनाकार की जिम्मेवारी बनती है कि वह सामाजिक यथार्थ को लेकर चिन्तनशील हो तथा वर्तमान से संवाद के प्रति सतत क्रियाशील और फिर इस दायित्वबोध के साथ रचना में संलग्न हो। साहित्य ही वह चिंगारी है जो विसंगति से विरोध की आग को सुलगाए रखती है। यही चिंगारी समय आने पर विस्फोट या क्रांति का रूप लेती है और समाज वांछित परिवर्तन से गुजरता है। इस दायित्वबोध का निर्वहन करती दिखाई देती हैं रश्मि शर्मा के कथा संकलन ‘बन्द कोठरी का दरवाजा’ की कई कहानियाँ – कुछ परिस्थितियों में सीधे हस्तक्षेप करती हुए तो कुछ में भावुकता के ताने बाने लेकर परोक्ष रूप से।
इस संकलन की बारह कहानियाँ एक जागरूक और सतर्क कथाकार की कहानियाँ हैं, जो समाज और परिवेश की घटनाओं के प्रति सजग हैं तो संवेदनाओं के जगत में भी अपनी पैठ बनाने में सक्षम। इसलिए इस संकलन में कहानियों की विविधता मिलती है। अपने प्रथम संकलन में ही रचनाकार ने कथा शिल्प पर अपनी पकड़ का परिचय दिया है। ये कहानियाँ अपनी सहज पठनीयता से पाठक को कहानी के आखिरी छोर तक ले जाती हैं। कहानियों में परिवेश और पात्रों के अनुकूल भाषा का ध्यान रखा गया है। यदि कहानी को ऐसा छोटा आख्यान कहा जाए जिसे एक बैठक में पढ़ लिया जाए तो रश्मि शर्मा की अधिकांश कहानियाँ इस कसौटी पर खरी उतरती हैं।
संग्रह की पहली कहानी में विरल प्रेम की सघन अनुभूति है। ‘महाश्मशान में राग विराग’ वास्तव में राग विराग की ही कहानी है। अयन का राग छोटी सी बात में विराग बन जाता है। अयन के पीछे अपराजिता का दौड़ते हुए ‘जावेद’ पुकार लेना उसे लग जाता है और अपराजिता का कश्मीर के लिए जाना वह बर्दाश्त नहीं कर पाता। इधर राग में भीगती अपराजिता अयन के इस कदम से विराग में धकेल दी जाती है। जावेद से बचपन का उसका राग आज उसके विराग का कारण बन जाता है। यह एक ऐसे असफल प्रेम की कहानी है जो पाठक के दिल को कचोटती है। लेकिन इस कहानी में कथा से भी ज्यादा जो चीज छूती है, वह है कथा का विकास और ट्रीटमेंट। घाट का किनारा, जल में काँपती परछाइयाँ, छोटी बच्ची का चुपचाप अगरबत्ती और दियासलाई रख जाना, नाव चलाने वाले लड़के का एकाकी बैठी अपरा से नाव पर घूमने के लिए पूछना और अपरा का नकारना, श्मशान की चर्चा, चिरायन्ध गन्ध – ये सब मिलकर बिल्कुल कथा के अनुरूप उदासी का एक परिवेश रच देते हैं जिससे कथा की घटना पाठक पर देर तक असर बनाए रखती है।
असफल प्रेम की एक और कहानी है मैंग्रोव वन, बल्कि ‘महाश्मशान में राग विराग’ में बने सुकोमल भावों और नॉस्टैल्जिक प्रभाव की दूसरे सन्दर्भो की प्रस्तुति है यह कहानी। ट्रीटमेंट यहाँ भी सफल और स्मृतियों में खो जाने वाली भारती के मन के भावों के अनुरूप। उस कहानी की अपराजिता की तरह भारती के प्रेम और स्मृति में भीगने का अनुकूल परिवेश यहाँ भी बनता है। अपरा गंगा तट पर खयालों में खोई है तो भारती वर्षा के झरते बूँदों की झमाझम के बीच। एक बनारस में तो दूसरी मुम्बई में। बल्कि दोनों कहानियों के पुरुष पात्रों में बेपरवाहपन या विराग भाव एक सा दिखता है। “सच कहता हूँ…… बनारस को अन्तिम ठिकाना मानकर ही आया था मैं। गंगा बहुत विशाल है। जी न लगा तो इस माँ की गोद में ही……… आखिर बनारस में मोक्ष प्राप्त करने ही तो लोग आते हैं। “…… ऐसा एक का पात्र अयन कहता है, तो दूसरे का पात्र अरिंदम कहता है “खालीपन है सीने में और है इन्तजार। उसका नहीं, मौत का। ” वैसे ‘मैंग्रोव वन’ में एक बहुत ही प्यारी सी पंक्ति है –“हम जैसे रोते रहने वालों से ही यह दुनिया खूबसूरत है।” प्रेम और स्मृति को बहुत बड़ा अनुदान है यह पंक्ति।
‘उसका जाना’ कहानी कैंसर पीड़ित माँ को खोने का दर्द बयाँ करती है। पर क्लास फ्रेण्ड सपना को देखते देखते प्रियम का माँ के ख्याल तक पहुँच जाना और माँ के पास रहते हुए सपना के ख्यालों में पहुँच जाना इस कहानी का एक नयापन है। जैसे प्रियम की माँ हर रंग में फबती हैं, वैसे सपना भी। क्लास की दोस्त से माँ और माँ से क्लास की दोस्त तक रंगों के सहारे आवाजाही कहीं न कहीं गहरी नजदीकी को एक अलग विस्तार देती है। माँ या पिता का जाना एक कटु सत्य है, पर यह जाना कैसे खाली कर देता है सन्तान को, यह कहानी इस बात को बखूबी रखती है।
‘नैहर छूटल जाए’ स्त्री अधिकार के लिए पुरजोर साहस और लड़ाई की कहानी है। शराबी पति मोहन महतो से ब्याही सिंदुरिया गाँव की लड़की कोयलिया, जिसके पिता ने उसी के नाम से कुछ जमीन खरीद रखी थी और मरने के पहले बेटों को उस खेत के मुआवजे की राशि कोयलिया को देने को कहा भी था, पहले तो भाइयों की बात मान कर पिता की मृत्यु के मुआवजे की राशि पर से अपना अधिकार छोड़ देती है, पर जब दोनों भाई उसके नाम वाले खेत की राशि भी हड़पना चाहते हैं और भाभियाँ गाँव में उसे अपमानित करती हैं तो वह लड़कर कोर्ट कचहरी के मार्फत अपना हक लेकर छोड़ती है। यह कहानी पिता की सम्पत्ति में लड़कियों के हक और खेत के लिए मुआवजे में उनके अधिकार के सरकारी प्रावधानों को रेखांकित करती है। “क्या मैं भाई होती तो मेरा हक मुझे नहीं मिलता” सोचने वाली लड़की को जब मालूम होता है कि पिता की सम्पत्ति पर लड़कियों का समान अधिकार है तो उसे बल मिलता है और सम्पति के अधिकार का मुकदमा वह जीतती है तथा कम्पनी से मिलने वाली मुआवजे की राशि का भी, दो भाइयों के साथ, तीन हिस्सा करवाती है। पितृसत्तात्मक स्थिति का जो विरोध इस कहानी का उद्देश्य है, उसमें यह बहुत हद तक सफल है।
कहानी में किस्सागोई का शिल्प है और अच्छे बिम्बों से प्रभाव पैदा किया गया है — जब विचारों में विरोध था तब बैठक के समय “अमावस की रात का अँधेरा उनके बीच भी पसर गया था” और “मानी कोयलिया तो आँगन का अमावस अँजोरिया में बदल गया। ” परिवेश के अनुकूल ‘अमावस ’ और ‘अंजोरिया’ का प्रयोग कथा – शिल्प के प्रति कथाकार की सचेतनता दिखाता है।
वैसे ,जमीन अधिग्रहण के विवाद में पुलिस और ग्रामीणों की मुठभेड़ में एक बार सत्रह साल के लड़के गोपाल और दूसरी बार सात ग्रामीणों की पुलिस की गोली से मौत जितनी बड़ी दुर्घटना है और ऐसी किसी घटना पर देशव्यापी हड़कम्प, मीडिया की गतिविधि, पक्ष-विपक्ष के नेताओं की जो सरगर्मी होती है, उसे कहानी में कहीं स्थान न मिलना कहानी की विश्वसनीयता और प्रभावोत्पादकता पर विपरीत असर डालता है।
पितृसत्तात्मकता पर ही गहरी चोट करने वाली एक और कहानी है ‘निर्वसन’, जिसमें अपनी बात के सफल सम्प्रेषण के लिए मिथ का सहारा लिया गया है। पुरुष की वर्चस्ववादी सोच पर पौराणिक कथा के बहाने जो संकेत से हस्तक्षेप किया गया है, वह प्रभावशाली बन पड़ा है। राम, जिसके लिए मर्यादा पुरुषोत्तम की छवि स्थापित-सी है, की भी मानसिकता पर प्रश्न उठाने का कौशल और साहस कथा लेखिका की क्षमता और मौलिकता का परिचय देता है। स्वर्ग सिधारे दशरथ के पिण्ड दान की प्रतीक्षा कर रहे दोनों हाथों को देख और पिण्डदान का समय निकलते जाते देख सीता द्वारा बालू का पिण्ड बनाकर पिण्डदान कर राम को पितृ कर्ज से उऋण कर देने जैसे महत्त्वपूर्ण कार्य की सराहना न कर ‘खीज, अधैर्य और अविश्वास से भर कर’ राम का खिन्न होना और सीता की बातों पर शक करना तथा यह कहना कि “पिण्डदान का अधिकार सिर्फ ज्येष्ठ पुत्र को है…….तर्पण का अधिकार तो सिर्फ पुत्र को ही दिया गया है, पुत्रवधू भला यह कैसे कर सकती है?”, उस पुरुष मानसिकता को दिखाता है जिससे हमारा समाज आज भी ग्रसित है और स्त्रियाँ विडम्बना की शिकार हैं। सीता को अपनी बात की सत्यता के लिए नदी, गाय और केतकी की झाड़ में से किसी का साथ न मिलना समाज की वैचारिक विपन्नता दर्शाता है और इस स्थिति के लिए एक तरह का क्षोभ उत्पन्न करता है। कुन्द होती मानसिकता के बीच भी कथाकार ने उम्मीद जगा रखी है। बटवृक्ष का स्वयं आगे बढ़ कर राम को सच बतलाना और लंका में अशोक वन के समीप बहती महाबली गंगा द्वारा कहना कि “खुद को कभी अकेली मत समझना सीता!” स्थापित करता है कि निराशा के बीच आशा की किरणों की तरह विवेक का साथ देने वाले तत्त्व भी समाज में मौजूद हैं ।
फल्गू की हिलोरों से उठती आवाज के द्वारा नदी का मानवीकरण, सीता का बार बार भावुक होकर अतीत में खोना कहानी की अतिरिक्त सुन्दरता है जो कथा के विकास में सहायक है। इन प्रयोगों के कारण यह कहानी कथ्य और शिल्प दोनों पहलूओं में सटीक उतरती है और लेखिका की कहानी-लेखन की सफल यात्रा का संकेत देती है।
एक कहानी है — ‘घनिष्ठ-अपरिचित’. रिटायर्ड श्वसुर के पार्किंसन से शिकार होने के साथ साथ वहम के दौरे ने बहू सोनल का जीना मुश्किल कर दिया। कभी चोर तो कभी साँप का भ्रम पालते पालते सोनल के श्वसुर को भ्रम हो जाता है कि उनकी बहू उन्हें मरवा डालना चाहती है जबकि बहू उन्हें पिता समान मानती है। पूरा परिवार अशान्त हो जाता है। सोनल अपने श्वसुर से दूरी बरतने लगती है। सोनल के पति सौरभ को कभी सोनल को तो कभी बाबूजी को समझाते एक अजीब से पशोपेश में जीना पड़ रहा है। इन्हीं परिस्थितियों को बुनती यह घटना प्रधान कहानी एक व्यस्त जीवन जीने वाले के अवकाश प्राप्त समय की परिणति को सामने लाती है।
आए दिन हत्या, बलात्कार की खबरें बाल मन को किस तरह दुष्प्रभावित करती हैं, और उस पर कैसा मनोवैज्ञानिक असर पड़ सकता है , कहानी ‘हादसा’ इसे प्रभावी ढंग से रखती है। बाल मनोविज्ञान पर ही कहानी है ‘लाली’ ।
गाँव में डायन के अन्धविश्वास के पीछे के सच को उजागर करती है कहानी ‘मनिका का सच’।
‘जैबो झरिया, लैबो सड़िया’ दिहाड़ी पर खटते धनिया और जीतन की करुण कहानी है, जो ज्यादा कमाई की लालच में राँची के रातू का इलाका छोड़ झरिया चले जाते हैं, ताकि वहाँ के कोयला खदानों में हो रही गैरकानूनी खुदाई में शामिल होकर ज्यादा कमा सकें। कोयला खदानों से जुड़े गैरकानूनी क्रियाकलापों का भण्डाफोड़ करती इस कहानी का समापन एक दिन अचानक जीतन के जमीन फटने के कारण गोफ(जमीन के अचानक फट जाने से बना बहुत गहरा गड्ढा) में समा जाने से होता है। आग की भट्ठी पर खड़े झरिया में ऐसी घटना आम है जिसे जानते हुए भी जान की बाजी लगाए मजदूर वहाँ खट रहे हैं और प्यार से लाई नयी साड़ी को पहन कर सुख मनाने का धनिया जैसी औरतों का सपना उनके उनके ‘जीतन’ की मौत के साथ आँसुओं की धार में बदल जाता है। जगजाहिर मौत की इस खाई की तरफ व्यवस्था का ध्यान खींचने की इस कहानी में प्रभावी तत्त्व हैं।
एक उम्रदराज विधवा के सूनेपन और अकेलेपन की कहानी है ‘चार आने का सुख’ । एक ओर अकेलेपन से उपजी कर्कशता और दूसरी ओर बाल सुलभ उत्सुकता और छोटी छोटी इच्छाओं के बीच टकराती यह कहानी सरसता को तरजीह देती है। उस विधवा के लिए बड़ी माँ की जगह बोलचाल में ‘बड़ा’ शब्द का रूढ़ हो जाना कहानी को स्वाभाविक बनाता है।
संग्रह की अन्तिम कहानी ‘बन्द कोठरी का दरवाजा’ नये विषय को छूती है। समलैंगिकता आज के समय में ऐसा विषय है जो वैधानिकता और सामाजिक स्वीकार्यता के बीच झूल रहा है। अपने पहले ही संग्रह में कथाकार ने ऐसे विषय को छूने का साहस किया है और अभी इस विषय की अग्राह्यता ने पारिवारिक परिवेश को जिस असमंजस में डाल दिया है, उसे रेखांकित किया है। कहानी की मुख्य पात्र नसरीन बिट्स पिलानी से इंजीनियरिंग पास और अब एक सरकारी महकमे में नौकरी कर रहे पति के समलैंगिक होने की जानकारी पाती है बल्कि वह अपनी आँखों से सबकुछ देख लेती है। शादी के बाद से ही पति के साथ चल रहे अस्वाभाविक रिश्ते की पोल खुल जाती है और उसका जीवन अन्धकारमय हो जाता है। नसरीन का संस्कृत में बी ए होना और अब संस्कृत में ही एम ए होकर संस्कृत की शिक्षिका बनने का ख्वाब पालना इस पात्र को विशिष्ट बनाता है–“वैसे भी किसी मुस्लिम लड़की के संस्कृत पढ़ने की बात सुनकर लोग-बाग उसकी ओर हैरत भरी नजरों से देखते हैं और वह ऐसे में बहुत खास होने के एहसास से भर जाती है। ” सम्भवतः कुछ खास होने के कारण ही नसरीन रेहान के गिड़गिड़ाने पर उससे सहानुभूति रख पाती है और जीवन की विडम्बना से समझौते की कोशिश करती है पर धारा 377 के नये प्रावधान उसके जीवन में नयी उम्मीद जगाते हैं। कथाकार ने इस विषय को उठाकर यों ही नहीं छोड़ा है। कहानी का अंश है – “चश्मे से झाँकती रूबीना(डॉ.) की अनुभवी आँखें नसरीन पर टिकी हैं…..समझने की कोशिश कीजिए। यह कोई रोग नहीं है जिसका इलाज हो सके। यह मनोवृत्ति है। इसे बदलना लगभग असम्भव है। ”
सम्भवतः यह विषय का नयापन ही है जिसने इस कहानी को थोड़ा अतिरिक्त विस्तार दे दिया है। सघनता हर रचना, चाहे वह कविता हो या कहानी, की उत्कृष्टता के लिए आवश्यक शर्त है। जब रचनाकर इसके प्रति सजग रहता है तो रचना अतिरिक्त सौन्दर्य पाती है और पाठक कहानी से अलग नहीं हो पाता।
‘बन्द कोठरी का दरवाजा’ संग्रह ऐसे कई दरवाजे खोलता है जिससे समस्याओं पर पड़ती रोशनी उन्हें और उजागर करती है ताकि उन्हें इग्नोर न किया जा सके। संग्रह की प्रायः कहानियों में सहजता और सरलता देखी जा सकती है जिसके प्रति कथाकार का सजग होना आवश्यक है क्योंकि इससे शिल्प के इस पार या उस पार हो जाने का खतरा बना रहता है, वैसे यह ‘सहजता’ रश्मि शर्मा के अपने शिल्प और कौशल के रूप में भी जगह पा सकती है। पूरे संग्रह में कथाकार का कथा के विकास में पात्र, परिवेश, कथ्य के प्रति सचेत और सतर्क होना दिखता है। जो कहानियाँ ग्रामीण परिवेश की हैं वहाँ अंचल की बोलचाल की भाषा एवं शब्दों जैसे – भिनसरिये, लेदरा, टुअर -टापर, जांगर, साड़ी पिन्धैबौ, खोंइछ, नपइया, रोते-काँदते, लुगा, छेगरी- के प्रयोग कथा के परिवेश को स्वाभाविक और प्रामाणिक बनाते हैं।
किसी भी कहानी का आधार कोई घटना ही होती है और कथाकार उसे ही कहानी में रखता भी है, पर एक सजग कथाकार उस घटना को कथा में चलते चले जाने के लिए नहीं छोड़ देता, बल्कि कभी परिवेश रचकर और उसे कथा से युक्त कर, कभी कथा के अनुकूल प्रकृति के वैविध्य की तलाश कर, कभी कथा में काव्य सी संवेदना पिरोकर घटना के साथ स्वयं उपस्थित रहता है और उसे कहानी में बदल देता है। घटना को कहानी के साँचे में ढालने की यह चिन्ता इस संकलन में मिलती है।
यह संग्रह एक नये और उभरते सक्षम कथाकार के कथा जगत में प्रवेश का दरवाजा इस ढंग से खोलता है कि इस रचनाकार द्वारा कहानी की विरलता और सघनता, कथा संसार में आवश्यक नर्म हवा और तेज धूप दोनों के पुष्टि की पुरजोर सम्भावना बनती है।
कथा संग्रह : बन्द कोठरी का दरवाजा
कथाकार : रश्मि शर्मा
प्रकाशक: सेतु प्रकाशन
मूल्य :260/-
———————————————————–

लेखक प्रतिष्ठित कवि और ‘सबलोग’ पत्रिका के संयुक्त सम्पादक हैं।
मो. 9279118427
shreeprakash.sh@gmail.com
