साक्षात्कार
रंगमंच व्यवसाय नहीं है
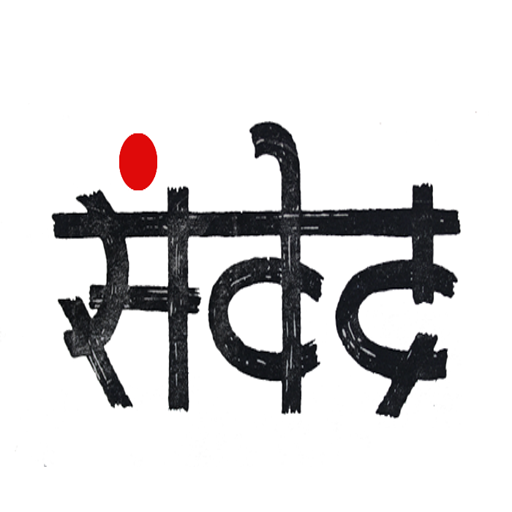
- उषा गांगुली
सन् 1970 ई– के बाद रंगकर्म की दुनिया में प्रवेश करने वाली उषा गांगुली के लिए आज तक थियेटर कोई व्यवसाय नहीं बल्कि संघर्ष और साधना है । हिन्दी और बांग्ला में समान रूप से यह साधना अनवरत जारी हैं वे मानती हैं कि तेजी से बदल रही दुनिया में रंगमंच की भूमिका और भी ज्यादा कारगर सिद्ध हुई है । क्योकि, रंगमंच बाजार के खिलाफ है । वैसा, बाजार जहाँ मानवीय सरोकारों से जुड़ी तमाम चीजें बेची जा रही हों और उसे खरीदा भी जा रहा हो । वे सीधे कहती है कि रंगमंच, फिल्म नहीं है जो पैसा देगा । अगर आपको धन चाहिए, तो फिल्मों में जाइए, टी–वी– सीरियल में काम कीजिए । रंगकर्म का दरवाजा इन सबकी इजाजत नहीं देतां यह तो सिर्फ संघर्ष, मेहनत और कला की दुनिया है, धन की नहीं । थियेटर धन तभी देगा, जब वो बाजार के साथ समझौता करेगा । भारतेन्दु से लेकर आज तक का इतिहास पलट लीजिए तो आप यही पाएँगे कि उसने कभी बाजार के साथ समझौता नहीं किया हैं वह बाजार को कभी महत्त्व नहीं देता । भूमण्डलीकरण के दौर में रंगमंच के सामने कई चुनौतियाँ हैं । चाहे वह किसी भी भाषा समाज का रंगमंच हों । रंगमंच, रोजगार नहीं दे सकता, धन नहीं दे सकता, ‘हाईप्रोफाइल’ जीवन–शैली नहीं दे सकता लेकिन रंगमंच इतना जरूर कर सकता है कि वह, आपको मानवीय एवं सामाजिक सरोकारों से जोड़े रख सकता है । देखा जाए तो चुनौतियाँ कहाँ नहीं है ? बड़ी–बड़ी उपलब्धि लेकर भी छात्र व युवा वर्ग बेरोजगारी की कतार में खड़े हैं । लेकिन वे दिन–रात प्रयासरत हैं, संघर्षरत हैं और युवा पीढ़ी इन चुनौतियों को हमेशा से स्वीकार करती आयी हैं । वे, हमेशा से आगे बढ़कर अपनी प्रतिभा का परिचय देते हैं । अपने हौसले को टूटने नहीं देते । यही समझ लीजिए कि चुनौतियाँ यहाँ भारी नहीं पड़ती, यदि उनका इरादा मजबूत है तो । रही बात हिन्दी रंगमंच की तो आप यह देख सकते हैं कि तमाम चुनौतियों के बाद, तमाम जानकारियों के बाद, समस्या से वाकिफ होने के बाद भी नयी पीढ़ी लगातार इनसे जुड़ रही है । देश के कोने–कोने में नाटक में रुचि रखने वाली पीढ़ी आपको मिल जाएँगी । इन सबके साथ जब आप तकनीकि विकास की बात करते हैं तो दुनिया बदलने के साथ–साथ रंगमंच की दुनिया में भी तकनीकी सामग्री और तत्वों का प्रवेश हो रहा है । यह अलग बात है कि कभी–कभी यह कुछ ज्यादा हावी हो जाता है और हिन्दी रंगमंच की दुनिया इसमें पीछे रह जाती है । यह भले ही परिवर्तित समय के साथ न चल पा रहा हो पूरी तरह लेकिन, इतना जरूर है कि परिवर्तित समय में दुनिया के सामने, समाज के समक्ष जो भी चुनौतियाँ आ रही है, चाहे वह आर्थिक असमानता हो, लिंग भेद हो, जातिवाद हो, साम्प्रदायिकता हो, सामन्तवाद हो, आधी आबादी (स्त्री उत्पीड़न) का मसला इत्यादि सभी समस्याओं को आज का रंगमंच प्रमुखता से उसे प्रस्तुत कर रहा है । लोगों को जागरुक बना रहा है । इसीलिए, मैं यह नहीं मानती कि समय के साथ चलना है तो तकनीकि विकास के आधार पर ही चलना होगा बल्कि, मेरा मत है कि समाज और राष्ट्र के समक्ष जो समस्याएँ सामने आए उसे रंगमंच के द्वारा सामने लाया जाए और इसे लाया भी जा रहा है सिर्फ हिन्दी रंगमंच में ही नहीं तमाम भाषाओं के रंगमंच में आप इनकी झलक पा सकते हैं ।
हिन्दी नाटक लेखन में आयी भारी कमी को उषा जी चिन्तित होकर स्वीकारती हैं । उनका मानना है कि नाटक लिखना जो कम हो गया है, उसकी कई वजहें हैं । एक वजह तो यह भी है कि आज साहित्यकारों की पीढ़ी में वैसे लोगों का अभाव है जो रंगमंच की पूरी तरह समझ रखते है । यही कारण है कि रंगमंच की दुनिया से जुड़े लोग खुद अपने हिसाब से नाटक तैयार करते हैं । आज नाटक प्रदर्शन के कई माध्यम हैं और स्रोत भी । कहानी, कविता उपन्यास, व्यंग्य रचना इत्यादि से नाटक तैयार हो रहे है । रहा प्रश्न नाट्यालेखों में अपने समय के रूखड़े यथार्थ को आत्मसात करने की जो बेशक, हिन्दी का रंगमंच इसमें सक्षम है । पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि आज तक रंगमंच ने बाजारवादी व्यवस्था के आगे घुटने नहीं टेके हैं । अब जब इसके खिलाफ जाने की हालात बनी है तब–तब रंगमंच इसके खिलाफ तैयार हुआ हैं नाटक के साथ एक पुरानी कहावत – ‘लोटा बेचो और नाटक करो, हमेशा से चरितार्थ रही है । आज दुनिया बड़ी तेजी के साथ बदल रही हैं टी–वी–, सिनेमा, सीरियल, इंटरनेट तमाम तरह के मनोरंजन के साधन उपलब्ध है जहाँ चौबीस घंटे रंगारंग कार्यक्रम जारी रहते हैं बावजूद इसके अपने अनुभवों के आधार पर यह कह सकती हूँ कि एक अच्छे नाटक की आप प्रस्तुति करते हो तो भीड़ जरूर आपको देखने, समझने और विचारने आती है । हाँ, प्रभावित तो करता है । ज़ाहिर सी बात है एक तरफ ‘गैलैमर’ की अनगिणत ताकतें हैं तो दूसरी ओर रंगमंच अकेला हैं लेकिन, जब दोनों का अनुपात निकालेंगे तो रंगमंच की दुनिया आपको ज्यादा ताकतवर नज़र आएँगी ।
दरअसल, नाटक सामाजिक सरोकारों और नैतिक मूल्यों के पक्ष में हमेशा से खड़ी रहे हैं वह हमेशा से सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करना जानता है । हाँ, उसके माध्यम और स्तर भले ही अलग–अलग हैं । नुक्कड़ नाटक, एकल रंगमंच इत्यादि अनेक माध्यम हैं जहाँ नाटक लोगों को समाज, राष्ट्र और कला के प्रति दायित्व का बोध कराता है । नाटक यह बोध कराने की कोशिश करता है कि समाज, राष्ट्र और कला के प्रति भी हमारा दायित्व है । निजी दुनिया के अलावा समाज और राष्ट्र की जिम्मेवारी भी हमारी जिम्मेवारी है ।
चाहे हालात कितने भी बुरे हों, परिस्थिति कितनी भी नकारात्मक हो, सृजन की दुनिया चकाचौंध से भर गयी हो लेकिन रंगमंच की दुनिया ने अब तक सब कुछ बचाकर रखा है । नाटक को व्यापक स्तर पर फैलाने के लिए यह व्यवस्था भी होनी चाहिए कि इसे पाठ्यक्रम से जोड़ा जाए । नाटक, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि, मंचित करने के उद्देश्य से पाठ्य–सामग्री का हिस्सा बने । सरकार को चाहिए कि शिक्षण संस्थानों में, विश्वविद्यालयों में उसके लिए विभाग खोले जाएँ । प्राध्यापकों, शिक्षकों की वेतन और बुनियादी सुविधाओं के साथ नियुक्ति हो । अगर नाट्य दल मंचन के लिए देश से बाहर जाएँ तो सरकार उनकी आर्थिक मदद करें ।
ऐसा होने से निश्चित रूप से नाटक के क्षेत्र में एक क्रान्ति आएगी । हिन्दी रंगमंच का वर्तमान और भविष्य दोनों संघर्षों से भरा जरूर है लेकिन काफी उज्ज्वल है । मैं नहीं मानती कि इसको लेकर निराश होने की कहीं से भी जरुरत है ।
(अश्विनी कुमार से बातचीत पर आधारित)
उषा गांगुली – जन्म 20 अगस्त, 1945, जोधपुर, राजस्थान । लम्बा, व्यापक और गहरा रंग–अनुभव । सुप्रसिद्ध निर्देशक, अभिनेत्री, रूपान्तरकार व परिकल्पक । नृत्य नाटकों में विशेष ख्याति । ‘रंगकर्मी’ नाट्य–संस्था की स्थापना । 2000 में ‘समन्वय’ नामक कार्यक्रम में देश–भर की महिला रंगकर्मियों को एक मंच पर इकठ्ठा कर संवाद का आयोजन । बांगला भाषी दर्शकों को हिन्दी नाटकों के प्रति आकृष्ट करने में अहम् भूमिका ।

