संघर्ष और समन्वय की कहानियाँ

अब्दुल बिस्मिल्लाह के चार कहानी संग्रहों को एक साथ मिलाकर 2014 में ‘ताकि सनद रहे’ के नाम से प्रकाशित किया गया है। इसमें सनद वाली बात ये है कि निम्नवर्गीय समाज, हिन्दू-मुस्लिम सम्बन्ध की बहुपरतीय जटिलता, स्त्री-संसार के बहुविध रूप, प्रेम और उससे जुड़ी तीखी विफलताएं, बेरोजगारी के डंक और इन सबके पीछे की राजनीति को कहानीकार किसी किस्सागो की तरह समाज को सुना रहा है। इस रचनात्मक बयान का देश-काल गालिबन 1970 से 2010 के आसपास का हमारा भारत है।
अब्दुल बिस्मिल्लाह मूलतः निम्न वर्ग के संघर्ष के कहानीकार हैं। उन्होंने आजादी के बाद उन्नीस सौ सत्तर के दशक से लेकर इक्कीसवीं सदी के पहले दशक के समाज का चित्रण अपनी कहानियों में किया है। जिसमें कभी-कभी मध्य वर्ग और अभिजात्य वर्ग के जीवन और समस्याओं की भी झलक दिखलाई पड़ती है। ग्रामीण, कस्बाई और अविकसित शहरी समाज में जीने के लिए मामूली जरूरतों को पूरा करने का संघर्ष इन कहानियों की एक मुख्य चिंता कही जा सकती है। अभाव और भूख अनेक कहानियों के केंद्र में हैं। प्रकारांतर से ये कहानियाँ अभाव और भूख को पैदा करने वाले शोषकों और शोषण के विभिन्न रूपों के बारे में भी हैं। जीने के लिए मामूली जरूरतों में एक नौकरी या निश्चित आमदनी है जिससे परिवार का महीने भर का खर्च चल सके। इस जरूरत को पूरा न कर पाने की स्थिति में इन कहानियों के अनेक पात्र अपनी पूरी ताकत लगाते और विफल होते हैं। कई बार अपने बच्चों को भी गरीबी के कारण अपने से दूर करते दिखते हैं। जिसे गरीबी रेखा से नीचे का जीवन कहा जाता है वह इन कहानियों की एक प्रमुख विषय-वस्तु है। इसमें बेरोजगारी की समस्या जुड़ी हुई है। इससे अधिकतर युवा-पात्रों का जीवन कठिनाई से बीत रहा है।
इन कहानियों की दूसरी प्रमुख चिंता हिन्दू-मुस्लिम सम्बन्ध है। कुछ लोगों के लिए हिन्दू-मुस्लिम धर्म एक अभेद्य दीवार से अलग की गई दो जीवन शैलियाँ हैं। जैसे ‘अतिथि देवो भव’ के हिन्दू दंपति के लिए। वहीं हिन्दू-मुस्लिम जीवन में समन्वय की उम्मीद दिखलाती ‘आधा फूल आधा शव’ जैसी कहानियाँ भी हैं। ‘दूसरा सदमा’ जैसी कहानियों में हिन्दू-मुस्लिम जीवन में आई दूरी का ही सदमा दिखाई देता है। किस प्रकार हिन्दू और मुसलमान मिलकर एक साथ प्यार से रह सकें इसकी अंतरप्रवाही संवेदना इन कहानियों में दिखती है।
स्त्री-जीवन के संघर्ष इन कहानियों की तीसरी प्रमुख चिंता है। गरीबी और सांप्रदायिकता की समस्या में भी स्त्री जीवन की कठिनाई बढ़ जाती है। अनेक स्त्री-पात्रों के कष्टों को इन कहानियों में चित्रित किया गया है। पति और उसके परिवार द्वारा अपमानित और पीड़ित की जा रही स्त्रियाँ इन कहानियों में खूब दिखलाई देती हैं। पति अकारण ही उनको पीटता है। घर से निकल जाने के लिए कहता है। घर से निकाल कर उसके दुखी जीवन को देखने और उसे नीचा दिखाने के लिए प्रयास करता है। भारतीय समाज में स्त्रियों की दशा को भी इन कहानियों में देख सकते हैं।
इन तीन प्रमुख चिंताओं के अलावा मानव-सम्बन्धों में लालच और कपट की भूमिका को अनेक कहानियों में चित्रित किया गया है। सम्बन्धों की ऊष्मा का अभाव भी एकाधिक कहानियों का विषय है। सम्बन्धों में धन की भूमिका पर अनेक कहानियाँ लिखी गई हैं।
प्रेम-सम्बन्धों के कई रूप हो सकते हैं। उनके असफल होने की भी अनेक कहानियाँ अब्दुल बिस्मिल्लाह ने लिखी हैं। गरीबी और बेरोजगारी की समस्या भारत के किसी एक धर्म अथवा समाज तक सीमित नहीं है। इसी तरह शोषण की मार भी केवल कोई एक विशेष धर्म नहीं सह रहा है। शिक्षा की रोशनी से समाज को एकजुट करने की जरूरत भी प्रायः सभी धर्मों और वर्गों के लोगों को है। अब्दुल बिस्मिल्लाह की कहानियों की टेक केवल धर्म के आधार पर किया जाने वाला अत्याचार ही नहीं है। सांप्रदायिकता की समस्या और समन्वय की आवश्यकता पर भी वे यादगार कहानियाँ लिख चुके हैं। दो लोगों के बीच के प्रेम को भी विभिन्न रूपों में उन्होंने अनेक कहानियों में दर्शाया है। बीसवीं शताब्दी के अंत में आए नव-पूँजीवाद अथवा भूमंडलीकरण पर भी प्रतीकात्मक रूप में ‘माटा-मिरला की कहानी’ जैसी मारक कहानी उन्होंने लिखी है।
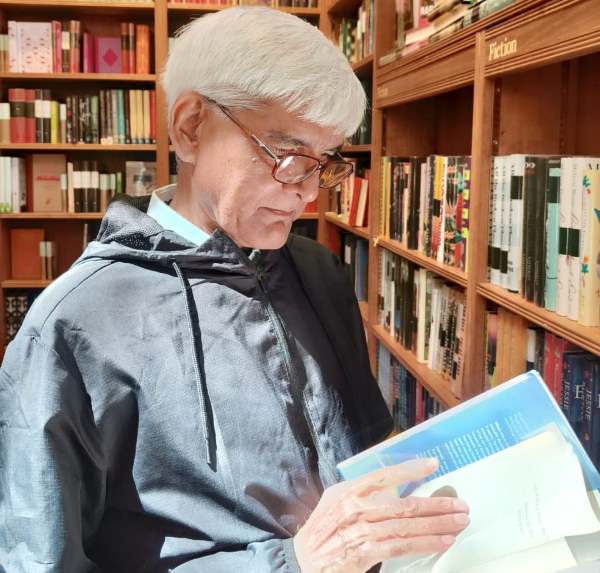
लेखक के अब तक सात कहानी-संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इन सात कहानी-संग्रहों के नाम हैं- ‘टूटा हुआ पंख’ 1981, ‘कितने कितने सवाल’ 1984, ‘अतिथि देवो भव’ 1990, ‘जीनिया के फूल’ 1991, ‘रैन बसेरा’ 1993, ’रफ रफ मेल’ 2000, और नवीनतम संग्रह ‘शादी का जोकर’ 2013 हुआ था। इनमें से चार संग्रहों (‘टूटा हुआ पंख’, ‘कितने कितने सवाल’, ‘जीनिया के फूल’, और ‘रैन बसेरा’) की सभी कहानियों को एक साथ मिलाकर ‘ताकि सनद रहे’ कहानी-संकलन 2014 में प्रकाशित हो चुका है।
इस लेख में उनके सभी सातों कहानी-संग्रहों को आधार बनाकर अपनी पाठकीय प्रतिक्रियाएँ दर्ज करना चाहूँगा। इन सात कहानी-संग्रहों में कुल एक सौ चौदह कहानियाँ हैं। इन सभी कहानियों का सार और विश्लेषण करना यहाँ मुश्किल होगा। पहले चाहता तो यही था कि सभी कहानियों पर बात करूँ। लेकिन सभी कहानियाँ पढ़ने और उनका सार लिखने के बाद लगा पृष्ठ संख्या काफी ज्यादा हो गई। इस लेख में दस पन्नों में ही अपनी बात मुझे कहनी है। इसलिए इस लेख में उन कहानियों का ही विशेष रूप से जिक्र करूँगा जिन्हें लेखक ने बतौर अपनी ‘विशिष्ट कहानियाँ’ दर्ज किया है और प्रकाशित करवाया है अथवा उन कहानियों को भी शामिल करूँगा जिन्हें एक पाठक के तौर पर हम सबको पढ़ना चाहिए।
कुछ ऐसी कहानियाँ छूट भी सकती हैं जो अन्य लोगों को बहुत प्रभावशाली लगी हों लेकिन मुझे नहीं लगीं। लेखक की सभी कहानियों में से ‘अतिथि देवो भव’, ‘खाल खींचने वाले’ और ‘शीरमाल का टुकड़ा’ ये तीन कहानियाँ मुझे बेहद प्रभावशाली लगीं। हिन्दू-मुस्लिम सम्बन्ध, शोषण और भूख इन कहानियों के विषय कहे जा सकते हैं।
अब्दुल बिस्मिल्लाह की कहानियों और उनके लेखन की विशेषताओं को दर्ज करते हुए आलोचक मधुरेश ने लिखा है- “अपने अनेक समकालीन लेखकों-असगर वजाहत, नासिरा शर्मा, मंजूर एहतेशाम आदि की तरह अब्दुल बिस्मिल्लाह ने मध्यवर्गीय मुस्लिम समाज के अंतरंग जीवन के विश्वसनीय अंकन के साथ ही हिन्दू समाज को केंद्र में रखकर भी समान अधिकार के साथ लिखा है। राजनीतिक अवसरवाद, मानवीय सम्बन्धों पर धन के वर्चस्व की प्रवृत्ति, वंचित या उपेक्षित वर्ग के जीवन की बहुविध समस्याएँ तथा दलित-वर्ग में घटित बदलाव आदि को केंद्र में रखकर अब्दुल बिस्मिल्लाह ने अनेक उल्लेखनीय कहानियाँ लिखी हैं।” (वाङ्मय पत्रिका, अक्टूबर-दिसम्बर 2015, संपादक डॉ. एम. फ़ीरोज़ अहमद, लेख ‘हाशिए के लोग और अब्दुल बिस्मिल्लाह की कहानियाँ’, मधुरेश, पृष्ठ 79)
‘दरबे के लोग’ कहानी में एक लड़का लकड़ी का बुरादा लेने एक जगह आता है। उस बुरादे से चूल्हा जलता है और उसकी माँ उससे खाना बनाती हैं। वहीं बुरादे वाली जगह एक लड़की मिलती है। उसका नाम खुतेजा है। उसके पिता साड़ी बनाने का काम करते हैं। उनके इस काम के कारण उनके ठेकेदार को पुरस्कार भी मिल चुका है। वह लड़का उस लड़की के घर भी जाता है। उसके प्रति आकर्षित होता है। कई बार उसी जगह वह लड़का उस लड़की से मिलता है। दोनों की जरूरतें यानी बुरादा दोनों के बीच अपनापन पैदा करने का माध्यम बनता है। दोनों के घर में अभाव है। लेकिन लड़की की आर्थिक स्थिति उस लड़के की आर्थिक स्थिति से ज्यादा खराब और नाजुक है। ऐसे ही मिलने के बाद एक बार वह लड़की बुरादे वाली जगह नहीं मिलती है। वह लड़की को खोजता हुआ उसके घर जाता है तो पता चलता है कि दरबे में रहने वाले वे लोग और लड़की जा चुकी है। उसके पिता के ठेकेदार उस पर बुरी नज़र रखते थे। जिससे बचने के लिए वे उस दरबे को छोड़कर चले गए। खुतेजा तलाकशुदा लड़की है। वह अपने अत्याचारी पति के साथ न रहकर अपने पिता के घर आकर रहती है। उसकी गरीबी और दुरावस्था का लोग लाभ उठाना चाहते हैं। उसके पिता का ठेकेदार जब ऐसा कुछ करने की सोचता है तो खुतेजा अपने परिवार के साथ उस जगह को छोड़कर ही चली जाती है।
स्त्री के प्रति पुरुष समाज का अत्याचारी व्यवहार किसी भी रूप में असहनीय है। भले ही इसके लिए अपने घर, पति और रोजगार को भी क्यों न छोड़ना पड़े। यहाँ भी अब्दुल बिस्मिल्लाह इस कहानी में खुतेजा और उसके परिवार का उस दरबे को छोड़कर जाने का जो कदम दिखाते हैं वह उनके स्त्री सम्बन्धी विचारों को दर्शाता है। वे शोषण को बदलने वाली व्यवस्था अथवा वहाँ से चले जाने के कदम को अपनी कहानियों में दिखाने का रास्ता चुनते हैं। ‘शत्रु’ कहानी में भी कन्नो अपने अत्याचारी पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर चली जाती है। ‘पुरानी हवेली’ कहानी में सभी लड़कियाँ मिलकर उस हवेली की संरक्षिका के खिलाफ आंदोलन करती हैं। उस हवेलीनुमा जेल से बाहर निकलती हैं।
गरीबी, बेरोजगारी और सांप्रदायिकता की समस्या इन कहानियों में बार-बार लक्षित होती हैं। इन समस्याओं के अलावा स्त्री समस्या को भी कई कहानियों में दिखाया गया है। ‘दरबे के लोग’, ‘शत्रु’ ‘पुरानी हवेली’ और ‘तलाक के बाद’ कहानियों में तीन स्त्रियाँ हैं। खुतेजा, कन्नो, पुरानी हवेली में बंद औरतें, और साबिरा को उनके आसपास के लोग किसी न किसी रूप में पीड़ित और भयभीत करते हैं। उन्हें पुरुष समाज से डर, अपमान और शोषण के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है।
‘खाल खींचनेवाले’ कहानी में भुनेसर मरे हुए पशुओं की खाल निकालकर बेचता है। रघुनाथ तिवारी का बैल मर गया तो उसे खबर की गई। वह भूखा-प्यासा जल्दी से उस जगह पहुँचा। देर हो गई तो चील-कौवे उस मृत बैल की खाल खराब कर देंगे। वह बहुत मुश्किल से बिना रुके अकेले उस बैल की खाल उतारता है। उसे बाजार लेकर जाता है। अगर खाल में कोई खराबी नहीं होती है तो अच्छे पैसे मिल जाते हैं। वह अपनी खाल के लिए तीस रुपए माँगता है उसे लोग बीस रुपए देने की बात कहते हैं। वह उन्हें खाल नहीं बेचता है। फिर वहाँ के बड़े व्यापारी बड़े मियाँ की ओर जाते हैं। वे उससे काम करवाते हैं और फिर शाम को उसे पंद्रह रुपए देते हैं। वह कुछ नहीं कह पाता है। मन में जरूर पहले सोचता है कि “हम लोग तो मुर्दा जानवरों की खाल उतारते हैं, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जिंदा आदमियों की खाल खींचते हैं और उन्हें दर्द तो दूर, घिन भी नहीं लगती।” (अब्दुल बिस्मिल्लाह की विशिष्ट कहानियाँ, शीर्षक प्रकाशन, संस्करण 1986, पृष्ठ संख्या 22)।

श्रम की वास्तविक कीमत और सम्मान ‘दरबे के लोग’ कहानी में खुतेजा के पिता और परिवार को भी नहीं मिलती है। मालिक-वर्ग मजदूर को इतने पैसे ही देना चाहता है जिससे वह मरे भी नहीं और सम्मान से जिए भी नहीं। उसका कोई विरोध भी समाज की गरीबी और अशिक्षा के कारण सामने नहीं आ पाता है। अगर कोई व्यक्ति मालिक-वर्ग के शोषण का विरोध करने के लिए खड़ा हो जाता है तो उसे ‘यह कोई अंत नहीं’ कहानी के गुलाम सरवर की तरह मरवा दिया जाता है। अब्दुल बिस्मिल्लाह अपनी कहानियों में शोषण को चुपचाप सहने वालों पात्रों को नहीं रचते हैं। भले भी वे कुछ न कर सकें लेकिन विरोध का विचार जरूर उनके मन में पैदा कर देते हैं। जैसे ‘खाल खींचने वाले’ कहानी में भुनेसर का यह वाक्य “हम लोग तो मुर्दा जानवरों की खाल उतारते हैं, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जिंदा आदमियों की खाल खींचते हैं।” उस अंतहीन शोषण में एक छोटे पत्थर की तरह यह वाक्य अपने पाठकों ने मन के ठहरे हुए पानी में भी एक हलचल पैदा करता है।
‘फौलाद बनता आदमी’ कहानी में दुलारे एक राजनेता दुर्गाचरण के यहाँ नौकर है। उसको उसके पिताजी ने यहाँ भेजा है। वह पढ़-लिखकर अच्छा आदमी बनना चाहता है। वह दुर्गाचरण का नौकर नहीं बनना चाहता था। लेकिन यहाँ उसे सिर्फ लोगों की सेवा में लगा दिया गया है। वह लोगों का शरीर भी दबाता है। उनकी मालिश करता है। वह एक दिन दुर्गाचरण को दरोगा की मालिश करने से मना कर देता है और काम से निकाल दिया जाता है। अपनी स्थिति को न बदल पाने के कारण वह इस काम और जगह को छोड़ देना बेहतर समझता है। अगर वह अपनी स्थिति से समझौता कर लेता और वहीं लोगों की सेवा में दिन बिताना ठीक समझता को संभव है उसे खाने-पीने की कोई समस्या न आती लेकिन वह पढ़-लिखकर समर्थ बनना चाहता है। इसलिए दुलारे उस काम को छोड़ देता है जिसमें उसके आत्म-सम्मान को ठेस लगती है।
‘तीर्थयात्रा’ कहानी में परदीप अपनी माँ को तीर्थयात्रा पर प्रयागराज लेकर जा रहा है। उसकी माँ पारवती काकी की यह बहुत सालों की इच्छा थी। परदीप के पिता रामेश्वर को उसी गाँव के ठाकुर ने पीट-पीटकर मार डाला था। दुसाधों का वहाँ के ठाकुर शोषण करते थे। वे अब शोषण नहीं सहन करते हैं। और न ही उनका कोई काम बेगार में करते हैं। परदीप ने किसी तरह से इस साल पचास रुपए बचा लिए हैं। उन्हीं पैसों से माँ को तीर्थयात्रा पर ले जा रहा है। स्टेशन पर उदैभान सिंह प्रयागराज जाने वाले यात्रियों को इंजेक्शन लगा रहा है। इससे बचने के लिए वह पैसे ले रहा है। उसने परदीप से पचास रुपए माँगे। इन्जेक्शन लगवाने से कुछ लोग मर भी जाते हैं, ऐसा उसे डर किसी ने समझा दिया है।
परदीप इन्जेक्शन न लगवाकर दस रुपए ही उदैभान सिंह को पर्ची बनाने के लिए देना चाहता है। वह उससे गिड़गिड़ाता है। लेकिन वह नहीं मानता। तभी परदीप की माँ पारवती काकी इन्जेक्शन लगवाने के लिए हाथ बढ़ा देती हैं। यहाँ भी गरीब वर्ग को एक नियम के कारण लूटने के लिए अमीर वर्ग उपस्थित है। गाँव के अमीर और तथाकथित सवर्ण वर्ग के लिए यह असहनीय बात है कि कोई गरीब अपनी इच्छा की पूर्ति करे। भले ही वह कितनी भी साधारण क्यों न हो। पारवती अपने पति रामेश्वर के जीवित रहने के समय से मन में यह इच्छा पाले हुए है कि कभी वह तीर्थयात्रा पर प्रयागराज जाएगी। अब बेटे ने किसी तरह मजदूरी करके पचास रुपए बचा लिए हैं तो इन पैसों को लेकर कथित सवर्ण-समाज में चर्चा है। वे लोग किसी भी तरह से परदीप और उसकी माँ को तीर्थयात्रा पर नहीं जाने देना चाहते हैं। यहाँ परदीप कमजोर पड़ता है। इन्जेक्शन के प्रभाव को सुनकर डर जाता है। लेकिन उसकी माँ बहुत मजबूत है। वह अपना हाथ इन्जेक्शन लगवाने के लिए आगे करके अपनी दृढ़ता का परिचय देती है। अब्दुल बिस्मिल्लाह के पात्रों में अन्याय से दबते रहने का भाव नहीं मिलता है।
‘बैरंग चिट्ठी’ कहानी में वहिद्दू अपने बेटे को कान्वेन्ट स्कूल में भेजना चाहता है। वह एक पोस्टमैन है। उसकी तनख्वाह उतनी नहीं है फिर भी वह कोशिश कर रहा है। बेटे का वहाँ इंटरव्यू होना है। वह बेटे को अंग्रेजी में कुछ चीजें रटवा रहा है। इंटरव्यू भी कुछ ठीक ही होता है। लेकिन उसका एडमिशन नहीं हो पाता है। वहाँ अमीर आदमी हाजी मोइनुद्दीन के बेटे का एडमिशन हो जाता है। वहिद्दू का बेटा गुड्डू बैरंग चिट्ठी की तरह घर लौट आता है। शिक्षा और अच्छी नौकरी की तलाश इन कहानियों के अधिकतर पात्र करते हैं। शिक्षा ही वह चाभी है जिससे बेहतर जिंदगी पाई जा सकती है। वहिद्दू अपने बेटे को अपनी तरह पोस्टमैन नहीं बनाना चाहता है। वह जानता है जिस तरह की कमजोर शिक्षा उसे मिली है वह उसके बेटे को इस गरीबी से मुक्त नहीं कर पाएगी। लगातार अभाव से मुक्ति का एक रास्ता अच्छी नौकरी हो सकता है। अच्छी नौकरी के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत को वहिद्दू बहुत बेहतर तरीके से समझ चुका है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने का रास्ता इतना आसान नहीं है। इसलिए उसके बेटे का दाखिला उस स्कूल में नहीं हो पाता है।
‘शत्रु’ कहानी में कल्लू अपनी पत्नी कन्नो को बहुत मारता है। उसके पिता बड़े मियाँ घर पर खाना खाने आते हैं और फिर मस्जिद चले जाते हैं। कन्नो हसनुआ नाम के पागल समझे जाने वाले आदमी के साथ चली जाती है। बाप बेटे एक दूसरे को इसके लिए शत्रु समझते हैं। कन्नो जैसे पात्रों के माध्यम से अब्दुल बिस्मिल्लाह स्त्रियों को अपनी स्थिति को बदलने के लिए एक रास्ता सुझाते हैं। पति की मार सहने की अपेक्षा अपने लिए एक बेहतर साथी तलाश करने का विकल्प देना भारतीय समाज के लिए कोई आसान बात नहीं है। यहाँ स्त्रियों के लिए अपने निर्णय लेने के अधिकार की पैरवी की गई है। ऐसा कई और कहानियों में भी दिखता है।
‘मुरीद’ कहानी में वाचक के दादा पीर साहब के मुरीद हैं। वे उनके हाथ चूमकर उन्हें कुछ पैसे देकर अपनी किस्मत अच्छी बनाना चाहते हैं। वाचक के पिता की मृत्यु हो चुकी है। चाचा मियाँ अपना घर अलग कर चुके हैं। दादा से कुछ होता नहीं है। पीर साहब जब आते हैं तो दादा उनके पास जाते हैं। आज वे अपनी पुरानी शेरवानी पहनकर पीर साहब के यहाँ पहुँचे। उन्होंने गंदे-मैले दो रुपए का नोट पीर साहब के हाथ में रखा और उनका हाथ चूमने की कोशिश की तो उन्होंने अपना हाथ दूसरी ओर कर लिया। दूसरे लोग दस-दस पाँच-पाँच के नोट उनको दे रहे थे। धर्म, अंधविश्वास और गरीबी का त्रिकोण यहाँ दिखाया गया। है। अपनी गरीबी और दुरावस्था में वाचक के दादा परिवर्तन धर्म के रास्ते से चाहते हैं। वे पीर साहब के यहाँ अपने जीवन को बेहतर बनाने की आशा से जाते हैं। वहाँ उन्हें तिरस्कार ही मिलता है। वे इसकी असलियत संभवतः अंत में समझ जाते हैं।
‘नया कबीरदास’ कहानी में एक व्यक्ति है। उसका घर हिन्दू और मुसलमानों के बीच है। उसका नाम कबीरदास है। वह कबीरदास के तरह ही विचार रखता है। उसकी पत्नी का नाम रामपुरिया है। वह हिंदुओं के सामने मुसलमानों की बड़ाई करता है और मुसलमानों के सामने हिंदुओं की। वह दोनों धर्मों को मिलाने की बात करता है। एक बार दंगा हो जाने पर उसके घर के बाहर कुछ लोग आ जाते हैं। वे घर का दरवाजा खटखटा रहे हैं। नया कबीरदास सोचता है कि अगर मुसलमान होंगे तो वह उनसे कहेगा कि वह भी मुसलमान है और हिन्दू होंगे तो खुद को हिन्दू कहेगा। लेकिन वे अजीब लोग थे। उन्होंने उसको झापड़ मारा और घर के भीतर घुस गए। लोग उसकी मान्यताओं का सम्मान करने की जगह नृशंसता से उसे खत्म करना चाहते हैं। उसकी पत्नी का बलात्कार करना चाहते हैं। वह उन लोगों के सामने अपने धर्म सम्बन्धी विचार भी बदलने के लिए तैयार है लेकिन इस बार उसका सामना ऐसे दंगाइयों से हो रहा है जो धर्म के लिए केवल दूसरों को मारने के लिए तत्पर हैं।

हिन्दू-मुस्लिम सम्बन्धों पर और उनके समन्वय के लिए अब्दुल बिस्मिल्लाह ने अनेक कहानियाँ लिखी हैं। ‘अतिथि देवो भव’ में समन्वय और अन्य धर्म के प्रति भय और दूरी का भाव दिखाया गया है। इस सम्बन्ध में अब्दुल बिस्मिल्लाह की कहानियों में व्यक्त चिंता के बारे में आलोचक प्रताप दीक्षित ने लिखा है- “हज़ार वर्षों से ज्यादा समय से एक साथ रहते हुए आम हिन्दू और मुसलमान एक दूसरे की संस्कृति, जीवन, तीज-त्योहारों में इसके दर्शन, रीति-रिवाजों ही नहीं उनके सुख-दुख के धरातल भी एक हैं। अब्दुल बिस्मिल्लाह की कहानी, उपन्यास के चरित्र, घटनाएं, चिंताएं इसका प्रमाण हैं।” (वाङ्मय पत्रिका, अक्टूबर-दिसम्बर 2015, संपादक डॉ. एम. फ़ीरोज़ अहमद, लेख, ‘जीवन के विभिन्न रंगों,सरोकारों से साक्षात्कार करती कहानियाँ (संदर्भ-टूटा हुआ पंख), प्रताप दीक्षित, पृष्ठ 86)।
अब्दुल बिस्मिल्लाह की एक प्रसिद्ध कहानी ‘आधा फूल आधा शव’ है। इस कहानी में उन्होंने दंगा होने की भूमिका और उसके शांत होने की स्थिति और कारण को दिखाने की कोशिश की है। जब कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जे की लड़ाई के लिए हिन्दू-मुसलमान लड़ने-मरने पर उतारू होकर आमने-सामने थे तभी वहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर ने एक दोनों धर्मों से एक-एक पंच बनाकर इस मामले को सुलझाने का बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य किया। दोनों धर्मों के लोगों ने अपने अपने पंच की पर्ची पुलिस इंस्पेक्टर को दी। और कमाल की बात यह की दोनों ने वहाँ के एक कॉलेज के प्रिन्सपल जो हिन्दू थे उनका नाम पर्ची में लिखा है।
दंगों को इस तरह से होने से टालने की एक घटना के बारे में आशुतोष वार्ष्णेय ने ‘हिन्दू मुस्लिम रिश्ते : नया शोध, नए निष्कर्ष’ किताब में लिखा है- “दिसम्बर 1992 में जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तब तक भिवंडी के नागरिकों, हिंदुओं और मुसलमानों, दोनों के बीच इतनी समझ, आपसी विश्वास और पक्का निश्चय विकसित हो चुका था कि उन्होंने अपनी बस्तियों और शहर की शांति भंग नहीं होने दी। यहाँ एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई।” (आशुतोष वार्ष्णेय, हिन्दू मुस्लिम रिश्ते : नया शोध, नए निष्कर्ष, राजकमल प्रकाशन, संस्करण 2005, पृष्ठ 310)। कुछ इसी तरह का प्रयोग अब्दुल बिस्मिल्लाह अपनी एक कहानी में करते हैं। और ‘नया कबीरदास’ कहानी में दंगा करने वाले लोगों की मानसिकता का भी चित्रण करते हैं। यह कहानी कहीं न कहीं नए दौर में कबीर की प्रासंगिकता पर भी प्रश्न उठाती है। यह नए कबीर नहीं बल्कि कबीर कालीन समाज और वर्तमान कालीन समाज के अंतर को सामने रखती है। जब हिन्दू और मुसलमानों को साथ लाने वाले के साथ कोई नहीं खड़ा होता है। उसकी लाचारगी कबीर की नहीं वर्तमान समय की लाचारगी है।
‘शीरमाल का टुकड़ा’ कहानी में महरून अपनी माँ नसीबन के साथ मुन्नू मियाँ के वलीमे के दिन बर्तन धो रही है। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। सब लोग खाना खा रहे हैं। वहाँ छोटे बच्चे भी हैं। जिनको सब कुछ खाने को मिल रहा है। भूख से महरून को चक्कर आने लगते हैं। वह सोचती है कि न जाने खाने को कब मिलेगा? सभी लोग खाना खाने लगे। वह प्लेटें उठाकर माँ की मदद कर रही है। उसे बहुत तेज भूख लगी है।
लोगों ने खाना खा लिया तो वहाँ बहुत सारा खाना नीचे गिरा पड़ा है। उसको साफ करके दूसरे लोग खाने के लिए बैठेंगे। उस नीचे पड़े खाने को फेंक दिया जाएगा। महरून वहाँ नमाज पढ़ने की नकल करते हुए बैठ जाती है। वहाँ शीरमाल का एक बड़ा टुकड़ा पड़ा हुआ है। उसे वह किसी तरह अपने दुपट्टे में लेकर आधा करके उठा लेती है और बाहर चली जाती है। भूख का बहुत मार्मिक वर्णन इस कहानी में किया गया है। अब्दुल बिस्मिल्लाह अपनी कहानियों में बच्चों को संवेदना का वाहक बनाने का काम बहुधा करते हैं। गरीबी और भूख के लिए महरून जैसी बच्ची से उपयुक्त पात्र कोई और शायद नहीं हो सकता था। उसके भीतर भूख की पीड़ा को पाठक अपने मन में महसूस करता है। बाल मनोविज्ञान के सहारे वह दूसरों बच्चों और अपने जीवन की तुलना करती है। उसकी आंतरिक संवादों में एक शिकायत का भाव उसके बाल मन की उपज है। अगर इतने सारे खाने में से उसे कुछ दे दिया जाता तो उस घर के लोगों का क्या बिगड़ जाता! वह प्रेमचंद के ‘हामिद’ और ‘बूढ़ी काकी’ जैसे पात्रों की दशा का सामूहिक रूप लेकर इस कहानी में उपस्थित है।
‘पुरानी हवेली’ कहानी में एक पुरानी हवेली में वेश्यावृति के अपराध में पकड़ी गईं साठ लड़कियां और औरतें रहती हैं। उन सबको वहाँ की अधीक्षिका का आदेश मानना पड़ता है। वह अपने अनुसार सबको दंड देती है। किसी को आराम से रखती है। वे उसका विरोध करके एक दिन गेट तोड़कर निकल जाती हैं। वहाँ की जिंदगी के अनेक किस्से इस कहानी में हैं। अनेक औरतों के अनेक दुख और यहाँ पहुँचने की अलग-अलग कहानियाँ हैं। यहाँ एक औरत झुन्नीबाई मार दी जाती है। कृष्णाबाई गायब हो जाती है। किसी के परिवार वाले उसे छुड़वाने आ जाते हैं और कभी किसी की शादी हो जाती है। सुधार के नाम पर जेल जैसा माहौल इस पुरानी हवेली का सच है। यहाँ भी कहानी के अंत में इस जेलनुमा सुधारगृह का दरवाजा वहाँ रहने वाली लड़कियाँ तोड़ती हैं। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए इस कैद से मुक्त होने के लिए वे एकजुट होती हैं।
‘तलाक के बाद’ कहानी में साबिरा को उसके पति सत्तार ने अपने वालिद के कहने पर तलाक दे दिया। उसने अपने मन से यह नहीं किया। धर्म के हिसाब से साबिरा अपने पिता के घर आ जाती है। उसे अपने पति की याद आती है। एक छोटी सी बात के कारण उसके ससुर इतना नाराज हुए और उसका तलाक हो गया। अब साबिरा की दूसरी शादी की बात चलाई जाती है। धर्म के हिसाब से जब तक वह किसी दूसरे से शादी करके तलाक नहीं लेगी तब तक अपने पहले पति के पास नहीं जा सकती। लेकिन एक दिन सत्तार आता है तो उसके साथ साबिरा चल देती है। मुस्लिम समाज में तलाक एक नाजुक मसला है। इस मुद्दे के धार्मिक पक्ष की अलग-अलग व्याख्याएँ मिलती हैं। पुरुष समाज ने इस मसले को अपने लिए ही अधिकतर इस्तेमाल किया है। अब्दुल बिस्मिल्लाह तलाक के विवाद पर न जाकर उसे प्रेम से सुलझाना चाहते हैं। इसमें किसी तरह की बाहरी धर्म-सत्ता की अनुपस्थिति दिखाकर उन्हें अप्रासंगिक घोषित करते हैं।
इस कहानी और तलाक के धार्मिक पक्ष पर डॉ. नगमा जावेद ने लिखा है- “‘तलाक के बाद’ कहानी में लेखक ने तलाक के सही रूप से परिचित कराने और उसकी विद्रूपता से भी अवगत कराने का प्रयास किया है। आमतौर पर यह समझ लिया गया है कि तीन बार तलाक कह देने से तलाक हो जाती है। यह गलत है। कुरान शरीफ में साफ अल्फाज में बताया गया है कि एक साथ तीन बार तलाक शब्द नहीं बोला जा सकता है।” (वाङ्मय पत्रिका, अक्टूबर-दिसम्बर 2015, संपादक डॉ. एम. फ़ीरोज़ अहमद, लेख ‘बयान जारी है….’ एक अवलोकन, डॉ. नगमा जावेद मलिक, पृष्ठ 91)।
‘कच्ची सड़क’ कहानी में गुलशन नाम का एक युवक है। उसकी शादी हो चुकी है। वह शहर में काम खोजता है। उसे पहले एक दोस्त की मदद से कॉपी होल्डर का काम और कुछ पैसे मिलते हैं। उतने पैसे में वह होटल में खाने का बिल भी नहीं दे पाता है। फिर उसके बाद उसे एक पत्रिका में प्रूफ रीडर की नौकरी मिलती है। लेकिन छह महीने के बाद उसे निकाल दिया जाता है। उसकी पत्नी उससे शहर ले चलने के लिए कहती है लेकिन न उसके पास किराये के पैसे हैं और अच्छी नौकरी। वह रोज कच्ची सड़क से अपने गाँव-घर लौटता है। उसकी जिंदगी कच्ची सड़क है जिस पर उसकी तरह अनेक लोग चल रहे हैं। जीवन निर्वाह के लिए भटकते असंख्य युवाओं और लोगों में से एक युवा गुलशन भी है। वह किसी तरह से अपने जीवन और परिवार को चलाना चाहता है। उसे किसी प्रकार की कोई नौकरी नहीं मिलती है। अगर एक नौकरी और कुछ वेतन मिलता भी है तो वह अल्पकालिक और अत्यंत कम होता है। वह अपनी पत्नी को शहर में अपने साथ रखना चाहता है। शहर में उसके ही जीवनयापन लायक पैसे गुलशन के पास नहीं हो पाते हैं। वह इतने कम वेतन में अपनी पत्नी को कैसे शहर में अपने साथ रख सकता है! वह इस स्थिति में शहर से गाँव तक कच्ची सड़क पर टूटी हुई साइकिल से रोज कई मील का सफर तय करता है। इसमें उसे रात हो जाती है। उसकी पूरी ताकत इसी काम में लग जाती है। जब तक उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी कम वेतन के बाद भी ठीक लय से चलने लगी है तभी पत्रिका के दफ्तर से उसकी हमेशा के लिए छुट्टी हो जाती है।
वहाँ का एक कर्मचारी गुलशन को बताता है कि यहाँ का यही नियम है। किसी को भी यहाँ छह महीने से अधिक के लिए नहीं रखा जाता है। छह महीने तक कम वेतन पर रखा जाता है और वेतन बाद में बढ़ाने का वादा किया जाता है। परन्तु न किसी की नौकरी पक्की की जाती है और न ही किसी का वेतन बढ़ाया जाता है। हर छह महीने बाद किसी दूसरे आदमी को नौकरी पर रख लिया जाता है। यहाँ नौकरी माँगने के लिए आने वाले लोगों की कमी थोड़े है। गुलशन अपनी इस अल्प वेतन वाली छह महीने तक चली नौकरी छूट जाने के बाद टूटी हुई साइकिल लेकर कच्ची सड़क पर शहर से गाँव लौट रहा है। उसे लगता है मेरी तरह असंख्य लोग पूरे देश में इसी कच्ची सड़क पर चल रहे हैं। कच्ची सड़क कच्ची नौकरी की तरह अनेक कठिनाइयों से भरी हुई है। जिसमें कुछ भी स्थिर अथवा पहले से निश्चित नहीं है। निश्चित और अच्छा वेतन और साधनों का अभाव इस कच्ची सड़क के जीवन का सत्य है।
‘काई’ कहानी में बड़ी बहन के पति के देहांत के बाद उनके घर वाचक जा रहा है। वह उनकी मृत्यु पर भी जा सकता था लेकिन गया नहीं। वह किसी प्रकार से अपने को सम्बन्ध की जिम्मेदारी और परेशानी में नहीं डालना चाहता है। बहन के घर जाकर भी जब उसकी बहन कहती है कि अब यहाँ बेटे-बहू की बातें सहने की जगह तुम्हारे साथ चलूँगी तो वह झूठ बोल गया। घर पर ही नहीं उसके ऊपर भी एक तरह की काई जम गई है। सम्बन्धों में कैसे जंग अथवा काई लगती है इसे भी इस कहानी में दिखाया गया है। भाई के प्रति बहन का बहनापा कितना सच्चा है और भाई के लिए उसका आर्थिक हित और सुविधा-असुविधा ही सर्वोपरि है। बहन के पति के देहांत के बाद भी वाचक उसके गाँव-घर जा सकता था लेकिन दो बार जाने के खर्चे के डर अथवा लालच के कारण वह बाद में अपनी शोक-संवेदना व्यक्त करने जाता है। यह शोक-संवेदना एक अभिनय और खाना-पूर्ति से अधिक कुछ नहीं है। बहन को भाई के जीवन की हर खुशी में जो अपेक्षा थी वह नहीं मिलता है। उसे भाई हमेशा कम से कम अथवा नजरअंदाज करने की श्रेणी में रखता है। बहन चाहती थी कि उसे उसका सम्पन्न भाई को उपहार दे लेकिन वह नहीं देता। बहन अब अपने बेटों और बहुओं के साथ न रहकर अपने भाई के परिवार में आराम से रहना चाहती है तो भी उसे अपने साथ ले चलने के स्थान पर दो दिन आने का झूठ बोलता है। बहन संभवतः भाई के मन को समझते हुए भी हर बार उससे कुछ अपेक्षा रखती है। भाई हर बार ही बहन के स्थान पर लोभ को वरीयता देता है।
इस पर भी बहन उसके लिए गरीबी के बावजूद रास्ते के लिए खाना बनवाकर देती है। उसकी आवभगत करती है। अपनी क्षमता से ज्यादा उसका ध्यान रखती है। भाई की क्षमता बहन से काफी अच्छी होने के बाद भी वह सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है।
‘मुक्ति’ कहानी में जमादार और सुगनी की कहानी है। एक दिन जमादार अपनी बेटी से मिलने शहर जाते हैं। वहाँ उनका सामान छीन लिया जाता है। उन्हें पुलिस वाले भीख माँगने के जुर्म में पकड़ लेते हैं। अब उनको सुगनी जेल से छुड़ाने आई है। वह किसी साहब की मदद लेती है। उसके पास सिर्फ साठ रुपए हैं। जमादार को एक हजार की जमानत और एक हजार का मुचलका भरना है। किसी तरह से साहब उसकी मदद करते हैं। वे बहुत गरीब लेकिन स्वाभिमानी लोग हैं। इस जेल से मुक्ति के बाद भी उनकी इस मदद को चुकाने से मुक्ति संभव नहीं है। गरीब व्यक्ति को भिखारी और स्वाभिमान से रहित सोचने के विचार का विरोध इस कहानी में है। यह आवश्यक नहीं है कि किसी की आर्थिक स्थिति अथवा वेशभूषा के आधार पर व्यक्ति के बारे में निर्णय किया जाए। सरकार और समाज के अनेक लोग इस प्रकार के निर्णय करने के आदी हो जाते हैं। जमादार और सुगनी के जीवन में इसी छवि-निर्माण के कारण भूचाल आता है। जमादार दूसरे शहर में रहने वाली अपनी बेटी से मिलने जाना चाहता है। वह जब उस शहर में पहुँचता है तो प्रशासन से जुड़े लोगों को भिखारी पकड़ने का अपना तय काम भी दिखाना है। इसी कारण से वे ऐसे कुछ लोगों को पकड़कर जेल में डाल देते हैं। जेल से उनको छुड़ाने के लिए कोर्ट में उनकी जमानत भरनी है। अब अगर किसी के पास इतने पैसे नहीं हैं तो वह जेल में ही रहने को मजबूर होगा। यह सरकारी तंत्र की अमानवीय स्थिति पर भी चोट करने वाली कहानी है। इस चिंता के अलावा जमादार और सुगनी के बीच प्यार भी इस कहानी के विषय कहे जा सकते हैं। वृद्ध दंपति के बीच प्रेम का भाव भी देखने लायक है।
