
जैसे विशाल वृक्ष की छाया कथित छोटे और महत्वपूर्ण वनस्पति के लिए ठीक नहीं समझी जाती उसी तरह रचनाकार की किसी विधा की महत्वपूर्ण रचना का असर उसी की दीगर विधा की रचना के लिए चुनौतियाँ दरपेश करता रहा है। अब्दुल बिस्मिल्लाह का नाम ‘झीनी झीनी बीनी चदरिया’ से इतना फैला कि नाटककार अब्दुल बिस्मिल्लाह को पाठक ठीक से जान ही नहीं पाए।
अब्दुल बिस्मिल्लाह पर केन्द्रित संवेद के आगामी अंक के लिए लिखा गया राजेश कुमार का यह लेख संवेद के पोर्टल के लिए प्रस्तुत है।
साहित्य की दुनिया में कोई लेखक जब कहानी लिखता है या नाटक, उसका मूल्यांकन बराबर का नहीं हो पाता है। या तो उसे बड़ा कहानीकार मान लिया जाता है या फिर नाटककार। अगर बड़ा कहानीकार मान लिया गया तो अक्सर उसका नाट्य पक्ष उपेक्षित रह जाता है। लोगों की नज़रों से उसका वो पक्ष नजरंदाज हो जाता है। हिन्दी साहित्य में ऐसे कई उदाहरण आपको देखने को मिल जाएँगे। मन्नू भंडारी को लोग जितना उनकी कहानियों, उपन्यासों को लेकर जानते हैं, उस पर विचार-विमर्श करते हुए दिखते हैं, उनके लिखे और खेले गये नाटकों के बारे में शायद बहुत ही कम जानकारी हो।
अमृत राय और फणीश्वर नाथ रेणु के अनुवाद-कहानी-उपन्यास पर तो पत्र-पत्रिकाओं में खूब चर्चा होती रहती हैं, लेकिन उनके लिखे नाटकों के बारे में शायद ही किसी को सलीक़े से जानकारी हो। कुछ ही साहित्यकार हैं जिनके दोनों पक्षों पर लोगों की नज़र गई हैं और उनकी कृतियों का सही मूल्यांकन किया है। धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, भीष्म साहनी और असग़र वजाहत ऐसे साहित्यकार हैं जिन्हें अगर लोगों ने कहानीकार-उपन्यासकार के रूप में सम्मान दिया तो रंगमंच की दुनिया में भी उतना ही यश पाया। उनकी कृतियाँ खूब सराही गई। सालों पूर्व लिखा गया नाटक अभी भी मंचित होते हैं और अपनी प्रासंगिकता का इज़हार करते रहते हैं। कभी-कभी तो लोगों के लिए तय करना मुश्किल हो जाता है कि वे कहानीकार-उपन्यासकार बड़े हैं या नाटककार? विशेषकर धर्मवीर भारती और मोहन राकेश का उनकी विधाओं के परस्पर तुलनात्मक अध्ययन करने पर तो संकट जरुर उपस्थित हो जाता है।
‘झीनी झीनी-बीनी चदरिया’ उपन्यास के लेखक अब्दुल बिस्मिल्लाह के सामने भी भी कुछ ऐसा ही परिदृश्य उपस्थित है। बनारस के बुनकरों के जीवन पर केंद्रित उनका वृहद् उपन्यास ‘झीनी झीनी-बीनी चदरिया’ से उनकी इतनी बड़ी पहचान बन गई है कि लोगों को शायद याद भी न आता हो कि उन्होंने नाट्य संसार में कितना महत्वपूर्ण कार्य किया है। इन्होंने पूर्णकालिक नाटक ‘दो पैसे की जन्नत’ तथा ‘काग़ज़ का घोड़ा’, ‘कलियुग का रथ’ और ‘जनता ख़ुद देखेगी’ जैसे लघु नाटक महत्वपूर्ण, उद्देश्यपरक नाटक भी लिखा है। सारे नाटक हिन्दी की प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। इनका सबसे चर्चित नाटक ‘दो पैसे की जन्नत’ सोमदत्त के संपादन में ‘साक्षात्कार’ पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बल्कि इसी नाम से अब्दुल बिस्मिल्लाह के सारे नाटकों का संकलन भी आया है।

‘साक्षात्कार’ के अंक में प्रकाशित होते ही इस नाटक ने पाठकों का ध्यान अपनी तरफ़ आकर्षित किया। रंगकर्मियों की नज़र इस पर पड़ी। लोग ढूँढ-ढूँढ कर पढ़ने लगे। वजह ये थी कि उन दिनों देश के जो हालात थे, सब अंदर से एक अजीब तरह की बेचैनी महसूस कर रहे थे। कोई खुल कर तो नहीं कह पा रहा था, लेकिन जिधर देखिए उधर लोग दबी ज़ुबान में कुछ न कुछ फुसफुसा रहे थे। शायद उनके सम्मुख कोई भय, आतंक व्याप्त हो। वे खुल कर कुछ भी कहने से बच रहे थे।ऐसे में अब्दुल बिस्मिल्लाह का यह जो नाटक आया, उसने अंदर के भय को जैसे दूर भगा दिया। यह केवल एक नाटक नहीं था, न केवल लिखने व छपने भर के लिए लिखा गया था। यह उस सत्ता के प्रतिपक्ष में खड़ा था। सत्ता की निरंकुशता के विरुद्ध प्रतिकार था यह नाटक। और इस नाटक की एक खूबी है कि भले यह आज से चालीस वर्ष पूर्व लिखा गया था, आज भी प्रासंगिक है। बल्कि आज की तारीख़ में जनता द्वारा चुनी गई सरकार जनतन्त्र की ओट में देश को फासीवाद की तरफ़ ले जा रही है, विकास और धर्म के नाम पर मुल्क की बहुसंख्यक जनता को साम्रदायिकता की गहरी खाई में धकेल रही है, यह नाटक लोगों को निरंतर सचेत करती है।
यह नाटक मंचन के पहले ‘साक्षात्कार’ में छपा था। इसकी पहली प्रस्तुति छपने के बाद हुई थी। सुरेश स्वप्निल के निर्देशन में 8 अक्तूबर, 1986 को इसका प्रथम मंचन भोपाल में हुआ था। ‘दो पैसे की जन्नत’ नाटक यथार्थ का चित्रण हुबहू वैसा नहीं करता है, बल्कि किसी लोक कथा के माध्यम से लोक शैली में दिखाने का प्रयास है। कई नाटककारों ने समसामयिकता को दिखाने के लिए मिथकीय व लोक कथाओं का सहारा लिया है। बरतानिया सरकार के समय धार्मिक, पौराणिक कथाओं के माध्यम से पारसी नाटकों में उस वक्त के नाटककारों ने देश की मौजूदा हालातों पर खूब टिप्पणियाँ की है। हालाँकि कई नाटक प्रतिबंधित भी हुई। फिर भी लोक कथाओं के सहारे कुछ कहने की छूट मिल जाती है, इसलिए अक्सर नाटककार इसको ढाल बनाकर अपनी बात कहने से चुकता नहीं है।

अब्दुल बिस्मिल्लाह ने लोक कथा के बहाने सामंती, पूँजीवादी सत्ता पर इस नाटक के रूप में जो निर्मम प्रहार किया है, वह उद्देश्य में सफल है। वे न अपने नाटक को कला के सौंदर्य में छुपाने की कोशिश करते हैं, न चलते-चलते किसी अनजान, अंधेरे मोड़ पर छोड़ कर तटस्थ होते हुए नज़र आते हैं। इस नाटक को भोपाल के सुरेश स्वप्निल ने पहली बार निर्देशित किया था। प्रस्तुति के बारे में उनका कहना है कि इस प्रस्तुति का आलेख पहले वाले आलेख से काफी भिन्न, पर कथ्य और उसके निर्वाह में कोई रद्दोबदल नहीं थी।
आलेख में थोड़ा-बहुत परिवर्तन होना स्वाभाविक भी था, क्योंकि प्रस्तुति के पूर्व कोई भी नाट्य आलेख परिपक्व नहीं हो पाता। पहले, दूसरे और तीसरे प्रदर्शन के पश्चात दर्शकों से खुल कर बातचीत करने व सराहनाओं से बचते हुए आलोचनाओं पर जब ध्यान केंद्रित किया तो पाया कि नाटक के संबंध में समसामयिकता का प्रश्न एक ख़ास प्रश्न के रूप में उभर कर आया, जिसके बारे में उनका मानना था कि यह नाटक किसी भी कालखण्ड में बांधा नहीं जा सकता -और यही इसकी शक्ति है। कुछ दर्शकों की यह प्रतिक्रिया भी आयी कि यह कोई समाधान प्रस्तुत नहीं करता। इस संबंध में निर्देशकीय वक्तव्य सारी शंकाओं को स्पष्ट कर देता है। उनका कहना है कि दर्शक अथवा पाठक के मन में समाधान प्राप्त करने की व्यग्रता उत्पन्न होना ही सबसे बड़ा समाधान है।

अब्दुल बिस्मिल्लाह के सारे नाटक बदलाव के स्वर वाले हैं। उनका कोई भी नाटक व्यवस्था के पक्ष में खड़ा हुआ नज़र नहीं आता है। अगर उन्हें व्यवस्था के अंदर असमानता, अन्याय दिखता है तो उसके विरुद्ध उनके नाटक मंच पर मोर्चा लेते हुए दिखते हैं। उदाहरण के लिये उनके सबसे चर्चित और देश भर में विभिन्न संस्थाओं द्वारा खेले गये नाटक ‘दो पैसे की जन्नत’ पर बात करेंगे तो बात स्पष्ट हो जायेगी। नाटक की कहानी इतनी सी है कि एक छोटी सी लड़की बाज़ार में दो पैसे में जन्नत बेच रही है। लड़की की बात रखने के लिए एक मज़दूर जन्नत ख़रीद लेता है। उसी समय बाज़ार से राजा की सवारी गुजरती है। छोटी लड़की की आवाज़ सुन कर राजा आता है और दो पैसे दे कर जन्नत देने के लिए कहता है।
लड़की कहती है कि जन्नत तो उसने उस मज़दूर को बेच दिया, अब उसके पास दूसरा नहीं है। राजा के आदेश पर सिपाही उस मज़दूर को पकड़ कर दरबार में लाते हैं। मज़दूर कहता है कि उसके पास कोई जन्नत नहीं हैं, वो तो लड़की की मन रखने के लिए दो पैसे में ख़रीद लिया था। चापलूस सलाहकारों के कहने पर राजा को जन्नत पाने की ऐसी सनक चढ़ जाती है कि उसने इसी धरती पर जन्नत बनाने का फ़रमान जारी कर दिया। फ़रमान की तामील करने के लिए राजा का पूरा तंत्र लग गया। जनता का जिस तरह दोहन हो सके, करने लगे। ख़ाली हो रहे ख़ज़ाना भरने के लिए जनता पर नये-नये टैक्स लगाए गये, उनका हर तरह से शोषण होने लगा। जन्नत में हूरों के लिए उनकी बहू-बेटियों को उठा-उठा कर रखे जाने लगे। इससे जनता काफ़ी क्षुब्ध हो गई। राजा के लड़के ने जब सत्ता के ख़िलाफ़ विद्रोह का बिगुल फूंका तो जनता उसके साथ हो गई। सत्ता परिवर्तन हो गया। अब जो नई व्यवस्था आई, जनता को लगा अब उनके दिन आ गये। लेकिन परिवर्तित व्यवस्था का चरित्र तो कोई अलग तो था नहीं। वह भी उसी रास्ते पर चलने लगी जिस पर उसके पहले वाले चल रहे थे।
नाटक का जो अंत है,शायद उसी को देख कर किसी ने प्रतिक्रिया की थी कि नाटक अंत में दर्शकों के सम्मुख कोई समाधान प्रस्तुत नहीं कर पाता है।ज़रूरी नहीं कि हर नाटक आपके सम्मुख कोई रास्ता दिखाएं ही।नाटक कई बार रास्ता दिखाता है और कई बार रास्ता दिखना ज़रूरी नहीं समझता है। गढ़ा हुआ या कृत्रिम-काल्पनिक रास्ता दिखाना नाटक के हित में नहीं होता है। राजनीति और धर्म से जुड़े लोग जिस तरह इंस्टेंट दिखाते हैं, नाटक या साहित्य की कोई विधा के लिये दिखा पाना संभव नहीं है। राजनीतिक रूप से प्रतिबद्ध या नाटक द्वारा जो पार्टी प्रचार का कार्य करते हैं, वे लोग अति उत्साह में आकर कभी-कभी नाटक के अंत में कोई हल दिखा देते हैं। ऐसे नाटक अक्सर आलोचना का विषय बनते हैं।
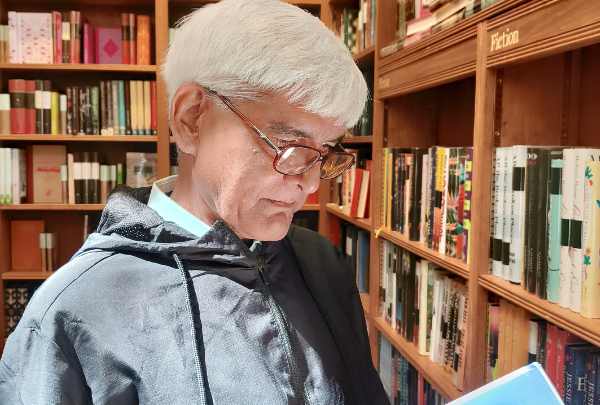
अब्दुल बिस्मिल्लाह ने जब ‘दो पैसे की जन्नत’ नाटक लिखा था, उस समय की राजनीतिक परिदृश्य ऐसी थी कि जनता के सामने कोई विकल्प नज़र नहीं आ रहा था।सत्ता परिवर्तन तो हो रहा था, व्यवस्था में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा था। सत्तर दशक से लेकर नब्बे दशक के बीच के दौर को गौर से देखें तो भारतीय राजनीति में काफी उथल-पुथल दिखाई देती है। सत्ता सुख पाने की राजनीतिज्ञ लोगों में जैसे होड़ लगी रहती थी। लोगों को जहां फ़ायदा दिख रहा था, उधर भाग कर चले जा रहे थे। सिद्धांत व विचार उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था। संभवतः इसी परिदृश्य को विश्लेषित कर अब्दुल बिस्मिल्लाह ने नाटक के अंत में कोई समाधान देना आवश्यक नहीं समझा होगा या नाटक के लिए न्यायोचित नहीं लगा होगा।
जैसे हिन्दी साहित्य में अब्दुल बिस्मिल्लाह की पहचान उनके उपन्यास ‘झीनी झीनी बीनी चदरिया ‘ से है, उसी तरह रंगमंच की दुनिया में अगर उनें जाना जाता है तो ‘ दो पैसे की जन्नत’ के नाटककार के रूप में। इस नाटक को देश की कई प्रतिष्ठित संस्थाओं ने विभिन्न शहरों, महानगरों में किया।लखनऊ की ‘दर्पण’ ने इसके कई मंचन किए। ‘दस्ता’ इलाहाबाद द्वारा फ़रवरी 1988 में उदय यादव के निर्देशन में किया गया। इप्टा, गोरखपुर ने डॉ. मुमताज़ ख़ान के निर्देशन में किया गया। इप्टा, भिलाई ने भी ‘जन रंग’ के सहयोग से इसकी कई प्रस्तुतियाँ मज़दूरों की बस्तियों, झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के बीच किया। नाटक का कथ्य भले लोक का हो, लेकिन जब भी जहां भी ये नाटक मंचित होता, देखनेवाले बिना किसी के बताये तत्कालीन सत्ता से जोड़ लेते थे। उन्हें एहसास हो जाता था कि नाटक का इशारा किधर है? नाटककार या निर्देशक किस दिशा की तरफ़ दर्शकों का ध्यान इंगित करना चाहते हैं।
ऐसा नहीं कि नाटक से जनता का रिश्ता केवल अब्दुल बिस्मिल्लाह के मात्र इसी नाटक में व्याप्त है। इसके अलावा उनके और भी जो नाटक है, सभी में आम जनता का दर्द, उसकी दुख-समस्या, शोषण के विरुद्ध उसकी लड़ाई, उसका संघर्ष सब मुखर रूप से उभर कर आया है। ‘काग़ज़ का घोड़ा ‘ नाटक में पिता की मृत्यु के बाद एक युवक बैंक से जमा राशि को निकालने के लिए जब जाता है तो उसे मृत्यु प्रमाणपत्र जमा करने के लिए कहा जाता है। पूरे नाटक में युवक उस काग़ज़ को जुटाने के लिए इधर से उधर भागता-फिरता है। कई अपमानजनक परिस्थितियों से उसे गुजरना पड़ता है। काग़ज़ का घोड़ा एक ऑफिस से दूसरे, एक टेबल से दूसरे टेबल तक, एक फाइल से दूसरे फाइल तक दौड़ता रहता है। युवक काग़ज़ी घोड़े के पीछे भागता रहता है। नौकरशाही की दलदली ज़मीन की तरफ़ नाटक इशारा करता है। कहीं न कहीं गहरा व्यंग्य करता है कि इसमें जिसका अगर एक बार पाँव फँस गया तो निकल पाना इतना आसान नहीं है।
‘कलियुग का रथ’ नाटक में रोज़ी-रोटी के लिये शहर में आये राम दुलारे मज़दूर की कहानी है। दिन भर दिहाड़ी मज़दूरी करने के बाद रात को सड़क के किनारे फुटपाथ पर सोने के लिये राम दुलारे जैसे व्यक्ति को किस तरह जद्दोजहद करनी पड़ती है, नाटक में बहुत ही चुटीले ढंग से लाया गया है।
‘जनता ख़ुद देखेगी’ नाटक में भी कुछ ऐसा ही स्वर है। गाँव का सामंत कैसे बुद्धू और सोमारू की ज़मीन धर्म और संस्कृति के नाम पर हड़प लेता है और जब जनता इनके कारनामों से वाक़िफ़ हो जाती है तो किस तरह प्रतिरोध की मुद्रा में आ जाती है, यही नाटक का मूल कथ्य है।
लब्बेलुआब अब्दुल बिस्मिल्लाह के चाहे ‘दो पैसे की जन्नत’ जैसे पूर्णकालिक नाटक हो या ‘काग़ज़ का घोड़ा’, ‘कलियुग का रथ’ या ‘जनता ख़ुद देखेगी’ जैसे लघु नाटक हो, सबका उद्देश्य है आम जनमानस की अभिव्यक्ति। इन नाटकों को पढ़ कर साफ़ नज़र आ जाता है कि नाटक किसे केंद्र में रख कर लिखा गया है? चारों नाटकों की कथावस्तु आमजन की पीड़ा है। एक आम आदमी को किस तरह आज भी धर्म -जाति- परंत-भाषा-बोली के आधार पर बाँटा जाता है, लुभावने नारों से उन्हें बहकाया जाता है, सुनहरे सपने दिखा कर भ्रमित किया जाता है, यही दिखाना नाटककार का लक्ष्य है।

अब्दुल बिस्मिल्लाह अपने नाटकों में यथास्थिति को केवल कथ्य के माध्यम से रख देना ही पर्याप्त नहीं मानते हैं। उससे आगे भी जाना चाहते हैं। ऐसे कई नाटककार हैं जो केवल यथास्थिति तक ही अपने को सीमित कर देते हैं। जनता के उभार को दिखाने से अक्सर परहेज़ करते हैं। उन्हें लगता हैं कि नाटक में जनता के प्रतिरोध को दिखाने से इसका कलात्मक पक्ष कमजोर हो जाएगा। लेकिन अब्दुल बिस्मिल्लाह अपने नाट्य लेखन में इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं।वे अपने नाटकों में अगर जनता पर ढाये गये शोषण-दमन को दिखाते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया में उनका जो ग़ुस्सा-आक्रोश किसी न किसी रूप में अभिव्यक्त होता है, उसे दर्ज करना भी नाटककार का दायित्व होता है। अगर इस पक्ष को जानबूझकर कर नज़रअंदाज़ का देते हैं तो यह एक प्रकार की बेईमानी समझी जायेगी। साहित्यिक कायरता कहलाएगी।
अब्दुल बिस्मिल्लाह अपने नाटकों में चरित्रों के संवाद बहुत सहज रखते है। इनके सभी नाटकों के संवाद आम बोल-चाल में है। कहीं से उनके संवाद में कृत्रिमता दिखाई नहीं देती है। बल्कि लघु नाटकों की भाषा और जिस तरह दृश्यों की संरचना की गई है, उस पर नुक्कड़ नाटक आंदोलन का काफ़ी प्रभाव दिखता है। जिन दिनों ये नाटक लिखे गये थे, देश भर में नुक्कड़ नाट्य आंदोलन देश भर में खूब खेले जा रहे थे और अपनी धमक से मुख्य धारा के रूप में पहचान भी बना ली थी। उसी का असर उस दौर के मंचीय नाटकों में भी दिखाई देता है। उस वक्त के मंच नाटकों में जन संघर्षों का चित्रण सही रूप से दिख जाता था।भाषा का अभिजात्यपन भी टूटा था। इसलिए इन नाटकों में अगर लोक शैली को देखें तो चौंकने की ज़रूरत हैं। ‘ दो पैसे की जन्नत’ के मूल में एक लोक कथा थी, इसलिए यथार्थवादी शैली के बजाए अगर यह नाटक के लोक शैली में अभिव्यक्त हुआ है तो इसके पीछे नाटककार की यह मंशा होगी कि इस रूप में नाटक के संप्रेषित होने की अधिक संभावना होगी। और नाटककार के सामने यह स्पष्ट होगा कि किस वर्ग के दर्शकों को नाटक दिखाना है।
उन दिनों सत्ता परिवर्तन के दौर में जब मुख्यधारा का रंगमंच तटस्थ मुद्रा में था, अभिजात्य वर्ग के गोद में बैठ गया था, सत्ता के विरोध में सामने आने से बचता था, अब्दुल बिस्मिल्लाह के नाटक अपने कथ्य और रूप पारंपरिक जड़ता को तोड़ कर जनता के बीच आ गये थे और प्रतिरोध की मुद्रा में आकर ऐसे खड़ा हो गये थे कि उन्हें एक कदम पीछे हटाना भी मुश्किल था। इसलिए ये नाटक आज भी ज़िंदा है। लोगों की स्मृतियों में है। आज भी मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहते हैं। एक नाटककार के रूप में यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।
