परिवेश को रचने की प्रक्रिया में मनुष्यता के मर्म की पहचान
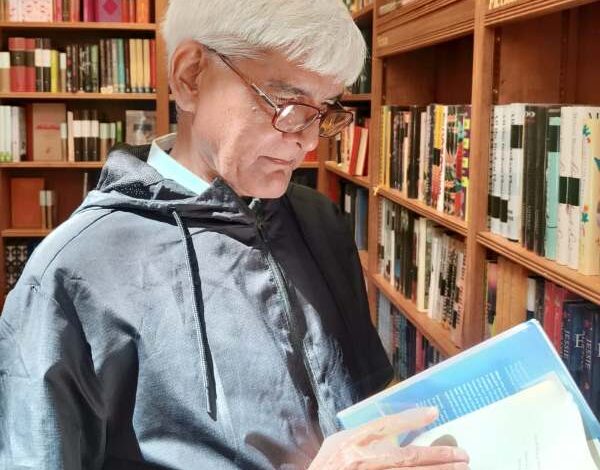
मनुष्यता के मर्म को आंक पाना कला के विविध ध्येयों में से एक रहा है। यहाँ तक पहुँचने के कई रास्ते हैं। अब्दुल बिस्मिल्लाह अन्य विधाओं के साथ कहानियों के जरिए भी उस ध्येय को साधते हैं। देश-समाज के प्रति लगाव, जीवन अनुभव, कहन का विशिष्ट सलीका वो गलियाँ हैं जो मनुष्यता के मर्म के रास्ते पर जाकर खुलती हैं। प्रस्तुत आलेख में जय प्रकाश जी ने इन्हीं नुक्तों के इर्द-गिर्द अब्दुल बिस्मिल्लाह की कहानियों को समझने का प्रयास किया है।
एक नागरिक के रूप में लेखक की निजी पहचान -उसकी सामुदायिक अस्मिता- क्या उसके रचना-संसार को गढ़ने में निर्णयकारी भूमिका में होती है? कभी-कभी कुछ लेखकों को पढ़ते हुए अनायास ही यह सवाल वेताल की तरह कंधे पर सवार हो जाता है। अस्मितामूलक साहित्य के सन्दर्भ में यह सवाल और भी विकट होता है।
सृजन, परिवेश और नागरिक अस्मिता
निस्संदेह रचना का शील-स्वभाव, उसका रूप-रंग और नैन-नक़्श बहुत हद तक लेखक के निजी परिवेश से निर्धारित होता है। लेखक अंततः अपने परिवेश अपने भोगे-जिये जीवन को रचता है; आसपास की दुनिया से, अपने इतिहास-भूगोल, यानी अपने प्रत्यक्ष अनुभव-संसार से ही सृजन का कच्चा माल और खाद-पानी लेता है। ऐसे में उसकी नागरिक अस्मिता लिंग, जाति, धर्म, समुदाय आदि पर आधारित निजी अस्मिता जिसके दायरे में उसका जीवन घटित होता है, अगर उसकी सृजनात्मकता को किसी-न-किसी रूप में प्रभावित करती है तो यह अचरज की बात नहीं है। लेकिन लेखक की नागरिक अस्मिता के बरअक्स उसकी व्यापक मानवीय दृष्टि भी बराबर सक्रिय होती है जो उसके अस्मिता-बोध का प्रतिवाद करती है। अस्मिता-बोध की संकीर्ण राजनीति और वृहत्तर मानवीय संवेदना के बीच एक अंतर्द्वंद्व उसके भीतर चलता रहता है। अस्मितामूलक और विमर्शात्मक लेखन में उसके पीछे की नियंत्रणकारी राजनीति वस्तुतः लेखक के गहन मानवीय सरोकारों पर हावी होने लगती है। फलस्वरूप दमित नागरिक अस्मिता की एक विक्षुब्ध, प्रतिवादी और आक्रामक मुद्रा में रचना ढल जाती है। दलित और स्त्री अस्मिता पर आधारित लेखन के सरोकार, कहने की ज़रूरत नहीं कि, प्रतिशोधात्मक जान पड़ते हैं। ज़ाहिर है, उनकी पहचान विवादी लेखन या एक तरह के अपवर्जनकारी लेखन के रूप में है जो साहित्य के व्यापक मानवीय सरोकारों को अस्मिता की संकीर्ण राजनीतिक छतरी के भीतर खींच कर समेट लेता है। अपने से इतर सामुदायिक अस्मिताएँ उसके लिये ‘अन्य’, इसलिये अपवर्जित, होती हैं।
समाज के तलछट पर छूटी हुई सामुदायिक अस्मिताओं का इस तरह की छतरियों में सिमट आना आकस्मिक नहीं है। इसके ठोस ऐतिहासिक कारण स्वयं सामाजिक वास्तविकता के भीतर मौजूद हैं। पितृसत्ता-केंद्रित और चातुर्वर्ण्य-आधारित सामाजिक सत्ता अपने होने के प्रबल तर्क के रूप में, या प्रतिरक्षात्मक रणनीति के तौर पर, धर्मसत्ता को चतुराई से आगे कर देती है जिसकी वैधता स्वयंसिद्ध मान ली गयी है। ऐसी स्थिति में समता और न्याय के पक्ष में खड़ी राजनीति स्वयं को एक प्रतितर्क के रूप में प्रस्तुत करती है और साहित्य-जैसे बौद्धिक-सर्जनात्मक उपक्रम को भी जबरन अस्मिता-बोध के भीतर खींच लाती है।
हिंदी-साहित्य में दलित-स्त्री-आदिवासी अस्मिता का सशक्त उभार अकारण नहीं है, उसके विमर्शात्मक घेरे यूँ ही नहीं बने हैं। मगर दिलचस्प है कि अपेक्षाकृत बड़ी जनसँख्या और अपनी दमित सामाजिक स्थिति के बावजूद मुस्लिम अस्मिता की वैसी पुकार कम-से-कम साहित्य के भीतर उठती नहीं दिखाई देती। हिंदी में मुस्लिम जीवन के चित्रण में मुस्लिम समुदाय से इतर साहित्यकारों की नगण्य उपस्थिति की चर्चा होती रही है, या स्वयं मुस्लिम साहित्यकारों के लेखन की ओर अपेक्षित ध्यान न दिये जाने की शिकायत की गयी है। लेकिन दलित-विमर्श या स्त्री-विमर्श की तरह मुस्लिम-विमर्श की चर्चा कभी नहीं हुई।

अब्दुल बिस्मिल्लाह-जैसे लेखक इस स्थिति को श्रेयस्कर मानते हैं। यह भी उचित है कि हिंदी में जातिपरक और लैंगिक पहचान की राजनीति के समानांतर धार्मिक पहचान की राजनीति का साहित्यिक संस्करण विकसित नहीं हुआ। इसका कारण सम्भवतः हिंदी साहित्य के मूलतः धर्मनिरपेक्ष चरित्र में निहित है जो दरअसल उसकी शक्ति और संभावनाओं का स्रोत है। इसलिए मुस्लिम जीवन पर केंद्रित साहित्य में धार्मिक संवेदना या सामुदायिक अस्मिता की जगह व्यापक मानवीय दृष्टि की प्रतिष्ठा हुई है, और इसके समानांतर हिंदू सामुदायिक अस्मिता पर इसरार करने वाली साहित्य-दृष्टि पूरी तरह नदारद है। अगर हिंदी साहित्य का कोई स्थायी एजेंडा है तो वह धर्मनिरपेक्षता ही है। यह सुकूनदेह है कि समकालीन राजनीति की क्षुद्रताओं से हिंदी साहित्य बहुत हद तक अभी भी सुरक्षित है, बल्कि वह उसका प्रतिपक्ष निर्मित करती है। वह संकीर्ण राजनीति का उपनिवेश बनने से बची रही है।
निजी तौर पर मुझे हिंदी में पिछले कुछ दशकों के दौरान विकसित हुए अस्मितामूलक साहित्य के अंदर उभरी अपवर्जक प्रवृत्तियाँ उसका स्वाभाविक विकास नहीं मालूम पड़ती हैं। लेकिन पिछले कुछ दशकों में दलित और स्त्री जीवन की विषमताओं पर एकाग्र साहित्य की अपनी धमक के साथ मौजूदगी को अलक्ष्य नहीं किया जा सकता। इस तथ्य को भी अलक्ष्य नहीं किया जा सकता कि हिंदी के कुछ मुस्लिम लेखकों ने भारतीय समाज के उन इलाक़ों में कथा की संभावनाओं की तलाश की है जो अन्यथा प्रायः अनन्वेषित और अज्ञात रह जाते। ये मुस्लिम जीवन के अँदरूनी कोने हैं जहाँ ये लेखक गये। लेकिन उन्होंने इसे अनुभव के पृथक प्रदेश के रूप में न देखकर भारतीय समाज के वृहत्तर यथार्थ से जोड़कर देखा है। न उसमें अस्मिता का आग्रह है, न अपवर्जन का। इसलिये उसमें प्रतिरोध की प्रवृत्ति भी नहीं है। न तो उसमें मुस्लिम नागरिक अस्मिता के स्वतंत्र बोध पर इसरार है, न ही व्यापक मानवीय अस्मिता से विलग होने की प्रतिश्रुति। नागरिक अस्मिता बनाम मानवीय अस्मिता का द्वैत यहाँ व्यर्थ हो जाता है।
इस बात पर अलग से ज़ोर देने की ज़रूरत नहीं कि अब्दुल बिस्मिल्लाह की कहानियों से गुज़रते हुए एक नागरिक के रूप में लेखक की निजी पहचान, उसके परिवेश और अनुभव-संसार के रचना पर प्रभाव आदि सवालों से बचकर नहीं निकला जा सकता। अपने परिवेश को स्वायत्त करते हुए अब्दुल बिस्मिल्लाह, स्वाभाविक है कि, अपने समय का सीधा साक्षात्कार करते हैं। परिवेश को स्वायत्त करने का सरल रास्ता, या उसकी प्रचलित प्रविधि उसे घटनात्मकता के बीच से उठा लेने की है। उन्होंने यही सीधा-सरल रास्ता अपनाया है। यानी लेखक का वर्तमान ही कहानियों का घटना-काल है। इसे प्रचलित भाषा में लेखक का समकालीन बोध कहा जा सकता है। उसका अपना समय यहाँ मूर्त्त हो उठता है। यह लगभग ठहरा हुआ समय है जिसमें बुलबुले की तरह उभरते हुए वृत्तांत हैं, अपनी समूची घटनात्मकता के साथ वे प्रकट होते हैं। इस घटनात्मक समय की विविध छवियाँ यहाँ दिखायी देती हैं।
कहानी में समय
यहाँ एक प्रश्न और भी उठता है। क्या इन छवियों में, कहानी भी अपना समय रचती है? क्या घटनात्मक समय ही कथा-समय है, या उसकी रचनात्मक प्रतिकृति है? कथा-समय और लेखक के वर्त्तमान काल के बीच आख़िर कितना और कैसा फ़ासला है? अब्दुल बिस्मिल्लाह की कहानियों में, जैसा कि ‘मेरी प्रिय कहानियाँ’ की भूमिका में वह स्वयं स्वीकार करते हैं, उनके बचपन से लेकर बाद तक के अनुभव प्रकट हुए हैं। ज़ाहिर है, उनकी कहानियों को उनके गतिशील वर्त्तमान के चलचित्र कहा जा सकता है। उनकी ज़्यादातर कहानियाँ 1980 के दशक में रची गयी हैं। इतिहास के भीतर समा चुके उस दौर के अनुभव यदि उनकी कहानियों में जीवंत हो पाते हैं तो देखना होगा कि क्या वे अपनी ऐतिहासिक जड़ों से विच्छिन्न होकर, अपने देश-काल की तात्कालिक चेतना से विलग होकर एक भिन्न समय को, वास्तविक कथा-समय को जीवंत कर पाते हैं जहाँ कहानी का अनुभव एक सार्वभौम संवेदना की कौंध में आलोकित हो उठता है?

अब्दुल बिस्मिल्लाह की कहानियों को पढ़ते हुए यह भी ध्यान रखना होगा कि कहानी सिर्फ़ परिवेश और समय से प्रभावित नहीं होती, न ही उसे चित्रित करना, या उसकी व्याख्या करना-भर कहानी का लक्ष्य होता है। दरअसल घटनात्मक समय कहानी के रचे जाने और पढ़े जाने की प्रक्रिया में उसके निजी समय में, एक स्वायत्त कथा-समय में, रूपांतरित होता है। तब घटनात्मक समय की विविध छवियाँ उसमें घुल जाती हैं।
सामान्य रूप से पिछली शताब्दी का आठवाँ-नवाँ दशक और उस दौरान उत्तर भारतीय मुस्लिम जीवन से ये कहानियाँ संदर्भित होती हैं। यही वह ऐतिहासिक समय है जो कमोबेश इनमें प्रतिबिंबित है। वह देश और काल के प्रत्यक्ष उल्लेख में व्यक्त नहीं होता, लेकिन कुछ कहानियों में ऐतिहासिक समय की झलक, कहीं झीनी-सी, दिखाई देती है। उदाहरण के लिए ‘नन्हीं-नन्हीं आँखें’ कहानी में डिंडौरी, जबलपुर के दंगे या ‘आधा फूल आधा शव’ में पडरौना का उल्लेख उन स्थानों से जुड़े समय की स्मृतियाँ जगाता है। ‘दूसरा सदमा’ में स्पष्ट तौर पर 14 अगस्त, 1965 की तारीख़ का उल्लेख है। (हालाँकि इस तथ्य का उल्लेख कहानी की संवेदना को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करता; उलटे उसे एक ख़ास समय में कीलित कर, रपट की तरह पढ़े जाने की तजवीज़ करता है।) ‘मेरी प्रिय कहानियाँ’ की भूमिका में लेखक ने न सिर्फ़ समय और परिवेश से प्रभावित होने के संकेत दिये हैं, बल्कि अपनी कहानियों की पृष्ठभूमि की भी चर्चा की है।
इसे कथानुभव से मिलाकर देखें तो उसमें लेखक के निजी अनुभव के स्रोत की पहचान की जा सकती है, या किसी हद तक उसकी कालगत संगति को भी अनुभव किया जा सकता है। लेकिन उस बिन्दु पर वह काल-जड़ित होने के ख़तरे से उबर जाता है जब ऐतिहासिक काल की लय अपनी तात्कालिकता तज कर ‘मानवीय’ और ‘सार्वभौम’ के आयाम में दाख़िल होती है। इस रूप में वह व्यापक मानवीय स्मृति का हिस्सा हो जाती है। इस मायने में ये कहानियाँ ‘काल-निबद्ध’ और ‘स्थान-बद्ध’ होते हुए भी अनुभव के विराट आयाम में अपना विस्तार सम्भव करती हैं। यही उनकी सफलता भी है। डिंडौरी, जबलपुर या पडरौना की स्थानिक स्मृतियाँ कथा-संवेदना में घुलकर अपना रंग छोड़ देती हैं और उससे एकाकार हो जाती हैं। इसी बिंदु पर कहानी की सार्वजनीन अपील उजागर होती है। इसी क्षण कहानी अपनी इतिहासबिद्धता से छुटकारा पाती है।
लेकिन कहानी की अंतर्वस्तु का इतिहास से मुक्त होना परिवेश से कथाकार की विच्छिन्नता से नहीं, उलटे उसमें निमग्नता से संभव होता है। एक साक्षात्कार में अब्दुल बिस्मिल्लाह कहते हैं कि ‘लेखन निजी अनुभव पर आधारित होता है। अनुभव के खरेपन से लेखन में प्रामाणिकता आती है, वह चाहे स्वयं का अनुभव हो या किसी अन्य का । महत्त्वपूर्ण यह है कि लेखक जो लिख रहा है, उसकी संवेदना में किस हद तक डूबा है।’ कहने की आवश्यकता नहीं है कि निमग्नता और मुक्ति के दुहरे उपक्रम में कहानी की वास्तविक मुक्ति होती है। यहीं कहानी का लौकिक समय उसके मोक्षकाल में बदलता है और वह उत्तर जीवन के लिए तैयार हो पाती है।
इसलिए डिंडौरी, जबलपुर या पडरौना की स्थानिक उपस्थिति हो, या मुस्लिम चरित्रों की मौजूदगी, अपनी संज्ञात्मक सत्ता को खोकर और लौकिक समय की प्रकट उपस्थिति से अप्रभावित रह कर कहानी अस्तित्त्व के एक भिन्न आयाम में, कथा की विस्तीर्ण भूमि पर पुनर्जन्म लेती है। बेशक, अब्दुल बिस्मिल्लाह की कहानियों में मुस्लिम चरित्रों की मौजूदगी से यह निष्कर्ष आसानी से निकाला जा सकता है कि ये मुस्लिम परिवेश की कहानियाँ हैं, या अब्दुल बिस्मिल्लाह मुस्लिम कथाकार हैं। लेकिन ऐसा कहा जाना क्या उचित होगा? क्या चरित्रों और स्थानों से निर्मित परिवेश को कहानी के संवेदनात्मक भूगोल में स्थानांतरित किये जाने पर वह अक्षत-अक्षुण्ण रह पाता है? और क्या वह उसकी पहचान का सटीक संदर्भ हो सकता है? चरित्र और स्थान लेखकीय परिवेश की उपज हो सकते हैं लेकिन वे कहानी में आकर कहानी के अपने देश-काल के अंग बन जाते हैं।
ऐसे में क्या मुस्लिम चरित्रों का होना इन्हें हिंदी की अन्य कहानियों से, या इसके लेखक को अन्य लेखकों से कुछ विशिष्ट बनाता है? अनेक लेखकों की कहानियों में सारे हिन्दू चरित्र हैं, मुस्लिम चरित्र बिल्कुल नदारद हैं। क्या उन्हें कभी हिन्दू परिवेश की कहानियों के रूप में जाना गया? क्या हिंदी के बहुसँख्यक लेखकों को हिंदू लेखक कहा जाना चाहिये? ज़ाहिर है, नागरिक अस्मिता से लेखक के रचना-संसार को जोड़कर देखना ग़लत निष्कर्ष की ओर ले जा सकता है। इसलिए अब्दुल बिस्मिल्लाह की कहानियों को महज़ मुस्लिम परिवेश की कहानियों के रूप में देखना भ्रामक सरलीकरण होगा। यह कहानी की सार्वभौमिक अपील को ख़ारिज कर उसे इतिहास के उत्पाद की तरह देखने की भूल होगी। ज़ाहिर है, कहानी इतिहास छाया या पिछलग्गू की तरह चलने वाली सचाई नहीं है। वह एक स्वायत्त निजी संसार रचती है जिसमें सारी सामुदायिक अस्मिताएँ व्यापक मानवीय अस्मिता में विलीन हो जाती हैं।
विशिष्ट अनुभव-क्षेत्र और विशिष्ट चरित्र
कहानी को निपट समाजशास्त्रीय पाठ के रूप में देखने या किसी सामाजिक परिघटना की आख्यानात्मक परिणति में उसे समझने के बजाय उसकी सौंदर्यात्मक और संवेदनात्मक मूल्यवत्ता की खोज के बिना उसे पढ़ने का उद्यम अधूरा है। कहानी में चित्रित जीवन, उसके भीतर मानवीय रागात्मकता के स्रोतों की तलाश और उसकी शिल्पविधि, को रेखांकित करने पर ही उसका पाठ पूरा होता है।

अब्दुल बिस्मिल्लाह ने हिंदी कहानी के अनुभव-कोष में बहुत कुछ नया जोड़ा है। जिस जीवन का चित्रण उन्होंने किया है, वह उसके कोनों-अँतरों से वाक़िफ़ हैं। उसके प्रामाणिक विवरण उन्होंने दिये हैं। उसके भीतर से ऐसे कथा-चरित्र उन्होंने चुने हैं जो बहुत जाने-पहचाने (टाइप्ड) नहीं, कुछ अलग और विशिष्ट हैं। सिर्फ़ इसलिए नहीं कि ज़्यादातर उनके यहाँ मुस्लिम पात्र हैं, बल्कि वे ऐसे चरित्र हैं जिन्हें हम पहली बार देख रहे होते हैं या जो कभी-कभार ही हमें मिल पाते हैं। ‘रैनबसेरा’ की सुम्बुल की अल्हड़ आकाँक्षाओं का यौवन की दहलीज़ पर थिरा कर किसी अनजाने आगंतुक पर एकाग्र हो जाना, ‘खाल खींचने वाले’ के भुनेसर के जुगुप्सा-भरे पेशे की दुश्वारियाँ, ‘आधा फूल, आधा शव’ के बाबू साहब का सौम्य बौद्धिक व्यक्तित्व और उन पर दो विवादी पक्षों का भरोसा, ‘जीना तो पड़ेगा’ के आकिल साहब की सनक-भरी हरकतें, ‘रफ़-रफ़ मेल’ का बद्दू मास्टर की अटूट जिजीविषा, ‘ख़ून’ के असलम की सदाशयता, ‘दंगाई’ के नैरेटर का व्यक्तित्वान्तरण, ‘नन्ही-नन्ही आँखें’ के सोना और मुन्ना की मासूम और निष्पाप छवियाँ- निस्संदेह रोजमर्रा के अनुभव की बात नहीं है। ये क्या ऐसे चरित्र हैं जो सहज ही, कहीं भी दिखायी दे जाते हैं? इन सबका चारित्रिक रूप से असाधारण और विशिष्ट होना उनके प्रति स्वाभाविक रूप से उत्सुकता जगाता है।
इनके बीच ‘अतिथि देवोभव’ या ‘तलाक़ के बाद’-जैसी कहानियों के चरित्र और उनमें वर्णित घटनाएँ भी हैं जो आम नागरिक जीवन के अनुभव का हिस्सा हैं। इनमें यथार्थ घटनात्मक विवरण में आकार लेता है। शायद समुदाय विशेष के लिये ये ऐसी घटनाएँ हैं, जो उसके सामाजिक जीवन में बार-बार घटती हैं, इसलिए सुपरिचित हों, लेकिन अन्य के लिये नहीं। जिस समुदाय के लिये ये सुपरिचित घटनाएँ हैं, उसके लिये, ज़ाहिर है, ये अप्रिय भी हैं। लेखक उसी सचाई को उजागर करने के लिए कहानी लिखता है जो मानवीय गरिमा को आहत करतीं हैं। इसके ज़रिये वह यथार्थ के अंतर्विरोधों को उजागर करता है। अब्दुल बिस्मिल्लाह ने ठीक ही लिखा है कि ‘जो घटनाएँ मुझे अप्रिय लगीं, उन पर मैंने कहानियाँ लिखीं।’
कहानी पढ़ने की सरल विधि यही है कि पढ़ना उसके कथ्य की तलाश के साथ शुरू होता है लेकिन जल्दी ही पाठक उसके शिल्प की गिरफ़्त में आ जाता है। फिर तो शिल्प उसे अपने ढंग से नियंत्रित करने लगता है। सीधी-सहज क़िस्सागोई का शिल्प कहानी को सरल, अकृत्रिम भाषा और स्पष्ट विवरणों के ज़रिए जब साध लेता है तो पाठक कहानी के प्रवाह के साथ उसकी सम गति में निर्बाध बहने लगता है। अब्दुल बिस्मिल्लाह की कहानियाँ पाठक के साथ यही करती हैं। वह उनके कथ्य में निहित उत्कंठा और शिल्प को सहजता के साथ हो लेता है । यह इसलिये हो पाता है कि उनका कथ्य अत्यंत मुखर है, और शिल्प संतुलित।
आधुनिक हिंदी कहानी का यह पारम्परिक या मान्य शिल्प है जिसमें आख्यान की एकरेखीय गति में यथार्थ धीरे-धीरे खुलता है, और अंत में उसके अंतर्विरोध या जीवन के किसी विडंबनात्मक क्षण को उजागर कर देता है। उदाहरण के लिये ‘अतिथि देवोभव’ में एक हिन्दू-परिवार की स्त्री द्वारा पड़ोसी की ग़ैर मौजूदगी में उसके आने की लंबी प्रतीक्षा के बीच उसके मेहमान को अपनी रसोई में बिठाकर आदरपूर्वक उसका सत्कार किये जाने का मानवीय कर्त्तव्य अकारथ सिद्ध होता है जब मेहमान के मुसलमान होने की सचाई उसके सामने सहसा उद्घाटित होती है। यह विडम्बना का मार्मिक क्षण है जो दुतरफ़ा आघात के साथ प्रकट होता है। एक तरफ़, ब्राह्मण स्त्री अपने चौके की पवित्रता नष्ट होने की ग्लानि से भर जाती है, उसकी जातिगत उच्चता का बोध खण्डित हो जाता है, और भय उसकी आँखों से झाँकने लगता है; दूसरी तरफ़ आगंतुक सलमान है, जिसने स्त्री की अहैतुक आत्मीयतावश उसे भाभी संबोधित किया है, मगर उसके बदले हुए व्यवहार में अचानक आत्मीयता और औत्सुक्य के ग़ायब हो जाने के बाद तिरस्कार की झलक उसका हृदय चीर कर रख देती है।
यहाँ हमारे वर्ण-विभक्त समाज के मनोविज्ञान में धार्मिक और जातिगत विभेद पर आधारित फाँक (हिन्दू-मुस्लिम द्विभाजन और उसके ऊपर ब्राह्मण-म्लेच्छ द्विभाजन) बेहद मार्मिक ढंग से प्रकट होती है। समाज का अंतर्विरोध कहानी में विडंबना के रूप में ढल जाता है। यह ऐसी विडंबना है जिसके समाजशास्त्रीय कारण (मुसलमानों के प्रति हिंदुओं के दुराव की मानसिकता) की तुलना में उसके मानवीय कारण (हिन्दू स्त्री के नस्लगत दम्भ पर आघात की तुलना में सलमान के भीतर संवेदनात्मक प्रत्याघात) कहानी में अधिक तीव्रता के साथ व्यक्त हुआ है। कहानी का लक्ष्य दरअसल इसी संवेदनात्मक प्रतिघात को प्रकट करना है। एक पल के लिए यदि ब्राह्मण स्त्री और मुस्लिम आगंतुक की धार्मिक-जातिगत पहचान को भूल कर उन्हें एक स्त्री और एक पुरुष के रूप में देखा जाए तो उनके बीच संबंधों की गुत्थी को समझना मुश्किल न होगा। उनकी सामुदायिक अस्मिता पर एकाग्र किये बिना उसे समझा नहीं जा सकता।
तो क्या अस्मिता की घेरेबंदी के भीतर रखकर इसे अस्मिता-विमर्श के राजनीतिक मुहावरे के साथ समझना होगा? दरअसल, स्त्री का ब्राह्मण होना और पुरुष का मुसलमान होना उस द्वंद्व की सृष्टि करता है जो हमारे सामाजिक जीवन की वास्तविकता के भीतर मौजूद है। इस अर्थ में ब्राह्मण स्त्री और सलमान दोनों अपने समुदाय के प्रतिनिधि हैं। ये दोनों चरित्र अपने सामुदायिक इतिहास, सांस्कृतिक बोध और जातीय जीवन की स्मृतियाँ धारण करते हैं। लेकिन उच्च मानवीय धरातल पर ये स्मृतियाँ अर्थहीन हो जाती हैं। अपनी सामुदायिक अस्मिता का त्याग कर ही वे उस स्थिति में पहुँचते हैं जहाँ उनके बीच संवेदना के स्तर पर केवल मानवीय संबंध की अपूर्व दीप्ति शेष रह जाती है। ‘अतिथि देवोभव’ इस संवेदना तक पहुँचने के ठीक पहले सामुदायिक अस्मिता के एकाएक जाग उठने और उसके द्वारा मानवीय संवेदना के स्खलित होने की कहानी है। ग़ौर करें कि जब तक सलमान की मुस्लिम पहचान उजागर नहीं हुई थी, ब्राह्मण स्त्री के मन में उसके प्रति स्नेह और सम्मान का भाव था। उसकी धार्मिक पहचान प्रकट होते ही भय और वितृष्णा से वह उससे विरक्त हो उठी— यहाँ तक कि एक और रोटी परोसे जाने का इंतज़ार कर रहे सलमान की ओर से बिलकुल उदासीन हो गयी। सामुदायिक अस्मिता और मानवीय संवेदनशीलता के बीच अंतर्विरोध को यह कहानी अत्यंत मार्मिक तरीक़े से खोलती है।
धर्म-आधारित सामुदायिक चेतना को झटका देने वाली कुछेक कहानियाँ यहाँ ध्यान खींचती हैं—उदाहरण के लिये ‘तलाक के बाद’ और ‘ग्राम-सुधार’। इन कहानियों में सामुदायिक चित्त के भीतर मौजूद उस ‘आम समझ’ (कॉमन सेन्स) को चुनौती दी गयी है जिसे धर्म के द्वारा स्थापित कर दिया गया है और जिसे संदेह या व्याख्या से परे या नितांत अप्राश्नेय मान लिया गया है। सामाजिकता के आंतरिक परिसर में इस ‘आम समझ’ का हस्तक्षेप प्रथा या परिपाटी के रूप में होता है। अंततः वह दमन का अस्त्र बन जाता है। उसकी स्वीकार्यता का मुख्य आधार तर्कबुद्धि नहीं, धर्म-व्यवस्था है जो रूढ़ होकर मानवीय स्वतंत्रता का हनन करने में नहीं झिझकती । इस्लाम में हलाला ऐसी ही प्रथा है जिसकी वैधता का स्रोत धर्मशास्त्र है और इस नाते वह इस्लाम के सामुदायिक व्यवहार का हिस्सा है । लेकिन धर्म-नियंत्रित सामुदायिक आचार-संहिता का व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप अंततः अमानवीय और विघटनकारी सिद्ध होता है। ‘तलाक के बाद’ कहानी इस प्रवृत्ति को प्रश्नांकित करती है; बल्कि वह उसका उत्कट प्रतिरोध रचती है। साबिरा और सत्तार के दाम्पत्य प्रेम पर साबिरा के ससुर की सनक का कहर जबरिया तलाक़ के रूप में बरपा होता है। लिखित तलाकनामे पर सत्तार को मजबूरन दस्तख़त करना पड़ता है लेकिन सत्तार और साबिरा दोनों का मन नहीं मानता।
अंततः सत्तार हलाला को मानने से इनकार कर साबिरा को साथ ले जाता है। सत्तार का यह खुला विद्रोह महज़ एक कुप्रथा के ख़िलाफ़ सामाजिक सुधार की पुकार, या निजी जीवन में धर्म की अतिक्रामकता का प्रतिवाद मात्र नहीं है, बल्कि मानवीय गरिमा और स्वतंत्रता का इसरार है। इस रूप में इस कहानी का सामाजिक सरोकार बिलकुल साफ़ है। लेकिन इतने-भर से कहानी मुकम्मल नहीं हो जाती। संवेदना के धरातल पर मानवीय गरिमा की परिणति दाम्पत्य प्रेम के गरिमापूर्ण क्षण में जब चरितार्थ होती है, वह एक विलक्षण सौंदर्यात्मक क्षण भी होता है। साबिरा को लिवाने आये सत्तार का साबिरा की अम्मी द्वारा सख़्त विरोध किये जाने के दरम्यान सत्तार के शब्द ‘नहीं चलोगी?’ का करुणा में भीगा एक-एक अक्षर साबिरा के दिल को छू लेता है, लेकिन सिर्फ़ साबिरा के दिल को नहीं छूता, पाठक भी उसकी आर्द्रता को महसूस करता है। हलाला की क्रूरता का यह मानवीय प्रतिवाद है।
‘ग्राम-सुधार’ कहानी भी व्यक्ति के कर्म-संसार में धर्मसत्ता के अपसरण के विरुद्ध प्रतिरोध का आख्यान रचती है। यह कहानी श्रमजीवी समाज में आजीविका की माँग और श्रम की वरीयता को धर्म के ऊपर स्थापित करती है। मौलवी के नमाज़ पढ़ने में देर होने पर झुँझलाये फजलाही के नमाज़ बीच में छोड़कर खेत की ओर निकल पड़ने को अगर धर्मद्रोह नहीं भी मानें तो यह मज़हब और दीन से ऊपर रोज़ी-रोटी की उसकी प्राथमिकता को प्रकट करता ही है। ज़ाहिर है, जीविका का संकट मज़हब की ज़रूरत से ऊपर है। कहानी सीधे नहीं कहती, लेकिन संकेत स्पष्ट है कि धर्म की मिथ्या चेतना यदि व्यक्ति को गिरफ़्त में ले ले तो वह उसकी बुनियादी ज़रूरत बना दी जाती है। अन्यथा रोज़ी-रोटी उसकी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है। धर्म, ज़ाहिर है, आध्यात्मिक भूख की तृप्ति को मनुष्य की बुनियादी ज़रूरत के रूप में स्थापित करता है।
लेकिन अपने घोर यथार्थवादी सन्देश के बावजूद ‘ग्राम-सुधार’ जीवन की स्वाभाविकता में निर्मित कहानी नहीं है। उसकी स्वाभाविकता और कलात्मकता पर एक गढ़ी हुई समाजशास्त्रीयता हावी है। वह अनुभव से नहीं, विचार से बुनी गयी है। इसमें बीते समय का ऐसा अविकसित गाँव है जहाँ कोई पढा-लिखा नहीं है। यह भूगोल में ही नहीं, इतिहास के भी दूरस्थ प्रान्तर में स्थित गाँव है। उसका अतीत-संगत संस्करण और कहानी में चित्रित उसका वर्त्तमान परस्पर बेमेल मालूम पड़ते हैं। सारे गाँववासी जाहिल हैं; न उनमें धर्म की चेतना है, न शिक्षा और विकास की ललक। गाँव में न मंदिर है, न मस्जिद। फिर भी यह हिंदुओं और मुसलमानों से आबाद गाँव है। हिंदू यहाँ अज्ञानी और मुसलमान जाहिल हैं।
धर्म और जाति की चेतना का उन्हें स्पर्श तक नहीं मिला है। यह एक कल्पित गाँव मालूम पड़ता है जहाँ कुछ बाहरी लोग आकर धर्म की चेतना जगाते हैं, और उन्हें धर्मपालन के लिए प्रशिक्षित करते हैं। वे गाँव के विकास के लिए बुनियादी सुविधाएँ जुटाने पर बल देने के बजाय धर्म को आवश्यक करार देते हैं। कहानी में इसके पीछे सक्रिय राजनीतिक शक्तियों की ओर संकेत किया गया है। वे ‘ग्राम-सुधार’ के नाम पर ग्रामीणों को धार्मिक चेतना से लैस करने का दुष्चक्र रचती हैं तथा वर्ण, जाति और सम्पदाय के आधार पर विभाजन के तमाम गुर अपनाती हैं। अंत में मुस्लिम समुदाय के भीतर उसके विरुद्ध प्रतिवाद का संकेत उभरता है जब इश्तियाक साहब की नमाज़ बीच में छोड़कर फजलाही खेत की ओर चल पड़ता है। लेकिन कहानी मुस्लिम सम्प्रदाय में विद्रोह को तो चित्रित करती है लेकिन उसके समानांतर हिन्दुओं के भीतर प्रतिरोध के उभार का संकेत नहीं देती (हालाँकि यह भी एक आरोपित या कृत्रिम युक्ति साबित होती) जो उसे प्रतिसन्तुलित कर सकती थी। कहानी अधूरे सच के निर्वाह में स्खलित हो जाती है। क्या यह बहुसँख्यक हिन्दू अस्मिता के अभेद्य होने और उसके निर्बाध अपसरण को सचाई के रूप में स्थापित करने के आग्रह का नतीजा नहीं है?
सच तो यह है कि यह पिछड़ा हुआ गाँव एक गढ़ंत है, वास्तविक गाँव नहीं। इसमें संदेह नहीं कि हिंदी के उदार बौद्धिक जगत ने धर्मनिरपेक्षता को मूल्य या विचारधारा के रूप में उचित ही अपनाया है। लेकिन उसके सहारे यदि कहानी लिखी जाएगी तो वह ‘ग्राम-सुधार’ से भिन्न नहीं हो सकती जो अनुभव और संवेदना को विचार की छेनी-हथौड़ी से तराशने पर सम्भव होती है। यह यथार्थ का पुनर्सृजन नहीं, उसकी प्रतिकृति है। इसमें अनुभव का प्राणतत्त्व यानी संवेदना की गरमाहट नहीं है। स्पष्ट है, यह कहानी सैद्धांतिक धरातल पर खड़ी है। उसके नीचे यथार्थ की ज़मीन पोली है।
भारतीय समाज में धर्मनिरपेक्षता का एक ख़ास संस्करण प्रचलित है। उसे साम्प्रदायिक सद्भाव के नैतिक आदर्श के रूप में सार्वजनिक मान्यता मिली है। धर्मनिरपेक्षता की इसी ज़मीन पर ‘आधा फूल, आधा शव’ कहानी भी खड़ी हुई है। लेकिन वह पूर्णतः गढ़ंत नहीं जान पड़ती; उसका अनुभव ठोस यथार्थ और उच्च मानवीय धरातल से उपजा है। यह कहानी भी नैतिक आदर्श को बौद्धिक इच्छालोक के स्तर तक ऊँचा उठाने का प्रयत्न करती है। लेकिन यह यथार्थ के प्राणतत्त्व से शून्य नहीं है शायद इसलिए भी कि स्वयं कथाकार ने इसे सच्ची घटना पर आधारित बताया है। इसलिए क़स्बे के क़ब्रिस्तान की भूमि के विवाद के निपटारे के लिए दोनों पक्षों द्वारा बाबू साहब को सरपंच चुना जाना अविश्वसनीय नहीं लगता। मगर यह तथ्य भी अपनी जगह है कि चार-पाँच दशक पहले आपसी पंचायत में विवाद निपटा लेने का धीरज और समझ समाज में मौजूद थी, लेकिन आज क़ानूनी तरीक़े से अदालत में निपटने के अलावा कहीं कोई विकल्प नहीं दिखाई देता। इस दृष्टि से देखें तो इस कहानी में यथार्थ की परिणति समकालीन संदर्भों में शायद पूर्णतः आश्वस्तकारी न जान पड़े। यह कुछ दशक पहले का यथार्थ था।
आज यदि वह कल्पलोक में स्थगित मालूम होता है तो कहना होगा कि इतिहास ने उसे निगल लिया है। तब की यथार्थवत्ता आज के स्वप्न या एजेंडा में तब्दील हो गयी है। यह धर्मनिरपेक्षता या सामाजिक सौहार्द का एजेंडा है। पाठक की उत्सुकता को जगाए रखते हुए यह कहानी जिस अप्रत्याशित मोड़ पर ख़त्म होती है, वहाँ सामाजिक सदाशयता, सम्मान और गरिमा अपने समूचे ताप के साथ विद्यमान होती है। प्रेमचंद की कहानी ‘पंच परमेश्वर’ जिस यूटोपिया को अतीत में अवस्थित करती है, वह यहाँ पुनः उठ खड़ा होता है। ‘पंच परमेश्वर’ कहानी अपनी ऐतिहासिक प्रामाणिकता से वंचित हो कर, आदर्शवाद के चरणों में समर्पित है; उसका नैतिक आदर्श एक कल्पित वास्तविकता और उजली भावुकता में स्पंदित होता है, फिर भी वह जीवन की मानवीय अर्थवत्ता या प्रासंगिकता को जगाए रखता है तो ‘आधा फूल, आधा शव’ कहानी भी अपनी कथात्मक वास्तविकता की रक्षा के प्रयत्न में अपनी भावुक परिणति को मानवीय आदर्श के उज्जवल क्षण के रूप में प्रस्तुत करती है। शतरंज की चाल और व्यवसाय की चाल दोनों में भारी पड़ते राय साहब और उनसे मात खाते हाफिज्जी के बीच सामुदायिक अस्मिता, जिसके वे अनायास प्रतिनिधि बन गये थे, का द्वंद्व यहाँ विसर्जित हो जाता है। आधा फूल, आधा शव का सामाजिक रूपक चरितार्थ हो उठता है। इस बिंदु पर यह कहानी एक अनूठे भावाकुल क्षण का सृजन करती है जहाँ अविश्वास और संदेह की अग्नि बुझ जाती है।

अब्दुल बिस्मिल्लाह के यहाँ अपने धार्मिक-सामाजिक और व्यक्तिगत आचरण में संदेह में घुलते अन्यान्य चरित्र भी मौजूद हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये समाज की ज़ेहनियत में पनपते आपसी अविश्वास की छायामूर्तियाँ हैं। ‘जीना तो पड़ेगा’ के अकिल मामू का सिरफिरापन इस संदेह से उपजा है कि हिंदू डॉक्टर उन्हें ज़हर का इंजेक्शन दे देगा। इसलिए वह इलाज के लिये उसके पास जाने से बचते हैं। लेकिन गुड्डन मियाँ के समझाने से उन्हें हिम्मत आती है और उनके भीतर की जिजीविषा पुनर्जीवित हो उठती है। अकिल मामू में हुआ यह बदलाव इंगित करता है कि समाज में पसरते निर्विवेकीकरण के विरुद्ध ज्ञान और विवेकशीलता के बल पर ही संदेह और अविश्वास को रोका जा सकता है।
संदेह और अविश्वास का यह ज़हर ‘दंगाई’ के कथानायक के भीतर घातक ढंग से चढ़ा है लेकिन शहर से यह ज़हर लेकर गाँव पहुँचने के बाद साम्प्रदायिक सद्भाव के दृश्य देखकर उसने स्वयं अपने भीतर गाँठ, ज़हर के स्रोत, को पाया और उसे लगा कि वह पतझर के पत्तों की तरह बिखरकर रह गया है—अवाक, हतप्रभ और किंकर्तव्यविमूढ़। उसने महसूस किया, सरलता के मंच पर वह कुटिलता के अभिनय का दुस्साहस कर रहा है, पर यहाँ वह पदार्थ नहीं है जो उसके भीतर के पदार्थ से मिलकर विस्फोट कर सके। संदेह और अविश्वास को घृणा में बदलते देर नहीं लगती, लेकिन यहाँ उसकी आग को प्रज्ज्वलित करने वाला रसायन नहीं है। कथानायक के भीतर अनायास एक क़िस्म का आत्मबोध जागता है, और उसका हृदय-परिवर्त्तन कर देता है। साम्प्रदायिक उचक्कों के आकस्मिक हृदय-परिवर्त्तन की यह कल्पना सुखद है लेकिन वह ज़मीनी हक़ीक़त से कोई तालमेल बिठा पाती है, इसे लेकर आश्वस्त होना मुश्किल है। आदर्शवाद की भूमि पर ऐसी निर्दोष कल्पना के बीज सहज ही अंकुरित होते हैं।
‘दूसरा सदमा’ का यथार्थ भी सामुदायिक मनोविज्ञान में धर्मपोषित ‘अन्यता’ और साम्प्रदायिक भेदभाव की राजनीति को प्रश्नांकित करता है। उसके प्रभाववश सामाजिक चित्त में हुए विचलन पर उँगली रखने के साथ ही यह कहानी जीवन में भाईचारा और सौहार्द के क्षरण की मर्मगाथा रचती है।
‘नन्हीं-नन्हीं आँखें’ कहानी में भय और संदेह के मारे दो मुस्लिम परिवार जबलपुर में दंगे होने और डिंडौरी के हिंदुओं के उनके गाँव आने की ख़बर पाकर जंगल में जा छिपते हैं। यह एक विलक्षण कहानी है जिसमें मासूमियत में लिपटा बाल-सुलभ प्रेम अपनी समूची निश्छल भंगिमा के साथ भय और संदेह का मानवीय प्रतिवाद रचता है। सोना और मुन्ना समझ नहीं पाते कि प्रेम के बीच धर्म क्यों आड़े आ जाता है और उसके कारण दंगे क्यों हुए। सोना की इस अबोध जिज्ञासा में साम्प्रदायिक कट्टरता का सशक्त प्रतिविमर्श छिपा हुआ है। कुछ दशक पूर्व चर्चित हुई कुछ कहानियों, मसलन ‘अँधेरा’ (अखिलेश) या ‘परिंदे का इंतज़ार-सा कुछ’ (नीलाक्षी सिंह), में साम्प्रदायिक दंगों के भयावह वृत्तांत के बीच युवाओं के प्रेम को प्रतिवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया था। लेकिन उनमें प्रेमी-प्रेमिकाओं के चरित्र यथार्थ के भीतर से स्वाभाविक रूप से विकसित होने के बजाय आख्यान की संरचना में युक्तिपूर्वक विन्यस्त किये गये जान पड़ते थे। वे सोचे-सुलझे हुए चरित्र थे—पढ़े-लिखे, वयस्क और बौद्धिक।
साम्प्रदायिक उन्माद के विवेकहीन अंधड़ में पनाह माँगती समझदारी और विवेक-दृष्टि के रूपक में ढले इन वयस्क प्रेमियों को मानो कथाकार ने सोच-समझ कर गढ़ा था। लेकिन ‘नन्हीं-नन्हीं आँखें’ के अवयस्क प्रेमी अपनी मासूमियत में कहीं अधिक स्वाभाविक और विश्वसनीय मालूम पड़ते हैं। हालाँकि दंगों का प्रत्यक्ष वर्णन यहाँ नहीं है लेकिन भय और असुरक्षा में उनकी बालसुलभ जिज्ञासा दंगों की भयावहता को परस्पर संदर्भित (जक्सटास्पोज़) कर कहानी एक व्यतिरेक रचती है जिसमें दहशत अधिक तीव्रता से महसूस होती है। इसमें आख्यान गढ़ा हुआ नहीं, इसलिए प्रेम की अभिव्यक्ति बेहद मार्मिक और सहज-स्वाभाविक रूप में हुई है। यह प्रेम और अनुराग की अद्भुत कहानी है जो संवेदना के स्तर पर साम्प्रदायिकता को सीधी चुनौती देती है।
प्रेम की ऐसी ही सहज और उत्कट संवेदना ‘रैनबसेरा’ में सम्भव हुई है। सोना का बालपन यहाँ सुम्बुल के चरित्र में अवतरित हो उठा है। छुटपन के प्रेम की गहन संवेदना, उसकी अल्हड़-अबोध अभिव्यक्ति और उसकी दुर्लभ सहजता यदि मुन्ना और सोना के चरित्र में प्रस्फुटित है तो सुम्बुल की असाध्य अल्हड़ता को भेद कर उसके भीतर से कुछ द्रवित हो उठता है। फिर तो अनुराग का जो अज्ञात सोता अकस्मात् फूटता है, उसका प्रबल वेग गहन वेदना में रूपांतरित होकर, उसके बेसुध रुदन में धार-धार बहने लगता है। स्त्री को पण्यवस्तु की तरह बरतने वाले समाज की क्षुद्र स्वार्थपरता की कलई उस क्षण खुल जाती है जब सुम्बुल को अपनी सुंदरता का धूर्त तरीक़े से सौदा करने वाली माँ के इरादे का अंदाज़ा लगता है कि वह नौजवानों को फाँस कर, उससे विवाह का झाँसा देती है, उनसे पैसे वसूलती है, और उम्र हो जाने के बाद भी पैसे उगाहने के लालच में उसके विवाह को टाल रही है।
सुम्बुल का आत्मज्ञान उसे सचेत कर देता है। रात बरसते पानी में टपकती झोपड़ी के भीतर सुरक्षित स्थान देख कर लेटी सुम्बुल माँ की तरफ़ देखकर वितृष्णा से थूक देती है। वह जान चुकी है कि जाल में फँसे एक नौजवान के रुपये और उसकी दी हुई नथुनी हड़प ली गयी है। उत्सुकतावश सुम्बली अचानक सन्दूक से नथुनी निकाल कर नाक पर फँसे नीम के तिनके की जगह उसे पहनती है। टूटे हुए आईने के सामने खड़ी होकर क्षण-भर अपनी नाक को निहारते ही उसके भीतर अनायास प्रणय का मेघ उमड़ आता है और आँखों से बरसने लगता है। उसकी अल्हड़ता भी मानो इस प्रवाह में बह जाती है। यह अद्भुत क्षण है जिसे अब्दुल बिस्मिल्लाह ने अत्यंत काव्यात्मक मर्मज्ञता के साथ रचा है—
‘सुम्बुल इतना रोई इतना रोई कि आसमान से बरसने वाली धारा थम गई। ‘रैनबसेरा‘ के इर्द–गिर्द झींगुर झन्नाने लगे, मेंढक टर्राने लगे और तमाम कीड़े–मकोड़े चारपाइयों के आस–पास आकर टहलने लगे। मगर सुम्बुल को होश नहीं—यहाँ तक कि एक मेंढक का ऐन उसके पेट पर आकर कूद रहा था।’
विडंबना के उद्धाटन की सटीक प्रविधि
अब्दुल बिस्मिल्लाह यथार्थ के भीतर निहित विडम्बना को कुशलता से उद्घाटित करते हैं। उन्होंने विडम्बना को कथा-युक्ति के तौर पर व्यापक रूप से इस्तेमाल किया है। उनका परिवेश इकहरा नहीं है। साम्प्रदायिक मनोविज्ञान पर केंद्रित रचनाओं के अलावा उनके कथा-संसार में समुचित विविधता है। ‘दूसरा सदमा’, खाल खींचने वाले’, ‘ख़ून’, ‘तीर्थयात्रा’ या ‘प्रतिद्वंद्वी’ आदि कहानियों में विडम्बना के सटीक शैल्पिक प्रयोग को लक्ष्य सकता है। उनके यहाँ आख्यान की नैसर्गिक अविरल गति में अनायास ढंग से बहुधा एक व्यतिरेक उत्पन्न होता है कहानी ऐसे मोड़ पर आ खड़ी होती है जहाँ यथार्थ एक मार्मिक बिंदु पर अर्थ की चमक से जगमगा उठता है। यहाँ कुछ अनायास, अनपेक्षित या अप्रत्याशित-सा घटित होता है और पाठक के हृदय को छू लेता है। मर्म को छू लेने का यह जादू वास्तविकता के भीतर निहित अंतर्विरोध के उद्घाटन के ज़रिए मुमकिन हो पाता है।
‘दूसरा सदमा’ में नौजवानों की चुहल से चिढ़ने वाले गुलामू चचा के लिए उनका यह अपमानजनक व्यवहार किसी सदमे से कम न था। लेकिन बाद में इस तरह की दैनिक हरक़तों के अभ्यस्त हो चुके गुलामू चचा के मनोसंसार में एक दिन अकस्मात कुछ ऐसा घटित हुआ कि वह सिवपरकसवा के चिढ़ाने पर बुरी तरह बिफर उठे और उस पर टूट पड़े। रोज़ मज़ाक बर्दाश्त करने के आदी गुलामू चचा की यह हरकत अप्रत्याशित थी। लेकिन इसके मूल में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों के ख़िलाफ़ पुलिस की एकतरफ़ा ज़्यादती की एक घटना थी जिसकी मुहल्ले में चर्चा थी और अपमान के दंश से पीड़ित लोग एहतेजाज (बदले की कार्रवाई) न होने से क्षुब्ध और सन्नाटे में थे। उस सन्नाटे के बीच हवा में तैरता प्रतिशोध का भाव दिलो-दिमाग़ पर छाया हुआ था। यूँ अब हिन्दू और मुसलमान लड़कों के रोज़ के मज़ाक़ से गुलामू चचा चिढ़ते नहीं थे, लेकिन मोहल्ले में पसरी एहतेजाज की उस मनोदशा में उनके भीतर एक हिन्दू लड़के के प्रति दुराव अनायास जाग पड़ा, और उस दिन सिवपरकसवा के मज़ाक पर बुरी तरह चिढ़ बैठे।
शायद उस दिन हिंदू सिवपरकसवा की जगह मुसलमान करीमवा ऐसी चुहल करता तो वह उससे न चिढ़ते। लेकिन चचा के हमले के जवाब में सिवपरकसवा ने अपने साथियों को बुलाकर जो बवाल खड़ा किया तो उसकी परिणति दंगे और कर्फ़्यू की भयावह त्रासदी में हुई। कर्फ़्यू ख़त्म होने के बाद भी स्थिति सामान्य नहीं रह गयी थी, माहौल में आतंक और भय की गंध बाक़ी थी, लेकिन अपने को उससे अप्रभावित साबित करने के लिए चचा जब इस उम्मीद से गली में निकले कि उनके लिए अब भी सब कुछ सामान्य है, और गली के शोहदे पहले की तरह उन पर फब्तियाँ कसने लगेंगे, तो यह देखकर उन्हें धक्का लगा कि उन्हें चिढ़ाने वाले लड़के बिलकुल चुप और उनकी तरफ़ से उदासीन हैं। यह अप्रत्याशित स्थिति थी। गुलामू चचा के लिए यह भी गहरा सदमा था जो उन्हें दूसरी बार लगा। यहाँ नितांत अप्रत्याशित स्थिति की उत्कट विडम्बना प्रकट होती है। सदमे में सिर्फ़ गुलामू चचा नहीं हैं, उनका समूचा परिवेश है, समूची गली और सारा मोहल्ला—सन्नाटे और उदासी में डूबा हुआ, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को अनमने ढंग से जीता हुआ । कहानी के इस अंतिम दृश्य में यथार्थ की विडंबना और ज़्यादा गहरी और मर्मभेदी हो उठती है।
अमानवीय तंत्र की अतिक्रामकता और कहानी का मर्म
अब्दुल बिस्मिल्लाह की कहानियाँ मनुष्य के इर्द-गिर्द रचे गये उस अमानवीय तंत्र के त्रासद अनुभवों को मूर्त्त करती हैं जहाँ समाज की तलछट के लोगों का संघर्ष है, और जहाँ श्रमजीवी समाज की जिजीविषा प्रकट होती है।
हिंदी कहानी में हाशिये के लोगों के जीवन के चित्रण की एक परम्परा स्थापित है जिसका सूत्रपात प्रेमचंद के समय में हो चुका था और आज भी जो निरन्तर गतिमान है, बल्कि अब तो यह प्रायः एक रूढ़ि का रूप ले चुका है। समाज में शोषण की व्याप्ति को समझने के समाजशास्त्रीय औज़ार के रूप में साहित्य के उपयोग की व्यावहारिक समझ सामंतवाद-पूंजीवाद की वर्गीय प्रक्रिया के इर्द-गिर्द एक ‘कॉमन सेंस’ निर्मित करती है जिसके चलते कहानी मानवीय शोषण के उद्घाटन का साहित्यिक औज़ार बन जाती है। इस ‘कॉमन सेंस’ और ‘समाजशास्त्रीय औज़ार के साहित्यिक औज़ार में रूपांतरण’ के फलस्वरूप उसके भीतर सौंदर्य-मूल्य का सृजन करने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है, क्योंकि कहानी में यथार्थ को सौंदर्यात्मक प्रक्रिया का परिणाम न मान कर सामाजिक प्रक्रिया का प्रतिफलन समझ लिया जाता है। इससे कहानी सामाजिक यथार्थ का निपट प्रतिबिम्ब बन जाती है और उसका अपना यथार्थ नितांत अलक्षित रह जाता है। पाठक और आलोचक दोनों इसी रूप में कहानी को लेते हैं। उनके तईं कहानी का लक्ष्य समाज, और उसके भीतर गतिशील यथार्थ है जिसका चित्रण करना उसका कर्त्तव्य है। ज़ाहिर है, कहानी को उसकी आत्मलक्षी प्रकृति में और उसमें चित्रित यथार्थ को सम्पूर्ण-स्वायत्त रूप में न देखने का नतीजा कहानी से अधिक यथार्थ पर—उस पर भी कहानी के यथार्थ पर नहीं, बल्कि समाज के यथार्थ पर—एकाग्र रूढ़ नज़रिये का प्रभुत्व है।
इस नज़रिये से देखने पर ‘खाल खींचने वाले’, ‘ख़ून’ और ‘तीर्थयात्रा’ का यथार्थ ऊपरी तौर पर सामाजिक वैषम्य को और उसके द्वारा खींची गयी विभाजन रेखा के भीतर, दुर्बल मनुष्य की जिजीविषा, प्रतिरोध या मानवीय संवेदनशीलता को उजागर करता है। लेकिन ये कहानियाँ अगर इतने में ही अपना लक्ष्य पाकर संतुष्ट रह जातीं तो शायद अपनी सार्थकता से वंचित हो जातीं। उनका लक्ष्य यथार्थ के विवरण देना-भर नहीं है। वे दरअसल यथार्थ के भीतर धड़कते मानवीय संदर्भों से अपनी कलात्मक अर्थवत्ता, अपने अस्तित्व की सार्थकता, हासिल करती हैं। ‘खाल खींचने वाले’ में खाल उतारने की क्रिया की बारीकियाँ, भुनेसर की संघर्षशीलता, उसकी उम्मीदें और जिजीविषा ही चित्रित नहीं है, बल्कि चमड़े को गोदाम के अम्बार में जबरन फेंक दिये जाने और उम्मीद के विपरीत बेहद मामूली दाम मिलने पर उसकी निराशा के चरम बिंदु पर पहुँच कर कहानी जब समापन तक पहुँचती है, तब उम्मीदों के टूट जाने की पीड़ा उसकी ज़बान के थरथराने, होंठ फड़फड़ाने, लाचारी में गिड़गिड़ाने और अंत में मुनीम से मिले कड़कड़ाते नोटों को मुट्ठी में मसल देने की हताश क्रियाओं में जीवंत हो उठती है।
उस वक़्त बड़े मियाँ की निष्ठुरता के बरअक्स भुनेसर की भंगिमा में झलकती मायूसी कितनी जीवंत, मानवीय और मर्मभेदी हो सकती है, इसकी कल्पना की जा सकती है। कथाकार ने इस त्रासद क्षण में भुनेसर की मुख-मुद्रा का चित्र नहीं खींचा है, लेकिन उसने इसकी गुँजाइश पाठक के लिए छोड़कर उसकी कल्पना को मुक्त होने का अवकाश दिया है। यही कहानी का यथार्थ है जो पाठ से निकलकर पाठक को संक्रमित कर लेता है। वर्ग वैषम्य से निर्धारित रूढ़ सामाजिक यथार्थ से भिन्न यह भुनेसर का जीवन-यथार्थ है जो उसकी त्रासदी में ही नहीं, पाठकीय कल्पना में साकार-स्वायत्त होता है। लेकिन शोषक-शोषित द्वैत की अतिक्रामकता कहानी और उसके यथार्थ की नियति को भी प्रभावित करती है। जिन कहानियों में यह द्वैत विद्यमान होता है, उनमें शोषित की नियति और यथार्थ की परिणति का अनुमान पाठक सहज ही लगा सकता है। ‘खाल खींचने वाले’ में भी यथार्थ की यही अनुमेयता है। कहानी के प्रभाव को यह कमज़ोर भी करता है।
अलबत्ता सामाजिक वैषम्य के घेरे में ही रची गयी ‘ख़ून’ कहानी में यथार्थ की अनुमेयता का अपेक्षाकृत कमज़ोर पड़ जाना आश्वस्त करता है। ग़रीब होने के नाते ‘सर’ के रिश्तेदार असलम की नियति का कुछ अंदाज़ा लगाया ही जा सकता है; हालाँकि कहानी से गुज़रते हुए पाठकीय उत्कंठा बराबर जाग्रत रहती है और ‘सर’ के नमाज़े-जनाज़ा की इजाज़त कौन देगा, की उत्सुकता निःशेष नहीं हो जाती। ‘सर’ के इंतकाल के बाद उनके कनाडा-स्थित परिजनों के न आ सकने के बाद नमाज़े-जनाज़ा की इजाज़त के लिए सगे रिश्तेदार की खोज होने पर बमुश्किल असलम का पता लगता है जो ‘सर’ की बीवी की बहन का बेटा है। फिर, असलम की खोज हो जाने के बाद उसके साथ आगे क्या होगा, यह प्रश्न निरंतर बना रहता है।
झुग्गी में रहने वाला ग़रीब असलम, जिसकी नौकरी की गुज़ारिश को ‘सर’ ने कभी टाल दिया था, अंततः अपनी बीवी के बरजने के बावजूद नमाज़े-जनाज़ा की इजाज़त देने के लिए राज़ी होता है। लेकिन अपनी इस सदाशयता और मानवीय संवेदनशीलता की क़ीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। यह कहानी प्रेमचंद की ‘मंत्र’ की याद दिलाती है। मानो डॉक्टर चड्ढा और भगत की कहानी यहाँ ‘सर’ और असलम के रूप में दुहरायी जा रही हो, और भगत की मनुष्यता का अक्स असलम में अवतरित हो गया हो। अपने बीमार बच्चे का इलाज करने के लिए गिड़गिड़ाते भगत को छोड़कर टेनिस खेलने चले गए डॉक्टर चड्ढा की संवेदनहीनता के बरअक्स इलाज के अभाव में बच्चे की मृत्यु के बावजूद डॉक्टर के बेटे के शरीर से सर्पदंश का ज़हर उतारने के लिए तैयार भगत की मानवीयता कितनी मूल्यवान है, बताने की आवश्यकता नहीं। नौकरी देने से ‘सर’ के इंकार के बावजूद असलम का नमाज़े-जनाज़ा के लिए तैयार होना भी उतना ही मानवीय है। बलवान के काम आने के बाद कमज़ोर को दूध से मक्खी की तरह बाहर फेंक देने की स्वार्थ-भरी निर्ममता अंततः इस कहानी के कथ्य को अतिरिक्त रूप से प्रभावी और उत्कट बना देती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि असलम की मृत्यु की मार्मिकता उसे दीप्त करती है।
‘तीर्थयात्रा’ में दलित दुसाध माँ-बेटे की प्रयागराज दर्शन की साध पूरी होने में गाँव के प्रभुत्वशाली सवर्णों ने छलपूर्वक अड़ंगा लगाया। उन्हें स्वीकार नहीं कि कोई दलित तीर्थयात्रा कर सवर्णों की बराबरी करे । उन्हें एक उपाय सूझा। परदीप को उन्होंने समझाया कि स्टेशन पर महामारी का टीका लगाए बिना रेल टिकट नहीं मिलेगी। ग्रामीणों में अफ़वाह भी थी कि सुई लगवाने पर बुख़ार आता है, कुछ लोग मर भी गये हैं। कड़ी मेहनत से बचाये रुपयों के साथ परदीप अपनी माँ पारवती को लेकर स्टेशन पहुँचा लेकिन वहाँ तैनात कम्पाउंडर उदैभान सिंह ने, जो गाँव के ही प्रभावशाली ठाकुर परिवार से है, टीका न लगने के एवज में पचास रुपये देने का दबाव डाला। यह राशि तीर्थयात्रा के लिए परदीप की कुल जमा पूंजी के बराबर थी जिसे देने के बाद तो यात्रा पर जाना ही असम्भव था। दलित परिवार को तीर्थयात्रा से रोकने की यह सवर्ण छलनीति थी। परदीप गिड़गिड़ाता रहा लेकिन उदैभान सिंह पर कोई असर नहीं हुआ। वह चाहता था कि परदीप और गिड़गिड़ाए। लेकिन आख़िर में तंग आकर पारवती सामने आ खड़ी हुई। क्षोभ और आक्रोश से भरकर वह फूट पड़ी— ‘ कुछ तो भगवान् से डरो ठाकुर साहब! इतनी अति नहीं की जाती। लो, लगाओ सुई, मरेंगे तब भी गंगा मैया की ही शरण जाएँगे।’ ठाकुर उदैभान सिंह के लिए यह अप्रत्याशित था। अकस्मात पारवती का यह रूप देखकर ठाकुर उदैभान सिंह के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं।
इस कहानी को ताक़तवर और कमज़ोर के टकराव या प्रभुत्वशाली और वंचित के द्वंद्व अथवा दलित प्रतिरोध के वृत्तांत के रूप में पढ़ा जा सकता है। ‘उदयभान सिंह के चेहरे पर उड़ती हवाइयों’ के विरुद्ध ‘पारवती काकी के हवा में किसी ठोस निर्णय की तरह तने हुए झुर्रियों-भरे हाथ’ के निहितार्थ को प्रतिवाद के रूपक की तरह रेखांकित किया जा सकता है। मार्क्सवादी और दलित सैद्धांतिकी के सहारे इसकी व्याख्या भी की जा सकती है। लेकिन उसके यथार्थ का यह अधूरा और स्थूल पाठ होगा । निस्संदेह पारवती के आक्रोश, क्षोभ, प्रतिरोध या उसकी पीड़ा के सामाजिक संदर्भ अवास्तविक नहीं हैं, लेकिन उसके मानवीय संदर्भ को समझे बगैर उसकी हर व्याख्या अधूरी रहेगी। जिस बिंदु पर जाकर कोई कहानी पूर्णता प्राप्त करती है, उसके सौंदर्यात्मक पहलू को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। यह पाठक पर कहानी के कुल प्रभाव के रूप में होता है।
पाठक यहाँ पारवती की जलती हुई आँखों से बरसती चिंगारी के प्रज्ज्वलित अनुभव की चपेट में आ जाता है जिसके उत्ताप से ठाकुर उदैभान सिंह का समूचा अस्तित्व झुलस गया है। यह एक धधकता हुआ जीवित क्षण है। कहानी उसे समय के झोंको के बीच हिलती हुई लौ की तरह गतिशील और स्पंदित रखती है। उसमें पारवती की सारी यंत्रणा मानो एकाग्र हो उठी है। कहानी का यही अंतिम सत्य, उसका चरितार्थ है । वह अनुभव के उस क्षण को ढूँढ़ निकालने के लिये बेचैन रहती है जो यूँ तो भाषा के भीतर किसी अँदरूनी तह में बेशक़ीमती रत्न की तरह छिपा हुआ है, मगर वास्तविकता की खुली मटमैली सतह पर हम उसकी चमक ढूँढ़ रहे होते हैं। शायद कहानी का लक्ष्य वास्तविकता के भूगर्भ में मौजूद इसी क्षण तक पाठक को पहुँचाना है। बाक़ी जगहों पर—मार्क्सवाद और दलित-विमर्श या किसी और सैद्धांतिकी अथवा किसी आलोचना-पद्धति का सहारा लेकर यथार्थ की व्याख्याओं तक—पाठक स्वयं पहुँच सकता है ।
अब्दुल बिस्मिल्लाह की कहानियों में किसी-न-किसी रूप में एक द्विचर युग्म (बाइनरी) सक्रिय है। यूँ भी कहानी में अंतर्विरोधों की उपस्थिति और उनका शमन द्विचर यथार्थ की मौजूदगी में ही सम्भव है। यह हिंदू-मुस्लिम, अमीर-ग़रीब, ताक़तवर-कमज़ोर, शोषक-शोषित, सुविधाभोगी-मेहनतकश, चतुर-नादान आदि अनेक रूपों में विद्यमान है। ज़्यादातर द्विचर वास्तविकता एक दूसरे के सम्मुख खड़ी दो विलोम इकाइयों के बीच अंतर्विरोधों को उजागर करती है। अब्दुल बिस्मिल्लाह के यहाँ ये द्विचर युग्म सामाजिक अंतर्विरोधों के बीच से प्रकट होते हैं। मगर कुछ कहानियाँ हैं जिनमें वे मनोवैज्ञानिक यथार्थ के भीतर से आए हैं। उदाहरण के लिए ‘प्रतिद्वंद्वी’ में सौतेले पिता और पुत्र के बीच का द्वंद्व।
कथानायक और विधवा अंजना के विवाह में अंजना का पुत्र गोपाल बाधा हो सकता है लेकिन कथानायक को उसे स्वीकारने में हिचक नहीं होती। लेकिन बाद में गोपाल की मौजूदगी को कथानायक बर्दाश्त नहीं कर पाता। सौतेले पिता की मनोवैज्ञानिक ग्रन्थि उसे जकड़ लेती है, और गोपाल में उसे दीगर होने (अदरनेस) का एहसास होता है। गोपाल के सामान्य कार्यकलाप भी उसे आपत्तिजनक लगते हैं और अंजना से वह कहता है कि उसे कहीं और जाने को कह दो। लेकिन एक दिन उसकी नाराज़गी के बाद सचमुच गोपाल घर नहीं लौटता। पूछने पर अंजना उसके घर छोड़ने की सूचना देकर फूट-फूट कर रो पड़ती है। गोपाल के कपड़ों के ख़ाली-ख़ाली हैंगरों को लटकते हुए देखकर कथानायक के भीतर कुछ पिघलने लगता है और उसे लगता है गोपाल उसका प्रतिद्वंद्वी है जिससे वह परास्त हो चुका है। गोपाल की छोड़ी हुई सिर्फ़ एक चीज़ घर में रह गयी है, वह कैलेंडर जिसे वह लेकर आया था। द्विचर युग्म के अंतर्विरोध का समाहार यहाँ पश्चाताप की व्याकुलता में होता। कहानी का मर्म और उसका संवेदनात्मक असर पाठक की चेतना को झकझोर देता है।
अब्दुल बिस्मिल्लाह की कहानियाँ परिवेश को रचने की प्रक्रिया में मनुष्यता के मर्म को पहचानने का प्रयत्न करती हैं। वे अस्मिता को इस मर्म की पहचान के आड़े नहीं आने देतीं।
