मानुषी विभीषिका के विरुद्ध

सामाजिक भाव-बोध का परिवर्तित स्वरूप रचनाकार अथवा रचनाओं की जीवन-यात्रा से जुड़ा होता है। यह यात्रा सकारात्मक रूप से सामाजिक चिन्हों को दर्ज करती है जिसका एकमात्र लक्ष्य मानवता की स्थापना होती है। यहाँ ‘स्थापना’ का सम्बन्ध ‘सम्भावना’ से जुड़ता है जो वास्तविक अर्थ में दुविधा पैदा करती है। यह दुविधा है- स्थापित हो जाने के बाद ‘सम्भावना’ पर आश्रित होने के प्रश्न पर। यह जटिल इसलिए भी है क्योंकि ‘स्थापना’ एक अर्थ में सिद्ध हो चुकी प्रमाणिक अवस्था है लेकिन ‘सम्भावना’ या तो स्थापना की प्रक्रिया से पीछे है या फिर प्रक्रियात्मक अवस्था में है। फिर प्रश्न उठता है कि स्थापित हो जाने के बाद ‘सम्भावना’ का औचित्य कैसा? कविता इसी औचित्य और अनौचित्य में अपना बसेरा बनाती है।
कविता के सन्दर्भ में यह जटिल इसलिए भी है क्योंकि जब मनुष्यता ही अपनी जटिलतम स्थिति को प्राप्त हो चुकी हो तब कविता की यात्रा भी स्वाभाविक रूप में उसी दिशा को प्राप्त हो जाती है। यहाँ जटिलता भाषा-बोध या कहने की रीति से सम्बन्धित नहीं है बल्कि यह परिस्थिति और परिवेशगत है। यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि ‘कहने की भाषा’ का सम्बन्ध सरलता या जटिलता के साथ जोड़ देने से काव्य न तो सरल हो जाता है और न ही कठिन। दरअसल यह बहस ही असाहित्यिक है। यह राजनैतिक विमर्श में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला तत्त्व है जहाँ जनता को नव-औपनिवेशिक मान्यताओं के आधार पर यह भ्रम परोसा जाता है कि वह (जनता) सब समझती है। जबकि स्थिति ठीक इसके विपरीत होती है। ‘ये पब्लिक है, ये सब जानती है’, जैसे सुगम गीत राजनीति का हिस्सा तो हो सकती है लेकिन साहित्य का नहीं। इस तरह की समझ समाज के प्रति दायित्व-बोध की इतिश्री का गैर-सामाजिक षडयन्त्र भर है और इससे अधिक कुछ भी नहीं।
यहाँ भाषा से अधिक परिवेश और परिस्थितियों की यात्रा का स्वरुप अधिक महत्त्वपूर्ण होता है। इसलिए कवि के लिए यहाँ ‘सम्भावना’ ही सबसे बड़ा अस्त्र है, उन त्रासकारकों के समक्ष जिनके लिए समाजभक्षण ‘अनिवार्य’ मूल्य होता है। दुर्गा प्रसाद गुप्त की कविताओं की दुनिया इसी ‘अनिवार्य’ बनाम ‘सम्भावना’ की दुनिया है, जहाँ एक तरफ अनुचित वैभव का प्रदर्शन है तो दूसरी ओर वैश्विक मनुष्यता का दर्शन।
इस सन्दर्भ में गम्भीरता से विचार करें तो यह प्रश्न उठता है कि- आखिर ऐसा क्या हुआ कि ‘अकेलेपन में भी इश्क सूफी है’ लिखने वाला रचनाकार लिख रहा है- गोलियाँ, बम, बारूद, धमाका, खून…… इत्यादि? क्या एक संवेदनशील समाज के लिए यह परिवर्तन सामान्य है? काव्य-रूप के कोमल भाव का यह परिवर्तित स्वरुप जिन जटिलताओं की ओर इशारा करता है वही जटिलता दुर्गा प्रसाद गुप्त के सामने चुनौती के रूप में है।
दुर्गा प्रसाद गुप्त की काव्य-यात्रा में इन सभी परिवर्तित त्रासदीपूर्ण तत्त्वों को देखा और समझा जा सकता है। लेकिन विचारणीय यह है कि कवि और कविता कहाँ खड़े हैं? इन सभी प्रश्नों पर गम्भीरता से विचार करने पर ही हम उनके काव्य-भाव को स्पर्श कर सकते हैं। वे कहते हैं कि-
“जब अन्याय की बारिश में बह जाती है मनुष्यता
हमारे प्रतिरोध को निगल जाती है दुनिया की खामोशी
तब दुःख के क्षणों में
बची रहती हैं थोड़ी सी प्रार्थनाएँ
हिंसा की इस दुनिया में !
इश्वर है या नहीं
यदि वह होता तो सबसे पहले सन्मति इजरायल को फिर अमेरिका को
उसके बाद यूरोप को देता
जो हिंसा तो एक साथ मिलकर करते हैं और समझ उसकी रखते हैं
अलग–अलग
न्याय और अन्याय की अद्भुत
व्याख्याएँ हैं उनकी!!” (फिलिस्तीन के लिए)
इन पंक्तियों में लगभग सारी बातें कह दी गयी हैं। जो विद्वान दुर्गा प्रसाद गुप्त की रचनात्मक दुनिया से परिचित हैं वे भली-भाँती जानते हैं कि उनके रचना विधान का स्त्रोत भारतीय चिन्तन विधान से मुक्त नहीं बल्कि गहरे अर्थों में युक्त होता है। इसे समझने के लिए हमें डॉ. अम्बेडकर के एक कथन को ध्यान में रखना होगा। वे कहते हैं कि- “इतिहास इस बात का समर्थन करता है कि राजनैतिक क्रान्तियों के पहले सदा ही सामाजिक और धार्मिक क्रान्तियाँ होती रही हैं।” इसी क्रम में वे आगे यूरोप के लिए लूथर द्वारा जारी किया गया धार्मिक संस्कार, इंग्लैंड के लिए प्युरीटिनिज्म, अमेरिका के लिए भी प्युरीटिनिज्म (धार्मिक आन्दोलन), अरबों के लिए हजरत मुहम्मद के साथ साथ भगवान बुद्ध और गुरु नानक द्वारा किए गये परिवर्तन को रेखांकित करते हैं (जाति भेद का उच्छेद)।
डॉ. अम्बेडकर के इस विचार को ध्यान में रखते हुए हमें दुर्गा प्रसाद गुप्त की ऊपर दी गयी पंक्तियों पर विचार करने की जरुरत है। यह बेहद महत्त्वपूर्ण और जरुरी प्रसंग है। वे जिस न्याय-अन्याय, प्रार्थनाएँ, इजराइल और यूरोप की बात करते हैं उसमें सबसे महत्त्वपूर्ण शब्द है- ‘सन्मति’। अर्थात शुभबुद्धि, सम्यक् बुद्धि। किसी भी समुदाय की मान्यता और उसके व्यवहार का सम्बन्ध उसके प्राचीन ग्रन्थों में निहित होता है। इस आधार पर देखें तो यहूदी धर्म ग्रन्थ ‘तोराह’ की पाँच पुस्तकों में से तीसरी पुस्तक है- लैव्यवस्था। इस ग्रन्थ का पहला शब्द ही है ‘और उसने पुकारा’। यह मानवीयता और भाईचारे का प्रतीक है। कविता में ‘बची हुई है फिलिस्तीन की आवाज’ के साथ ‘और उसने पुकारा’ से क्या जाहिर होता है? इसी ग्रन्थ में कहा गया है कि ‘अपने पड़ोसी से ऐसे प्रेम करो जैसे स्वयं से’। मलाकी की पुस्तक ‘तनख’ में जो मूल्य स्थापित हैं वह है- याजकीय नैतिकता (प्रिस्टली एथिक्स), सामाजिक न्याय (सोशल जस्टिस) और इश्वर से भय (फियर ऑफ़ गॉड)।
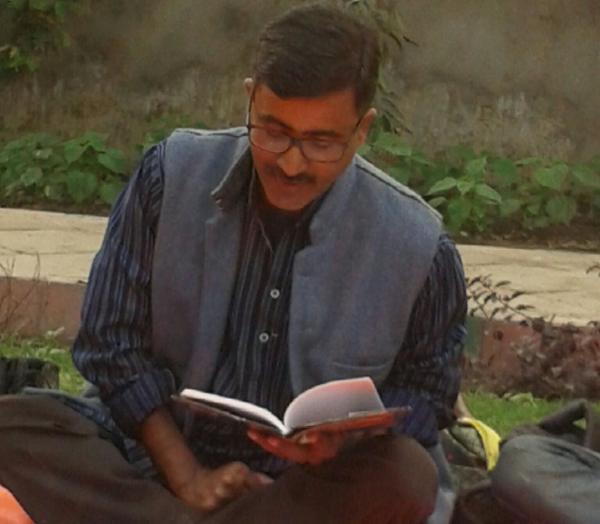
दुर्गा प्रसाद जिस ईश्वर के बारे में कहते हैं कि ‘इश्वर है या नहीं / यदि वह होता तो सबसे पहले सन्मति इजरायल को’ इन पंक्तियों के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए। मनुष्यता को तार-तार करने वालों के ‘ईश’ किस अर्थ में हैं? क्या उनके यहाँ ‘सन्मति’ की कोई नींव नहीं है? इस बिंदु पर गहराई से विचार करें तो ‘तोराह’ की अन्तिम पुस्तक है- ‘व्यवस्थाविवरण (ड्यूटरोनौमी ) जिसे हिब्रू में देवरिम (देवरिम) कहा गया है, जिसका अर्थ है ‘वचन’ या ‘शब्द’। यह मूसा के अन्तिम भाषणों का संकलन है, जो उन्होंने इजराइलियों को वाचा भूमि (प्रोमिस्ड लैंड) में प्रवेश से पहले दिया था। इस ग्रन्थ के मूल सरोकार हैं- विधवाओं, अनाथों, परदेसियों के प्रति करुणा और न्याय की आवश्यकता। दुर्गा प्रसाद की कविता ‘सभ्य होने की निशानी’ (सम्भवतः अप्रकाशित) की पंक्तियाँ हैं- ‘हमारे बच्चों, स्त्रियों और घरों को / बेरहमी से / उड़ा देने वाले बमों में / तुम्हारी बर्बरता ही नहीं / तुम्हारे सभ्य होने की निशानी भी दिखती है। अब जरा इन पंक्तियों को ‘तोराह’ की अन्तिम पुस्तक के मूल सरोकार के समक्ष रखें तो ‘सभ्य ढाँचे में छुपी असभ्यता का आवरण’ स्पष्ट रूप में दिखने लगता है। ग्रन्थ विधवाओं के प्रति न्याय की बात करता है लेकिन यहाँ विधवाओं की अनुचित निर्माण-व्यवस्था है, ग्रन्थ अनाथों की रक्षा की बात करता है लेकिन यहाँ बच्चों को यतीम बनाने की व्यवस्थाएँ संचालित हैं।
दुर्गा प्रसाद गुप्त की पहली कविता (फिलिस्तीन) पर फिर से लौटें और उसके आधार पर विचार करें तो प्रसिद्ध यहूदी विद्वान हिलेल का कथन ध्यान में आता है जिसमें वह ‘तोराह’ का मूल भाव संक्षेप में स्पष्ट करते हुए कहता है कि- ‘सह-अस्तित्व और भाईचारा ही इसका मूल है’। क्या हिलेल के इस मूल भाव और कविता में उठाए गये प्रश्नों का किसी के पास कोई जवाब है? कवि जिस ‘सन्मति’ के आदर्श को स्थापित करता है, क्या उस व्यवस्था या परम्परा से यह लोक शून्य है? और यदि ऐसा नहीं है फिर अपनी ही परम्परा के ठीक विरोध में खड़े होकर अत्याचार को मानवता के ऊपर स्थापित करने की क्या मजबूरी है? इस प्रश्न की आवश्यकता और इसके कारणों की ओर इशारा कविता की आगे की पंक्तियों में स्पष्ट है।
‘सबसे पहले सन्मति इजरायल को/ फिर अमेरिका को/ उसके बाद यूरोप को देता’ यह पंक्ति ‘कहन’ की संरचना में इस प्रकार से पूर्ण है कि इसकी अलग से व्याख्या की जरुरत ही नहीं महसूस होती। ‘न्याय और अन्याय की अद्भुत व्याख्याएँ हैं उनकी’, सारी व्याख्याएँ बदल चुकी हैं।
तोराह, तनख, और तलमूद जैसे ग्रन्थों की व्याख्या बदल चुकी है। ईसाई धर्म ग्रन्थ की भी व्याख्या बदल चुकी है, जहाँ जरुरतमंदों के पक्ष में आवाज उठाने की व्याख्या है। यहूदी धर्म ग्रन्थ हो, ईसाई ग्रन्थ हो या इस्लामिक ग्रन्थ, सभी का आधार मानवता के पक्ष में है, लेकिन वर्तमान षडयन्त्रवादी माहौल में सारी परिभाषाएँ बदल दी गयी हैं। दुर्गा प्रसाद गुप्त इसलिए ‘सन्मति’ की बात करते हैं क्योंकि यही वह भाव-बोध है जिससे हम भूलते मानवीय पक्ष को फिर से आकार दे सकते हैं।
‘अँधेरे की रुलाइयाँ’ शीर्षक से लिखी कविता में उन्होंने इस मानवीय पक्ष के मिट जाने से जो अमानवीयता पैदा हो रही है, उसका कारुणिक चित्रण किया है। ‘अँधेरे की रुलाइयाँ सुनी तो जा सकती है / पर देखी नहीं जा सकती है’। इन पक्तियों में कारुणिक स्थिति का ऐसा दृश्य उभरता है जिसकी कल्पना मात्र से मनुष्य में सिहरन पैदा हो जाए। यह पंक्ति भावनाओं के शिखरतम लेखक शरतचंद्र की याद को ताजा कर देती है। ‘अँधेरा’ और ‘रुदन’ के अलग-अलग भावों के आन्तरिक स्पर्श की जो व्याख्या उनके कथा साहित्य में है, उसका एक रूप आधुनिक विडंबनाओं में यहाँ प्रस्तुत हुआ है। शरदचंद्र के यहाँ अँधेरे का रूप और शक्ल है लेकिन उसे देखने की दृष्टि सभी के पास नहीं है। इसलिए अँधेरे के यथार्थ को खारिज करने के षड्यन्त्र पर वे भड़क कर कहते हैं कि –‘यह कौन मिथ्या प्रचार कर रहा है कि अँधेरे का रूप और शक्ल नहीं होता? दृष्टिविहीनता को देख पाने के लिए भी दृष्टि की ही जरुरत होती है और यही दृष्टि रचनाकार को विशिष्ट बनाती है। शरतचंद्र जिस रूप और शक्ल की बात करते हैं उसे सभी तरह की दृष्टियाँ आखिर क्यों नहीं देख पाती? यही प्रश्न इस कविता की सार्थकता को सिद्ध करती है जिसमें पूंजीवादी समाज द्वारा प्रदत्त दृष्टिविहीनता पर कवि प्रश्न खड़ा करता है।
कविता की इस पंक्ति का दूसरा शब्द है- ‘रुलाइयाँ’। रुलाइयाँ या रुदन एक तरह से बहुआयामी अभिव्यक्ति है। इस कविता में रुदन का जो स्वरुप अभिव्यक्त हुआ है वह बेहद मार्मिक है। यह रुदन भूख, दर्द, भय या अन्य शारीरिक पीड़ा से उत्पन्न नहीं है। यह ‘मौन-रुदन’ है, जहाँ आवाज गौण होती है। इस रुदन में सामाजिक अस्वीकार का भाव है, इसलिए इसकी पीड़ा अवर्णनीय हो जाती है। इस अवर्णनीय पीड़ा को देखने के लिए, महसूस करने के लिए सिर्फ गम्भीर होना अपर्याप्त है, इसके लिए मौनशीलता का होना जरुरी है। मौनशीलता से युक्त ह्रदय ही ‘अँधेरे की रुलाइयाँ’ को अभिव्यक्त कर सकता है। एहसाह करने की यही अवस्था है जिसमें डूबकर कवि कहता है कि- ‘इसलिए अपनी यातना में तुम नहीं / मैं फिलिस्तीन हूँ’। यह दूसरे के दुःख को स्वयं महसूस करने की चरम अवस्था है।

दुर्गा प्रसाद गुप्त की कविताओं की एक विशिष्ट बात यह है कि उनके यहाँ ‘मनुष्यता’ किसी खास वर्ग या समूह के लिए अभिव्यक्त नहीं होता है। इसलिए आसानी से देखा जा सकता है कि शांति, समानता, अधिकार और बन्धुत्व की भावना से निर्मित ‘मनुष्यता’ का स्वरुप किसी पक्ष-विपक्ष के दायरे से मुक्त है। इसे और अधिक सरलता में समझें तो पूंजीवादी समाज हमारे सामने पक्ष-विपक्ष से लिप्त ‘विकल्प’ पेश करता है। इसका सबसे अधिक प्रभाव राजनैतिक अनुशासनों में देखा जा सकता है। वहाँ ‘मनुष्यता’ पर ‘पक्षीय-स्वभाव’ केंद्रीय मूल्य है। इसलिए वहाँ कोई ‘मनुष्य’ के पक्ष में न होकर या तो फिलिस्तीन के पक्ष में है या फिर इजराइल के पक्ष में है। ‘फिलिस्तीन के लिए’ कविता में कवि कहता है कि – ‘अंत में अपनी बची-खुची सन्मति / शेष दुनिया के उन देशों को देता / जो हिंसा में विश्वास रखते हैं! फिलिस्तीन के लिए ही नहीं / दुनिया में / जहाँ कहीं भी हिंसा हो’/ उसके लिए भी। कविता का शीर्षक है – ‘फिलिस्तीन के लिए’ और इसमें ‘मनुष्यता’ का स्वरूप है सारी दुनिया के लिए। ‘फिलिस्तीन के लिए ही नहीं’ से स्पष्ट हो जाता है कि कवि और कविता का पक्ष अन्ततः ‘मानवीयता’ का पक्ष है, इसलिए यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि कवि एकपक्षीय है।
दुर्गा प्रसाद गुप्त की कविताओं में अपनी परम्परा की खोज का स्वरूप हमेशा से जुड़ा रहा है। उनके संग्रह ‘अकेलेपन में भी इश्क सूफी है’, में जहाँ तुलसी, कालिदास, बाबा नागार्जुन से लेकर वली दकनी, हज़रतबल, अमजद साबरी तक की परम्परा से जुड़ाव दिखता है, वहीं इस काव्य में बुद्ध और गाँधी की अहिंसा का निराकरणीय स्वरूप भी प्रस्तुत होता है। निराला ने लिखा था कि – “देश-काल के शर से बिंधकर / यह जागा कवि अशेष, छविधर”। वर्तमान और अतीत को एकसूत्र में देखते हुए त्रासद परिस्थितियों के समाधान के लिए यह आवश्यक शर्तें हैं जिससे हमेशा अलगाववादी दृष्टि परहेज करती आयी है।
समुचित रूप में देखें तो दुर्गा प्रसाद गुप्त की कविता – ‘फिलिस्तीन के लिए’, ‘अँधेरे की रुलाइयाँ’, फिलिस्तीन हूँ मैं’, ‘एक दीया’, ‘सभ्य होने की निशानी’ में क्षत-विक्षत मनुष्यता की कराहती आत्मा की आवाज है। मार्मिक यथार्थ-बोध का गतिशील स्वरूप जो बुद्ध और गाँधी की अहिंसा से गुजरते हुए वैश्विक न्याय की अवधारणा की संपूर्ण संरचना पर प्रश्न खड़ा करती है। यह वैश्विक क्रूरता पर वैश्विक मनुष्यता का काव्य प्रश्न है, जिसे दुनिया ने अनुत्तरित छोड़ दिया है। समुचित रूप में देखें तो दुर्गा प्रसाद गुप्त की कविता – ‘फिलिस्तीन के लिए’, ‘अँधेरे की रुलाइयाँ’, फिलिस्तीन हूँ मैं’, ‘एक दीया’, ‘सभ्य होने की निशानी’ में क्षत-विक्षत मनुष्यता की कराहती आत्मा की आवाज है। मार्मिक यथार्थ-बोध का गतिशील स्वरुप जो बुद्ध और गाँधी की अहिंसा से गुजरते हुए वैश्विक न्याय की अवधारणा की संपूर्ण संरचना पर प्रश्न खड़ा करती है। यह वैश्विक क्रूरता पर वैश्विक मनुष्यता का काव्य प्रश्न है, जिसे दुनिया ने अनुत्तरित छोड़ दिया है।



ऐसा लेखन कम देखने को मिलता है।
लेखक ने अत्यंत मौलिक और दार्शनिक ढंग से दुर्गा जी की कविताओं की शिनाख्त की है।
बधाई