दंतकथा की जिजीविषा : मनुष्यता की हार

अब्दुल बिस्मिल्लाह का उपन्यास ‘दंतकथा’ उस गहरी विडम्बना को बेपर्दा करता है, जहाँ सभ्यता की विजय दरअसल मनुष्यता की पराजय बनकर उभरती है। प्रखर लेखिका और आलोचक सुप्रिया पाठक का इस उपन्यास पर लिखा यह लेख एक देसी मुर्गे की दृष्टि से रची गयी कथा में छिपी सामाजिक क्रूरताओं, असमानताओं और प्रकृति के साथ हुए छल को मार्मिक ढंग से उद्घाटित करता है। यह मुर्गा महज एक पक्षी नहीं, बल्कि उस निरीह मनुष्य का प्रतीक है, जो जाति, वर्ग, लिंग और आर्थिक शोषण के दुष्चक्र में फँसा हुआ है। सवाल यह है कि क्या सभ्यता के नाम पर अर्जित की गयी यह हिंसा वास्तव में हमें ‘मनुष्य’ बनाती है? यही सवाल इस लेख की केंद्रीय संवेदना बनकर उभरता है। सुप्रिया पाठक ने इस लेख के माध्यम से अब्दुल बिस्मिल्लाह की कथा-दृष्टि, उनके रचनात्मक सरोकारों और प्रतीकों की सघन व्याख्या करते हुए स्त्रीवाद, पर्यावरण और मानवता के अन्तःसम्बन्धों की भी गहराई से पड़ताल की है। यह न केवल ‘दंतकथा’ को नये सन्दर्भों में देखने का अवसर प्रदान करता है, बल्कि मनुष्यता की पुनर्रचना की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है — जहाँ एक मुर्गे की जिजीविषा, हमारी चेतना के दर्पण में झाँकने का साहस कराती है।
‘वह दौड़ रहा था। वह उड़ कर इधर-उधर छिप रहा था। वह भयग्रस्त आतंकित था। वह अपनी जान बचाने के लिए कोई सुरक्षित स्थान खोज रहा था. क्यों? शायद उसने कोई खतरा देख लिया था! या फिर ऐसी स्थितियों से वह पहले भी दो-चार हो चुका था, कि अचानक उसे एक बड़ा-सा छेद दिखाई पड़ा और वह उसमें घुस गया। वह छेद एक नाबदान यानी घर का गंदा पानी बहाई जानी वाली नाली का था। नाली के मुँह पर यूँ तो लोहे की जाली गली रहती थी, मगर जाली टूट गई थी। इसलिए वह निकाल दी गई थी…। कुछ इसी प्रकार का दृश्य था वह, जिसमें अपने नायक को मैंने अभिनय करते हुए देखा था नायक, यानी एक मुर्गा। देसी मुर्गा! देसी मुर्गा पोल्ट्री फ़ार्म के मुर्गे से भिन्न होता है। पोल्ट्री फार्म के मुर्गे को एक छोटा-सा बच्चा भी आसानी से पकड़ सकता है। मगर देसी मुर्गा! उसे पकड़ने में अच्छे-अच्छों के छक्के छूट जाते हैं। जी हाँ, मेरा नायक वही था। एक देसी मुर्गा।‘
–अब्दुल बिस्मिल्लाह
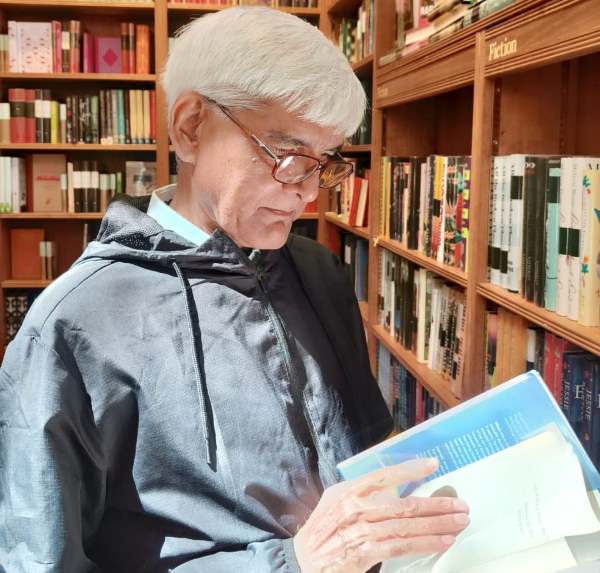
अब्दुल बिस्मिल्लाह मेरे प्रिय लेखकों में से एक हैं जिन्हें पढ़ते हुए मानव समाज में कई परतों में मौजूद गैर बराबरी, शोषण और मानवीय संबंधों में अंतर्निहित स्वार्थ-द्वेष की समझ विकसित हुई। उनकी रचनाओं में सबसे पहले मैंने झीनी झीनी बीनी चदरिया पढ़ी। बनारस ,गाजीपुर और उसके आस पास रहने वाले हम जैसे पाठकों के लिए वह सिर्फ एक उपन्यास नहीं था ,बल्कि हमारे समाज का वास्तविक आख्यान था जिससे जाने-अनजाने हमें दूर रखा गया था। जिन बनारसी साड़ियों से हमारे घरों की स्त्रियों का शृंगार होता था और वे अपने नए वैवाहिक जीवन में प्रवेश करती थीं, उसे बुनने वाले जुलाहा समुदाय की जीवन परिस्थितियाँ इतनी विषम थीं कि उस साड़ी को सिर्फ एक बार पहन लेने का चाव लिए उनके समाज की स्त्रियां इस दुनिया से विदा हो जाया करतीं। इस बात की कल्पना मात्र ही बेहद पीड़ादायी है। इससे बड़ी विडंबना भला इस मानव समाज में क्या होगी कि पकाने वाले हाथों ने कभी खुद उसका स्वाद नहीं चखा। बनारस के बुनकर समुदाय के जीवन और हिन्दू समाज के साथ उसके आर्थिक ताने-बाने की कड़वी तस्वीर पेश करते इस उपन्यास ने मेरे जैसे सैकड़ों पाठकों के मन को उद्वेलित किया होगा। अब्दुल बिस्मिल्लाह हिन्दी साहित्य जगत के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं जो लगभग तीन दशक से साहित्य सृजन में सक्रिय हैं। ग्रामीण जीवन व मुस्लिम समाज के संघर्ष, संवेदनाएं, यातनाएं और अन्तर्द्वंद उनकी रचनाओं के केन्द्र बिन्दु रहे हैं। कुठाँव, अपवित्र आख्यान, मुखड़ा क्या देखे, समर शेष है, ज़हरबाद,दंतकथा, रावी लिखता है, अतिथि देवो भव, रैन बसेरा, रफ़ रफ़ मेल,शादी का जोकर, ताकि सनद रहे ,वली मुहम्मद और करीमन बी की कविताएँ, छोटे बुतों का बयान, दो पैसे की जन्नत, अल्पविराम, कजरी, विमर्श के आयाम, दस्तंबू जैसी महत्वपूर्ण रचनाओं के रचयिता के अत्यंत महत्वपूर्ण उपन्यास ‘दंतकथा’ की चर्चा आज के समय में मनुष्यता के लगातार होते क्षय की दृष्टि से समीचीन है। अब्दुल बिस्मिल्लाह को पढ़ने का अर्थ है—हाशिए पर खड़े समाज की नब्ज को महसूस करना, उसके दुख-सुख, द्वंद्व और प्रतिरोध को गहराई से जानना। उनकी रचनाओं में जीवन किसी भावुक कल्पना की तरह नहीं, बल्कि जीती-जागती विडम्बनाओं, संघर्षों और उम्मीदों से बना यथार्थ है। मुस्लिम समाज की आन्तरिक जटिलताएँ हों या बुनकरों की रोज़मर्रा की मुश्किल ज़िन्दगी, हिन्दू-मुस्लिम रिश्तों की सामाजिक परतें हों या स्त्री जीवन की मार्मिक गाथाएँ—बिस्मिल्लाह हर जगह अपनी विशिष्ट दृष्टि और गहरी आत्मीयता के साथ उपस्थित होते हैं। उनकी कथा-भूमि में गाँव है, कस्बा है, शहर की सरहदें हैं लेकिन सबसे प्रमुख है इंसानी चेतना, जो सामाजिक-सांस्कृतिक जड़ताओं से टकराती है, कभी टूटती है, तो कभी पूरे आत्मबल के साथ टिके रहने की कोशिश करती है। उनका लेखन यथार्थ की जड़ता को केवल दर्ज नहीं करता, बल्कि उसमें छिपी परिवर्तन की सम्भावनाओं को भी टटोलता है।[1]
1990 के प्रारंभ में प्रकाशित उपन्यास ‘दंतकथा’ कई दृष्टियों से चर्चा के योग्य है। प्रथमतया यह रचना प्रक्रिया एवं भाषा शिल्प की दृष्टि से अनूठा उपन्यास है जिसमें अपनी प्राण रक्षा के लिए नाबदान में जा फंसे एक मुर्गे की व्यथा-कथा के जरीए लेखक ने हमारे मानव समाज में जानवरों एवं कमजोर समुदायों के प्रति मौजूद क्रूर यातनाओं से मिलने वाले पाशविक आनंद तथा जीवन के अंतिम क्षणों में एक निरीह जीव के मन में मृत्यु को लेकर पैदा होने वाले डर को एक साथ रचा है। किसी रचनाकार के लिए जानवरों एवं पशु पक्षियों के मन में मनुष्य समाज के प्रति मौजूद भावों को मुकम्मल तौर पर,पूरी संवेदना के साथ रचना में उतार पाना इतना सरल और सहज नहीं होता जितनी सहजता से लेखक ने अपनी इस छोटी सी रचना में कर दिखाया है। अपनी रचना प्रक्रिया के अनुभवों के संबंध में अब्दुल बिस्मिल्लाह लिखते हैं : मैंने कहीं पढ़ा था, संभवत: किसी महान कथाकार का कथन है, कि मनुष्यों पर लिखने से अधिक कठिन है पशु-पक्षियों पर लिखना। नि:संदेह यह बात सही है। क्योंकि मनुष्य के मनोभावों को हम आसानी से पकड़ लेते हैं। उनके चारित्रिक उतार-चढ़ाव को भी समझना अपेक्षाकृत सरल होता है। बहुत-सी बातें वार्तालाप से स्पष्ट हो जाती हैं। पशु-पक्षियों के संदर्भ में यह सहज सम्भव नहीं है। इसलिए जब मैंने इस ‘दंतकथा‘ की योजना बनाई तो ऐसा कर पाना मेरे लिए एक बड़ी चुनौती जैसा था। फिर भी मैंने इस विषय पर सोचना शुरू कर दिया।[2]
यह नाबदान में फंसे एक मुर्गे की कहानी होने के साथ-साथ प्रकृति, जीव और मनुष्यों के बीच मौजूद गहरी खाई की सम्यक पड़ताल भी है। मनुष्य समाज ने अपने अहंकार के सामने प्रकृति के अस्तित्व को लगभग खारिज सा कर दिया क्योंकि अपनी विकास यात्रा में उसने जल, जंगल और जमीन को नियंत्रण में करना सीख लिया था। प्रकृति की जिस पहेली को वह सुलझा नहीं पाया,उसने उसे ‘ईश्वर’ का नाम देकर उसकी पूजा शुरू कर दी। उसके अंदर प्रारंभ से ही विजेता का भाव रहा जिसने हमेशा प्रकृति को ‘अन्य’ समझा। ठीक उसी भाव में पुरुष समाज ने अपनी स्त्रियों को‘अन्या’बनाए रखा। इस भाव में ही हिंसा निहित थी जिसने कालांतर में जाति, धर्म, वर्ग और लैंगिक असामानता और शोषण को पोषित किया। जीवन और मृत्यु के बीच फंसा मुर्गा न आगे बढ़ सकता है और न पीछे खिसक सकता है क्योंकि लोहे की वह नुकीली छड़ उसके जिबह की प्रतीक्षा में है। अपने पंखों के नीचे लगातार रिसते गंदले पानी और उसके साथ बहकर चले आए चावल और दाल के टुकड़ों के सहारे अपनी जीवन यात्रा की खट्टी मीठी स्मृतियों में खोया हुआ मुर्गा लेखक का वह सांकेतिक पात्र है जो मनुष्यों का भी प्रतिनिधित्व करता है। इस पृथ्वी पर सम्मानजनक जन्म एवं मृत्यु का अधिकार प्रत्येक जीव को है। मुर्गा मनुष्यों के हाथों नृशंस हत्या का पात्र नहीं बनाना चाहता और न ही वह अपने जैसे अन्य मुर्गे-मुर्गियों की तरह जिबह किए जाते व्यक्त मनुष्यों के बच्चों को छुरे के चलने के बाद उठने वाले खून के फव्वारे को देखकर आनंदित होने का स्वर्गिक सुख देना चाहता है। उसे अब भी याद है अपनी बीमार मां की बेबस ‘हत्या’ जिसे मारे जाने के बाद उसके शरीर से खून नहीं निकला बल्कि पीली सी लार निकली जो उसके मालिकों की देन थी। जल्दी जल्दी अंडे और चूजे पाने की लालच में उन मुर्गियों को दी जाने वाली गोलियों ने उनपर ऐसा असर दिखाया कि वे ‘कुड़क’ हो गई जिसके बाद वे उनके किसी काम की नहीं बची ,फिर एक दिन घर वालों ने उसका गोश्त पकाया और मजे से खाया। हमारा पुरुष समाज भी तो अपनी स्त्रियों के साथ हमेशा से यही करता आया है, आज भी उनकी उर्वरता का बाजारीकारण अनवरत जारी है। आँकड़े बताते हैं कि सेरोगेसी के इस बाजार में निर्धन तबके की मजबूर और मजबूत स्त्रियाँ प्रतिवर्ष निःसंतान विदेशियों और देशी दम्पत्तियों के लिए ‘हेल्थ टूरिज़्म’ का साधन बनती हैं और यह सिलसिला तब तक चलता है जब तक उस स्त्री में गर्भ धारण करने की क्षमता बची रहती है। बाजार और पुरुषों के हाथ आई कृत्रिम गर्भाधान की तकनीक ने प्रकृति, जीव –जंतुओं और स्त्री सभी के साथ छेड़छाड़ किया है। मुर्गा अपनी माँ की तरह बेबस मृत्यु नहीं चाहता,वह चाहता है एक गरिमामय जीवन। भूख और ठंढ से बेहाल और निढाल होने के बावजूद वह उस अंधेरे नाबदान में एक सुनहरे भविष्य का ख्वाब देखता है।
इस उपन्यास को पढ़ते हुए लगातार पाठकों के अंदर यह जिज्ञासा बनी रहती है कि आखिर यह कहानी किसकी है मनुष्य की या मुर्गे की? क्योंकि उसका बचपन, बेखौफ गाँव के खेत खलिहानों में घूम आने, बांग लगाने, अपने जैसे दूसरे चूजों और मुर्गे-मुर्गियों संग साथ दाना चुगने और सुबह की पहली किरण के साथ बांग देने की स्मृतियाँ ठीक वैसी ही हैं जैसी किसी मनुष्य के बचपन की स्मृतियाँ। जिस रोज उसके मालिक ने उसे किसी और के हाथों बेचा और थैले में कपड़ों के बीच दबा वह जब शहर की आबोहवा में पहुँचा तब जाकर उसे जीवन और मनुष्यों की वास्तविक क्रूरता का एहसास हुआ। दड़बे में उसके जैसे बंद कई मरियल मुर्गों की हालत एक जैसी थी जो इधर-उधर से पकड़ कर जमा गए थे और घरवालों के मनोरंजन और जिबह के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। मुर्ग़ा इस कैद में लगातार सोचता है अपने बारे में, अपनी जाति के बारे में। और सिर्फ़ सोचता ही नहीं, दम घोंट देनेवाले उस माहौल से बाहर निकलने के लिए जूझता भी है। वह लड़ता है भूख से, मौत से, और सबसे ज़्यादा उस नियति से जो उसे मनुष्य के हाथों हलाल होते देखने को मजबूर करती है।
नाबदान में फंसा पड़ा वह मुर्गा मनुष्यों के स्वभाव के बारे में सोचता हुआ मुस्कुराता है कि किस तरह उन्होंने हंसने, रोने, सुख-दुख, हर्ष-विषाद जैसी स्वाभाविक क्रियाओं पर भी अपना एकाधिकार बना रखा है। अपने आप को संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी समझने वाला मनुष्य अन्य सभी जीव-जंतुओं को भावहीन समझते हैं। इसलिए कैद करके ले जाते हुए मुर्गे की आवाज कोई सुन न सके और न वह भाग सके इसके लिए उसकी चोंच और टांगें दोनों ही पतली रस्सी से बांध दी गई थीं। वह बंधन इतना सख्त था कि प्रकृति से साथ अपने नियत समय पर बांग देने वाला मुर्गा उस दिन ठीक से अपनी आवाज भी नहीं निकाल पाया। शहर और गाँव की जिंदगी का फ़र्क भी उस दिन उसे पहली बार समझ में आया। गाँव के जीवन में जो सरलता थी, अपने पालतू जीवों के प्रति जो प्रेम और दुलार का भाव था उसके विपरीत शहर का यथार्थ बेहद कठोर था। यहाँ प्रेम करने की भी आजादी नहीं थी। मुर्गा उस नाले में बंद अपने प्रेम के दिनों और अपनी प्रिय पोई की सुखद स्मृतियों को भी जीता है। मनुष्यों की तरह पशु पक्षियों का प्रेम जाति, धर्म के नियमों में बंधा नहीं होता, बल्कि बहुत उन्मुक्त होता है। वहाँ प्रेम में प्रेयसी की इच्छा का सम्मान है, प्रतीक्षा और समभाव है। वहाँ प्रेम सखा भाव से संचालित होता है, पराधीनता और बंधन की सीमा से मुक्त। मृत्यु के समीप दंतकथा का मुर्गा इस दुनिया में व्याप्त भय,असुरक्षा,असंतोष और आतंक से पाठकों का साक्षात्कार कराता है। साथ ही, वह इन विषम परिस्थितियों में भी अपनी जिजीविषा से मनुष्यों की लोलुपता और हिंसा का सामना करता है ताकि हम सबके मन में जीवन और उसके उत्स के प्रति उम्मीद बची रहे। मनुष्य प्रकृति के रहस्यों और जीवों से लगभग विलुप्त हो रही मानवीय भावनाओं का सबक फिर से सीख सकें।
[1]https://rajkamalprakashan.com/blog/post/abdul-bismillah-at-75-literary
[2] https://kartavyasadhana.in/view-article/abdul-bismillah-on-his-book-dantkatha


