घाघ की कविताई बजरिए स्वराज आश्रम…

लोक कवि घाघ से प्रथम परिचय – दर्जा पाँच में घाघ की कुछ पंक्तियाँ मिली थीं – ‘छोटी सींग और छोटै पूँछ, ऐसा बरधा लो बेपूछ। छोटा मुँह और ऐंठा कान, यही बैल की है पहचान। नीला कंधा बैंगन खुरा, कभी न निकले कंता बुरा’…आदि।
तब इनके अनुसार हम घूम-घूम कर गाँव के सारे बैलों की पहचान किया करते थे – उनकी अच्छाई का परीक्षण। फिर कभी रौ में आकर जब इन कविताओं को चिल्ला-चिल्ला के गाते, तो सुनते ही गाँव के लोग भी कोई न कोई पंक्ति बता दिया करते थे और उन्हें यह भी पता होता था कि यह किसी घाघ नामक व्यक्ति का लिखा हुआ है, जो उनके लेखे कोई मँजा हुआ अनुभवी किसान रहा होगा, जो कबित्त भी करता रहाँ…।
फिर धीरे-धीरे घाघ हमारे चेतन मन से प्राय: निकल गये। लेकिन बी.ए. में कुछ मजबूरन कुछ मनभावन के योग से जब प्रमुख विषय (ऑनर्स कहते थे) के रूप में हिंदी साहित्य पढ़ने में लगा और मालूम पड़ा कि अच्छी कविता का एक बड़ा मतलब उसका जनसामान्य तक पहुँचना होता है तथा इस लियाक़त में सिरमौर कबीर-सूर-तुलसी-रहीम…आदि के नाम आये, तो मुझे उस बचपन की जानिब से घाघ की बड़ी याद सताने लगी थी, जो बिना किताब के मुखामुखम ही किसानोपयोगी रूप में जन-जन तक पहुँचा। पाँचवीं कक्षा की उस कविता में खेती-किसानी को सर्वोत्तम व्यवसाय बताया गया था – उत्तम खेती, मध्यम बान। निषिध चाकरी भीख निदान। लेकिन ध्यातव्य है कि घाघ के समय में जो चाकरी निषिद्ध थी, आज उसी ‘एगो नौकरी ख़ातिर’ सारी खेती-बारी छोड़के हम जैसे लोग बनेवा बन के शहर-शहर भटके और गाँवों में खेती करने वाले लोग बचे नहीं, न बची उस माटी से पैदा होते संस्कारों में घुली ममता व मनुष्यता…।
उक्त लोकप्रियता के साथ इस खोये हुए को याद दिलाने की प्रासंगिकता के लिए घाघ की कविताएँ खोजने लगा। तब किताबें पाने के ज्यादा सूत्र पता न थे और सूत्रवान हो जाने की स्थिति तक आते-आते घाघ के लिए वह बेचैनी इतनी मद्धम पड़ गयी कि खोजने की सुध ही भूल गयी…। लेकिन अभी पिछले 17 जून को अचानक व अनपेक्षित रूप से वह किताब हाथ आ गयी। कैसे, के लिए एक छोटा-सा घटना-क्रम शायद आपको ज्यादा अरोचक न लगे…!!
घाघ-भड्डरी : प्राप्ति की यात्रा-कथा – बनारस के अपने अनुजवत पड़ोसी-मित्र प्रो. रामप्रकाश द्विवेदी ने जाने किस दैवी-मानवी प्रेरणा से मुझे और दीदी को शूल टंकेश्वर ले चलने की पेशकश कर दी और मैंने वैसी ही किसी प्रेरणा से बिना कुछ सोचे-समझे हाँ कर दी। शूल-टंकेश्वर…जिसके लिए मान्यता है कि औगढ़ भगवान शंकर जब हिमालय से चले, तो वहीं गंगा-किनारे अपना त्रिशूल गाड़ दिया। शिव के त्रिशूल पर टिकी काशी बाद में बसी तो वहाँ से 5-6 किमी उत्तर, लेकिन वह स्थल भी ‘शूल टंकेश्वर’ नाम से एक पवित्र पूजा-दर्शन स्थल के रूप में ख्यात है और काशी देखने आये हर यात्री का वहाँ आना भी अ-निवार्य यात्रा-कर्म है। और अब तो इस कदर विकसित हो रहा है कि वहाँ भी एक ‘छोटका (मिनी) काशी’ बस जाए, तो ताज्जुब नहीं। हम सभी कई बार जा ही चुके हैं, पर आज अनुज के कहने में कई बातें एकजुट हो गयीं…एक तो कहीं इस तरह चलने की उनकी यह पहली पेशकश थी। दूसरे यह कि कई दिनों से घर बैठे होने की एकरसता में कुछ बदलाव लाने की तबियत भी थी…लेकिन सबसे अधिक प्रेरक यह हुआ कि देवस्थानों के प्रति मेरी दीदी के मन में सहज ही तीव्र भक्ति-भाव बसता है, और इसी से कहीं जाने में अदम्य उत्साह रहता है…, जो हम समयाभाव से ज्यादा करा नहीं पाते। लिहाज़ा ऐसे बहु-बहु उद्देश्यीय प्रयोजनों से लैस प्रिय द्विवेदीजी की गाड़ी में चल पड़ा त्रिमूर्त्ति-क़ाफ़िला…।
प्रिय रामप्रकाशजी अपनी प्रकृति से ही बेहद विनोदी हैं। बात-बात में कुछ विनोदपरक बातें निकाल के ज़ोरों की हहास उनका स्व-भाव व सु-भाव है। मुझे भी यह कम प्रिय नहीं, सो नहले पे दहला लगता रहता है – विनोदी जुगलबंदी चलती रहती है …। इस तरह छोटी-सी यात्रा पलक झपकते ही मंज़िल तक पहुँच गयी।
मैं तो पूजा-पाठ, दर्शन-भक्ति के लिए मंदिर में जाता नहीं, स्थापत्य व धार्मिक प्रतीकों की प्रयुक्ति के लिए अवश्य जाता हूँ, जो सब इस बार मंदिर के तमाम परिष्कार से ज्यादा आकर्षक महसूस हुआ। लेकिन दीदी तो पूजा-चढ़ावा की तमाम सामग्रियों से सन्नद्ध होके गयी थी और मंदिर में भीड़ भी न थी। सो, जब तक वह विधिवत अपना पूजा-कर्म सम्पन्न करे, हम दोनो भाई नदी किनारे घूम आये…, जो अतिशय ताप के कारण सुखद तनिक भी न था। ख़ास बात यह हुई कि प्रिय अनुज की हल्की-सी इच्छा को गाढ़ा करते हुए मंदिर के पुजारी के हाथों भर माथे पर शीतल चंदन लगवाया गया – वरना ऐसे आचारों से लगभग आधी शती से मैं सुविचारित रूप से विरत रहा, लेकिन प्रेमल-इच्छा भरे प्रस्ताव के आगे सब फेल…!!

स्वराज-आश्रम एवं सनातनी संस्कृति से समक्षता – इस षट्कर्म के बाद प्रयाण हुआ इस यात्रा की मूल मंज़िल और घाघजी पर इस लेख के बीज घाघ की पुस्तक ‘घाघ भड्डरी’ के प्राप्ति-स्थल ‘स्वराज-आश्रम’ की ओर…। जी हाँ, गांधीजी वाला स्वराज ही – उनकी कल्पना को साकार करता हुआ…। इस आश्रम के नियामक सर्वश्री रामानंदजी सनातनी हैं, जो मूलतः तो उत्तरप्रदेश के उन्नाव ज़िले में प्रतापनारायण मिश्र के गाँव (बेथर) के हैं, लेकिन नेपाल में स्थापित व पुन: अर्धविस्थापित होकर बनारस आये और यहाँ ऐसे स्थापित हुए कि बनारस-मय हो गये तथा एक अल्पांश ही सही, बनारस को भी रामानंदमय बना सके। उनके करने व किये के परिणामों को लेकर बहस-मुबाहसा हो सकता है, लेकिन उनके संकल्प व उसके प्रति उनकी आस्था पर संदेह नहीं किया जा सकता। ‘स्वराज-आश्रम’ सच्चे अर्थों में स्व-राज्य – याने आत्मनिर्भर आश्रम है। वहाँ अपने जाने से जुड़ा प्रमाण ही दूँ, तो द्विवेदीजी के साथ उनकी बात वहाँ हमारे नाश्ते की हुई थी। लेकिन हमें विलम्ब से आते देख उन्होंने नाश्ते व दोपहर के खाने को एक करते हुए, जिसे अंग्रेज़ी वालों ने ठीक ही ‘ब्रंच’ (ब्रेकफास्ट-लंच) नाम दिया है, जो कुछ खिलाया, वह सब उसी आश्रम का ही उत्पाद था – दही, पराठा, भाजियाँ, बुकनी और कई फलों के मिश्रण से बना भरपूर सलाद। कुछ भी बाहर से आया न था। यही हमारी भारतीय व्यवस्था व कृषि-संस्कृत्ति भी रही है। हमारा किसान इतना ही आत्मनिर्भर होता था। बाज़ार उसके पास आता था। वह कहीं न जाता था। वह जीवन व व्यवस्था की धुरी था। आज उलटा हो गया है। गेहूं-चावल के सिवा बाक़ी सब कुछ के लिए, हर छोटे से छोटे सामान के लिए बाज़ार की तरफ़ भागता आदमी परमुखापेक्षी ही नहीं, बाज़ार का मोहताज हो गया है…।
इस स्वराज आश्रम में खेती की तमाम फ़सलें एवं फूल-फलों के बाग-बगीचे हैं। गोशाला है, गायें हैं। नाट्य-मंच है। अखाड़ा है। मूल गृह के चहुँ ओर सचित्र सूत्रवत रूप में समूची सनातन जीवन-पद्धति के आयाम नियोजित हैं, जिन्हें हर आगंतुक के साथ रामानंदजी पूरी विनम्र विद्वत्ता के साथ साझा भी करते हैं…। इन सबसे बने वातावरण में असीम शांति है, सुख है, आह्लाद है। लेकिन इन सबके मूल मंत्र स्वरूप सनातन धर्म भी रामानन्दजी में कूट-कूट कर भरा है। वे इसके साथ एकाकार हैं। इसका प्रमाण भी ‘अनभै साँचा’ (अपने अनुभव के सच) से ही दूँ…तो परिसर में पहुँचते ही मुख्य द्वार तक लेने आने के बाद कक्ष में प्रविष्ट होते ही सनातनी आचार-पद्धति में ‘अपवित्रो पवित्रो व सर्वावस्थां गतोsपि वा…य: स्मरेत पुंडरीकाक्षम् स बाह्याभ्यंतर: शुचि:’। के स्तवन के साथ चंदन-तिलक व माला-फूलादि के अर्पण भी तत्संबंधी श्लोक-पाठ के साथ हुए…। और सनातनीजी की सधी-दत्तचित्त बातचीत व मृदु-विनम्र व्यवहार …आदि सब कुछ में सनातन संस्कृति व स्वराज आश्रम की महिमा-गरिमा मनसा-वाचा-कर्मणा सम्यक् रूपेण व्यक्त होती रही…। एक पवित्र-लोक में विचरण का अनुभव कराती रही…।
और तीन-चार घंटे के इस संत-समागम के बाद विदा होते हुए रामानंदजी ने मुझे तीन छोटी-छोटी किताबें भेंट कीं – ज़ाहिर है कि अपने ‘पिलग्रिम्स’ प्रकाशन से छपी हुई। इनमे एक तो ‘पिलग्रिम्स : एक विचार यात्रा’ है, जो बनारस शहर में दुर्गाकुंड पर स्थित विशाल व समृद्ध पुस्तकालय के रूप में उनके योगदान का आकलन है, जिस पर चर्चा के लिए ऐसे ही एक अलग आलेख की दरकार होगी। दूसरी पुस्तक स्वयं रामानंदजी द्वारा संकलित है – ‘ब्रह्मचर्य’, जिस पर कुछ कहने का अधिकारी मैं नहीं – बस सिवाय इसके कि ब्रह्मचर्य की यात्रा भोग को त्याग कर नहीं, बल्कि पुस्तक के एक सूत्र के साक्ष्य पर ही उसके बीच से होके निकलती है – ‘भग बिच लिंग, लिंग बिच पारा, जो सेवे सो गुरू हमारा’। और तीसरी किताब है – ‘घाघ भड्डरी’।
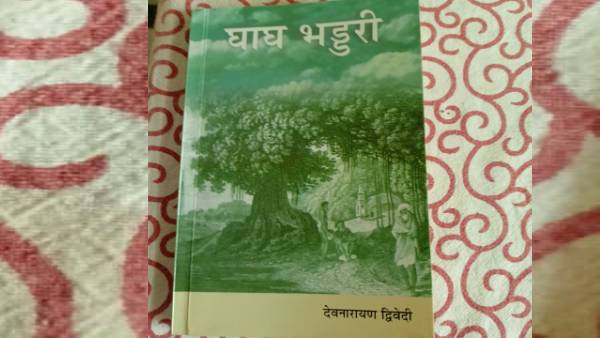
अथ घाघ भड्डरी – देवनारायण द्विवेदी द्वारा तैयार की गयी और सम्पादित यह पुस्तक ‘घाघ भड्डरी’ तनिक चौड़ी डायरी के आकार में 126 पृष्ठों की है। पहला पन्ना खोलते ही ‘दो शब्द’ नाम से एक छोटी सी भूमिका है। ये ‘दो शब्द’ जिन दो शब्दों को व्याख्यायित करते हैं, वे हैं यही – घाघ और भड्डरी। ये एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं – याने घाघ ही भड्डरी भी थे। दोनो ही रूप कविताओं में पाये जाते हैं। पहले के साहित्य में बातचीत व संवाद के बीच ही रचनाएँ नियोजित होती थीं। बाणभट्ट की पूरी ‘कादम्बरी’ राजा-तोता व इस-उस के बीच संवाद ही तो है। ‘लीलावती’ नामक गणितीय ज्योतिष का पूरा ग्रंथ वक्ता पंडितजी द्वारा अपनी बेटी लीलावती को सम्बोधित है। सर्वाधिक लोकप्रिय ‘रामचरित मानस’ के चार वक्ता व चार श्रोता विश्रुत हैं ही। तद्युगीन इसी भारतीय शैली में घाघ व भड्डर के घाघिनी और भड्डरी के लिए सम्बोधन हैं – ‘कहें घाघ घाघिनी से’ और ‘कहें घाघ सुनु भड्डरी’…के रूप में।
घाघ के जन्म की रोचक कथा – इस ‘दो शब्द’ के अंतर्गत मिश्रबंधु के हवाले से बाताया गया है कि कवि घाघ का जन्म संवत् 1753 तदनुसार सन् 1696 में कानपुर में हुआ था। वे कान्यकुब्ज ब्राह्मण बताया थे। और लेखक ने उनके जन्म को लेकर एक रोचक कथा भी बतायी है, जो उन्हीं के अनुसार किंवदंती ही है – याने लोक में बहव: प्रचलित, पर इसका कोई ऐतिहासिक या तथ्यपरक प्रमाण नहीं। इस कथा के अनुसार घाघ के पिता बहुत बड़े ज्योतिषी थे। एक बार ज्योतिष में उन्होंने पाया कि ऐसा समय आने वाला है, जब यदि गर्भाधान हो, तो जो संतान पैदा होगी, वह त्रिकालदर्शी होगी – ऐसे दृष्टांत कई लोकगाथाओं में आते हैं। वे पत्नी के पास चल पड़े, पर इतने दूर थे कि वहाँ पहुँचने में मुहूर्त्त निकल जाता। रास्ते में उन्हें एक स्त्री दिखी। उन्होंने हिम्मत करके यह प्रस्ताव उसके सामने रख दिया और वह मान गयी। स्त्री किसी राजा के रनिवास में नौकरानी थी। समय पर पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम रखा गया – भड्डर। जब वह पाँच साल का हो गया, राजा को पुत्ररत्न की प्राप्ति हुई, जिसके लिए ज्योतिषियों ने बताया कि बालक घोर दुराचारी होगा। इसके कारण माता-पिता पर बड़ी विपत्तियाँ आयेंगी। अत: राजा के आदेश से उसे कहीं बाहर रखा दिया गया कि जीव-जंतु उसे खा जाएँ। लेकिन भड्डर ने सूतिका गृह के द्वार पर लिख दिया कि इस भाग्यशाली बालक का कोई भी बाल बाँका नहीं कर सकता। इस लिखे को सुनकर राजा ने लिखने वाले को हाज़िर होने का आदेश दिया। तब भड्डर ने आके बताया कि उसने सच लिखा है। राजा को क़यास था कि बालक मर चुका होगा। लिहाज़ा उसने भड्डर से करार कराया कि बात ग़लत हुई, तो कठोर से कठोर सजा मिलेगी। लेकिन वहाँ देखा गया, तो बच्चे के ऊपर अपना फन फैलाए हुए एक विकराल साँप पास में बैठा है। साँप की गरदन में मधुमक्खियों ने छत्ता लगा रखा है, जिससे बच्चे के मुँह में बूँद-बूँद मधु टपक रही है। बस, क्या था भड्डर की ख्याति बचपन से ही बड़े ज्योतिषी के रूप में फैल गयी…। मेरी आज की कलयुगी समझ मानती है कि यह कहानी भड्डर की योग्यता देखने के बाद बना दी गयी है – जैसे पैदा होते ही तुलसी के पाँच वर्ष के होने व ‘राम राम’ कहने…आदि की किंवदंतियाँ उनके तुलसी हो जाने के बाद लोकमन ने गढ़ी होंगी। उसी प्रकार घाघ की प्रतिष्ठा के बाद ये लोक-प्रचलित कहानियाँ बनी होंगी और दुनिया में फैलकर सबके मन का विश्वास बन गयी होंगी…।
लेकिन ज्योतिष का ऐसा असर ‘घाघ भड्डरी’ नामक इस पुस्तक में है कि घाघ के ज्योतिष पढ़ने का पक्का विश्वास दिला देता है। कुछ कविताएँ तो ज्योतिष के शुरुआती ग्रंथो में लिखी व्यवस्थाओं की हूबहू अनुवाद हैं। उदाहरण के लिए यात्रा नामक अध्याय में जिस दिशा में जिस दिन जाने को शास्त्रों में दिशाशूल कहा गया है, उसे वैसे का वैसे घाघ ने भी लिखा है –
‘सोम सनीचर पुरब न चाल’ (‘शनौ चंद्रे त्यजेत् पूर्वं), ‘मंगल बुद्ध उतर दिसि काल’ (बुधे भौमे तथोत्तरे’),
जो बीफै को दक्खिन जाय, बिना गुनाहै जूता खाय (दक्षिणाम् च दिशं गुरौ)
ध्यातव्य है कि पुस्तक में शुक्र-रवि को पश्चिम न जाने वाली पंक्ति (शुक्रे सूर्ये पश्चिमायाम्) छूट गयी है और बुध को उत्तर न जाने का आगे दुहराव भी हुआ है। ज़ाहिर है कि देवनारायणजी को न मिला होगा। और मज़ा यह है कि हमारे गाँव में भी इतना ही कहा-सुना जाता है। इसमें ‘बिना गुनाहै जूता खाय’ के बदले हमारे यहाँ कहा जाता है – ‘बीफै के ज़े दक्खिन जाई, चार लात पैंड़े (रास्ते) में खाई’। इसी के साथ यह भी कि यदि दिशाशूल के दिन जाना अ-निवार्य ही हो जाये, तो सनातन व्यवस्था इसका संज्ञान रखती है कि जीवन और काम किसी भी चीज़ से बड़े हैं। अत: उसके नियम इतने लचीले व व्यावाहारिक भी हैं कि सब कुछ के लिए कोई न कोई परिहार नियोजित है। यथा, सोम को पां खाके, मंगल को गुद-धनिया खाके…आदि –
रवि ताम्बूल सोम को दरपन, भौमवार गुड़-धनिया चरबन।
बुद्ध मिठाई, बिहफै राई, सुक़्र कहे मोहिं दही सुहाई।
सन्नी बायभिरंगी भावै, इंद्रहिं जीति पुत्र घर आवै।
इस प्रकार इतना तो तय है कि घाघ की कहावतों का सारा आधार वही ज्योतिष वाला ही है – दिन, नक्षत्र (नखत), तिथियाँ, महीना…। ‘दिन-ग्रह-राशि’ व ‘ग्रहण-शकुन-अपशकुन’ जैसे अध्याय इसके पुख़्ता प्रमाण हैं। ज्योतिष का एक और मुख्य आधार बारह राशियाँ हैं। लेकिन ‘कर्क राशि पर गूरु’ व ‘सिंह राशि पर शुक्र’ जैसे दो उल्लेखों के अलावा मेष-वृष…आदि राशियों के अनुसार बातें नहीं हुई हैं, जो घाघ-काव्य को विशुद्ध ज्योतिष से अलगाता है। तो यह भी सिद्ध होता है कि ज्योतिष घाघ-काव्य का आधार है, आधेय नहीं। उनके लेखन में गहन अनुभव का ताप है। उससे नि:सृत दृष्टि का प्रकाश है। फिर उन्होंने व्यक्ति के लिए नहीं, समाज के लिए लिखा है। याने उनके सोच का आधार या मूल सरोकार मनुष्य व समाज था – व्यक्ति नहीं। और लोक में लोक (समूह) के सामने व्यक्ति होता भी नहीं। ख़ैर, कालांतर में बालक घाघ की जीवन-कथा में उसके ज्योतिषी पिता आये और मां के लाख मना करने के बावजूद भड्डर को अपने साथ लेके चले। रास्ते में भड्डर ने एक किसान को खेत में धान छींटते (बोते) हुए देखा कि कुछ धान के दाने बग़ल वाले खेत में भी फेंका जा रहे थे। उसने रुक कर किसान से पूछा कि क्या उस खेत का धान भी वही काटेगा? किसान ने उत्तर दिया – फसल खेत की होती है, बीज की नहीं। वह तो उपादान है। लिहाज़ा जिसका खेत है, वही फसल काटेगा। बस, पिता को बीज व खेत की सचाई सुनाके ‘बीज खेत का होता है’, को सार्थक करते हुए भड्डर चलते बना – मां के पास।

वही भड्डर या घाघ यह मशहूर व लोकप्रिय कवि घाघ है, जिसके बताये के मुताबिक़ मेरे किशोर-काल याने 1970-75 तक उत्तर भारत का किसान भी अपना जीवन निर्धारित करता रहा। जोतने-बोने से लेकर बैल ख़रीदने, कहीं आने-जाने, बारिश के होने या दुर्भिक्ष पड़ने, ग्रह-नक्षत्र की गति पहचानने और मानव जीवन पर उनके उनके असर…हर कुछ में किसान भड्डर या घाघ को अपना मानक मानते…।
घाघ के विषय : प्रासंगिकता के निकष पर – उक्त विषयों को लेकर ही ‘घाघ भड्डरी’ नामक इस पुस्तक में तेरह अध्याय हैं – सुकाल और अकाल, वर्षा, जोताई-बोवाई, ग्रहण-शकुन-अपशकुन, यात्रा, वायु परीक्षा, बीज की मात्रा और नक्षत्र, वर्षा नक्षत्र, महंगाई और दुर्भिक्ष, पैदावार, नीति, दिन-ग्रह-राशि, बैल की परख।
इन विषयों को देखकर अब लगा कि दर्जा पाँच में जो पाठ हमारी किताब में था, वह बैल की परख से ही लिया गया था, जो इस पुस्तक में न जाने क्यों एकदम अंत में संग्रहीत है। और वही एक ऐसा है, जो आज पूरी तरह अप्रासंगिक याने बेकाम का हो गया है, क्योंकि अब बैल तो किसी के पास भी नहीं हैं। ट्रैक्टर आ जाने से बैलों की ज़रूरत ही न रही। जितनी उपेक्षा-दुर्दशा गायों के बछड़ों की आज है, न और किसी की है, न बछड़ों-बैलों की कभी थी। और तब बैल जितने काम के थे, उतने काम का कोई न था। बक़ौल घाघ स्वयं – ‘उत्तम खेती जानो वाकी, होय मेवाती गोई जाकी’। इसलिए किसान तो बैल की नींद जागता-सोता था। इस रूप में घाघ का महत्त्व ऐतिहासिक है। और घाघ तो अच्छी खेती के लिए छोटे और कमजोर या कम औक़ात वाले बैलों को बेचकर अच्छी औक़ात वाले मज़बूत बैल लेने की सलाह देते थे – ‘नाटा-गोटा बेचि के चार धुरंधर लेहु, आपन काम निकारि के औरन मँगनी देहु’।
चार धुरंधर बैलों से खेती का अपना काम करके औरों के माँगने पर उन्हें भी दो। यह किसान-जीवन का मंत्र रहा है कि सभी एक दूसरे की मदद करते रहे…। जिस दिन अपने घर काम न हो रहा हो, तो बैल से लेकर खेती के अन्य साधन-सामान किसी को भी देने की स्वस्थ परम्परा थी। स्वतंत्र भारत में इसे सहकारिता कहा गया था, पर अब मशीनों ने सहकारिता की ज़रूरत ही ख़त्म कर ड़ी। आदमी को स्वयं में सक्षम बना दिया। लेकिन इससे जो व्यक्तिवादिता आयी है, जो सामाजिकता का लोप हुआ है, उसका आकलन कोई मशीन कर नहीं सकती। मशीनों की यह सीमा कवि के शब्दों में – ‘हर ताप नापा, पर नपा आज तक मन का ताप नहीं’!!
लेकिन बाक़ी सभी अध्याय आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, जितने तब थे। यह बात अलग है कि अब न इनकी चर्चा है, न इनके उल्लेख हैं। लोक के सारे आयाम जिस तरह उपेक्षित हो गये हैं – उनके स्थान ले लिये हैं तकनीकी उपकरणों ने, उसी तरह खेती का भी हुआ है। कृषि-कार्य की सारी पुरानी शब्दावली बदल गयी है। ‘घाघ भड्डरी’ का पहला अध्याय है – ‘अकाल-सुकाल’, जो आज एकदम कालबाह्य हो गया है। नयी पीढ़ी के बच्चे अकाल या दुर्भिक्ष नहीं जानते, तो सुकाल भी क्या जानेंगे? पानी न मिलने से धान में दाने आये नहीं और सिर्फ़ पौधे कट गये, जो चंद दिनों पशुओं के चारे भर के काम आये। इसी को ‘धान की मुंगारी कट जाना’ कहते थे। यह शब्दावली ही आज नदारद है। ‘मुंगारी कटना’ अशुभ व दुखमय भविष्य की सूचना होती थी। लेकिन आज वर्षा भले न हो, मुंगारी नहीं कटती, वैसा अकाल-दुर्भिक्ष नहीं पड़ता। नहर या नलकूपों से कुछ पानी मिल ही जाता है। कुछ धान हो ही जाता है। इस पुस्तक में दोनो को मिलाकर दुर्भिक्ष एवं महंगाई नाम से अलग अध्याय बना दिया गया है। शायद अध्यायों के ऐसे विभाजन-सम्पादन देवनारायण द्विवेदी ने किये हैं, जो पाठक के लिए काफ़ी सुगम हो गया है। पाँच पृष्ठों के इस अध्याय में घाघ के लिखे पचासों ऐसे नक्षत्र-योग-भोग समाहित हैं, जो वस्तुतः महंगाई व दुर्भिक्ष के कारण होते हैं। स्वयं महंगाई व दुर्भिक्ष भी एक दूसरे के कारण-कारक है – अकाल का कारक महंगाई और महंगाई का कारण अकाल। तब उन कारणों से बचना ज़रूरी था, जिनसे अकाल…आदि पड़ते थे। बचा न जा सके, तो जाना तो जाये ही, जिससे इसे सहने की मानसिक शक्ति तो मिल जाये। यथा – ‘कृत्तिका तो कोरी गयी, अर्द्रा मेंह न बूँद, तो यों जानो भड्डरी, काल मचावे दंद’ – याने कृत्तिका-आर्दा में पानी न बरसा, तो काल ही नाचेगा। यही घाघ की उपयोगिता थी – किसानों का आधार था। इसीलिए इन सबके लक्षण बताते हैं घाघजी, जो आज भी मौजूँ हैं, पर न अंदाज़े जाते, न परखे जाते…।
पुस्तक के दूसरे अध्याय में ‘वर्षा’ पर विचार हुआ है कि फसलों के लिए वर्षा याने पानी के क्या फ़ायदे-नुक़सान हैं और आठवें अध्याय में वर्षा-नक्षत्र के अंतर्गत किन-किन नक्षत्रों की बारिश भिन्न-भिन्न फसलों के लिए फ़ायदे व नुक़सान की होती है…के निर्देश दिये गये हैं। नक्षत्रों के अनुसार हुई वर्षा फसलों के लिए कैसी सिद्ध होती है, इस पर अलग से बहुत विस्तार से विचार हुआ है। और देखें, तो नहर-नलकूप की सारी तैयारी के बावजूद वर्षा की उपयोगिता हर देश-काल में रहने वाली है और वर्षा होने के लक्षण तथा होने या न होने से खेती के नुक़सान-फ़ायदे आज भी वैसे ही हैं। खेती के अलावा और वातानुकूलित कमरों के बावजूद वर्षा की आतुर प्रतीक्षा पूरे संसार में रहती है। इसके भी होने के समय के अनुसार खेती के फ़ायदे तथा उससे प्राणि मात्र के सुख-दुःख के आकलन के रूप में घाघ की वाणियाँ स्मरणीय हैं – ‘जब बरसेगा उत्तरा, नाज़ न खाये कुत्तरा’। याने उत्तरा नक्षत्र में पानी बरसे, तो कुत्ते भी अनाज न खायें – इतनी अच्छी फसल होगी। यह घाघ की शैली है। एक और देखें –
‘रोहिनि बरसे मृग तपे, कछु कछु अद्रा जाय, कहें घाघ सुनूँ घाघिनी स्वान भात नहिं खाय’।
दो अध्यायों में हुए वर्षा-विचार के बाद एक अध्याय है पैदावार, जिसमें हमने अनाज के उपज के लेखे-जोखे की उम्मीद की थी, लेकिन इसमें भी वर्षा के ही विचार व कथन समाहित हैं। असल में आज के पानी के साधनों के सिवा यदि 50 साल पहले का जीवन देखें, तो रहीम का कहा ही किसान-जीवन का लेखा था – ‘दादुर मोर किसान मन, लागि रह्यो घन मांहि’। याने बादल-वर्षा-पानी के बिना जीवन की कोई गति नहीं थी। पानी बरसाने के अनेक अनुष्ठान-यज्ञ व लोक-विहित आयोजन किये जाते थे – कड़ाहा चढ़ता था, गाँवमध्ये की पूजा होती थी। हमारे बचपन में एक लोकाचार या टोटका ऐसा भी होता था कि हम बच्चों को भूमि पर लोटा देते थे। बड़े लोग घड़े-घड़े, बाल्टी-बाल्टी भर के हम पर पानी फेंकते थे और हम खुश होकर लोटते -पोटते हुए चिल्ला-चिल्लाकर गाते थे – ‘मेघा मेघा पाने दे, नहीं त आपन नानी दे’। ‘जल जीवनम्’ जैसा संस्कृत का मुहावरा इसी का प्रमाण है। भगवद्गीता के अनुसार यज्ञ का मक़सद भी धुएँ से बादल बनाना ही था – ‘यज्ञाद्भवति पर्जन्य:’। कहने का तात्पर्य यह कि पानी ही जीवन का मूल होता था – इसका तब कोई विकल्प न था। लिहाज़ा, बादल को प्रसन्न करने के कई उपाय-उद्योग लोक से लेकर वेद तक प्रचलित थे। बादल को दैव (भगवान) की संज्ञा दी गयी थी – ‘दऊ बरसिहैं ना का’! इसलिए पानी के फल रूप में पैदावार का आकलन है, लेकिन 95% कविताओं में कारण (पानी) ही कार्य (पैदावार) हो गया है। बची 5% का उदाहरण प्रस्तुत है – पानी बरसे आधे पूस, आधा गल्ला आधा भूस।… साँवा साठी साठ दिना, जब पानी बरसे रात-दिना।
उक्त में आधा गल्ला, आधा भूसा और साठ दिनों में साठी नामक धान के होने की बात ही पैदावार की तरफ़ इंगित करती है…। वर्षा याने पानी के साथ ही हवा बहने के फलाफल पर भी अध्याय है – ‘वायु परीक्षा’। इसमें चारो दिशाओं -पुरवा, पछुआ, उतरहिया, दखिनहियाँ- के साथ चारो कोनो -ईशान, नैऋत्य, वायव्य, आग्नेय- के साथ ऊपर व नीचे की ओर चलने वाली को मिलाकर दसो दिशाओं की हवाओं के शुभाशुभ फल बताये गये हैं…एक बानगी – जौ पुरुवा पुरवाई पावै, झूरी नादिया नाव चलावै। और ‘सावन मास बहै पुरवाई, बरधा बेचि बेसाहौ गाई’ – याने सावन में पुरवा बहे, तो फसल न होगी। इसलिए बैल बेच के गाय ख़रीद लेना बेहतर।
हवा-पानी के साथ मिट्टी याने खेत की चर्चा भी हुई है, जिसे बनाने में जुताई का बड़ा हाथ होता है। फिर बीज किस तरह मिट्टी में डाले जाते हैं याने बुवाई की बात भी साथ में ही हुई है। इस अध्याय का नाम जुताई-बुवाई है और दोनो ही चर्चाएं काफ़ी अच्छी हैं। इसमें बुवाई के अनुकूल-प्रतिकूल नक्षत्रादि के भी विवेचन हैं। धान के खेत को गहरे तक नहीं जोतना चाहिए और कम बाँह (बार) जोतना भी कहा गया है, जबकि गेहूं-जौ के लिए दो-चार से सोलह बाँह जोतने के निर्देश हैं। बारिश में कुछ खेत ख़ाली छोड़ दिए जाते, जिसे चौमस कहते। पूरे चौमासा (बारिश) उसे जोतने की होड़ लगती – बीस-बाइस बाँह जोतने के मानक बनते। फिर गेहूं-जौ की फसल के लिए कितनी बार जोतने की संख्या का महत्त्व है, तो धान बोने के बाद खेत को हल्के हल से जोत देने (बिदहने) को अच्छी उपज के लिए श्रेयस्कर कहा गया है – गेहूं बाहें, धान बिदाहें। गन्ने के खेत को तो ज्यादा ही बनाते। लेकिन गन्ना बोने के बाद घाघ का मानक यह – ‘तीन कियारी तेरह कोड़, तब ताका हौदा की ओर’ – याने बोने के बार तीन बार पानी से पूरे खेत को डुबा दो और तेरह बार गुड़ाई करो, फिर हौदे की तरफ़ देखो – याने कितना गुड़ हुआ। इस प्रकार हर फसल में पानी-हवा-मिट्टी तथा खेत की तैयारी का पूरा व्योरा सुलभ है।
इसी प्रकार बीज की मात्रा और नक्षत्र नामक अध्याय में बीज की गुणवत्ता व मात्रा के साथ ही विशिष्ट नक्षत्रों में बोने के सुपरिणामों की चर्चा हुई है –जौ-गेहूं बोवै सार पसेर, मटर बिगाहे साठे सेर। बोव चना पसेरी तीन, दो सेर बिगहा जोन्हरी कीन। रोहिन-मृगसिर बोवे मक्का, उरदी मंडुआ दे नहिं टक्का। मृगसिर में जो बोवे चेना, ज़मींदार को कछु नहिं देना।
इस प्रकार घाघजी ने तत्कालीन जीवन के वृहत्तर समाज के लिए, उनके दैनंदिन के सरोकारों से युक्त सभी पक्षों के शास्त्र सम्मत विचार लोकभाषा में मुहय्या कराने का बड़ा काम किया है। संकलन-सम्पादन कर्त्ता स्वयं द्विवेदीजी के मुताबिक़ घाघ की मूल भाषा में बहुरूपता थी, जिसे द्विवेदीजी ने एक मानक रूप ड़े दिया है। यह करना कितना उचित था, भी विचारणीय है। उसी भाषा में होता, तो कैसा होता…, को जानना तो तभी सम्भव होता, जब मूल सामने होता। अत: यदि कवि के मूल रूप के साथ यह मानक रूप दे दिया जाता, तो कवि के साथ ज्यादा न्याय होता और उस भाषा-रूप को जानने वाले लोग उनके मौलिक स्वाद का आनंद ले पाते…। लेकिन भाषा न सही, भावों को अवाम तक पहुँचा देने का यह कार्य भी कम सराहनीय नहीं। घाघ के सारे नियम-विधान के साथ कर्म-आधारित यह बात बहुत भाती है – जोते खेत घास ना टूटे, टेकर भाग साँझ ही फूटे।
