नाटक
रंग महोत्सवों की बाढ़ के निहितार्थ
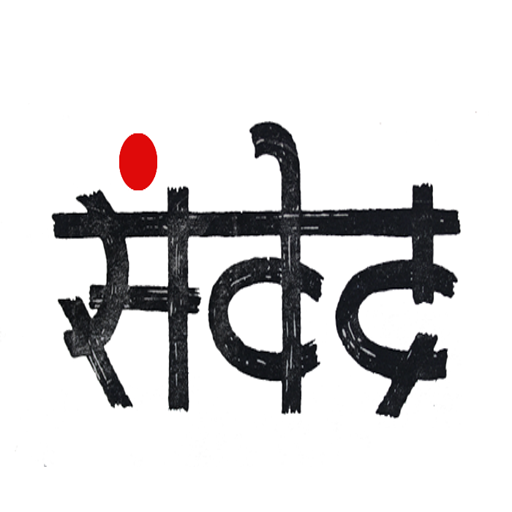
- मृत्युंजय प्रभाकर
सभी कला माध्यमों में रंगमंच सबसे ग्लैमरविहीन रहा है, कारण कि संगीत, नृत्य और सिनेमा के तो बड़े महोत्सव देश भर में आयोजित होते रहते थे लेकिन नाटक के महोत्सव उस बड़े स्तर पर कम ही आयोजित होते थे । कल तक शौकिया रंगकर्मी अपनी मेहनत से कोई नाटक तैयार कर भी लेते थे तो उन्हें एक–दो प्रदर्शन के बाद अपने नाटक बंद करने पड़ते थे क्योंकि ऐसा कोई मंच नहीं था जहां वे अपने नाटकों को बार–बार प्रस्तुत कर सकें लेकिन रंगमंच का यह सूखा अब खत्म हो गया है । आज देश भर में नाट्य महोत्सवों की बहार आ गई है । सरकारी, अर्धसरकारी और कॉरपोरेट सभी लोगों के सहयोग से नाट्य महोत्सव देश भर में सालों भर आयोजित हो रहे हैं । राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा दिल्ली में आयोजित भारत रंग महोत्सव हो, पृथ्वी थिएटर, मुंबई का महोत्सव हो, नांदीकार, कलकत्ता का महोत्सव हो या सुदूर केरल में आयोजित होने वाला अंतर्राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव हो, ये सभी देश के बड़े रंग महोत्सवों में शुमार हैं । इनके अलावा भोपाल, जबलपुर, रायपुर, रायगढ़, चंडीगढ़, पटना, बेगूसराय से लेकर देश के सुदूर अंचलों तक छोटे–बड़े पैमाने पर नाट्य महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं । महोत्सवों की इसी भीड़ में एक और नाम ‘मेटा थिएटर फेस्टिवल’ है जिसे महिन्द्रा जैसा बड़ा कॉरपोरेट घराना आयोजित कराता है ।
भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय भी महोत्सवों के आयोजन पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहा है । देश भर में संस्थाओं को महोत्सव आयोजित करने के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान किया जा रहा है । इससे प्रयोजित होकर भी छोटी–छोटी संस्थाएं अपना नाट्य महोत्सव आयोजित कर रही हैं । अब ऐसे में क्या यह मान लेना चाहिए कि रंगमंच अब केंद्र में आ रहा है ? क्या रंगमंच के प्रति समाज, सरकार और दर्शकों का रवैया बदला है ? इससे भी बड़ा सवाल यह है कि इन महोत्सवों से आखिर रंगकर्म, रंगकर्मियों और दर्शकों को क्या फायदा मिल पा रहा है ?
इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि निरंतर आयोजित किए जा रहे नाट्य महोत्सवों के कारण अब रंगकर्मियों, निर्देशकों और रंग समूहों को भागीदारी का अवसर ज्यादा मिल पा रहा है । इसका सीधा फायदा उन रंगकर्मियों को मिल रहा है जो पहले संसाधनों के अभाव में एक–दो प्रदर्शनों के बाद ही नाटक बंद कर देने को मजबूर हो जाते थे । नाटक अगर अच्छा बन पड़ा है तो उसे प्रदर्शन मिल रहे हैं । लेकिन क्या वास्तव में इतना ही सरल है जितना कि दिखाई देता है ? यह कहना तो आसान नजर आता है लेकिन अधिकांशत: नाट्य महोत्सवों में शामिल नाटकों की फेहरिस्त इस बात की चुगली करती है कि नाटकों के चयन के कई दूसरे मापदंड ज्यादा हावी होते हैं । ज्यादातर छोटे और सरकार पोषित महोत्सवों में उन्हीं लोगों के नाटक भागीदारी करते दिखाई देते हैं जो कहीं से भी सरकारी कमिटी के हिस्से हैं या उसे अपने तरह से प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं । कई सारे महोत्सव तो सीधे तौर पर एक–दूसरे को उपकृत करते नजर आते हैं । इससे होता यह है कि कुछ नाम हर महोत्सव में देखने में आ ही जाते हैं । नाट्य महोत्सवों से जुड़ा यह एक भयावह सच है जो दर्शाता है कि हालात उतने भी अच्छे नहीं हैं जितने दिखाई देते हैं । रही बात इन महोत्सवों में नए लोगों के प्रवेश की तो उसकी भी वही परिपाटी बन चुकी है । अपनों और दूसरों में फर्क यहां भी किया जाता है । सबसे मजेदार बात यह है कि अपनों को चुनने की प्रक्रिया भी अलग–अलग लोगों के लिए अलग–अलग होती है । अब तक तो यही देखने में आ रहा है कि इन महोत्सवों में ज्यादातर लोग एक समूह की तरह काम करते हैं और आयोजकों द्वारा सत्ता पोषित एक खास समूह इसमें आसानी से अपनी जगह बना पाता है ।
इन महोत्सवों से दर्शकों को जो सीधा फायदा होता दिखता है वह यह कि उन्हें एक ही जगह पर तरह–तरह के नाटक देखने को मिल जाते है । इस तरह वह कई तरह के नाटकों का आस्वाद ले सकते हैं । भिन्न–भिन्न रंगकर्मियों का काम अपने शहर में होते हुए देख सकते हैं । लेकिन चूंकि महोत्सव में आने वाले नाटकों का चयन अपने आप में एक विवादित प्रश्न है इसलिए दर्शक भी वही देख पा रहे हैं जो आयोजकों या प्रयोजकों की पसंद हैं । हां, यह जरूर हुआ है कि दिल्ली और दूसरे बड़े शहरों में दर्शक अब नाटकों के प्रति भी रुझान रखने लगे हैं ।
जहां तक रंगकर्म का सवाल है । इसे इससे जो भी फायदा हुआ है वह मूलत: शैलीगत ही है । रंगकर्मी एक–दूसरे का काम देखकर सीखते हैं । सो, एक साथ ज्यादा से ज्यादा रंगमंच देख पाना निश्चित ही उनके लिए लाभकारी अनुभव है, पर इसका नुकसान यह है कि ‘कॉपी कैट’ निर्देशक बढ़े हैं । रंगकर्मी किसी खास निर्देशक का कोई नाटक देखकर अपने छोटे शहर में जाकर हूबहू वही सब कर अपना सिक्का जमाने की कोशिश करते हैं, हालांकि यह भी कोई नया चलन नहीं है ।
इस तरह के महोत्सवों में आने वाले नाटकों में एक और खास बात जो अपनी तरफ ध्यान खींचती है वह यह कि रंगमंच अब ‘यूनिवर्सल’ हो गया है । पहले के निर्देशकों और रंग समूहों के ऊपर अपने समाज और संस्कृति की स्पष्ट छाप नजर आती थी । उनकी रंग शैली उनकी संस्कृति और समाज के बीच से निकलते थे, इसलिए रंगमंच के जितने भी बड़े निर्देशक रहे हैं उनके काम मंे उनकी स्थानीय संस्कृति को आसानी से चिन्हित किया जा सकता है । लेकिन आज के निर्देशक अपनी जगह, वहां के दर्शक, वहां की संस्कृति, समाज, समस्याओं और जरूरतों का जरा भी ध्यान नहीं रखते । इसलिए कई बार ऐसा लगता है कि यह नाटक तो कहीं का भी हो सकता है । नाटकों के लिए स्थानीयता एक बड़ी शर्त है । यह अब नाटकों से गायब हो गई है । आप कहीं रहकर भी ‘यूनिवर्सल थिएटर’ कर सकते हैं जिसका अपनी संस्कृति से कोई लेना–देना नहीं होता है ।
इन महोत्सवों पर एक नजरिए से और बात की जा सकती है । हालांकि, यह कई लोगों को दूर की कौड़ी नजर आएगी लेकिन मेरे खयाल से नाट्य महोत्सवों के इस पक्ष पर बात किए बिना यह लेख अपने आप में अधूरा है । यह देखने में आ रहा है कि भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय देश भर में सांस्कृतिक संस्थानों को बहुत ही उदारता से धन देता आ रहा है । यह कोई नई बात नहीं है । देश भर की सांस्कृतिक संस्थाएं और संस्कृतिकर्मी वर्षों से इन योजनाओं से लाभान्वित होते आ रहे हैं । प्रोडक्शन ग्रांट से लेकर बिल्डिंग ग्रांट तक की योजनाओं से कई संस्कृतिकर्मी अपना पेट और घर भरते रहे हैं । इनमें ज्यादातर नाम ऐसे हैं जिनका इस क्षेत्र में न तो कोई नाम है, न ही पहचान और न ही वे सांस्कृतिक गतिविधियां करते ही हैं । सरकार चूंकि कागजी काम को स्वीकार करती है अत: वह कागजों पर ही सबकुछ पूरा कर लेते हैं और उनका काम चल जाता है । सरकार और उनका प्रशासन तंत्र इसकी कमियों पर ध्यान नहीं देता । सरकार इसलिए ध्यान नहीं देती क्योंकि जहां हजारों करोड़ के खेल दूसरे मंत्रालयों में चल रहे हैं वहां संस्कृति मंत्रालय का पूरा बजट ही कुछ सौ करोड़ में सिमटा है । ऐसे में यह बहुत महत्व का मंत्रालय नहीं है । प्रशासन तंत्र का ध्यान इसलिए नहीं जाता क्योंकि उन्हें आंख बंद करने का लाभ मिलता है ।
लेकिन यह वह बात नहीं है जो मैं कहना चाह रहा हूं । सरकार के सहयोग से देश भर में जो महोत्सवों की बाढ़ आई है उसके निहितार्थ उतने भी सीधे नहीं हैं जितने कि दिखते हैं । यह महोत्सव भले ही नाटक के हों, संगीत के हों, साहित्य का हो, सिनेमा का हो या कला की दूसरी विधाओं के हों इसके दो छुपे हुए भाव हैं जिनकी ओर ध्यान देना अतिआवश्यक है क्योंकि इसके निहितार्थ इतने गहरे और गंभीर हैं कि इनकी ओर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में हमारा देश एक बड़े सांस्कृतिक संकट से गुजरता नजर आएगा ।
संस्कृति के महोत्सवीकरण के पीछे के छुपे हुए भावों को समझने की कोशिश करें तो पहली बात यह समझ में आती है कि संस्कृति को एक उत्पाद की शक्ल दी जा रही है । संस्कृति जो जीवन और समाज का हिस्सा रहा है उसे जीवन और समाज से अलग कर एक भौतिक उत्पाद के रूप में ढाला जा रहा है । यह काम इतने महीन तरह से किया जा रहा है कि हम न सिर्फ आसानी से उसमें ढलते जा रहे हैं बल्कि उसकी भयावहता को समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं । संस्कृति जब जीवन का हिस्सा न रहकर एक भौतिक उत्पाद के रूप में बदल दी जाएगी तब संस्कृति समाज के निर्माण और विकास में जो भूमिका निभाती थी, इसकी वह भूमिका खत्म हो जाएगी । संस्कृति एक ऐसी चीज होकर रह जाएगी जिसके निर्माण में समाज और समुदाय की भूमिका न के बराबर रह जाएगी । कुछ खास लोगों के हाथों में ही यह रह पाएगी और समाज के शेष लोग इसके निर्माता न रहकर इसके उपभोक्ता के रूप में बचे रह जाएंगे । आप इसे बाजार से खरीद तो सकेंगे लेकिन इसके निर्माण में आपकी कोई भूमिका नहीं रह जाएगी । यही वह भूमिका है जो समाज को जोड़ने का काम करती है । किसी भी सत्ता के लिए संस्कृति की यही भूमिका सबसे खतरनाक नजर आती है जहां वह लोगों को जोड़ने का काम करती है । दूसरी बात यह कि कला समाज के लिए कभी भी सिर्फ मनोरंजन की वस्तु नहीं रही है । वह समाज को मनोरंजन नहीं बल्कि सौंदर्यबोध देने का काम करती रही है । इसके साथ ही वह एक खास समाज द्वारा लंबे ऐतिहासिक कालक्रम में अर्जित किए गए ज्ञान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम भी करती रही है । इसके साथ ही संस्कृति और खासकर नाटक अपने समय और समाज की चिंताओं को पूरे समाज के सामने रखने और उस पर सोचने को विवश करने का काम करती रही है । संस्कृति और नाटकों के भौतिक उत्पाद में बदल जाने से उसकी यह भूमिका भी खत्म हो जाएगी ।
यह प्रयास पिछले कुछ सालों से संगीत और सिनेमा के क्षेत्र में तेजी से सफल रहे हैं और अब रंगमंच की बारी है । भारत सरकार ने भारतीय लोक कलाओं को आयोजनों में प्रदर्शन और मनोरंजन की की वस्तु बनाकर इसकी शुरुआत 80 के दशक में ही कर दी थी जब समाज के भीतर के संस्कृति के पोषकों को समाज से बाहर की दुनिया दिखा, उसे समाज विमुख बनाने की शुरुआत की थी । कल तक जो लोग अपने समाज के लिए नाटक और गीत–संगीत तैयार करते थे आज वही पर्यटकों और उपभोक्ताओं के लिए यह कर रहे हैं । देश भर के कला रूपों में यह देखने में आ रहा है । अब बारी उस शौकिया रंगकर्म की है जो आज तक सरकार के सामने चुनौती के रूप में मौजूद रहा है ।
बड़े पैमाने पर रंग महोत्सवों के आयोजन करवाकर सरकार दोहरे खेल कर रही है । उसका पहला और सीधा मकसद तो देश की गुलाबी तस्वीर आम जनता के बीच पेश करने की है । देश भर में कलारूपों के बड़े महोत्सव देश की वह रंगीली तस्वीर पेश करती है जोकि देश की हकीकत से कहीं से भी मेल नहीं खाता है । सरकार की विभेदकारी नीतियों की वजह से ही देश के भीतर जो एक बड़ा मध्य वर्ग पैदा हुआ है, वह उसे इस भ्रम में रखना चाहती है कि देश की हालत बहुत अच्छी है । बड़े पैमाने पर और देश भर में हो रहे महोत्सव इसमें सरकार की मददगार की भूमिका में हैं । चूंकि यही वह वर्ग है जिसके सपने भी विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के बाद दरकने लगी थे और यही वह वर्ग है जिसके सड़क पर उतरने से सत्ता और सरकार में खलबली मचती है, इसलिए इस वर्ग को तरह–तरह से खुश रखना इसके पीछे एक बड़ी वजह है । विभिन्न कलारूपों से जुड़ा यही मध्य वर्ग इन महोत्सवों में हिस्सा ले रहा है और उसे इस वजह से लग रहा है कि सरकार उसके लिए कुछ कर रही है । इस प्रकार सरकार उनकी चुप्पी खरीद रही है क्योंकि वह अपने कलारूपों में आम जनता की समस्याओं को सामने लाकर सरकार के सामने मुश्किलें खड़ा कर सकता है ।
दूसरे सरकार बहुत ही आसानी से कला रूपों को भौतिक उत्पाद में बदलने में कामयाब हो रही है । इसके अलावा वह शौकिया रंगकर्मियों की टोली के सामने भी एक तरफ तो अवसर की जूठी गुठली फेंक रही है, दूसरी तरफ जो इस महोत्सव कल्चर का हिस्सा नहीं बन पा रहा है उसे मुख्यधारा से बहिष्कृत किया जा रहा है क्योंकि भारी सरकारी समर्थन की वजह से संस्कृति का यही रूप मुख्यधारा बना दिया गया है । अगर इन चिंताओं पर ध्यान दें तो देश भर में आयोजित हो रहे रंग महोत्सवों के बड़े गहरे निहितार्थ हैं जिनकी अनदेखी देश की संस्कृति और समाज के लिए बड़ा घातक सिद्ध होने वाली है ।
मृत्युंजय प्रभाकर : 1995 में पटना से अपने रंगकर्म की शुरुआत करने वाले मृत्युंजय प्रभाकर पिछले एक दशक से लगातार दिल्ली में रहकर रंगकर्म कर रहे हैं । 2005 से वह ‘सहर’ रंग समूह के साथ अपने रंगकर्म के काफिले को बढ़ावा दे रहे हैं । वह एक समर्थ युवा नाटककार, रंग समीक्षक, कवि, निर्देशक के रूप में अपनी पहचान रखते हैं । उन्होंने आधा दर्जन से अधिक मौलिक नाटकों की रचना की है, साथ ही, कुछ विदेशी नाटकों का भारतीय रूपान्तरण किया है । आधुनिक नाट्य विमर्श को सम्बोधित उनकी पुस्तक ‘समकालीन रंगकर्म’ प्रकाशित है । साहित्य अकादमी ने उनके कविता संग्रह ‘जो मेरे भीतर हैं’ का प्रकाशन किया है । फिलवक्त वह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कला एवं सौंदर्यशास्त्र विद्यालय से नाट्य कला में पी–एच–डी– कर रहे हैं और विश्व भारती विश्वविद्यालय, शान्ति निकेतन में संगीत भवन में नाट्य कला के सहायक प्रोफेसर हैं ।
सम्पर्क : 919910417507
