राष्ट्रभाषा का प्रश्न

- गजेन्द्र पाठक
भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन के इतिहास में 1942 के महत्त्व से हम सब परिचित हैं। लेकिन आज आपके गौरवशाली ऐतिहासिक संस्थान में 1942 की बात करने नहीं आया हूँ। मैं आपको उससे सौ साल पीछे 1842 में ले चलूँगा। इसी वर्ष इस नगर की स्थापना हुई थी और जिस व्यक्ति को उसका श्रेय है उनके नाम पर आपके परिसर में एक छात्रावास भी है। मैं प्रोबी कोटले को याद करना चाहता हूँ। गंगा कैनाल और आपका यह कॉलेज उनके सपनों और श्रम का सुफल है। जो लोग कोटले साहब को जानते हैं उन्हें पता होगा कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा बार बार खड़ी की जाने वाली आर्थिक अड़चनों के बावजूद उन्होंने बारह वर्षों में अपने समय की दुनिया की सबसे बड़ी नहर प्रणाली को सच करके दिखाया। हरिद्वार के पण्डा लोग इस नहर के विरोध में थे। कोटले साहब ने उन्हें बहुत प्रेम और सम्मान से समझाया कि इस नहर के जरिये पक्के घाटों से गंगा मईया और हरिद्वार की रौनक कितनी बढ़ जाएगी। विघ्न विनाशक गणेश जी की पूजा से गंगा नहर की शुरुआत के द्वारा भी उन्होंने हिन्दुओं की श्रद्धा का पूरा ख्याल रखा। आज का पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड का यह इलाका अगर देश की एक बहुत बड़ी आबादी का पेट भरने में कामयाब हुआ है तो इसके पीछे उनके सपनों और आत्मा का उजास शामिल है। बड़ी सोच से बड़ी बाधाएँ भी दूर हो जाती हैं। रुड़की आकर लगता है कि अँग्रेजों ने सिर्फ बुरा ही नहीं सोचा। गाँधी जी अगर अँग्रेजों से सिर्फ नफरत ही नहीं, संवाद की भी जरूरत समझते थे तो इसका कारण शायद कोटले और थॉमसन जैसे लोग ही रहे होंगे। कोटले साहब इंजीनयर भी थे। मैं भी इसलिए कह रहा हूँ कि इसके अलावा उनका एक परिचय और है। वे पैलीयोन्टोलोजी के भी विद्वान थे। सभ्यता के प्रारम्भिक काल में उनकी गहरी दिलचस्पी थी। अठारहवीं शताब्दी में फ्रांस में जॉर्ज कुविर को पैलीयोन्टोलोजी का जनक माना जाता है। कोटले पर उनका गहरा प्रभाव था। ज्ञान का यह अद्भुत अनुशासन दरअसल विलुप्त प्रजातियों और जीवित प्रजातियों में सम्बन्ध सूत्रों की पड़ताल करता है। मेरा मन कहता है कि कोटले गंगा घाटी की प्राचीन सभ्यता और उसके किनारे विलुप्त प्रजातियों की पड़ताल के लिए भी एक लम्बी खुदाई कर रहे थे। लेकिन यह खुदाई पुरातात्त्विक खुदाई भर नहीं थी बल्कि इसमें चिन्ता इस बात की भी थी कि जो पानी व्यर्थ बह जाता है, उसे दोआबे की धरती पर पहुँचा कर खेतों को सोने की खान में तब्दील कर दिया जाए। दुनिया की सभी प्राचीन सभ्यताएँ नदी घाटी सभ्यताएँ हैं, वे जानते थे। वे यह भी जानते थे कि इन पुरानी सभ्यताओं को बचाने में आधुनिक इंजीनियरिंग की भी भूमिका हो सकती है। मैं उनकी सोच और स्मृति को प्रणाम करना चाहता हूँ।

आपके परिसर में जिस दूसरे व्यक्ति को मैं अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूँ उसके पहले मैं लार्ड मेकॉले को याद करना चाहूँगा रुड़की की स्थापना से आठ साल पहले 1834 में लार्ड मेकॉले को ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने शिक्षा सम्बन्धी एक पब्लिक इंस्ट्रक्शन कमिटि का अध्यक्ष बनाया था। 2 फरवरी 1835 को उन्होंने नौ पन्नों का अपना प्रस्ताव तत्कालीन वाइसराय लार्ड विलियम बेंटिक को सौंपा था। वे बहुत अच्छे वक्ता थे। आक्रामक भी। कुतर्कों को भी तर्क जैसा सिद्ध करने में निष्णात थे। भारत की उनकी यात्रा एक नये अध्याय की शुरुआत थी। भारतीय भाषाओं के वे घनघोर विरोधी थे। यह अलग बात है कि वे भारतीय भाषाओं से अपना अज्ञान स्वीकार करने में ग्लानि नहीं बल्कि गर्व महसूस करते थे। अपने प्रस्ताव में उन्होंने संस्कृत, अरबी और फ़ारसी के अध्ययन और अध्यापन को बोझ बताया था। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के एक लाख रुपये के प्रस्तावित बजट को वे इन फालतू के विषयों और भाषाओं पर नाहक लुटाने के विरोध में थे। अँग्रेजी भाषा के गौरव के नशे में चूर वे स्वयं यह भूल गये थे कि अँग्रेजी भाषा का निर्माण ज्ञानियों ने नहीं चरवाहों और गणेरियों ने किया था। संस्कृत और फ़ारसी के परम ज्ञानी को भी वे महामूर्ख समझते थे। राजा राम मोहन राय के हवाले उन्होंने अपनी मान्यता को पुष्ट किया कि आधुनिक भारत निःशुल्क गुरुकुल और मदरसों से बाहर निकल कर पैसा खर्च कर अँग्रेजी पढ़ना चाहता है। उनकी मान्यता थी कि अँग्रेजी पढ़कर नया भारत बाकी दुनिया से बेहतर सम्बन्ध बना सकता है।
वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में जो मदरसा स्थापित किया था उसे मेकॉले ने बंद करने की सिफारिश की। बनारस का संस्कृत कॉलेज यद्यपि उन्हें कलकत्ता के मदरसे से बेहतर लगा, तथापि वे इसे नये युग में प्रासंगिक मानने के पक्ष में नहीं थे। अपने प्रस्ताव की शुरुआत में ही उन्होंने समिति की उस आम सहमति से परिचित कराया था जो हिन्दुस्तानी बोलियों के साहित्यिक और वैज्ञानिक दारिद्र्य को रेखांकित करती थी। लेकिन इस समिति की चिन्ता उस वर्ग को लेकर थी जो उच्च शिक्षा हासिल तो करना चाहता था लेकिन उसके पास विकल्प नहीं थे। समिति में ऐसे लोग भी थे जो संस्कृत और अरबी में उच्च शिक्षा के पैरोकार थे। लेकिन उनकी संख्या कम थी। अँग्रेजी के पक्षधर ज्यादा थे और जब मेकाले जैसे लोगों का मार्गदर्शन और प्रेरणा हो तब पूछना ही क्या? जिनके लिए यूरोप के किसी पुस्तकालय का एक सेल्फ जब पूरे हिन्दुस्तान और अरब पर भारी पड़ता हो उनके सामने कोई तर्क चलने वाला नहीं था। मेकॉले साहब जिस उद्देश्य से आये थे वह यही था कि एक लाख रुपया जो संस्कृत और अरबी पढ़ाने और किताब छापने में खर्च होता था उसे कैसे बचाया जाए। एक तीर से कई शिकार हुए। ये पैसे भी बचे, अँग्रेजी बेचकर पैसे कमाने का बंदोबस्त भी हुआ और दीर्घसूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत अँग्रेजी पढ़ने से एक ऐसा वर्ग भी निर्मित होना था जो रक्त और रंग की दृष्टि से तो भारतीय था लेकिन स्वाद, विचार, नैतिकता और बुद्धि की दृष्टि से अँग्रेज हो। आम के आम और गुठली के दाम ही नहीं, हर्रे लगे ना फिटकरी रंग आवे चोखा। इस प्रकरण में अद्भुत बात यह है कि मेकॉले साहब को ‘पब्लिक मनी’ के बर्बादी की बहुत चिन्ता थी। रुड़की का इंजीनयिरिंग कॉलेज भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है। 1847 ई. में जेम्स थॉमसन( 1804-1853)ने इसकी स्थापना की थी। लन्दन में पढ़ाई पूरी कर उन्होंने आजमगढ़ में कलेक्टर के रूप में काम शुरू किया था। बाद में तत्कालीन उत्तर पश्चिमी राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रहे। उम्र कम मिली पर काम कम नहीं किया। जिस मेकॉले ने भारत की जड़बुद्धि को बार बार कोसा था और वैज्ञानिक चेतना का अभाव भारत के रग रग में देखा था, उसके ठीक 12 साल बाद इंजीनियरिंग कॉलेज का विचार साधारण बात नहीं थी। थॉमसन साहब ने सिर्फ यही नहीं किया भारत में प्रारम्भिक ग्रामीण पाठशाला के जनक भी वही हैं। बरेली जहाँ उन्होंने अपने जीवन की आखिरी साँस ली उसके आसपास उन्होंने 897 विद्यालयों की स्थापना की थी और उन्होंने लार्ड मेकॉले से अलग राय रखते हुए वर्नाकुलर शिक्षा को श्रेयस्कर माना। थॉमसन साहब के लिए ग्रामीण, गरीब, देशी होना अपमान का विषय नहीं था। न ही उनके लिए देशी भाषाओं में पढ़ना लज्जा और पिछड़ेपन की निशानी थी। वे जानते थे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास दुनिया भर में मातृभाषाओं में पढ़ने वाले बच्चों से ही हुआ है। रुड़की का इंजीनयिरिंग कॉलेज आज अगर दुनिया के मानचित्र पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाने में कामयाब हुआ है तो यह उसी सोच का परिणाम है जो सिर्फ इंजीनयिरिंग कॉलेज खोलने तक सीमित नहीं थी बल्कि उसमें दाखिला लेने भावी विद्यार्थियों को गाँव की पाठशाला में, उसी की मातृभाषा में पूरे आत्मविश्वास के साथ तैयार करने में यकीन रखता था। लार्ड मेकॉले और जेम्स थॉमसन एक ही देश से थे, लेकिन सोच में 36 का रिश्ता था। हम उनकी स्मृति को प्रणाम करते हैं।
दुनिया के इतिहास में बुध्द पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मातृभाषाओं की ताकत को पहचाना था। इतिहास की यह विडम्बना है कि हमने न तो बुद्ध को ठीक से पहचाना और न ही अपनी मातृभाषाओं की ताकत को। इतनी पुरानी गौरवशाली परम्परा के बावजूद हम चूक गये। ज्ञान और श्रम को जब तक हमने एक जैसा सम्मान दिया तब तक सोने की चिड़िया बने रहे और हर शिकारी के आकर्षण का केन्द्र भी रहे। बुद्ध ने पाखण्ड और हिंसा के खिलाफ जो संदेश दिया उसे भी हमने नहीं सुना। जन्मना पवित्रता और अपवित्रता को अपने धर्म का मूल मान लिया। जिनके शरीर से श्रम का पसीना ज्यादा बहता था उन्हें अछूत बना दिया। श्रम का यह अपमान देश पर भारी पड़ा। एक बहुत बड़ी आबादी को ज्ञान और विचार की प्रक्रिया से बाहर कर देश और राज्य की चिन्ता सिर्फ चापलूस और भयभीत दरबारियों के भरोसे छोड़ने से जो हुआ वह अब इतिहास का विषय है। बुद्ध को जिन्होंने पहचाना और उन्हें सम्मान दिया, वे देश आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी में दुनिया में सबसे आगे हैं। मातृभाषाओं के बल पर ही हम किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं।
मुझे प्रीतिकर आश्चर्य हुआ कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के केन्द्रीय पुस्तकालय का नाम महात्मा गाँधी पुस्तकालय है। गाँधी जी को अपने देश में बहुत सारे लोग औद्योगिक संस्कृति का विरोधी मानते थे। 1925 में गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने ‘कल्ट ऑफ चरखा’ नामक अपने ऐतिहासिक निबन्ध में गाँधी जी की सोच को पुरातनपंथी सिद्ध कर दिया था। हिन्दी के मशहूर आलोचक रामविलास शर्मा हिन्दी नवजागरण में ओद्योगिक संस्कृति के विरोध को गाँधी का प्रभाव मानते हैं। दिलचस्प बात यह है कि रामविलास जी हिन्दी नवजागरण की दो बड़ी कमजोरियों के पीछे क्रमशः महात्मा गाँधी और गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर का प्रभाव मानते हैं। बहरहाल आपके ऐतिहासक परिसर में गाँधी को पाकर मैं चकित भी हूँ और उत्साहित भी। 150 साल बाद गाँधी अपने देश के जनमानस में कितने रचे बसे हैं इसे व्याख्यायित करने की जरूरत नहीं है। गाँधी जी तथाकथित पढ़े लिखे लोगों को कितना पसन्द करते हैं यह आप सब जानते हैं। वे जानते थे कि बुद्धिजीवी वर्ग कहता कुछ और है और करता कुछ और है। इसलिए वे महसूस करते थे कि महत्त्वपूर्ण यह नहीं कि बुद्धिजीवी कह क्या रहा है बल्कि यह देखा जाना चाहिए कि कर क्या रहा है?। बहरहाल, यह भारी मन से स्वीकार करना पड़ता है कि रवीन्द्रनाथ ठाकुर, जवाहरलाल नेहरू और रामविलास शर्मा जैसे लोग गाँधी के प्रतीकों को समझ नहीं पाए थे। गाँधी जी यन्त्र और विज्ञान के विरोधी होते तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की के केन्द्रीय पुस्तकालय का नामकरण उनके नाम पर नहीं होता। उन्होंने 1924 में एक बातचीत में कहा था कि, “मैं जानता हूँ कि यह शरीर भी एक नाजुक यन्त्र ही है। खुद चरखा भी एक यन्त्र ही है, छोटी दाँत कुरेदनी भी यन्त्र है। मेरा विरोध यन्त्रों के लिए नहीं है, बल्कि यन्त्रों के पीछे जो पागलपन चल रहा है,उसके लिए है। आज तो जिन्हें मेहनत बचानेवाले यन्त्र कहते हैं, उनके पीछे लोग पागल हो गये हैं। उनसे मेहनत जरूर बचती है, लेकिन लाखों लोग बेकार होकर भूखों मरते हुए रास्तों पर भटकते हैं। समय और श्रम की बचत तो मैं भी चाहता हूँ, परन्तु वह किसी खास वर्ग की नहीं, बल्कि सारी मानव जाति की होनी चाहिए। कुछ गिने -गिनाये लोगों के पास सम्पति जमा हो ऐसा नहीं, बल्कि सबके पास जमा हो ऐसा मैं चाहता हूँ। आज तो करोड़ों की गरदन पर लोगों के सवार हो जाने में यन्त्र मददगार हो रहे हैं। यन्त्रों के उपयोग के पीछे जो प्रेरक कारण हैं, वह श्रम की बचत नहीं है, बल्कि धन का लोभ है। आज की इस चालू अर्थ-व्यस्था के खिलाफ मैं अपनी तमाम ताकत लगाकर युध्द चला रहा हूँ। “गाँधीजी ने सिंगर सिलाई मशीन को विज्ञान की बहुत बड़ी उपलब्धि माना था”। उन्होंने लिखा है कि, “सिंगर की सीने की मशीन का मैं स्वागत करूँगा। आज की सब खोजों में जो बहुत काम की थोड़ी खोजें हैं, उनमें से एक यह सीने की मशीन है”। उसकी खोज के पीछे अद्भुत इतिहास है। सिंगर ने अपनी पत्नी को सीने और बखिया लगाने का उकताने वाला काम करते देखा। पत्नी के प्रति रहे उसके प्रेम ने गैर – जरूरी मेहनत से उसे बचाने के लिए सिंगर को ऐसी मशीन बनाने की प्रेरणा दी। ऐसी खोज करके उसने न सिर्फ अपनी पत्नी का ही श्रम बचाया, बल्कि जो भी ऐसी सीने की मशीन खरीद सकते हैं उन सबको हाथ से सीने के उबानेवाले श्रम से छुड़ाया है।”
हिन्द स्वराज में गाँधी ने भारत के परम्परागत वस्त्र उद्योग के विनाश के पीछे अँग्रेजों की चालाकी और मैनचेस्टर के कपड़ा मिलों को जिम्मेदार माना था। यूरोप में मशीनो ने जिस भस्मासुरी प्रवृति का परिचय देते हुए उसे उजाड़ने का काम किया उसका वीभत्स रूप दुनिया के सामने दो दो विश्वयुद्धों के रूप में आया। गाँधी विनाश की उस आँधी से परिचित थे। वे नहीं चाहते थे कि विनाश की वह आँधी भारत को भी अपने चपेट में ले ले। मेरा अनुमान है कि गाँधी की यन्त्र दृष्टि के पीछे मनुष्यता और स्वाधीनता की जो पुकार है उसे आपके संस्थान ने समझा है। सर कोटले, जेम्स थॉमसन और महात्मा गाँधी के विचार और कर्म की इस त्रिवेणी में अपने को पाकर मैं कृतार्थ महसूस कर रहा हूँ।
गाँधी जी ने आज से लगभग 100 साल पहले यह घोषणा की कि वे अँग्रेजी भूल गये हैं। हिन्द स्वराज में अभिव्यक्त उनके विचारों से गोखले जी लगभग असहमत थे। भारत को नजदीक देखने के निर्देश का उन्होंने अक्षरशः पालन करते हुए फिर वे उसी निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि भारत को जोड़ने के लिए एक भाषा की जरूरत है और वह भाषा अनिवार्य रूप से हिन्दी ही हो सकती है। “हिन्द स्वराज” में ही वे इस बात से चकित थे कि अपने देश में स्वधीनता की बात भी अँग्रेजी में की जाती है। अँग्रेजी पढ़े लिखे लोगों को गाँधी से बेहतर कौन जानता था? वे जानते थे कि, “करोडों लोगों को अँग्रेजी की शिक्षा देना उन्हें गुलामी में डालने जैसा है। मेकॉले ने शिक्षा की जो बुनियाद डाली, वह सचमुच गुलामी की बुनियाद थी। उसने इसी इरादे से अपनी योजना बनाई थी, ऐसा मैं नहीं सुझाना चाहता। लेकिन उसके काम का नतीजा यही निकला है। यह कितने दुख की बात है कि हम स्वराज्य की बात भी पराई भाषा में करते हैं?” अँग्रेजी तालीम पाने वाले लोगों को वे राष्ट्र की गुलामी का वास्तविक कारण मानते थे। अपने देश में इंसाफ पाने के लिए भी पराई भाषा के पास जाना पड़े इससे बड़ी विडम्बना क्या हो सकती है?
भारत में भाषा का प्रश्न सदियों से चिन्तन और चिन्ता का विषय रहा है। मैंने बुद्ध की चर्चा की है। बुद्ध का ही प्रकाश भक्ति आन्दोलन में संस्कृत के खिलाफ देशी भारतीय भाषाओं की मुक्ति का अभियान बना। यूरोप के नवजागरण से पहले भारतीय भाषाओं का जागरण। गाँधी पर उस भक्ति आन्दोलन का गहरा असर था। वे भारतीय भाषाओं की ताकत से परिचित थे। इन्हीं भाषाओं में देश की स्वाधीनता की चेतना सुरक्षित है,वे जानते थे। उन्होंने तालीम की भाषा को लेकर हिन्द स्वराज में ही स्पष्ट शब्दों में अपनी राय दी “मुझे तो लगता है कि हमें अपनी सभी भाषाओं को उज्ज्वल – शानदार बनाना चाहिए। हमें अपनी भाषा में ही शिक्षा लेनी चाहिए-इसके क्या मानी है, इसे ज्यादा समझाने का यह स्थान नहीं है। जो अँग्रेजी पुस्तकें काम की हैं, उनका हमें अपनी भाषा में अनुवाद करना होगा। बहुत से शास्त्र सीखने का दम्भ और वहम हमें छोड़ना होगा। सबसे पहले तो धर्म की शिक्षा या नीति की शिक्षा दी जानी चाहिए। हरेक पढ़े-लिखे हिन्दुस्तानी को अपनी भाषा का, हिन्दू को संस्कृत का, मुसलमान को अरबी का, पारसी को फ़ारसी का और सबको हिन्दी का ज्ञान होना चाहिए। कुछ हिन्दुओं को अरबी और कुछ मुसलमानों और पारसियों को संस्कृत सीखनी चाहिए। उत्तरी और पश्चिमी हिन्दुस्तान के लोगों को तमिल सीखनी चाहिए। सारे हिन्दुस्तान के लिए जो भाषा चाहिए, वह तो हिन्दी ही होनी चाहिए।”
न्गूगी वा थयोंगों के नाम और काम से आप सब परिचित हैं। जिस तरह गाँधी ने अँग्रेजी छोड़कर अपनी मातृभाषा में काम करने का निर्णय लिया था उसी तरह न्गूगी ने अपनी मातृभाषा गिकियू में ही लिखने का निर्णय लिया था। अपने देश केन्या समेत समस्त अफ्रीकी महादेश में वे अँग्रेजी से नष्ट हुई अफ्रीकी भाषाओं की अस्मिता की रक्षा को अफ्रीकी स्वाधीनता की चेतना की रक्षा के एक बड़े सांस्कृतिक अभियान के रूप में देखते हैं। नगूँगी की नजर लम्बे समय से भारत की तरफ रही है। गाँधी और रवीन्द्रनाथ ठाकुर की भाषा दृष्टि और सांस्कृतिक चेतना के वे मुरीद रहे हैं। बलवंत गार्गी और बलराज साहनी के हवाले उन्होंने गाँधी और रवीन्द्रनाथ के क्रमशः गुजराती और बांग्ला लेखन के जरिये उनकी मातृभाषाओं से प्यार को बेहद कीमती मानते हैं।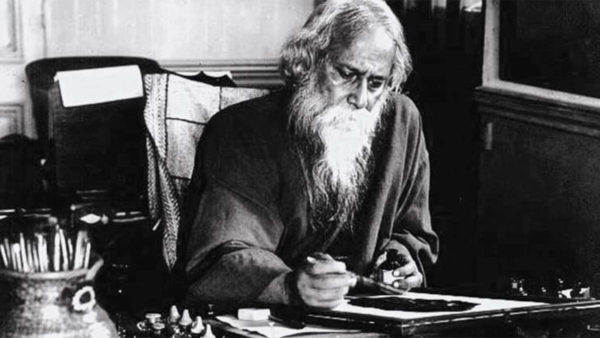
गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने 1932 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के अपने एक मशहूर व्याख्यान में कहा था कि, “हमारे देश में जब मातृभाषा को शिक्षा के आसन पर प्रतिष्ठित करने का सुझाव दिया गया तब अँग्रेजी जानने वाले विद्वान बेचैन हो उठे। उन्हें आशंका थी कि जिन थोड़े से लोगों को अँग्रेजी भाषा का व्यवहार करने का सुयोग प्राप्त है उनका अधिकार कम न हो जाय। दरिद्र की आकांक्षा भी दरिद्र ही होती है।” यूरोपीय विद्या को वे भारत में स्थानान्तरित अचल जलाशय के रूप में देखते थे जिसमें जीवन और गतिशीलता दोनों का अभाव है। अँग्रेजी को वे प्रयोजन सिद्धि की भाषा मानते थे। इसी कारण हमारी शिक्षा व्यवस्था को वे विदेशी भाषा के प्रति लोभ के रूप में देखते थे और इसे प्रेमी की प्रीति नहीं बल्कि कृपण की आसक्ति मानते थे।
रवीन्द्रनाथ ठाकुर इस बात पर चकित होते थे कि जिस देश में तक्षशिला, नालन्दा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय रहे हों उस देश को अँग्रेज आधुनिक यूनीवर्सिटी देने का दम्भ भरते हैं। और विडम्बना यह कि यह यूनिवर्सिटी मॉडल पराये देश में पराई भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाती है। जबकि सच यह है कि, “सुनने में यह बात स्वतः विरोधी लग सकती है,लेकिन वास्तव में भाषा-स्वातन्त्र्य से ही योरोपिय विद्या में सहकारिता का आरम्भ हुआ। इस स्वातन्त्र्य ने यूरोप के चित्त को खण्डित नहीं बल्कि संयुक्त किया है। स्वदेशी भाषाओं द्वारा विद्या को जब मुक्ति मिली, यूरोप में ज्ञान का ऐश्वर्य वृद्धिगत हुआ, पड़ोसियों और दूर देशों की ज्ञान साधना से उसका योग स्थापित हुआ- मानो अलग अलग खेतों का शस्य यूरोप के साधारण भण्डार में एकत्रित हुआ हो। आज वहाँ के विश्वविद्यालय उदार भाव से सभी देशों के होते हुए भी विशेष रूप से अपने-अपने देश के हैं।”
“निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल” सिर्फ यूरोप में विश्वविद्यालयों के विकास और उत्थान तक सीमित नहीं था बल्कि मध्ययुग में एशिया में बौद्ध धर्म के विकास में अपने अपने देशों की भाषाओं की क्या भूमिका रही गुरुदेव इसे रेखांकित करते हैं, “मध्ययुगीन एशिया में तिब्बत, चीन और मंगोलिया ने बौद्ध धर्म को ग्रहण अवश्य किया, लेकिन अपनी भाषाओं में ही उन्होंने इस धर्म को अपनाया। इसीलिए बौद्ध धर्म इन देशों की जनता का आन्तरिक धर्म बन सका और मोह के अन्धकार से उनका उद्धार कर सका।”

1930 में निराला जी ने सुधा के एक अंक में राष्ट्रभाषा का प्रश्न नाम से एक लेख लिखा था। इस लेख में उन्होंने राष्ट्र भाषा के प्रश्न को राष्ट्रीयता की भावना के साथ अनिवार्यतः जुड़ा हुआ माना था। इस लेख के प्रारम्भ में ही उन्होंने रोमन साम्राज्य के सुनहरे दिनों में लैटिन भाषा के उत्थान और दुनिया भर में वर्चस्व की चर्चा की है। रोमन साम्राज्य के पतन के बहुत बाद पुनर्जागरण काल में यूरोपीय भाषाओं के उत्थान की चर्चा करते हुए उन्होंने लिखा है कि,”जब यूरोप के जन समाज में प्रजातन्त्र के भाव उदय हुए और जब यूरोपीय देशों में राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ तब लैटिन की रौनक कम हुई, और अनेक राष्ट्र भाषाओं का उदय हुआ। स्वयं इटली ने लैटिन को छोडक़र इटालियन भाषा की श्री वृद्धि की। राष्ट्र संघटन के लिए एक भाषा का होना परम आवश्यक और उपयोगी समझा गया, इसी कारण अँग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन आदि अनेक भाषाएँ लैटिन की स्पर्द्धा में उठ खड़ी हुईं।” निराला जी ने यूरोप के प्रबुद्ध और प्रभुवर्ग के मन में लैटिन के प्रति लम्बे समय तक बने रहने वाले मोह की चर्चा करते हुए ऑक्सफ़ोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के लैटिन प्रेम की चर्चा की है जिनकी दिलचस्पी राष्ट्रीयता और स्वदेशी भाषाओं से ज्यादा लैटिन के प्रति रही। लन्दन विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ अँग्रेजी का सम्मान कैसे बढ़ा इस बात की चर्चा भी उन्होंने की है।
निराला जी भारत में अँग्रेजों की कुटिलता पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि, “भारतवर्ष अँग्रेजों की साम्राज्य लालसा का सर्व प्रधान ध्येय रहा है। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति अँग्रेजों की सभ्यता और संस्कृति से बहुत कम मेल खाती थी, पर सात समुद्र पार से आकर इतने विस्तृत और इतने सभ्य देश में राज्य करना जिन अँग्रेजों को अभीष्ट था, वे बिना अपनी कूटनीति का प्रयोग किये कैसे रह सकते थे? अँग्रेजों की नीति हुई-भारत के इतिहास को विकृत कर दो, और हो सके तो उसकी भाषा को मिटा दो। चेष्टाएँ की जाने लगीं। हमारा प्राचीन इतिहास अन्धकार में डाल दिया गया। बाकायदा अँग्रेजी की पढ़ाई होने लगी। इस देश का शताब्दियों से अन्धकार में पड़ा हुआ जन समाज समझने लगा कि जो कुछ है, अँग्रेजी सभ्यता है, अँग्रेजी साहित्य है, और अँग्रेज हैं।” आज से नब्बे साल पहले निराला जी ने जो चिन्ता प्रकट की थी वह अँग्रेजों के जाने के इतने सालों बाद भी किस रूप में मौजूद है इसे जानने के लिए बहुत शोध की दरकार नहीं है। मानसिक गुलामी प्रत्यक्ष गुलामी से भी ज्यादा खतरनाक होती है। आज तक अगर हम एक मजबूत राष्ट्र बनने के बावजूद एक राष्ट्रभाषा को लेकर संशय और दुविधा की स्थिति में हैं तो यह चिन्ता और चिन्तन का विषय है। बहुभाषिकता को हमारी कमजोरी के रूप में पेश कर अँग्रेजी को एक मजबूत राष्ट्रीय विकल्प के रूप में पेश करने वाली सोच सिर्फ अँग्रेजों तक सीमित होती तो बात समझ में आती थी। लेकिन ऐसी सोच यदि स्वाधीन भारत में भी बनी हुई है तो इसके लिए सिर्फ अँग्रेज दोषी नहीं हैं। बहुत आसान होता है कि हम अपनी समस्याओं की जिम्मेदारी किसी पर डाल कर निश्चिन्त हो जाएँ। बहुत कठिन होता है कि हम आत्मावलोकन करें कि आज तक अगर हिन्दी को एक मजबूत राष्ट्रभाषा के रूप में अगर हम नहीं देखना चाहते हैं तो इसके लिए हम और हमारे मन में मौजूद ग्रन्थि कितनी जिम्मेदार है? हम अपने नौनिहालों को आज भी अँग्रेजी रट कर बोलते हुए देख कर पुलकित होते हैं। स्वाभाविक रूप से अपनी मातृभाषा में अपने बच्चों को सपने देखने की इजाजत भी नहीं है। ऐसे देश में, ऐसी सोच से हिन्दी और मातृभाषाओं का क्या होगा यह तो कल्पना का विषय है लेकिन मुझे भय है कि गुलामी का सदियों पुराना दंश सहने वाला देश ऐसी सोच से अपनी स्वाधीनता की चेतना को कब तक बचा कर रख पाएगा?
4 नवम्बर 2019 को भारतीय प्रद्योगिकी संसथान रुड़की में दिये गये व्याख्यान का संसोधित स्वरुप।

लेखक हिन्दी विभाग, हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद में प्रोफेसर हैं|
सम्पर्क- +918374701410, gpathak.jnu@gmail.com




