तेंदुए के विष-नेत्र, दहकती घृणा और सांप

अज्ञेय ने ‘ शरणार्थी’ नामक कविता लिखी है। यह कविता 11 उपखंडों में बँटी है और 12 अक्टूबर 1947 से लेकर 12 नवम्बर 1947 के बीच लिखी गई है। सभी उपखंडों के अलग- अलग शीर्षक हैं। देश को आजादी तो मिली थी, लेकिन वह सांप्रदायिक हिंसा में जल रहा था। एक ही देश के लोग दो हिस्से में बँट चुके थे और अपने लिए सुरक्षित स्थल ढूंढ रहे थे। पाकिस्तान के हिस्से से लोग भारत आ रहे थे और भारत के हिस्से से पाकिस्तान। दोनों देश में से शरणार्थी थे। दोनों तरफ के शरणार्थियों में गुस्सा था, क्षोभ था, नफरत थी। अज्ञेय की ‘शरणार्थी’ कविता के पहले उपखण्ड का शीर्षक है- मानव की आँख। शरणार्थियों की आँख में उस वक्त क्या था? अज्ञेय की पंक्ति है- “कोटरों से गिलगिली घृणा यह झांकती है/ मान लेते यह किसी शीत रक्त, जड़ दृष्टि/ जल-तलवासी तेंदुए के विष नेत्र हैं।” आँखों के कोटरों में घृणा है और ये आँखें तेंदुए के विष नेत्र में तब्दील हो गयी हैं। इन आँखों में जिनमें कभी प्रकाश दीप्त होता था, लेकिन अब शत्रु- भाव है। ये आँखें दूसरे की आँखों से मिलती हैं, लेकिन वहाँ भातृ-भाव नहीं, बल्कि “मानव से मानव की मिलती है आँख पर/ कोटरों से गिलगिली घृणा झांक देती है।”
अज्ञेय आजादी के आंदोलन के सक्रिय सेनानी रह चुके थे। वे लंबे समय तक कारावास में भी रहे। उन्होंने स्वयं के बारे में लिखा है-“ एक समय था जब मैं एक क्रांतिकारी संगठन का सदस्य था और ब्रितानी साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ रहा था, उस युद्ध में मैंने सभी साधनों का उपयोग किया था।” वे बम बनाते हुए 1930 के अंत में पकडे़ गये थे। वे भगत सिंह को छुड़ाना चाहते थे। इसका कुल नतीजा था कि वे 1930 से 1936 तक विभिन्न जेलों में रहे। जेल में कविताएं भी लिखीं और ‘ शेखर : एक जीवनी’ नामक चर्चित उपन्यास भी।’ शेखर : एक जीवनी’ की भूमिका में अज्ञेय लिखते हैं- “इतना बता सकता हूँ, जब आधी रात को डाकुओं की तरह पुलिस मुझे बंदी बना ले गई, थोड़ी सी मारपीट भी हो गई, तब मुझे दिखने लगा मेरे जीवन का इति अब शीघ्र होने वाला है।

“जाहिर है कि अज्ञेय ने व्यक्तिगत रूप से आजादी के लिए दुख भी झेला था और संत्रास भी। अज्ञेय नाम भी इसी वजह से उन्हें मिला था। अज्ञेय ने जेल से एक कहानी प्रेमचंद के पास अवैद्य तरीके से छपने के लिए भेजी थी। वे एक षड्यंत्र केस में बंदी थे। उनके नाम सच्चिदानंद हीरानंद के नाम से यह कहानी छापी नहीं जा सकती थी, इसलिए प्रेमचंद ने अज्ञेय के नाम से कहानी छाप दी। जिस आजादी के लिए अज्ञेय ने कष्ट झेला था, जब वह मिली तो खंडित थी और थी खून से सनी हुई। शरणार्थी कविता के दूसरे उपखण्ड का शीर्षक है- पक गयी खेती। यह कौन- सी खेती है जो पक गयी है? क्या किसी फसल की है जो पकी है? नहीं, वह आजादी की खेती थी जो नेताओं द्वारा की गई और नतीजा हुआ- “वैर की परनालियों से हँस- हँस के/ हम ने सींची जो राजनीति की रेती/ उस में आज बह रही खूँ की नदियां हैं।” सांप्रदायिक हिंसा में देश दग्ध हो गया। अज्ञेय लिखते हैं- “घृणा की आज उस में पक गयी खेती/ फसल काटने को अगली सदियां हैं।” 1947 में यह कविता लिखी गई, आज 2021 है और कविता में लिखी अज्ञेय की भविष्यवाणी सौ-फीसद सही साबित हुई है। 1947 के सांप्रदायिक विद्वेष की आज भी खेती हो रही है, राजनीतिक फसलें काटी जा रही हैं। पता नहीं कब तक काटी जायेंगीं!
शरणार्थी कविता के चौथे उपखण्ड का शीर्षक है- ठांव नहीं। शरणार्थी जब आये तो उनके ठांव का कोई ठिकाना नहीं। कविता की पंक्तियां हैं- “शहरों में कहर पडा है और ठांव नहीं गांव में/ अन्तर में खतरे के शंख बजे, दुराशा के पंख लगे पांव में/ त्राहि! त्राहि! शरण- शरण! / रुकते नहीं चपल चरण।” शरणार्थियों के अंदर एक ही गूँज है- “कैसे बचें कैसे बचें कैसे बचें कैसे बचें।” कवि को लगता है कि यह जो हालत है, उसकी वजह है -‘आन? मान? वह तो उफान है गुरूर का।’ शरणार्थी कविता के चौथे उपखण्ड का शीर्षक है- मिरगी पड़ी। कवि को ऐसा लग रहा है कि मानव जगत को मिरगी लग गई है। जैसे राह चलते मिरगी का रोगी अचानक थोड़ी देर के लिए होश खो देता है, कुछ ऐसा ही हुआ है। कविता की पंक्तियां हैं- “मिरगी का दौरा है/ चेतना स्तिमित है।” कवि को मिरगी में शिथिलता नहीं दिखती- “ किन्तु कहीं भी तो नहीं दिखती शिथिलता-/ तनी नसें, कसी मुट्ठी, भिंचे दांत, ऐंठी मांस-पेशियां/ वासना स्थगित होगी किन्तु झाग झर रहा मुँह से।”
कवि चिंतित है- “आज जाने किस हिंस्र डर ने/ देश को बेखबरी ने डँस लिया! /संस्कृति की चेतना मुरझा गयी! / मिरगी का दौरा पडा, इच्छाशक्ति बुझ गयी।” हालत यह है कि जीवन हुआ है रुद्ध मूर्च्छना की कारा में। मुक्ति की चाहत में जो देश संघर्षरत था, उसकी देह लोथ हो गई है। कविता के पांचवें उपखण्ड का शीर्षक है- ‘रुकेंगे तो मरेंगे।’ शरणार्थियों के ठहरने का ठांव नहीं, वे करे तो क्या करे? तय किया उसने कि वे चलते रहें। रुके तो मृत्यु निश्चित है। कविता की पंक्तियां इस भयावह सच को यों उकेरती हैं- “नाक में नकेल डाल जो भी खींच ले चलेगा/ उसी को! चलो, चलो, चाहे कहीं ले चलो, बस बहने दो:/ व्यवस्था के, शांति, आत्मगौरव के, धीरज के/ ढूह सब ढहने दो-/ बुद्धि जब जड हो तो/ मांस-पेशियों के तड़पन को/ जीवन की धड़कन मान लें।” शरणार्थियों की नाक में जो भी नकेल डालेगा, वह उसके साथ चल पडेगा। उनके अंदर के आत्मगौरव, शांति और धीरज के परखचे उड गये हैं। व्यवस्था ढह गयी है। हालात यह है कि मांस-पेशियों के तडपन को ही जीवन मान लिया गया है। कविता इन पंक्तियों पर खत्म होती है- “भागो, भागो, चाहे जिस ओर भागो/अपना नहीं है कोई, गति ही सहारा यहाँ/ रुकेंगे तो मरेंगे।”

शरणार्थी का छठा उपखण्ड सात खंडों में विभक्त है और इस उपखण्ड का शीर्षक है-‘ समानांतर सांप। ’ यह सांप और कुछ नहीं आदमी के मन-मिजाज को मारनेवाली सांप्रदायिकता है। यह कहीं बाहर नहीं है। हमारे ही अंदर है। वह जिसमें बस जाती है, वह सांप से भी ज्यादा जहरीला हो जाता है। कविता की पहली पंक्ति है- ‘हम एक लंबा सांप हैं। ’ और फिर कवि मैं पर आता है-‘ मैं- कहीं उस सांप की गुंजलक में उलझा हुआ- सा / एक बेकस जीव हूँ। ’ फिर कवि के सामने 1947 का भयावह चित्र आता है-“ बगल से गुजरे चले तुम जा रहे जो/ सिर झुकाये, पीठ पर गट्ठर सँभाले/ गोद में बच्ची लिये/ उस हाथ से देते सहारा किसी बूढे या कि रोगी को/ पलक पर लादे हुए बोझा जुगों की हार का-/ तुम्हें भी कैसे कहूँ तुम सृष्टि के सिरताज हो?/ तुम भी जीव हो बेबस।” वह जो मंजर था जिसमें दस लाख से भी ज्यादा जानें गंवायीं, कोई मामूली परिघटना नहीं थी। जो लोग शिकार हुए, अपने परिवार को ढोते हुए इधर से उधर और उधर से इधर आये, उनके बारे जब कवि कहता है कि ‘तुम्हें भी कैसे कहूँ तुम सृष्टि के सरताज हो’ तो ह्रदय दहल जाता है। यह जो सांप है सांप्रदायिकता का, एक-दूसरे को प्यारा लगता है।
कवि लिखता है-“ यह हमारा सांप है/ हम जा रहे हैं उस ओर, जिस में सुना है/ सब लोग अपने हैं; / वह तुम्हारा सांप/ तुम भी जा रहे हो, सोचते निश्चय, कि वह तो देश है जिस में/ सत्य होते सभी सपने हैं।” सांप तो एक ही है। दोनों को डंस रहा है- हिन्दुओं को भी मुसलमानों को भी, भारत को भी और पाकिस्तान को भी। लेकिन हिन्दू अपने सांप पर न्यौछावर है तो मुसलमान अपने सांप पर। दोनों के सांप एक- दूसरे को भरोसा दिलाते हैं- “यह हमारा सांप/ इस पर हम निछावर हैं/ जा रहे हैं छोड कर अपना सभी कुछ / छोड कर मिट्टी तलक अपने पसीने-खून से सींची/ किन्तु फिर भी आस बांधे/ जहाँ पर हम को निराई भी नहीं करनी पडेगी/ फल पर रहेगा चमन अपना/ अमन में आशियां लेंगे।” दोनों ने अपने- अपने सांप को पाल रखा है। वह उसे घिनौना लगता है, जहरीली भाफ उगलता है, तब भी कलेजे से लगाये है- “वह तुम्हारा सांप / तुम्हें दीक्षा मिली है सब घृण्य हैं फूत्कार हिंसा के/ किन्तु जब वह उगलता है भाफ जहरीली/ तुम्हें रोमांच होता है/ तुम्हारा सांप जो ठहरा।”
कवि कहता भी है कि यह सांप किसी का नहीं है। यह एक दिन किसी को भी काट खायेगा- “सांप डस लेंगे, निगल जाएँगे/ तुम्हें वह, तुम जिसे अपना सांप कहते हो/ हमें यह, जो हमारा ही सांप है।” कवि परेशान है। पहचानना चाहते है कि इसके बावजूद इंसानियत की लौ कहीं जिंदा है या नहीं। इस सांप ने अलग- अलग रूप धारण कर लिया है, लेकिन हम एक हैं। मनुजता के पतन की इस अवस्था में दोनों पतित हुए हैं। इसलिए ‘केंचुलें हैं, केंचुले हैं, झाड दो/ छल- मकर की तनी झिल्ली फाड दो! / सांप के विष- दांत तोड उखाड दो।” यह सही है कि कठिन वक्त है, लोगों ने जानवरों की खालें पहन रखी हैं- “गले गीदड- लोमड़ी की/ बाघ की खाल कांधों पर/ दिल ढंका है भेड की गुलगुली चमड़ी से/ हाथ में थैला मगर की खाल का / और पैरों को/ जगमगाती सांप की केंचुल/ बनी है श्री चरण का सैंडल।”, लेकिन भेड़-बकरी, बाघ-गीदड, सांप जैसे बहुरूप के भीतर रौंदा हुआ सनातन मानव मौजूद है। कवि कहता है- “गिलगिले ये सांप बैरी हैं हमारे/ इन्हें आज पछाड़ दो।”
4 नवम्बर 1947 को अज्ञेय काशी में थे। वहीं उन्होंने कविता लिखी- ‘ शरणार्थी-7: गाड़ी रुक गयी।’। रात के वीराने में एक गाड़ी रुक गयी है, क्योंकि किसी ने किसी को छुरा मार कर फेंक दिया है। कवि को लगता है कि महज रेल ही नहीं रुकी है, बल्कि मनुजता की रेल रुक गयी है। कविता के अंत में कवि हिन्दू या मुसलमान को नहीं धिक्कारता, बल्कि धिक्कारता है अपनी मनुजता को। इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन मनुजता जग नहीं रही। काशी में ही कविता लिखी- ‘शरणार्थी -8: हमारा रक्त’।
सांप्रदायिक हिंसा में रक्त बह रहा है- “ यह इधर बहा मेरे भाई का रक्त/ वह उधर रहा/ उतना ही लाल/ तुम्हारी एक बहिन का/ रक्त/ बह गया, मिलीं दोनों धारा/ जा कर मिट्टी में/ हुई एक/ पर धरा न चेती। ” कवि को चिंता है कि धरा चेत नहीं रही है, इसकी वजह है कि हमारा रक्त ही हो गया है अशक्त, निवीर्य और निस्तेज। अज्ञेय रेल से काशी से इलाहाबाद जा रहे थे तो रेल पर ही कविता लिखी-‘ शरणार्थी-9: श्री मद्धर्मधुरंधर पंडा।’ चांदपुर, नोआखाली, फेनी य चट्टग्राम, त्रिपुरा आदि जगहों में सांप्रदायिक हिंसा से धरती कांप रही थी, असंख्य पददलित और स्त्रियां चीख रहे थे। एक बवंडर बह रहा था। आकाश भी थर्रा रहा था। ऐसे वक्त में श्री मद्धर्मधुरंधर पंडा के कानों पर जूं तब रेंगी, जब एक दुखियारी उसके पास आयी। दुखियारी मलेच्छ-धर्षिता थी। पंडे ने भी दुर्व्यवहार किया। दया का टुक्कड फेंकनेवाला इस पंडे के कान पर जो जूं रेंग रहा था, वह भी ठहर गया। कवि लिखता है- ‘मानवता को लगीं घोटने फिर गुंजलकें/ मरु रूढि की।’
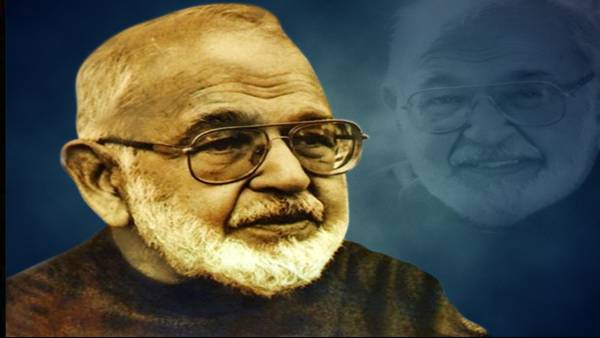
अज्ञेय जब इलाहाबाद आये तो 7 नवम्बर 1947 को उन्होंने कविता लिखी-‘शरणार्थी-10: कहती है पत्रिका’। कविता की पंक्तियां हैं- “कहती है पत्रिका/ चलेगा कैसे उन का देश?/ मेहतर तो सब रहे हमारे/ हुए हमारे फिर शरणागत/ देखें अब कैसे उन का मैला ढुलता है।” सांप्रदायिकता की लहक से समाज बिंध गया है, मगर मेहतर यहाँ रहें या वहाँ, क्या उनकी स्थिति भी बदलेगी? शरणागत हुए देश में मेहतर तो मैला ही ढोयेंगे।’ यह क्या कम है यहाँ लौट कर/ जनम- जनम तक जुगों- जुगों तक/ मिले उन्हें अधिकार, एक स्वाधीन राष्ट्र का/ मैला ढोवें?” अज्ञेय तो यायावर थे। 12 नवम्बर 1947 को मुरादाबाद स्टेशन पर थे तो कविता लिखी- ‘शरणार्थी-11: जीना है बन सीने का सांप’।
औपनिवेशिक सत्ता से संघर्षरत देश से उम्मीद थी कि जब स्वराज मिलेगा तो सभी सुखी होंगे। सबका सिर ऊँचा होगा। सभी एकताबद्ध रहेंगे। लेकिन सांप्रदायिकता रूपी सांप ने सबकुछ छिन्न- भिन्न कर दिया है। कविता की पंक्तियां हैं- “जानते हैं पर आज/ अपने ही बल के/ अपने ही छल के / अपने ही कौशल के/अपनी समस्त सभ्यता के सारे/ संचित प्रपंच के सहारे/ जीना है हमें तो, बन सीने का सांप उस अपने समाज के।” कवि इस सांप को ‘अक्षन्तव्य शत्रु’ से संबोधित करता है। अक्षन्तव्य शत्रु यानी किसी भी तरह क्षमा न करने लायक। तब भी हम उसके मोहताज हैं, क्योंकि हम भिखारी शरणार्थी हैं। अज्ञेय एक स्वाधीनचेता रचनाकार थे। उनकी कविताओँ में आत्मान्वेषण भी है और आत्मबोध भी। उन्होंने अपनी कविताओं में दायित्वपूर्ण सामाजिकता का भी निर्वाह किया है। इसका साक्षात प्रमाण है, यह कविता। ’शरणार्थी‘ कविता के माध्यम से उन्होंने युग सत्य को अभिव्यक्त किया है, साथ ही भविष्यवाणी भी कि अगली सदी में भी सांप्रदायिकता की फसलें काटी जायेंगी।

लेखक वरिष्ठ प्राध्यापक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं प्रखर टिप्पणीकार हैं।
सम्पर्क- yogendratnb@gmail.com


