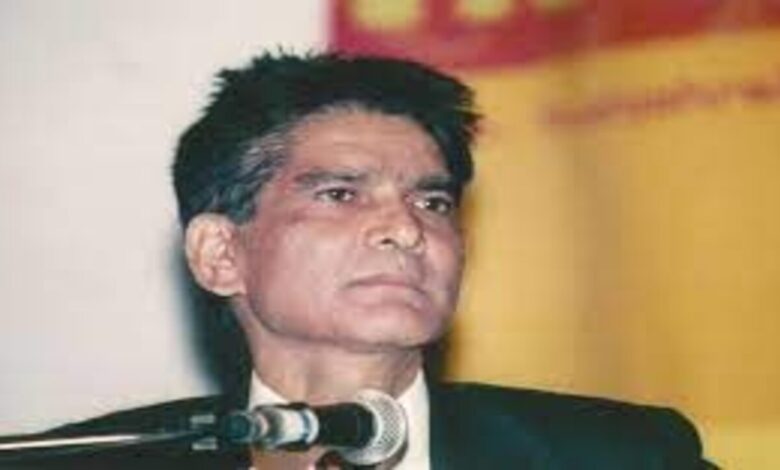
स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी कथा साहित्य में प्रगतिशील चिंतन धारा के लेखकों में अब्दुल बिस्मिल्लाह की ख्याति उनके उपन्यास झीनी बीनी चदरिया के कारण हुई। इस उपन्यास पर उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी मिल चुका है। ‘समर शेष है’ उनका चर्चित उपन्यास है। ‘अतिथि देवो भव’ ‘रफ रफ मेल’ उनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। अब्दुल बिस्मिल्लाह का बनारस से गहरा रिश्ता है। वे एक मस्तमौला, फक्कड़ाना मस्ती के साथ जीवन जीने वाले कथाकार हैं। उन्होंने मध्य वर्ग और निम्न वर्ग के जीवन को अपने कथा साहित्य में प्रमुखता से जगह दी है। हिन्दी कथा साहित्य में अमरकांत उनके आदर्श हैं। एक प्रकार से यह भी कहा जा सकता है कि नयी कहानी के सर्वाधिक लोकप्रिय लेखक अमरकांत की परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया है। नयी कहानी के मुख्य स्वर ‘मोह भंग’ और ‘पीड़ा भरी प्रतीक्षा’ को अब्दुल बिस्मिल्लाह की कहानियों में देखा जा सकता है, हालाँकि ये नयी कहानी और सातवें दशक की कहानी के बाद के कथाकार हैं।
अब्दुल बिस्मिल्लाह की एक कहानी ‘सारिका’ पत्रिका के फरवरी, 1984 अंक में छपी थी, जिसका शीर्षक था ‘बैरंग चिट्ठी।’ उस समय की यह सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पत्रिका थी। कहानी की इस पत्रिका में छपना एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में जाना-समझा जाता था। ‘बैरंग चिट्ठी’ एक पोस्टमैन अब्दुल वाहिद की कहानी है। लेखक ने कहानी में अब्दुल वाहिद के लिए वहिद्दू लिखा है और पोस्टमैन के लिए ‘चिट्ठीरसा’ शब्द का प्रयोग किया है। वहिद्दू की पढ़ाई दसवीं कक्षा तक ही हो पाई है, तब तक उनके अब्बा के एक दोस्त ने उन्हें पोस्टमैनी दिलवा दी थी। अब्दुल वाहिद अपनी ड्यूटी में कभी नागा नहीं करते, बल्कि जब-तब उनके साथ काम करने वाले साथी के छुट्टी पर चले जाने के बावजूद उसकी भी ड्यूटी वही निभाते हैं। लेखक ने इस कहानी में वहिद्दू के माध्यम से पोस्टमैनों की स्थिति तथा मनःस्थिति का बड़ा ही वास्तविक चित्रण किया है। कहानी में एक बदरुद्दीन आते हैं। उनके हाथ में मनीआर्डर देने पर वहिद को कुछ अतिरिक्त रुपये मिल जाते हैं, लेकिन उनकी पत्नी के हाथ में देने पर कुछ नहीं मिलता। पोस्टमैन लोग पैसे के लोभ में कुछ छुट्टे पैसे या रुपये मनीआर्डर के रुपये में दे देते हैं, ताकि कोई ‘चेंज’ होने का बहाना न बनाये। एक पोस्टमैन की यही ऊपरी आमदनी है, क्योंकि उनकी तनख्वाह इतनी कम होती है कि उससे घर चलाना मुश्किल होता है। वहिद्दू इस बात को किसी से छिपाते नहीं। अतिरिक्त पैसा लेने के लिए वहिद्दू झूठ बोलने में भी संकोच नहीं करते। इससे स्पष्ट है कि लेखक वहिद्दू को एक आदर्श चरित्र के रूप में प्रस्तुत करना नहीं चाहता। इससे कहानी की विश्वसनीयता और पठनीयता बनी रहती है।
‘बैरंग चिट्ठी’ में वहिद्दू की एकमात्र इच्छा से हम अवगत होते हैं कि बेटा गुड्डू ‘पढ़-लिखकर बड़ा अफसर बने।’ वास्तव में हमारे समाज के हर वर्ग के माता-पिता की यह बलवती इच्छा होती है कि उसका बेटा या बेटी ऐसी पढ़ाई करे कि वह अफसर बने। बड़ा अफसर बनने के लिए चाहिए अच्छी-से-अच्छी शिक्षण संस्था और हमारे यहाँ अच्छी शिक्षण संस्था का मतलब है कान्वेंट स्कूल, क्योंकि कान्वेंट स्कूल में पढ़ने से एक तो अंग्रेजी भाषा की समुचित जानकारी हो जाती है और दूसरी बात कि तथाकथित बड़े लोगों वाली चाल-ढाल, वेश-भूषा आदि भी आदमी सीख जाता है। वहिद्दू ने लोगों से सुन रखा है कि बड़ा अफसर वही लड़का बनेगा, जिसने कान्वेंट स्कूल में शिक्षा पायी हो। मेरी समझ से अब्दुल बिस्मिल्लाह यहां भारत की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। सरकारी स्कूलों की हालत इतनी खराब कर दी गई है कि कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए वहाँ पढ़ाना नहीं चाहता। अंग्रेजी माध्यम के ईसाई मिशनरियों द्वारा बोले गये कान्वेंट स्कूलों ने सरकारी स्कूलों को श्रीहीन कर दिया है। अब तो ईसाई मिशनरियों की तर्ज पर नवधनाढ्य लोगों ने भी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलकर शिक्षा व्यवस्था में दखल देने लगे हैं। हमारे यहाँ एक अजीब विडंबना की स्थिति है कि सरकारी स्कूलों में अध्यापक की मोटी तनख्वाह है, लेकिन पढ़ाई के नाम पर कुछ भी हासिल नहीं। कान्वेंट स्कूलों में तनख्वाह कम है, लेकिन अध्यापक से काम ज्यादा लिया जाता है। बेरोजगारी के बदले काम चलाऊ विकल्प के रूप में नियुक्ति पाया अध्यापक जी-जान लगाकर बेहतर परिणाम देना चाहता है। शिक्षा की इस बदतर स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है?
खैर, पोस्टमैन वहिद्दू अपने बेटे के कान्वेंट में दाखिला के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। जबकि अनपढ़ उनकी पत्नी इसका विरोध करती है। अपने व्यावहारिक ज्ञान से वह इतना तो समझती ही है कि छोटी तनख्वाह से घर-गृहस्थी तो ठीक से चलती नहीं, कान्वेंट स्कूल की फीस कैसे दी जा सकेगी? वहिद्दू अपनी पत्नी का मुँह बंद करने के लिए बार-बार डाँटते-फटकारते हैं, अपशब्द बोलते हैं, पर घर की बोल-चाल की भाषा में बदलाव भी चाहते हैं, क्योंकि बेटे गुड्डू को एडमिशन के लिए पहले इंटरव्यू से गुजरना पड़ेगा। रोज-रोज की तरह जब उनकी पत्नी बेटे को गुडुवा-गुडुवा कहकर बुलाती है तो वहिद्दू टोक देते हैं ‘यह गुडुवा-फुडुवा क्या लगाये रहती हो? कहो कि गुड्डू बाबू आइए। गुड्डू बाबू चाय पीजिए।’ इस पर वहिद्दू की पत्नी का जवाब बड़ा मारक, स्वाभाविक और दिलचस्प है- ‘न जाने कइसा कनवेंट-फनवेंट का इस्कूल है कि अपने आगे नेकर खोलकर घूमने वाले को भी आप-जनाब कहना जरूरी है।’ अधिक खर्चे वाले कान्वेंट स्कूल में बेटे को पढ़ाने की अपनी हिम्मत का जब वहिद्दू बखान करते हैं, तब भी उनकी पत्नी टोकती है ‘हाँ तब मरिये भूखों, फिर पता चलेगा।’ वहिद्दू कितनी भी हिम्मत दिखाएँ, उनकी पत्नी यथार्थ स्थिति को लेकर चिंतित है। ऐसा नहीं है कि वह अपने बेटे के भविष्य को बेहतर नहीं देखना चाहती, लेकिन वह जानती है कि उसकी औकात इतनी नहीं है कि खर्चीले स्कूल में बेटे को पढ़ा सके। अंततः एक व्यंग्य से अपनी बात खत्म कर देती है- “करिये भइया खूब ऊँचा माथा, पढ़ाइए खूब अंग्रेजी-फारसी, हमसे का मतलब है?” वहिद्दू की पत्नी के इस व्यंग्य में कितना दर्द है, इसे आसानी से समझा जा सकता है। इस व्यंग्य में उसकी बेचारगी भी भी स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती है कि घरेलू स्त्री घर के निर्णयों में वाजिब दखल भी देती है तो डाँट-डपटकर उसे चुप करा दिया जाता है।
कान्वेंट स्कूल में दाखिले के पहले वहिद्दू अपने बेटे की भाषा बदलना चाहते हैं। वे सिखाते हैं कि नीला की जगह ब्लू, हरा के लिए ग्रीन और कविता के लिए पोएम बोलना होगा। यही नहीं जिस वाहिददू ने कभी बेटे को ‘सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा’ कविता रटवाई थी, नहीं वहिद्दू अब पोएम के नाम पर ‘ट्विंकिल ट्विंकिल लिटिल स्टार’ रटवा रहे हैं ताकि दाखिले के पूर्व होने वाले इंटरव्यू में लगे कि लड़का अंग्रेजी सभ्यता-संस्कृति वाले परिवार का है। यहाँ लेखक यह दिखाना चाहता है कि कान्वेंट कल्चर ने किस प्रकार हमारी स्वाभाविकता को बरबाद किया है। उसके आकर्षण में मध्य या निम्न मध्य वर्ग की आर्थिक स्थिति संकटपूर्ण तो हो ही रही है, हम अपनी स्थानीयता, मातृभाषा, आचार-विचार और संस्कार को भी अलविदा कहने के लिए विवश हैं। इस कान्वेंट कल्चर ने हमारी प्रतिरोध की क्षमता को भी प्रभावित किया है।
कहानी में एक अस्वाभाविक स्थिति तब उत्पन्न होती है, जब वहिद्दू इंटरव्यू के लिए अपने बेटे को लेकर हाजी मोइनुद्दीन के घर जाता है। फलों के व्यापारी हाजी साहब उनके पुराने परिचित हैं और उनके पप्पू को भी इंटरव्यू देना है। वहीं हाजी साहब गुड्डू के पैर में चप्पल न देखकर घबरा जाते हैं और गुड्डू को पप्पू की चप्पल दिलवाते हैं। इस वाकया का लेखक ने बहुत दिलचस्प चित्रण किया है- “नीले पट्टों वाली नन्हीं-नन्हीं दो हवाई चप्पलें गुड्डू के सामने बैठी मुस्करा रही थीं। गुड्डू ने जब उन्हें पहना तो वे और मुस्करा उठीं।” यहाँ व्यंजना बहुत अर्थपूर्ण और मार्मिक है, क्योंकि चप्पलों की मुस्कराहट मानो गुड्डू की अभावग्रस्त स्थिति पर गंभीर चोट करती प्रतीत हो रही है।
भोजपुरी में एक कहावत है’ सिखावल बुद्धि अढ़ाई घरी।’ यानी दूसरे की सिखाई हुई बात का असर ढाई घड़ी तक ही रहता है। वहिद्दू ने बेटे को जो कुछ रटवाया था, इंटरव्यू में वह सब भूल गया और उसने वही जवाब दिया, जो पहले का पढ़ा हुआ या याद किया हुआ था। इंटरव्यू लेने वाली का और कमरे का लेखक ने अति सूक्ष्म वर्णन किया है। इसे ही सूक्ष्म निरीक्षण की शक्ति कहते हैं। अब्दुल कादिर ने कविता के नाम पर ‘सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा’ तो सुनाया ही, इसके रचयिता इकबाल का नाम भी बताया। इंटरव्यू के संदर्भ में ही एक ऐसा प्रश्न आया, जिसका उत्तर सुन किसी का भी हृदय द्रवीभूत हो जायेगा। जब इंटरव्यू लेने वाली स्त्री उससे पूछती है कि “तुम्हारे लिए खिलौने कौन लाता है?” तब अब्दुल कादिर जवाब देता है कि “हमारे लिए खिलौना कोई नहीं लाता!” मेरी समझ से पूरी कहानी में प्रयुक्त यह एक वाक्य अपने सम्पूर्ण प्रभाव के साथ हमारे मन-मस्तिष्क को विस्मित कर देता है। इस एक वाक्य में बच्चे के मन का जो दर्द छिपा हुआ है, उसे अभिव्यक्त करना मुश्किल है। हद तो तब हो जाती है, जब स्त्री कादिर से नाचने के लिए कहती है और वह साफ इनकार देता है। एडमिशन न होने की धमकी पर वह स्त्री से सीधे कहता है कि “एडमिशन नहीं होगा तो गोली मार देंगे।” कादिर का यह क्षोभ, यह गुस्सा क्या तात्कालिक है? क्या जिस परिवेश में उसकी परवरिश हुई है, उसके प्रति उसका क्षोभ नहीं है? निश्चित रूप से कादिर अपने घर और पास-पड़ोस की स्थितियों के प्रति सचेत होगा, तभी उसका गुस्सा फूट पड़ा होगा, क्योंकि वहाँ निर्द्वन्द्व होकर अपनी बातें रख रहा था। कादिर का गोली मारने की बात कहना मेरी समझ से पूरी व्यवस्था के प्रति आक्रोश दर्शाना है। ज्ञातव्य है कि अब्दुल बिस्मिल्लाह अपने को उस समय लेखक के रूप में तैयार कर रहे थे, जब नक्सलवादी आंदोलन जोर पकड़ रहा था।
‘बैरंग चिट्ठी’ कहानी की त्रासदी चरम पर तब पहुँचती है, जब वहिद्दू कान्वेंट स्कूल नोटिस बोर्ड पर प्रवेश पाने छात्रों की सूची में अपने बेटे अब्दुल कादिर उर्फ गुड्डू नाम गायब पाते हैं। यह त्रासदी और ज्यादा दुखदायी तब लगने लगती है, जब वे देखते हैं कि हाजी मोइनुद्दीन का पप्पू प्रवेश पाने में सफल हो गया है। हाजी साहब फलों के व्यापारी हैं। एक व्यापारी के लड़के ने पोस्टमैन के लड़के को शिक्षा भूमि में पैसे के बल पर परास्त कर दिया था। वहिद्दू ने जिस इकलौते बेटे को कॉन्वेंट में पढ़ाकर बड़ा अफसर बनाने का सपना देखा था, वही उनका बेटा अब नगरपालिका के स्कूल में लाल रंग की बुश्शर्ट और गंदा निकर पहने पढ़ने के लिए मजबूर है। यहाँ सपना सिर्फ वहिद्दू का ही नहीं, उनके बेटे गुड्डू का भी टूटता है। हम सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि एक टूटे सपने के साथ जिन्दगी शुरू करने वाले बच्चे के मन पर भविष्य को लेकर क्या प्रभाव पड़ता होगा। मुझे ऐसा लगता है कि कहानी में वहिद्दू का सपना वैसे ही टूटता है, जैसे अमरकांत की कहानी ‘डिप्टी कलक्टरी’ के शकलदीप बाबू का। उन्होंने भी अपने लड़के को डिप्टी कलक्टर बनाने का सपना देखा था। अंतर यही है कि शकलदीप बाबू के यहाँ पढ़ाई-लिखाई की वह समस्या नहीं थी, जो वहिद्दू के साथ है। यहाँ तो वाहिदू के बेटे की जड़ पर ही प्रहार किया गया है। ‘मोह भंग’ नयी कहानी की जो एक मुख्य प्रवृत्ति थी, उसे ‘बैरंग चिट्ठी’ में भी देखा जा सकता है।
कहानी का शीर्षक वाहिद्दू की नौकरी के सर्वथा अनुकूल है। जिस बैरंग चिट्ठी को हम महत्त्वहीन समझते हैं, उसके प्रति उपेक्षा का भाव रखते हैं, वहिद्दू का बेटा गुड्डू भी बैरंग चिट्ठी की तरह लगने लगा है। उसके कंधे से सफेद झोला लटक रहा है और उसमें टिन की एक स्लेट पड़ी हुई है। कहानी का अंत अब्दुल बिस्मिल्लाह ने बड़े मर्मस्पर्शी वाक्यों के साथ किया है कि सब कुछ के बावजूद “गुड्डू को नहीं लगता कि उसके पापा उसे नगर महापालिका की किसी स्याहीगिरी टाटपट्टी पर बैठाकर चुपके से खिसक जाएंगे और वह माकूल टिकट के अभाव में नष्ट होते पत्रों के बीच कहीं खो जाएगा।” बच्चे की भावनाओं से जुड़े ये वाक्य हमें संवेदना के उच्च धरातल पर पहुँचा देते हैं।
अप्रैल 1983 की ‘सारिका’ पत्रिका में अब्दुल बिस्मिल्लाह की एक कहानी छपी थी ‘पुरानी हवेली’। भारत में जो लोग स्त्रियों की वास्तविक स्थिति जानना चाहते हैं, उनके लिए यह बहुत जरूरी कहानी है। देश के संभवत: हर शहर में नारी संरक्षण गृह बनाये गये। संरक्षण गृह का नाम दूसरा हो सकता है, लेकिन ये संरक्षण गृह सरकारी सहायता प्राप्त होते हैं और उनको चलाने वाले क्षेत्र के दबंग लोग हुआ करते हैं। उन संरक्षण गृहों में बेसहारा स्त्रियाँ रखी जाती हैं। उनमें ऐसी भी स्त्रियाँ होती हैं, जो बलात्कार की शिकार होती हैं, परित्यक्ता होती हैं और नारी संरक्षण गृह में उनके रहने और खाने-पीने की किसी प्रकार व्यवस्था हो जाती है। पुरानी हवेली एक प्रकार से स्त्रियों के लिए संरक्षण गृह ही है, लेकिन हवेली में रहने वाली स्त्रियों के साथ जैसा व्यवहार होता है, उसके आधार पर इस संरक्षण गृह को यदि हम एक ‘यातना गृह’ कहें तो यह ज्यादा सही होगा। हवेली में बूढ़ी, जवान, कमसिन कई प्रकार की स्त्रियाँ होती हैं।
कहानी की शुरूआत एक विचित्र स्थिति से होती है कि दो औरतें वेश्यावृत्ति के अपराध स्वरूप हवेली में गिरफ्तार करके लायी गई थीं और उन्हें संभ्रान्त किस्म के बदमाश लगने वाले दो लोग छुड़ाने आये थे- सक्षम अधिकारी के आदेश के साथ। तत्काल वे इसलिए नहीं छूट सकीं, क्योंकि शाम के वक्त पाँच बजे के बाद किसी स्त्री को छोड़ने का नियम नहीं है। गिरफ्तार दो औरतों के साथ हवेली की ‘लड़कियों’ का संवाद किसी भी मन को झकझोर देने वाला है। जब लड़कियाँ पूछती हैं कि “एक दिन कितने मर्दों के साथ सोती हैं? तो स्त्रियों का जवाब है कि “जितने मिल गये।” फिर जब उनसे पूछा जाता है कि ‘थकती नहीं? औरतों का जवाब आता है कि “रंडी जब थकने लगे तो हो चुका धंधा।” औरतों के जवाब से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्रकार की लाखों स्त्रियाँ किस प्रकार के नरक में अपनी जिन्दगी काट रही होंगी। इस हवेली की अधीक्षिका सर्वेसर्वा है। हवेली के अंदर वह पूरे ठाट से रहती है। हवेली की सभी स्त्रियों पर वह रोब गाँठती है। जो स्त्री उसकी चापलूसी करती है, उसे वह अपने साथ रखती है। उसकी विशेष सेवा में सुन्दर लड़की होती है। हवेली की हर लड़की के साथ कोई-न-कोई ऐसी घटना घटी है कि घर-परिवार से उसे बाहर कर दिया गया है। पितृ सत्तात्मक समाज से वे बहिष्कृत तो हैं ही, जिस हवेली की अधीक्षिका, संचालिका स्त्रियाँ हैं, वे भी हवेली में रखी गई लड़कियों से अत्यंत क्रूरतापूर्ण व्यवहार करती हैं। कहानी में उनकी क्रूरता के तो कई कारनामे हैं, यहाँ एक उदाहरण काफी होगा। होता यह है कि हवेली की एक लड़की कृष्णा का प्रेम पत्र उसके साथ रहने वाली ईश्वरी के हाथ लग जाता है और उसे वह अधीक्षिका की मुख्य सेविका दुलारी को पकड़ा देती है। फिर क्या, अधीक्षिका कृष्णा की पीठ पर डंडा बरसाने लगती है और अंततः कृष्णा गायब हो जाती है। कहने का मतलब कि पुरुष वर्चस्व वाले समाज में ही नहीं, स्त्री वर्चस्व वाली जगहों में भी प्रेम के दुश्मनों की कोई कमी नहीं है। नारी संरक्षण गृह में स्त्रियाँ कितनी असुरक्षित हैं, अब्दुल बिस्मिल्लाह की इस कहानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। कहानी में यह एक बड़ा सवाल है कि हवेली की अधीक्षिका नयी से नयी और सुंदर लड़कियों को ही अपनी विशेष सेवा में क्यों रखती है? या तो वे ऊपर के अधिकारियों का दिल बहलाने’ के काम आती हैं या ‘धंधा’ कराकर पैसा कमाने के काम आती हैं। नारी संरक्षण गृह के नाम पर स्त्री-देह का किस तरह शोषण होता है, कहानी में लेखक ने बड़े साहस से इसका उद्घाटन किया है। मुन्नीबाई की कहानी ऐसी ही है। जब वह अधीक्षिका के कहने पर एक मर्द के साथ सोने से इंकार करती है। यह इंकार मुन्नीबाई का काल बन जाता है। हवेली की अधीक्षिका न सिर्फ उसे बुरी तरह पीटती है, बल्कि जलाकर मार डालती है। मुन्नीबाई के साथ घटी इस घटना का लेखक ने बड़ा हृदय विदारक वर्णन किया है। अधीक्षिका का क्रूरतम चेहरा हवेली की हर स्त्री के मन में दहशत पैदा करता ही है, अधिकार पा जाने पर कोई स्त्री भी कितना अमानवीय हो सकती है, लेखक ने इसका बड़ा प्रभावशाली चित्रण इस कहानी में किया है।
‘पुरानी हवेली’ कहानी का अंत अब्दुल बिस्मिल्लाह ने इस ढंग से किया है कि पाठक के मन में दुविधा उत्पन्न होती है। अंतत: हवेली का फाटक टूटा कि नहीं? प्रायः देखा गया है कि जब दमन चरम पर पहुँच जाता है, तब दमन के शिकार लोगों में एकजुटता आती है और वे बड़ा से बड़ा खतरा उठाने का निर्णय लेते हैं। इस कहानी में मुन्नीबाई की हत्या से उपजा आक्रोश एक बड़े संघर्ष में बदल जाता है और हवेली की स्त्रियाँ हवेली से मुक्ति के लिए बड़ा फाटक तोड़ डालने के लिए दौड़ पड़ती हैं। उनकी इस कार्रवाई के विरोध में जो भी स्त्री आती है, उसकी दुर्गति होती है। अधीक्षिका तो अपनी जान बचाने के लिए भाग जाती है। उसकी नयी नयी चहेती बनी रत्ना गिरा-गिराकर पीटी जाती है और हवेली की एक स्त्री देवबाला के आह्वान पर सभी स्त्रियाँ हवेली के फाटक को तोड़ने पर अपना ध्यान केंद्रित करती हैं।
सारे संघर्ष, शोर और दौड़ा-दौड़ी के बावजूद कहानी में फाटक के टूट जाने का जिक्र नहीं है, लेकिन यह तो स्पष्ट है कि स्त्रियों की ‘मुक्ति की आकांक्षा’ का स्वर कहानी का सबसे ऊंचा स्वर है। वैसे भी, सत्ता-व्यवस्था के चक्रव्यूह का फाटक तोड़ना आसान नहीं है। हवेली की स्त्रियों का यह एहसास कि वे गुलाम हैं, दमन और शोषण की शिकार हैं, उन्हें अपने इस वर्तमान से मुक्त होना है, कहानी को विश्वसनीय बनाता है। अब्दुल बिस्मिल्लाह ने इस कहानी को भी छोटे-छोटे संवादों के द्वारा आगे बढ़ाया है। किसी भी स्तर पर घुमावदार शिल्प का उन्होंने प्रयोग नहीं किया है। भाषा उनकी चिर-परिचित सहज और सीधी है। हालाँकि कहानी में घटनाएँ कई हैं, लेकिन वे मुख्य कथ्य से जुड़ी हुई हैं। लेखक ने स्त्रियों की मनोदशा और विवशता का सफल चित्रण कर स्त्री जीवन के दबे-ढँके ऐसे क्षेत्र की गहरी पड़ताल की है, जो बाहर से देखने पर तो साफ-सुथरा लगता है, लेकिन उसके भीतर कितनी गंदगी है, यह ठीक-ठीक कहना आसान नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि ‘पुरानी हवेली’ कहानी का आसानी से नाट्य रूपांतरण किया जा सकता है। इसका मंचन तो निश्चित रूप से बहुत प्रभावशाली होगा और तब यह कहानी अपना संदेश छोड़ने में अपेक्षाकृत अधिक सफल होगी।
‘हंस’ पत्रिका के फरवरी, 1992 अंक में अब्दुल बिस्मिल्लाह की कहानी छपी थी। ‘कर्मयोगा’ कहानी है तो बहुत छोटी, लेकिन एक कार्यालय के बाबू से लेकर चपरासी और बॉस तक किस प्रकार जमीन की दलाली के धंधे में लगे हैं, इसका बहुत दिलचस्प वर्णन इस कहानी में किया गया है। लेखक ने इस कहानी को पाँच उपशीर्षकों में बाँटा है, हालाँकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि एक तो कहानी लम्बी नहीं है और दूसरे कि इसमें पात्रों की संख्या भी ज्यादा नहीं है। कहानी का कथ्य एक ही है और उसमें कोई घटनात्मक मोड़ या कौतूहल जैसी कोई बात नहीं है। कहानी की शुरुआत कृष्णप्रताप के स्कूल के दिनों से होती है, जब वे परीक्षा में ‘बेरोजगारी की समस्या’ पर पूछे गये प्रश्न पर कई निबंध लिख चुके थे। यहाँ लेखक ने थोड़ी चुटकी ली है कि अब समस्या पर प्रश्न पूछते हुए भी शिक्षक शर्माने लगे हैं कि यह विषय आउटडेटेड हो गया है। ऐसा नहीं है कि देश में बेरोजगारी की समस्या हल हो गई है। आज की तारीख में यह समस्या बड़ी ही है, बल्कि वो कहें कि विकराल रूप धारण कर चुकी है, लेकिन एक ही विषय पर बार-बार सवाल करने से शिक्षक उब गये हैं। शिक्षकों की ऊब गहरे अर्थ की बोधक है।
कहानी के मुख्य पात्र कृष्णप्रताप को बहुत दिनों के बाद ‘कठिन तपस्या’ और ‘भगवान की कृपा’ से देश की राजधानी में बाबू (क्लर्क) की नौकरी तो मिल जाती है, लेकिन नौकरी मिलने की खुशी आदि का कहानी में कोई जिक्र नहीं है। लेखक सीधे अपने मंतव्य पर आ जाता है कि कैसे इस पूँजीवादी सभ्यता ने आदमी को स्व-भाव में नहीं रहने दिया है। कृष्ण प्रताप या तो काम करते हैं या खाली समय में उपन्यास पढ़ते हैं। ऐसे व्यक्ति को किस प्रकार दलाल अपने जाल में फँसाना चाहते हैं, इसका बड़ा दिलचस्प वर्णन कहानी में मिलता है। उनके पास पहले ऑफिस का चपरासी आता है, जिसका नाम दिनेश है। चूँकि कृष्णप्रताप किसी भी प्रकार के भेद-भाव के खिलाफ हैं, इसलिए दिनेश को अपने पास कुर्सी पर बिठाते हैं। अब दिनेश अपना जाल फैलाना शुरू करता है। वह राजधानी में जमीन लेने, मकान बनवाने, बाल-बच्चों का भविष्य संवारने की बात कर कृष्णप्रताप को यहाँ तक प्रभावित कर लेता है कि वे गाँव का खेत बेचकर राजधानी में जमीन लेने का निश्चय कर लेते हैं। यहाँ लेखक ने गँवई मध्यवर्ग के मिजाज को बहुत गहराई से पकड़ा है कि वह अपने वर्तमान को कष्ट में डालकर भविष्य की चिन्ता ज्यादा करता है। गाँवों में कहावत भी चलती है कि ‘अग्र सोची, सदा सुखी’ अब कृष्णप्रताप भी अपनी नौकरी से सुखी जीवन जीने की बजाय प्लाट खरीदने की चिंता में डूब जाते हैं। सन् 1992 में लिखी गई यह कहानी आज ज्यादा प्रासंगिक इसलिए है कि बड़े-बड़े शहरों में प्लाट या फ्लैट का लोभ दिखाकर बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ अपने एजेन्टों और चमक-दमक वाले विज्ञापनों के द्वारा लोगों को फाँसती हैं, वे यदि पास में पैसा न हो तो बैंकों से ऋण दिलाकर, खेत बंधक रखवाकर प्लाट या फ्लैट खरीदने के लिए आदमी को मजबूर कर देती हैं।
‘रीयल स्टेट’ के ये कारोबारी आज हर शहर में अपना पाँव जमाये हुए हैं। अन्ततः होता यह है कि ऊँची ब्याज दर पर कर्ज लेने वाला निम्न और मध्यम आय वर्ग का आदमी जीवन भर या तो किश्त भरता है या अत्यधिक मानसिक दबाव में आत्महत्या कर लेता है।
‘कर्मयोग’ कहानी में दिलचस्प मोड़ तब आता है, जब ऑफिस में यह प्रचार हो जाता है कि कृष्णप्रताप शहर में प्लाट लेने वाले हैं। उनके ऑफिस का बाबू लियाकत सुबह-सुबह उनके घर आ धमकता है और अपने बहनोई के माध्यम से एक अच्छा प्लॉट दिलाने की बात करता है। लियाकत यह बताता है कि दिनेश दलाल है और फ्रॉड है। बात यहीं तक नहीं रुकती। जब कृष्णप्रताप ऑफिस जाते हैं तब उनका बॉस उन्हें अपने कमरे में बुलाकर अच्छा प्लाट दिलाने का वादा करता है। कृष्णप्रताप को आत्मीय बनाने के लिए बॉस पहले तो दिनेश और लियाकत को फ्रॉड सिद्ध करता है और विश्वास दिलाता है कि वही उसका असली हितचिन्तक है। इसके लिए वह दोनों के ब्राह्मण होने की बात भी करता है। अंततः कृष्णप्रताप को ज्ञान की प्राप्ति होती है कि सारा संसार कर्म योग में लगा हुआ है तो उन्हें भी इसी मार्ग पर चलना चाहिए और वे खुद प्लाट खरीदने और बेचने के धंधे में आ जाते हैं।
‘कर्मयोग कहानी को पढ़ते हुए प्रेमचन्द के निबंध ‘महाजनी सभ्यता’ की याद आती है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि इस सभ्यता में सिर्फ पैसे का बोलबाला होगा। आदमी के आत्मीय रिश्ते भी पैसे से निर्धारित होंगे। अब तो एक और शब्द चल पड़ा है- चंचल पूँजी। इस पूँजी ने आदमी के आदर्श, नैतिकता को छिन्न-भिन्न कर दिया है। अब्दुल बिस्मिल्लाह ने कहानी में ऑफिस का परिचय तक नहीं दिया है कि किस विभाग का ऑफिस है। एक प्रकार से ऑफिस का मूल क्रिया-कलाप कहानी में अनुपस्थित है और इस अनुपस्थिति का अपने आप में बहुत महत्त्व है। अपना मूल काम छोड़कर चपरासी, बाबू, बॉस सभी जमीन के धंधे में यानी दलाली में लगे हैं यानी पैसा चाहे जैसे आये, लेकिन आये। चंचल पूँजी यही करती है। दलाली का यह धंधा लोगों के दिल-दिमाग पर इस कदर हावी है कि इसके चक्कर में लोग आपसी रिश्ते की भी बलि दे देते हैं। अपने-अपने तरीके से ऑफिस के सभी लोग एक दूसरे की शिकायत कर कृष्णप्रताप को अपनी गिरफ्त में लेना चाहते हैं। कृष्णप्रताप किसी आदमी की गिरफ्त में तो नहीं आते, लेकिन लोगों की धूर्त चाल का उन पर इतना असर होता है कि अमूर्त-सा लगने वाला धंधा उन्हें अपनी गिरफ्त में जरूर ले लेता है। इस कहानी को पढ़ते हुए प्रेमचन्द्र की ही कहानी ‘नमक का दारोगा’ की याद भी ताजा हो उठती है। यह विडंबना ही कही जायेगी कि जिस नौकरी से कृष्णप्रताप ने कुछ सपने देखे होंगे, उनके पूरे होने के पहले ही वे जमीन के गोरखधंधे में फाँस लिये जाते हैं। कहने का मतलब कि यदि स्वतंत्र होकर हम कुछ निर्णय भी लेना चाहें, तो यह व्यवस्था हमें निर्णय नहीं लेने देगी। हमारा मस्तिक भी अब किसी अदृश्य सत्ता के हाथ का खिलौना बना दिया गया है।







