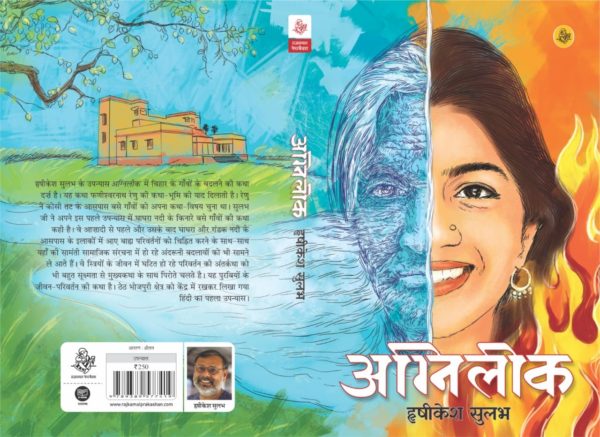राकेश तिवारी की कहानियाँ : फंतासी की नज़र से यथार्थ की तस्वीर

(एक गहरा सच: पंक्तियों के दरम्यान)
मुक्तिबोध ने कला के ‘तीसरे क्षण’ में जिन तीन क्षणों की बात की है वो सृजन के बीज सूत्र हैं। मुक्तिबोध लिखते हैं, “कला का पहला क्षण है जीवन का उत्कट तीव्र अनुभव-क्षण। दूसरा क्षण है इस अनुभव का अपने कसकते- दुखते हुए मूलों से पृथक हो जाना और एक ऐसी फैंटेसी का रूप धारण कर लेना मानो वह फैंटेसी अपनी आँखों के सामने खड़ी हो। तीसरा और अंतिम क्षण है इस फैंटेसी के शब्द बद्ध होने की प्रक्रिया का आरम्भ और उस प्रक्रिया की परिपूर्ण अवस्था तक की गतिमानता। शब्द बद्ध होने की प्रक्रिया के भीतर जो प्रवाह बहता रहता है वह समस्त व्यक्तित्व और जीवन का प्रवाह होता है। फैंटेसी को शब्द-बद्ध करने की प्रक्रिया के दौरान जो-जो सृजन होता है- जिसके कारण कृति क्रमश: विकसित होती जाती है- वही कला का तीसरा और अंतिम क्षण है।”
कला के पहले क्षण के लिए सबसे अनिवार्य घटक सम्वेदनशील, सहृदय, सचेतन मनुष्य है। कोई भी घटना, प्रकरण, रोजमर्रा के जीवन में टकराने वाले पात्र व चरित्र हर व्यक्ति पर अलग-अलग प्रभाव डालते हैं। उस प्रभाव का बल (इंटेंसिटी) व्यक्ति दर व्यक्ति निर्भर करता है। कलाकार होने की पहली शर्त है, समय के साथ अपने परिवेश से उसका तादात्मीयकरण व उससे उत्पन्न उत्कट अनुभूति। भले ही इस अनुभूति का प्रस्फुटन कला के किसी फॉर्म में हो अथवा न हो किन्तु इतना तय है कि इसके अभाव में कला का कोई भी फॉर्म कला की श्रेणी में नहीं आएगा । सृजन में जीवन का संचार इसी से सम्भव है। कला का दूसरा क्षण सृजन की रचनात्मकता से जुड़ा है। इसके कारण ही कोई रचना व्यक्ति (लेखक) की निजी अनुभूति से होते हुए, निज की सीमाओं को तोड़कर समाज/देश/दुनिया के हर व्यक्ति की अनुभूति बन जाती है, जहाँ व्यक्ति ही नहीं देश और काल की सीमाएं भी ध्वस्त हो जाती हैं। और तीसरा क्षण रचना का सृजन प्रक्रिया से गुजरते हुए अपनी परिणति तक पहुंचने का है।
मुक्तिबोध का उपरोक्त सृजन के सन्दर्भ में दिया गया बीज सूत्र किसी भी रचना के अनुभूत रस व उसकी आलोचकीय समझ के लिए बेहद ज़रूरी है। साठ के दशक में ‘वसुधा’ में प्रकशित हुए मुक्तिबोध की डायरी के हिस्से में दर्ज़ व बाद में ‘एक साहित्यिक की डायरी’ के नाम से प्रकाशित उपर्युक्त परिभाषा सृजन से जुड़ा सर्वाधिक सुचिंतित व अनुभवपगा आत्मकथन है। इसे कालातीत कथन कहा जा सकता है। जिसके परिप्रेक्ष्य में हम आज भी उन रचनाकारों के सृजन के न सिर्फ़ सूत्रों को खोज सकते हैं, बल्कि आलोचकीय आलोक में रचना और उसकी रचनाधर्मिता को भी समझ सकते हैं, जिनका लेखन समय की सीमाओं को तोड़ते हुए हमारे समय को ख़ास तरह से दर्ज़ कर रहा है।
21 वीं सदी के दूसरे शतक के झरते हुए वर्ष, अगस्त 2020, में यदि नई सदी के पिछले दो दशकों की ओर देखें तो हिन्दी कहानी के क्षेत्र में मात्रात्मक रूप से हुई अपार वृद्धि एक साथ हर्ष मिश्रित चौंकाने वाली व आशंकित करने वाली है। आशंका है ‘बल्क’ में लिखे जाने वाले साहित्य की गुणवत्ता की। क्या ये साहित्य साहित्य कहलाने लायक आधारभूत गुणधर्मिता से युक्त परिपक्व साहित्य है या फिर जिसकी ओर पिछले कुछ समय से आलोचक वैभव सिंह संकेत करते आ रहे हैं साहित्य के ‘कमोडिटी’ में तब्दील कर दिये जाने के, उस दिशा में अग्रसर है? निश्चित तौर पर साहित्य की सत्ता तभी बची रहेगी जब साहित्यिक रचनाधर्मिता की ख़ास शैली के साथ-साथ रचनाकार की समाज व जीवन के प्रति गहरी अनुभूति,तादात्मीयकरण, महती सम्वेदनाएं व विवेकी दृष्टि जुड़ी होगी। नहीं तो अन्तत: व उम्मीदन समय के साथ बड़ी मात्रा में ‘थोथा’ उड़ा देने पर हमारे पास धरोहर के रूप में एक ऐसा साहित्य ही बचा रह जाएगा जिसके आईने से आने वाली पीढ़ी इस दौर के बरअक्स अपने समय को देख सकेगी।
कुछ सार्थक बचे/बचाए रहने की उम्मीद में वरिष्ठ पत्रकार व कथाकार राकेश तिवारी के कथा साहित्य को भी देखा जाना चाहिए। उनके लेखन की ताकत उनके व्यक्तित्व में मौजूद निर्भीक दृढ़ विचारधारा से युक्त पत्रकार व सम्वेदनशील साहित्यकार की मिली जुली शख्सियत है। ऐसी शख्सियतों के धारदार लेखन के चुनिन्दा उदाहरण साहित्य के आधुनिक काल से लेकर अब तक हम देख सकते हैं। इस दौर में ‘अनिल यादव’ का कथा साहित्य भी इसकी शानदार मिसाल है, हालांकि तुलना करना यहाँ उद्देश्य नहीं। फिर भी यदि आज के दौर में पत्रकार-साहित्यकारों की कहानियों/उपन्यासों को देखें तो इतना निश्चित है कि अनुभव क्षेत्र के व्यापक होने पर, चमकदार भाषा व अन्य तमाम युक्तियों के होने पर भी रचना को ‘रचना’ बनाने वाले ‘बेसिक सब्सटेंस’ के अभाव में अधिकांश का लेखन कमज़ोर ही साबित हुआ। राकेश जी के लेखन की तुर्शी, सामाजिक-राजनैतिक-आर्थिक सम्बन्धों के समीकरण और उनके प्रतिफलन को समझ पाने योग्य दूरदर्शिता, पूँजी और सत्ता के चालाक खेलों को चिह्नित कर पाने की बारीक दृष्टि, निकट भविष्य के संकटों/साजिशों को भाँप लेने की क्षमता व विवेक, शोषित तबके (विशेष तौर पर लैंगीय मुद्दों) के प्रति गहरी सम्वेदनशीलता,विषयविविधता और व्यापक रेंज उनके लेखन को कहानी साहित्य में अलग से चिह्नित करते हैं।
राकेश जी के पास कहानी कहने की अद्भुत क्षमता है। वो कोई भी विषय लें, उसे बड़े धैर्य के साथ बरतते हैं। कहानी अपने आप आगे बढ़ती चलती है, बिना किसी तयशुदा अन्त अथवा निष्कर्ष के। इसी वजह से उनकी कहानियाँ अपने पूरे फ्रेम में अत्यंत सजीव हो उठती हैं। मौज़ूदा समय की विद्रूप तस्वीर को खींचने का उनके पास सबसे कारगर हथियार है उनकी गहरी व्यंग्यात्मक भाषा और उसमें भी बहुस्तरीय, बहुअर्थीय जटिल फैंटेसी का प्रयोग। उन्होंने जिन कहानियों में इस युक्ति का प्रयोग किया है, उन रचनाओं के गहरे मायने कदाचित एकाधिक पाठ से ही सम्भव हो सकें, हालंकि तब भी नए अर्थ संधान की गुंजायश बनी रहती है। जिन रचनाओं में उन्होंने फैंटेसी का प्रयोग किया है, वे रचनाएं अपेक्षाकृत आकार में लम्बी व सांद्र हैं। ऐसी अविस्मरणीय रचनाओं में उपन्यास ‘फसक’, व कहानियों में ‘मुकुटधारी चूहा’, ‘मुर्गीखाने की औरतें’, ‘मंगत की खोपड़ी में स्वप्न का विकास’ का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। फैंटेसी सर्जनात्मक साहित्य का चरम उत्कर्ष है जो अपना जीवन और प्रवाह सर्जक के जीवनानुभव से लेती हुई आगे बढती है। रचनाकार का अनुभव, उसकी चेतना और उसकी भाषा की व्यंजना शक्ति जितनी प्रबल होगी ‘फैंटेसी’ उतनी ही दूरगामी व अनिश्चित होगी। सृजन की प्रक्रिया की तह तक जाने के लिए, उनके अनुभव से गुजरना सत्य की खोज की तरह है। उपरोक्त चारों रचनाएँ इसी सन्दर्भ में देखी-समझी जा सकती हैं।
राकेश जी को थिएटर का अनुभव भी रहा है। शायद अन्य वजहों में यह भी एक वज़ह है कि उनकी कहानियों को पढ़ते हुए पाठक अनायास अपने आपको किसी थिएटर अथवा बड़े पर्दे के दर्शक के रूप में महसूस करता है। कहानी की किस्सागोई व उसका रचनात्मक विधान उसे श्रव्य जगत से दृश्य जगत तक ले आता है। ये एहसास कम रोचक नहीं है। इसका सम्मोहन व प्रभावान्विति राकेश जी की कहानियों के उस बड़े पाठक समूह से समझी जा सकती है,जो कहानी में अक्सर कहानीपन की बात करते हैं और जिन्हें ‘कहानीरस’ इन कहानियों में आकर ही मिलता है।
उनकी अब तक चालीस से अधिक कहानियाँ व एक उपन्यास प्रकाशित हो चुका है। उनके प्रकाशित साहित्य में अब तक तीन कहानी संग्रह ‘उसने भी देखा’, ‘मुकुटधारी चूहा’, ‘चिट्टी जनानियाँ’, एक उपन्यास ‘फसक’, एक बाल उपन्यास ‘तोता उड़’, एक बाल कथा संग्रह ‘थोड़ा निकला भी करो’, पत्रकारिता के क्षेत्र में ‘पत्रकारिता की खुरदरी ज़मीन’ शामिल हैं, और इसके अलावा आगे के लेखन का सफ़र निरंतर जारी है।
राकेश जी का कहानी लेखन से वास्ता बेहद पुराना है। उनकी पहली कहानी आज से लगभग 40 वर्ष पूर्व प्रकाशित हुई, जब वो किशोरावस्था में थे। कई बार अन्तराल लम्बा रहा, हालांकि ये किसी लेखक के लेखन के अच्छे या ख़राब होने की कसौटी नहीं किंतु राकेश जी की कहानियो के लिए कह सकते हैं कि समय के साथ अनुभवपगा लेखन और परिपक्व होता गया। ‘धर्मयुग’, ‘सारिका’, ‘रविवार’ जैसे अपने समय के सर्वाधिक प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हुए उनका पहला कहानी संग्रह ‘उसने भी देखा’ आया और उसके इक्कीस साल बाद उनका दूसरा कहानी संग्रह 2014 में ‘मुकुटधारी चूहा’। इस संग्रह में कुल ७ कहानियाँ हैं। जिनमें 3 कहानियाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, ‘मुकुटधारी चूहा’, ‘मुर्गीखाने की औरतें’ और ‘कठपुतली थक गयी’। इन तीनों कहानियों की सबसे ख़ास बात मौज़ूदा समय की विद्रूप तस्वीर को पेश करने के लिए ख़ास तरह की प्रतीकात्मक भाषा और फैंटेसी का प्रयोग। उपरोक्त उल्लिखित कहानियों में से पहली दो कहानियाँ ख़ासतौर पर इस तरह की शानदार प्रस्तुति हैं।
जुलाई 2014 में ‘कथादेश’ पत्रिका में प्रकाशित ‘मुकुटधारी चूहा’ उनकी बाकी कहानियों के बरअक्स लम्बी कहानी है। 27 पृष्ठ के वितान में फैली यह कहानी अपने शानदार कथ्य, चुस्त संरचना व इस दौर के सबसे खतरनाक संकट के आगाज़ के बेहतरीन अंदाज़ के कारण अविस्मरणीय कहानी है। कैसे एक बेहद मामूली घटना को, जो बच्चों की नासमझी भरे खेल में घटित हुई, फिरकापरस्तों द्वारा संगठित तौर पर, कस्बे से निकालकर उसे केन्द्रीय स्तर की चिंता बनाकर, सांप्रदायिक रंग में रंगने की पुरजोर उच्च स्तरीय कोशिशें की जाती है, ये खेल देखना बड़ा दिलचस्प है। दरअसल ये नव उदारवादी दौर की क्रूर, अति मह्त्वाकांक्षी सत्ता, आवारापूँजी और अपराध जगत के गठजोड़ के खतरनाक समय के अभूतपूर्व, अविश्वसनीय लगभग असम्भव सी लगने वाली घटनाओं के अन्तहीन खूनी दौर के शुरू होने की कहानी है।
उत्तर प्रदेश के एक छोटे कस्बे ऊधमगंज में आ बसे कामगार निम्न वर्गीय परिवार का बच्चा मुक्की अर्थात मुकेश और उसके चार दोस्तों द्वारा एक चूहे की खेल-खेल में हुई मौत, और उन बच्चों द्वारा उसे उछाले जाने पर घंटियों वाले अहाते में गिरना, आम दिनों में आम आदमी के लिए बेहद मामूली सी लगने वाली घटना थी, किन्तु ये ‘आम दिन’ कहाँ थे, ये ‘ख़ास दिन’ थे, ‘अच्छे दिन’ आने वाले थे, लेखक को इसका आभास था, जहाँ ‘चूहा’ जैसा छोटा सा जीव अपने विकराल रूप (आशय) में आकर मुक्की जैसों की ज़िन्दगी तबाह कर सकता था। 10 वीं का रिजल्ट भी बच्चे को नसीब न हुआ और उसे बदहवासी के हालात में अपने पिता,माँ बहन के प्यार और साए से महरूम होना पड़ा। जैसे-जैसे चूहे की मौत एक धर्म विशेष के ध्वज वाहकों के लिए बड़ा मुद्दा बन रही थी, वैसे-वैसे मुक्की के लिए अदना सा चूहा विशालकाय रूप में उसके जीवन में प्रवेश कर उसके जीवन के लिए सबसे बड़ा आतंक बनता जा रहा था। अपने कस्बे को छोड़ कर वह पहाड़ के किसी कस्बे में एक ढाबे के मालिक के पास दीन-हीन अवस्था में शरण पाता है, लेकिन मूषक रक्षकों का दल अब कस्बे की चौहद्दी को तोड़ देश की सीमाएं नाप रहा है। उन्हें तलाश है मूषक हत्यारे की, वो चेहरा नहीं पहचानते, हिंसक भीड़ नारे लगाती घूम रही है, ‘जिसने मारा मूसक राज, कोढ़ में उसके फूटे खाज।’ ‘मूषक राज को जिसने मारा, पकड़ के लाओ वो हत्यारा’। ये भीड़ खून की प्यासी है, मुक्की का मूषक भय उसके सर चढ़कर बोल रहा है। अबकी बार मुक्की वहाँ से भागकर दिल्ली की शरण लेता है। किन्तु इतने बड़े शहर में आना भी उसके लिए एक सदमे की तरह है। एक खूबसूरत फ़रेब।
एक घटना उसे एक ऐसे स्वप्नलोक में ला छोड़ती है जिसमें सब कुछ मुक्की के लिए एक खूबसूरत रहस्य की तरह है। रूप,रस,गंध की एक अद्भुत मायानगरी। एक दयालु शरण देने वाली उच्चवर्गीय स्त्री, जिसकी करुणा के प्रवाह में मुक्की अपनी माँ को देखना चाहता है किन्तु देख नहीं पाता। मुक्की की समझ का दायरा उसके परिवेश, वर्ग, उम्र के कारण सीमित है। उसके जीवन में चल रहे अभी तक के गेम में अब एक नए दुश्चक्र का प्रवेश है, जिसे मुक्की थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करके भी समझ पाने में असमर्थ है, “उस स्त्री की बड़ी-बड़ी आँखें झील में भटकती कश्तियों की तरह थीं। उन आँखों में आकर्षण के अलावा भी कुछ था। क्या था , यह समझना बड़ा मुश्किल था। उन पनीली आँखों में अथाह गहराई थी और उसे नापे बिना उस ‘अलावा’ को पहचानना लगभग असम्भव था।” (मुकुटधारी चूहा, राकेश तिवारी)
ये सम्भ्रांत स्त्री खूबसूरती, अभिजात्य और दयालु स्वभाव की प्रतिमूर्ति है, किन्तु एकाकीपन की शिकार है। उम्र चालीस के आस-पास है। इकलौती बेटी बाहर रहकर पढ़ रही है और पति अपने बिजनेस के कामों में बेतरह मशगूल है। खाने की टेबल पर भी काम। अक्सर घर से बाहर रहता और जब घर में भी होता तो भी पति-पत्नी में सम्वाद का कोई सूत्र न होता। ऐसे सम्बन्ध मुक्की की समझ के बाहर हैं। स्त्री अपना अकेलापन प्राय: सहेलियों के साथ मंहगे होटलों की पार्टियों, शॉपिंग में दूर करने का प्रयास करती। किन्तु कभी-कभी के लिए ही ये बहलावे और छलावे काम आ सकते थे। साथ-सम्पर्क की उसकी जरूरत सिर्फ़ रूहानी नहीं ज़िस्मानी भी है। मुक्की की ओर उसकी करुणा सिर्फ़ यूँ हीं नहीं उसकी ओर आकर्षण भी है। बमुश्किल 16 वर्ष का लड़का स्त्री के लिए सिर्फ़ भावनात्मक रूप से अकेलेपन का सहारा नहीं, शारीरिक ज़रूरत को भी पूरा करने का ज़रिया है। स्त्री द्वारा गाहे-बगाहे मुक्की को छूना, उसे आलिंगन में भरना आदि कई ऐसे अवसर उसके लिए एक अबूझ पहेली की तरह है। कहानी के अन्त में ‘भली स्त्री’ मुक्की को अपने जादुई पाश में ले, उससे पहले फिर से मूषक राज का प्रवेश होता है। चूहे की मौत के बाद मूषक राजा की स्तुति में पैम्फलेट और किताबें छपी हैं, चुनाव आने वाले हैं, दिल्ली की ज़िम्मेदारी स्त्री के बिजनेसमैन पति पर है क्योंकि पार्टियों के लिए पैसा खर्च करना इन्वेस्टमेंट की तरह है। एक बेहद मदहोस करने वाले समय में स्त्री का प्रकाशक को किताबों के लिए कन्फर्मेशन, मुक्की के सामने ऐसे समय में मूषक राजा का ज़िक्र, जब उसे लगने लगता है कि वो उस सदमे से आगे बढ़ चुका है, उसे विक्षिप्त बनाने लगता है। उसे ये सब अब एक खतरनाक जाल की तरह लगने लगता है, जिसमें वह ‘भली स्त्री’ भी शामिल है। स्त्री का उससे शारीरिक सम्बन्ध बनाने के उद्देश्य और उपक्रम में की गयी सारी उसकी हसीन कोशिशें मुक्की को ‘पूतना का छल’ लगता है। इन मिथकों को सच मानने वाला मुक्की अन्तत: बदहवासी में वहाँ से ये कहकर भाग उठता है कि, “उसे मैंने मारा …..लेकिन पूतना मुझे नहीं मार सकती…मैं दूध नहीं पियूंगा…पूतना के हाथ नहीं आऊँगा।” … ‘बाहर निकलकर वह बेतहाशा दौड़ने लगा। वह दौड़ता रहा…उसे लग रहा था कि कोई विशालकाय चूहा उसके पीछे पड़ा है। उसने मुकुट पहना है और उसका एक दांत मुक्की की पीठ में या पिछवाड़े में घुसना मानो तय है…लेकिन नशे और गुस्से के बावजूद उसे इस बात का मलाल है कि छह महीने का वेतन डूब गया।’ इन बदहवास स्थितियों में मुक्की को अपना मेहनताना याद है, यह उसकी पीड़ा का भी बयान है। इस का उद्देश्य वर्गगत कटु सत्य और पीड़ा को तो लाना है ही साथ ही ये भी पाठकों तक सम्प्रेषित करने की कोशिश है कि मुक्की पूरी तरह अभी पागल नहीं हुआ। नहीं तो व्यवस्था ने कोई कसर नहीं छोड़ी।
प्रायोजित आतंक ने एक अदने से जीव चूहे को ‘मुकुटधारी चूहा’ में तब्दील कर सामान्य, सचेत व्यक्ति के जीवन की बेहद मामूली खुशियों और हकों को भी निगल लिया, ये वही दौर था जब जगह-जगह गौ कथाएँ हो रहीं थीं … और उसके बाद गौ के नाम पर जो हुआ, जिससे देश बखूबी वाकिफ़ है, उसका आगाज़/ चेतावनी इस कहानी में है। छल चहुँतरफ़ा है। व्यक्ति का जीवन और उसकी चेतना दांव पर है। इस कहानी के घटना क्रम अतीत और वर्तमान दोनों स्तरों पर चलते हैं। जिन्हें बड़े कौशल से संगुम्फित किया गया है ताकि सहजता व लयात्मकता बनी रहे। गहरे व गम्भीर अर्थ वाली प्रतीकात्मक व व्यंजनात्मक भाषा में बंधी यह कहानी छोटे-छोटे पैराग्राफ में अपनी गढ़न व कहन में हमारे दौर के दस्तावेज़ की तरह है।
इस संग्रह की एक अन्य कहानी का ज़िक्र ज़रूरी है; ‘मुर्गीखाने की औरतें’। यह कहानी अपनी दो ख़ास वज़हों से पाठकों को ठहरने पर मजबूर करती है; एक शानदार रूपक में गढ़ी फंतासी शैली व तीखी व्यंग्यात्मक भाषा वाली इसकी संरचना के लिए, दूसरे कहानी में उठाए गये मुद्दे के लिए। कहानी के मूल में सत्य घटना प्रेरित विचार ‘Honour killing’ का है (बकौल राकेश तिवारी जी)। स्त्रियों को वस्तु मानकर अपनी इज़्ज़त रूप में सम्पत्ति मानने वाली सामंतवादी सोच ने स्त्रियो की स्थिति दड़बे में बन्द मुर्गियों की सी कर दी है। उनके शरीर के साथ उनके दिमाग व आवाज़ भी बंद हैं। भारत की न जाने ऐसी कितनी स्त्रियाँ होंगी, उनकी ऐसी दुखद स्थिति को मुर्गी के रूप में ‘कुक-कुक’ करती स्त्रियो के रूप में ऐसे अद्भुत रूपक में ढालना जितना कमाल का है उतना ही कहानी का एक बेहद संगीन मुद्दे पर तीखी व्यंग्यात्मक भाषा में बर्ताव। ये व्यंग्यात्मक व चित्रात्मक शैली मनोहर श्याम जोशी की याद दिला जाती है। ये राकेश जी के लेखन की ख़ासियत है कि वो गम्भीर से गम्भीर विषयों को बोझिल व भारी नहीं होने देते।
कहानी एक ऐसे नामर्दों के मर्दवादी शापित गाँव की है जहाँ उन के वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक ठेके (किराए)के ‘मर्द’ की ज़रुरत है। ये किराए का मर्द है ‘रबिया’। इस गांव के सभी मर्द, जो अब नामर्द हो चुके हैं, गहरे आलस्य ,थकान, और उम्र से पह्ले आयु के पक जाने के शिकार हैं। वे अपनी समस्याएं जानते हैं किंतु मानते नहीं। आख़िर अपनी कमज़ोरियों को जो स्वीकार कर ले वो मर्द कैसा! उनकी लस्त-पस्त हालत और उस पर मर्दानगी की ठसक कमाल की है। “ मूंछे खड़ी और झुकी नज़रें– “उनकी पिंडलियों में लगातार दर्द रहता था। मांसपेशियाँ शिथिल पड़ गईं थीं। हर वक्त थकान महसूस होती।।।रीढ़ ने झुकने और टांगों ने लंगड़ाने की आदत बना ली थी।।।।औरतों की सुन्दरता देख कर तूफ़ान उठता और फिस्स कर जाता। नज़रें झुकी-झुकी रहतीं।।।।कुछ लोग तो कई वर्षों से इस तरह की शिकायत कर रहे थे। लेकिन पिछले एक दो वर्षों में एक-एक कर गाँव के सारे मर्द पस्त हो गये।।।इस खोखलेपन का कोई संदेश बाहर न जा पाए इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा था। गाँव के सम्मान का प्रश्न था। (मुर्गीखाने की औरतें, राकेश तिवारी)
गाँव के सम्मान और खुद के सम्मान के लिए वे खुल कर न बोलते थे, और स्वीकार करने का तो प्रश्न ही न बनता था। बल्कि इसके उलट वे यह स्पष्ट तौर कहने व मानने लगे कि गाँव की औरतें बाँझ हैं। सन्तान न पैदा होने पर गांव के पुरुषों ने दूसरी शादियाँ भी कर लीं। तब भी औरतों ने न कभी सवाल किया न शक । गांव में औरतों की इज़्ज़त दो कौड़ी की रह गयी थी। मर्द उन्हें दुत्कारते। दिन-रात ताने मारते। खेतों में काम कराते। घर की औरतों को बुलाने के लिए चपरासी बुलाने वाली घंटी का इस्तेमाल करते। ‘हालांकि मर्दों की आवाज़ में धमक नहीं रह गयी थी। वे स्वर को मद्धम से ऊपर खींच नहीं पाते थे…। फिर एक दिन सब कुछ उलट गया। मर्द मूछें मरोड़ने को हाथ उठाएं तो हाथ लूला हो जाए। वे झेंप मिटाने के लिए ज्यादा तन कर चलने की कोशिश करें, लेकिन रीढ़ झुक जाए और पसलियाँ कड़-कड़ करने लगें।” मज़े की बात ये कि ‘इस सबके बावज़ूद औरतों के मुँह प्रेशर कुकर की तरह बंद थे। उनसे खुशी के मौकों पर सीटी जैसे गीत फूटते, गम में लयबद्ध दहाड़ें निकलतीं। खाते-पीते वक्त मुंह ढाई इंच तक खुल जाते। बाक़ी मौक़ों पर, कोई वाल्व था जो गले में डाट की तरह लग जाता। मुंह खुलता ज़रूर था, पर जम्हाई लेकर बंद हो जाता। अगर दम लगाकर अंदर की गैस निकालना चाहें तो मुंह से मुर्गियों की तरह ‘कुक-कुक’ निकलती। वह बोली आज तक कोई मर्द समझ नहीं पाया था। पता नहीं डर की भाषा थी, या वे मर्दों को कोसती थीं।’
जब उस गाँव की स्त्रियों को बाँझ घोषित किया गया, जबकि उनके पति नपुंसक थे, उस गाँव की स्त्रियाँ क्या सोचती थीं, और तब भी जब उनके संतानोत्पत्ति के लिए आँख में पट्टी बाँधकर किराए के मर्द ‘रबिया’ से सम्बन्ध बनवाए गये। स्त्रियों की मर्ज़ी-नामर्जी का प्रश्न ही नहीं उठता। दरअसल ये स्त्रियाँ मनुष्य योनि में मुर्गियाँ हैं। लेखक ने संकेत भर किया कि पता नहीं संसर्ग के समय उन्हें समझ आया कि नहीं कि वे अपने पति के साथ हैं या किसी अन्य पुरुष के साथ। हालांकि लेखक भी ये जानते होंगे कि स्त्रियों को ये समझ न आया हो ऐसा संभव नहीं। ऐसे कई प्रसंगों बल्कि पूरी कहानी में ही ‘स्त्रियाँ क्या सोचती थीं’, इस दिशा में वो गये ही नहीं। और ऐसा करके उन्होंने अच्छा कदम उठाया। प्रसंग व परिस्थितियों के अनुरूप उन्होंने घटनाएँ रचीं, जहाँ स्त्रियाँ ‘वस्तु’ हैं, कहानी व जिस समय का वो सच बयाँ कर रहे हैं, उस माँग के अनुसार, ‘वो क्या सोचती या महसूस करती हैं’ इस ओर जाने से कहानी का बल दूसरी ओर चला जाता, इस प्रकार दूसरी तरतीब से उन्होंने बिना स्त्री विमर्श के घोषित कहानी के स्त्रियों के प्रति निःसंग सी प्रतीत होने वाली अघोषित शानदार स्त्री पक्ष की कहानी रची है।
मर्दों के छल पर ऐसे ही पर्दा पड़ा रहता यदि गांव की एक स्त्री फुल्लो की कोख, प्रेम में अपनी तड़प का वास्ता देते, शादी से पहले के अपने एक पूर्व प्रेमी द्वारा न भर दी गयी होती। अपने आप को गांव की अन्य औरतों की तरह बांझ समझती, व ‘ईश्वर और मर्द कभी झूठ नहीं बोलते’ मानने वाली फुल्लो ने ‘आसमान की तरफ देख कर गले की डाट खोली तो उथल-पुथल मच गयी’। पंच कान में रुई डालकर आरोपी की सफाई सुनते रहे, पर वे संतुष्ट न हुए , फुल्लो चीखी फिर शेरनी की तरह दहाड़ी और दहाड़ती रही, वह कहना चाह्ती थी कि औरतें बांझ नहीं बल्कि मर्द नामर्द हैं। ये सुनना पंचो और पुरुषों के लिए बिल्कुल न काबिल ए बर्दाश्त था। ‘सुन कर पंच हत्थे से उखड़ गये।।किंतु आरोप तो पहले ही तय हो चुका था, फैसला अडिग था। फुल्लो कसूरवार थी। उसकी सज़ा मुकर्रर हुई कि बारी-बारी उसके मुंह पर थूका जाए.. ‘पहला हक माखन (उसका पति) का था … लोग गुस्से में ढेर सारा थूक मुंह के अंदर जमा करते और फुल्लो के मुंह पर थूक की पिचकारी मार देते। उनके चेहरों पर गहरा संतोष दिखाई पड़ता। विडम्बना देखिए मर्द तो मर्द, औरतें भी पीछे नहीं रहीं…. लेकिन उस औरत का जीवट देखिए, जितनी बार कोई मर्द थूकता , वह दहाड़ती – ‘हट! साल्ले नामरद।’ इन परिस्थितियों में फुल्लो का इससे बड़ा शायद ही कोई प्रतिकार अथवा प्रतिशोध हो सकता था, मर्दों की उस कमज़ोर नब्ज़ पर वार जो उनकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमज़ोरी थी।
फुल्लो पर थूकने वालों में औरतें भी शामिल थीं, जो अपने मर्दों के दिमाग से चालित थीं। वे सन्न थीं किंतु अभी भी चुप थीं – ‘उनका मन शोकगीत गाने का हो रहा था किंतु मुंह जम्हाई लेकर रह गया। ‘इस घटना ने गांव के पुरुषों के मन में एक अज़ीब खुटक ज़रूर पैदा कर दी, अपनी मर्दानगी को लेकर बढ़ती उनकी चिंता ने गांव में मरघट सा सन्नाटा भर दिया। फुल्लो ने उसी रात बरगद के पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली।
‘रबिया’ गाँव की सारे नियम शर्तों को मानता कुछ वर्षों तक चुपचाप तटस्थ भाव से अपना काम करता रहा। किन्तु अफ़सोस ये शापित गाँव.. रबिया भी जल्द ही उन्हीं की पंक्ति में खड़ा हो गया। अब वो किसी काम का नहीं। जिस काम में उसने इन मर्दों की मदद की अब वही काम उसे अपने गले के लिए फांसी का फंदा बनता दिख रहा है। उसे एक ही शर्त पर अपनी जान छूटती दिखती है कि वह उन्हें अपने जैसा ही एक बंधुआ मर्द लाकर दे। मरता क्या न करता … रबिया को आख़िर एक शहरी युवक ‘प्रेम’ मिल ही जाता है। नाम भी प्रतीकात्मक। प्रेम ‘प्रेम’ की बयार लेकर गाँव आया और इस बयार में गाँव के सरपंच डोरीलाल की बहू मीना को अपने साथ उड़ा ले गया। मीना के साथ यह सम्भव इसलिए भी हो सका क्योंकि वह अन्य औरतों की तरह ‘कुक-कुक’ नहीं करती और ‘तुर-तुर’ नहीं भागती थी।
लाख न चाहते हुए भी, भूत-प्रेत के कई झूठे किस्से गढ़ने के बावजूद गाँव वालों के सामने सच फुदकने गया। सबसे बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन मुर्गी रूपी औरतों में दिखने लगा, ‘ वे एक दूसरे के कानों में फुसफुस कर रहीं थीं। अचानक ही वे मिलकर गीत गाने लगीं… डोरीलाल चिल्ला रहे थे। उनकी आवाज़ में गाने के स्वर गडमड हो रहे थे। ऐसा लग रहा था औरतें हंस रहीं हैं।’ औरतों में पहली बार मुर्गियों से स्त्री में बदलने के कुछ गुण प्रकट हुए। पूरे गाँव के ऊपर बदनामी का खतरा चील की तरह मंडरा रहा है, डोरीलाल गुस्से में पागल हुए जा रहे हैं। वो रबिया और प्रेम को जान से मरवा देने के लिए उतावले हैं। उन्हें ढूँढने के लिए उनके लठैत अपने हथियारों के साथ निकल चुके हैं। डोरीलाल के करीबी सलाहकार मुक्कान की वज़ह से ही रबिया को पहले छोड़ दिया गया था और उसकी जगह प्रेम को भी लाया गया था। मुक्कान प्रेम द्वारा सिखाए पाठ के अनुसार दबी ज़बान में नपुंसकता के इलाज़ की भी बात करता है। किन्तु डोरीलाल जैसे पुराने ख्याल के व्यक्ति के लिए इससे अधिक शर्म से डूब मरने वाली बात क्या होगी! किन्तु हवा की दिशा अब बदल चुकी है। नई पीढ़ी के लड़के के प्रतीक रूप में मुक्कान और सरपंच डोरीलाल का बेटा प्रेम और मीना को ढूंढ कर मारने के बजाय गाड़ी का रास्ता शहर की ओर ले लेते हैं ताकि वहाँ जाकर अपना इलाज करा सकें। अन्तत: एक दहशतशुदा खूनी सामन्ती प्रथा कम से कम कहानी में एक नयी आशा की किरण दिखाती हुई ख़त्म होती है।
एक लेखक की पक्षधरता हमेशा समाज के शोषित वर्ग के प्रति होती है। साहित्य में बात ‘स्वानुभूति’ की तो जा सकती है किन्तु ‘साहित्य में सहानुभूति’ मेरी समझ में एक अनुचित टर्म है। वो साहित्य जो सिर्फ ‘सिम्पैथी’ के कारण फलीभूत हो सका हो, उसकी जबरन वाली गढ़न चुभेगी, जबकि उसकी जगह वहाँ ‘एम्पैथी’ की यानी ‘परानुभूति’ की बात की जानी चाहिए। राकेश जी जब अपनी कहनियों में ‘जेंडर इशूज़’ लेकर आते हैं, तब यही ‘परानुभूति’ साफ़ महसूस की जा सकती है। वैसे तो उनकी तकरीबन हर कहानी में आए स्त्री पात्र इस दृष्टि से समझें जा सकते हैं किन्तु ‘मुर्गीखाने की औरतें’, ‘चिट्टी ज़नानियाँ’, ‘छन्ने की लौंडिया गुनगुनाती हैं’, ‘मुचि गयी लड़कियाँ’ व ‘खतरनाक’ इस सन्दर्भ में विशेष रूप से देखी जानी चाहिए। नामवर जी राकेश जी की कहानियों में आए स्त्री पात्रों के विषय में कहते हैं, ‘ उनकी कहानियों में स्त्रियों का जो चरित्र आया है। उसमें स्त्रियों का आक्रोश सामने आया है। स्त्रियों का कड़ा संघर्ष है। उनकी तेजस्विता दिखाई देती है।’- (प्रो। नामवर सिंह, सबद निरंतर-दूरदर्शन)
स्त्रियों का संघर्ष, उनकी तेजस्विता का बेहतरीन उदाहरण उनकी कहानी ‘चिट्टी जनानियाँ’ है। यह सम्बोधन पहाड़ के अंचल में रहने वाली स्त्रियों के लिए है। पहाड़ के परिवेश पर आधारित यह कहानी वहाँ के एक ऐसे परिवार की चार चिट्टी ज़नानियों अर्थात गौर वर्णीय स्त्रियों की कहानी है, जिनके लिए इंसानी रिश्ते दुनिया की किसी भी शै से अधिक कीमती हैं। ये स्त्रियाँ अपने उसूलों पर जीती हैं, जिससे कोई लालच अथवा दबाव इन्हें डिगा नहीं सकता। ये बेहद दृढ़ व आत्मनिर्भर स्त्रियाँ है। इनके परिवार में अब कोई पुरुष नहीं।
नैरेटर दिल्ली से इस जगह प्रॉपर्टी खरीदने के उद्देश्य से आया है, जिसे दान सिंह (दलाल), जो इस परिवार को करीब से जानता है, के पास ले आता है। इन स्त्रियों को पैसों की ज़रुरत है जिसके चलते ये अपनी ज़मीन बेचना चाहती हैं। नैरेटर को ये बुतनुमा ‘चार सफेद ठंडी औरतें’ बेहद रहस्यमयी व काफ़ी हद तक डरावनी लगती हैं। दान सिंह कुछ दिन दिल्ली में नौकरी कर चुका है, वह शहरी प्रवृत्ति को थोड़ा बहुत समझता है और पहाड़ के लोगों को तो समझता ही है, इसीलिए वह पहले से ही नैरेटर को कम से कम बोलने और न हँसने की हिदायत दे देता है। इन स्त्रियों में एक बृद्धा, उसकी बहू और उसकी दो पोतियाँ हैं । परिवार की सबसे बड़ी स्त्री का एक नैरेशन देखिए, ‘जिसके गले में पट्टा (सरवाइकल कॉलर) और एक हाथ में प्लास्टर बंधा था, धीरे-धीरे कदम बढ़ाती हुई पर्दे के पीछे से अवतरित हुई और नब्बे के अंश पर देखती हुई आगे बढ़ती चली आयी। वह सफ़ेदी की चलती फिरती दीवार लगती थी। …वह गर्दन नहीं हिला रही थी। शायद उसने मुझे देखा भी नहीं। उसके आगे के दो दांत टूटे थे और बाल भुट्टे के बालों जैसे छितरे हुए थे। चेहरे पर इतनी झुर्रियाँ थीं जैसे बासी सेब हो। वे चारों हद से ज्यादा गोरी थीं। लेकिन रक्तहीन।’ ( चिट्टी ज़नानियाँ-राकेश तिवारी)
नैरेटर ने उस वज़ह पर तवज़्ज़ो नहीं दी जिसके कारण इस परिवार की बड़ी बेटी रूपा ने दिल्ली की अपनी नौकरी छोड़ दी। यहीं पर वो चूक गया। उसके लिए बेहद ग़ैरमामूली चीज़ इन ज़नानियों के लिए बेहद- बेहद अहम है, वो चीज़ है मानवीय रिश्तों की कद्र। प्रॉपर्टी का सौदा नैरेटर की इच्छानुसार पूरी तरह पटने को है। नैरेटर को जो स्त्रियाँ बुत जान पड़ती हैं, असली हृदय तो उनमें ही धड़कता है। इन ‘बुतों’ के रक्तहीन चेहरों, ‘पागल’ व ‘खिसकी’ जान पड़ती बुढ़िया की अवस्था के पीछे की वजह उसके बेटे का गायब हो जाना है, जो दो साल पहले ऋषिकेश गया था, जिसके कपड़े नदी किनारे मिले थे, जिसके लिए बाकी लोग मानते हैं कि उसकी नदी में डूबकर मौत हो गयी या ये भी हो सकता है कि वो साधू हो गया हो। किन्तु माँ अर्थात बूढ़ी स्त्री इसे स्वीकार नहीं करती। उसे हर रोज अपने बेटे के आने की प्रतीक्षा है। जिसका मान और मन परिवार में बाकी अन्य तीन स्त्रियाँ अर्थात बहू और दोनों पोतियाँ पूरी शिद्दत से रखती हैं। वो अपने बगीचे की ज़मीन इसीलिए बेच रही हैं कि अपने घर को पड़ोसी के घर की तरह दुमंजिला बनवा लें ताकि उन्हें अपने बेटे की राह ताकने पड़ोसी के घर न जाना पड़े। घर के दुमंजिले की बालकनी पर बैठकर सड़क देख सकें। बेटे की राह ताकती बूढ़ी स्त्री की लाचारी और बदहाली की कहानी पर दोनों पोतियों की आँखें बार-बार डबडबा जातीं। ये वो स्त्रियाँ हैं जिन्हें ज़मीन के लिए ज़्यादा अच्छे पैसे की जगह अच्छे लोग चाहिए।
उनकी जमीन खरीदने वाला अच्छा इन्सान अर्थात नैरेटर पूरी तरह धार्मिक है, इस बात का ज़िक्र उन स्त्रियों पर कोई फर्क नहीं डालता। उन्हें उसके परिवार व पारिवारिक रिश्तों में ज्यादा रूचि है। नैरेटर द्वारा अपने तीन लोगों के परिवार का ज़िक्र, जिसमें माता-पिता शामिल नहीं, पिता अलग रहते हैं, माँ आती-जाती रहती हैं, माता-पिता को न अपने साथ रखना चाहते हैं न रहना चाहते हैं, पिता का तीन कमरों का फ़्लैट बिकवा कर उन्हें छोटे घर में शिफ्ट करा दिया और उन्हीं के पैसों से अपने लिए अलग घर खरीद लिया और उससे बाकी बचे पैसों से अब ये ज़मीन लेने आया है, ये सब बातें इन स्त्रियों को हत्थे से उखाड़ देती हैं। अपनी बात बताते हुए नैरेटर चालाकी से जिन बातों को छिपा रहा था, उसका यहाँ कोई मोल नहीं और जिन बातों को बेफिक्री से बता रहा था उसने उसके सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। और उन्होंने अपना फैसला सुना दिया कि ‘ज़मीन नहीं बेचनी’। नैरेटर के लिए यह किसी सदमे से कम न था, उसकी व दान सिंह की सारी कोशिशे बेकार गईं किन्तु वो अपने फैसले से नहीं डिगीं।
नैरेटर के लिए ये विषय हार का तो है ही उससे ज्यादा अबूझ पहेली। ‘मेढकमुखी’ ‘अंडबुद्धि’ लगने वाले चापलूस दान सिंह ने दिल्ली से आई पार्टी को पूरी तरह कन्वेंस करने की कोशिश कर ली कि ये ज़नानियाँ पागल हैं, और वो उसे इससे भी अच्छी डील दिला देगा किन्तु जीवन के कड़वे सच की एक गहरी फाँस नैरेटर के भीतर कहीं गहरे धंस गयी, इन ज़नानियों ने उसे आइना दिखाया था, ‘चारों चिट्टी ज़नानियाँ सफ़ेदी की तरह मेरे अंदर फ़ैल रहीं थीं। उसी सपने में या नीम बेहोशी में धीरे-धीरे मुझे लग रहा था कि यह जो उजली औरतें और उनकी सफ़ेदी मेरे अंदर पसर रही है, वह मुझे लोरी जैसा सुकून दे रही है, मुझे धीरे-धीरे चैन की नींद आने लगी है। शायद आ चुकी है। और इसी नींद में उदास व बीमार पिता जी मेरे सपने में प्रवेश कर रहे हैं। (हंस, फरवरी 2019 में प्रकाशित, चिट्टी ज़नानियाँ संग्रह में संग्रहित)
कहानी का रस उसके पूरे फैलाव में है, यदि निष्कर्ष अथवा निचोड़ की तरफ़ भागने की हडबड़ाहट की गयी तो उसके कहानीपन से हाथ धो बैठेंगे। छोटे से कथ्य वाली इस कहानी का ट्रीटमेंट इस तरह किया गया है कि उसे उसके हर पैराग्राफ और हर पंक्ति में पकड़ना ज़रूरी है । ये विशेषता नयी सदी की बेहतरीन कहानियों की भी है, कहानी इस तरह कही जाए कि कई बार हर पैराग्राफ अपने आप में एक मुक्कमल कहानी लगे, इस तरह की कहानियों में योगेन्द्र आहूजा व रवीन्द्र आरोही की कहानियाँ भी देखी जा सकती हैं।
कहानी शुरूवात से ही एक कौतूहल (कभी-कभी अंजाना सा भय), रोमांच और सिनेमा के कैमरे की आँख से देखे गये दृश्यबंधों में बंधी आगे बढ़ती है। गज़ब की सिनेमाटोग्राफिकल शैली, बेह्तरीन सेन्स ऑफ़ ह्यूमर व wit वाला कसा हुआ गद्य इस कहानी की अतिरिक्त विशेषता है।
राकेश जी की लैंगीय पक्षधरता व सम्वेदनशीलता का एक और उदाहरण उनकी कहानी ‘खतरनाक’ है। पुरुष का अहम और सर चढ़कर बोलता है यदि वो ‘पॉवरफुल’ भी हो। ‘पॉवर’ यदि सत्ता की हो तो क्या ही कहने! और उस सब पर कवि की कोमलता, सम्वेदनशीलता, व अभिजात्यपने का मुलम्मा। इन सारे मुखौटों से लैस एक स्त्रीखोर पुरुष, जो अपनी पत्नी को ही अपने व्यभिचार के किस्से सुनाता है। ऐसे ‘खतरनाक’ व्यक्ति की पत्नी या तो विद्रोह करती, या समझौता।। और यदि ये दोनों स्थितियाँ सम्भव न हों तो उसके पास मुक्ति का क्या रास्ता है? कदाचित कोई रास्ता न मिलने पर ही वह विक्षिप्त अवस्था में पहुंच सकती है, या फिर अंतिम रास्ता हत्या या आत्महत्या का है। जिसके संकेत कहानी के अन्त में दे दिये गये हैं। कहानी किसी निष्कर्ष तक न ले जाकर पाठकों को अपनी तरह से अन्त तय करने अथवा न करने के लिए छोड़ देती है। एक मनोचिकित्सक से काउंसलिंग सेशन में इस कहानी का केन्द्रीय पात्र अपनी मन: स्थति के अनुसार उलझी भाषा में अपनी बात और हालात का सिरा देती है। इस सिरे से जिस मूल तक पहुंचा जाता है, वह भीतर तक हिकारत से भर देता है। हालंकि कहानी में मनोचिकित्सक का चरित्र कन्वेंसिंग नहीं रहा। जिसका प्रोफेशन ऐसा हो, वो बेहद चतुराई से मनोरोगी के अनकहे को भी पकड़ लेता है, जबकि यहाँ मनोरोग से पीड़ित स्त्री को अपनी बात की गुत्थियों को खुद ही खोलना पड़ता है, कदाचित यह प्रयास पाठकों के समक्ष कहानी खोलने के लिए था, किन्तु इस प्रयास ने मनोचिकित्सक के पात्र को संदेहास्पद, किंचित हास्यास्पद व थोड़ा खीझ पैदा करने वाला बना दिया। इस तरह एक कहानी यादगार कहानी होने से रह गयी।
इसी वर्ष अर्थात 2020 में प्रकाशित ‘चिट्टी जनानियाँ’ संग्रह की अमूमन कहानियाँ वहशी व्यवस्था द्वारा आम आदमी के विक्षिप्त कर दिये जाने की क्रूरताओं का ज़िन्दा बयान हैं। इस संग्रह में कुल 10 कहानियाँ संग्रहित हैं। ये सभी कहानियाँ पिछले पाँच वर्षों में प्रकाशित हुईं हैं। इनके विषय भले ही समकालीन प्रतीत होते हैं, किन्तु वास्तविकता में इनका फैलाव समकालीन मुद्दों से होते हुए सर्वकालीन मुद्दों तक है। सत्ता व वर्चस्ववादी ताकतों का चरित्र नहीं बदलता। इन कहानियों में नोटबन्दी के कारण मध्य, निम्नमध्य वर्गीय व्यक्ति के टूटते-बिखरते सपनों की कराह (‘छन्ने की लौंडिया गुनगुनाती है’), धर्म-सत्ता-पूँजी के गठबन्धन से पैदा हुआ एक नए तरह का उन्माद तथा शब्द-सम्वेदना और कला व बुद्धि के दमनचक्र की नयी साजिशें (‘कीच’), नए तरह के गुन्डा राज (पुलिस बल व असामाजिक बाहूबली) में आम आदमी की दयनीय व दहशत ज़दा ज़िन्दगी (‘कीकर की झाड़ियों में’), व्यवस्था द्वारा दिखाए गये हसीन सपनों से बेतरह ठगा गया आम आदमी (मंगत की खोपड़ी में स्वप्न का विकास) व तकनीक व बाज़ार के गठबन्धन से पैदा किए गये नए तरह के फ़रेब, साज़िशों, लालच व प्रदर्शन के शिकार एक नए उपभोक्ता वर्ग (निम्न वर्ग का युवा वर्ग) की त्रासदी (‘कठपुतली थक गयी’, २०१४ में प्रकाशित संग्रह मुकुटधारी चूहा में संग्रहित) की अनुगूंज यहाँ सुनाई देती है।
Last but not least की तर्ज़ पर लेख के अन्त में एक दृष्टि राकेश जी की बेहद प्रासंगिक व उम्दा कहानी ‘मंगत की खोपड़ी में स्वप्न का विकास’ पर;
कहानी फैंटेसी शिल्प के करीब है, ‘मुकुटधारी चूहा’ की तरह यहाँ पाठक कई बार यथार्थ और फैंटेसी में फ़र्क नहीं कर पाता। कदाचित यथार्थ अब इतना विद्रूप और भौंडा हो गया है कि उसमें व फंतासी में बहुत लम्बा फ़ासला नहीं रह गया है। अब हमारी आँखों के सामने जो सच बनकर गुजरता है, वो फंतासी लगता है और फंतासी सच। विश्वनाथ त्रिपाठी का यह उद्धरण इस सन्दर्भ में देखा जाना चाहिए, “यह जो उच्छ्रन्खलता या ऊटपटांग है वह उस पारम्परिक और सामन्तवादी व्यवस्था में बची हुई मानवीय सम्बन्धों की आचरण संहिता को तोड़कर नवसाम्राज्यवाद के अनुकूल संहिता की स्थापना की चेष्टा है। इसका चित्रण हमें फैंटेसी जैसा लगता है, वह विसंगत जन सामान्य के लिए है, उच्च, उच्चतर वर्ग के लिए वह दैनदिन व्यवहार है।”( यथार्थ का भय और मुक्ति का स्वप्न- विश्वनाथ त्रिपाठी, समीक्षा-मुकुटधारी चूहा, कथादेश,जून-2015)
बेतरह असमान व आवारा नवपूंजीवादी व्यवस्था ने सबसे ज्यादा छल निम्न वर्ग के साथ किया। यह दोहरा शोषण था। आर्थिक व सामजिक शोषण के चक्के में पिसता, सर्वाइवल के एक मात्र संकट से जूझते इस वर्ग के लिए बड़े सपने देखना मना नहीं, सपने बशर्ते सपने रहें। सत्ता आश्रित पूंजीवादी व्यवस्था (इसका उलट भी कह सकते हैं) में सब बिकता है, सपने भी। यहाँ बेहतर जीवनाकांक्षी/लालायित निम्न वर्ग के लिए सुनहरा जाल बिछा हुआ है, थोड़ी सी चूक में वह शिकारियों के हत्थे चढ़कर हमेशा के लिए अपने पर कतरवा सकता है, यदि जान बची रही तो।
आलोचक जानकी प्रसाद शर्मा इस सन्दर्भ में लिखते हैं, ‘ एक सर्वहारा के अंदर निम्न पूंजीजीवी आकांक्षाएं और सपने, यह व्यवस्था किस तरह पैदा करती है।।।कैसे एक सर्वहारा के अंदर झूठे सपने जगा दिये जाते हैं और श्रम के रास्ते से विचलित होकर रातों-रात धनपति बनने के सपने में वह जीने लगता है। यह हमारे दौर की एक बहुत प्रकट सच्चाई है। मज़दूर वर्ग का लुम्पनीकरण (लुम्पेन उस मज़दूर वर्ग को कहते हैं, जो श्रम के रास्ते छोड़कर या तो अपराधों का रास्ता अपना ले, या किसी जादू-टोने की शरण में चला जाए) हो रहा है।”(कथा-कहानी –एक: कहानी के नए-पुराने चिराग- जानकी प्रसाद शर्मा )
मंगत अर्थात मंगत राम एक छोटा सा दर्जी है। जिसकी अपनी कोई दुकान नहीं, बस किसी रिहायशी इलाके का कोना उसका ठिकाना बन जाता है, जहाँ मशीन रखकर वह उधड़ी सीवन आदि को सीने का काम करता है। जिसके पिता भी दर्जी थे। जिन्हें किसी गाड़ी वाले ने कुचल दिया और अब वह उनकी छोड़ी सिलाई मशीन के साथ उसके कब्ज़े वाली ढाई गुणा तीन फुट की जगह पर बैठने लगा।
मंगत की बीवी बसंती उस दिन को कोसती है, जब मंगत को 5 साल पहले एक फटे पड़े मिले बटुए में ‘टोनही लक्ष्मी’ अर्थात 500 रुपए मिले थे, जिसने मंगत को ‘आदमी’ से ‘चकरघिन्नी’ बना दिया। ‘उसे न जाने क्यों ऐसा लगने लगा कि किसी दिन उसे ठीक इसी तरह पाँच-पाँच सौ की गड्डियाँ मिल जाएँगी।” दरअसल ‘स्वप्नदर्शी’ मंगत राम यूँ ही स्वप्नदर्शी नहीं हो गया। जानकी प्रसाद जी ने जिस लुम्पनीकरण की बात की वह व्यवस्था का एक बड़ा षड्यंत्र है, जिसकी ज़द में अंजाने ही व्यक्ति आता जाता है। सत्ता के लिए यह वर्ग वोट बैंक के अतिरिक्त कुछ नहीं, इनकी जगह सिर्फ़ आंकड़ों में है। लाल किले के बुर्ज से उड़ कर आया मायावी कबूतर मंगत के दिमाग में सुनहरे ख्वाब का बीज डाल गया। बीज के अब पनपने की बारी है। ये सुनहरे ख्व़ाब ‘अच्छे दिन’ आने के हैं। ये ख्वाब लेकर उसके पास आया एक छुटभैया नेता। ‘ अब काहे का गरीब? अब तुम्हारे दिन भी फिरने वाले हैं।’।।यह सुनकर, ‘ यह ज्योतिषी तो नहीं? मंगतराम के पैर और सिलाई मशीन दोनों चौंककर रुक गये।।।।वह पुतलियाँ उलटकर अपनी ही पलकों के अंदर देखते हुए गुटरगूं-गुटरगूं बोलने लगा था इसलिए माना जाता है कि बेडौल आदमी ने लाल किले के बुर्ज़ से उड़कर आए किसी कबूतर के बारे में बताया, जिसके पैरों में गरीबी के दिन फिरने का संदेश बंधा था।।।।बस यहीं से शुरुआत हुई थी। विकास का सपना देखने वाले महान लोकतंत्र के एक निरीह नागरिक की खोपड़ी में स्वप्न के विकास की।”
अंतिम पंक्ति बेहद मार्मिक है, लोकतंत्र बनाम छलतन्त्र में गरीब आदमी के सपनों का सौदा हो रहा है। श्रमिक वर्ग के व्यक्ति की सबसे बड़ी पूँजी उसकी श्रम शक्ति है, उसकी कर्मठता ही उसकी अपनी निजी ताकत व ठसक है। हसीन सपने दिखाकर, फिर निर्ममता से स्वप्नदर्शी को तिल-तिल कर तबाह होने का तमाशा देखने वाला गिरोह हर तरह से इस दुश्चक्र में फंसे लोगों का इस्तेमाल अपने-अपने फ़ायदे के लिए करता है। लाल किले के बुर्ज से उड़ कर आया मायावी कबूतर मंगत के दिमाग में सुनहरे ख्वाब का बीज डाल गया। बीज के अब पनपने की बारी है। धीरे-धीरे यह स्वप्न मंगत की खोपड़ी से भी बड़ा होता जा रहा है, ‘मंगतराम की खोपड़ी के अंदर एक सुखद सपना खमीर चढ़कर फूल गया। सपना खोपड़ी से बड़ा होता जा रहा है। छोटे दिमाग वाले आदमी का सपना इतना बड़ा हो जाए तो ज़ाहिर है दिमाग का क्या होगा। वे (मास्साब) गहरी सांस खींचते, ‘कबूतर ऐसी ही खाली खोपड़ियों में घर बनाते हैं।’
इस कहानी में दो अन्य पात्र व उनकी भूमिका भी बेहद अहम है, पंकज मास्साब और मंगत की बीवी बसंती। मास्साब एक चेतनशील, शिक्षित मध्यवर्गीय पात्र की भूमिका में हैं और बसंती एक ऐसी निम्नवर्गीय स्त्री के रूप में जिसका हास-उल्लास, दुःख-सुख सब पति पर निर्भर करता है। मंगत के फितूर के कारण उसकी दिन प्रति दिन गिरती हालत और उसके कारण उसके परिवार की दुर्दशा मास्साब को कचोटती है उससे भी ज्यादा कचोटती हैं चुलबुली बसंती की वो पनीली आँखें, जिनमें कभी खेलने वाला बच्चा अब गुमसुम और उदास बैठा है। बसंती के प्रति मास्साब के भीतर एक सहज झुकाव व करुणा दिखती है, लेकिन उन्होंने कभी अपना स्वार्थ साधने की कोशिश की हो, ऐसा कहानी में कहीं नहीं दिखता।
2019 के रमाकांत स्मृति सम्मान से पुरुस्कृत राकेश तिवारी की यह कहानी अपने पूरे कलेवर में शानदार कहानी है। इस कहानी में मंगत की दयनीय स्थिति उदय प्रकाश की ‘पालगोमरा का स्कूटर’ की भी याद दिलाती है, लेकिन दोनों में सामन्य व्यक्तियों के विसंगत से विक्षिप्त हो जाने की अवस्था के कारणों, स्थितियों, समय व हालात का फ़र्क है। राकेश जी अपनी उन्हीं कहानियों में कमाल कर सके जहाँ उन्हें खेलने के लिए ‘पिच’ लम्बी मिली, छोटी कहानियों में वे चूक जाते हैं। वो अपनी कहानियों में अपनी भाषा और ख़ास तरह के शिल्प के कारण कमाल कर जाते हैं, ये भाषा केशव की तरह चमत्कार प्रदर्शन के फलस्वरूप नहीं बल्कि उनकी सहज प्रतिभा के फलस्वरूप है। उनके लेखन पर जिस तरह बात होनी चाहिए थी, अफ़सोस उस तरह अभी नहीं हुई। किन्तु उम्मीद पूरी है, आख़िर रोशनी को हथेली की ओट से कब तक ढका जाएगा।

अनुराधा गुप्ता
लेखिका कमला नेहरु कॉलेज, दिल्ली विश्विद्यालय में सहायक प्रवक्ता (हिन्दी विभाग) हैं।
सम्पर्क +919968253219, anuradha2012@gmail.com
.