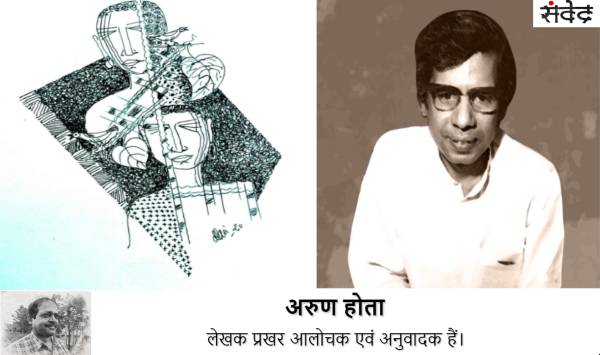अगिनखोर : झूठे विद्रोह की कथा

यदि यथार्थ के विभिन्न अर्थों का कोई लोकतन्त्र है, जो वह केवल उस स्वतन्त्रता में ही उपलब्ध होता है, जिसे हर कलाकृति अपने भीतर लेकर चलती है, जो न किसी एक अर्थ से अपने को नत्थी करती है, न किसी दूसरे अर्थ की तानाशाही स्वीकार करती है।
— निर्मल वर्मा
अगिनखोर फणीश्वरनाथ रेणु की अल्पचर्चित कहानी है। यह धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका में 1972 के 5 नवम्बर- 12 नवम्बर वाले अंक में प्रकाशित हुई थी। इसे उसी वर्ष अगिनखोर कहानी-संग्रह में संकलित किया गया है। रेणु जी की पहली कहानी वट बाबा साप्ताहिक विश्वमित्र में 27 अगस्त 1944 को प्रकाशित हुई थी। भित्तिचित्र की मयूरी उनकी आख़िरी कहानी है, जो नवम्बर 1972 में साप्ताहिक हिन्दुस्तान में छपी। उनके तीन कहानी-संग्रह प्रकाशित हुए — एक आदिम रात्रि की महक ( ),ठुमरी ( ) और अगिनखोर ( )। अपने 28 वर्षों के रचना काल में रेणु जी ने कुल 62 कहानियाँ लिखीं। रसप्रिया उनकी पहली ऐसी कहानी है, जिसने हिंदी के वृहत्तर पाठक-वर्ग का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। इस पर ध्यान तो उस समय के प्रखर आलोचक नामवर सिंह का भी गया। लेकिन वे इस पर चर्चा नहीं कर सके। यह कहानी 1955 में इलाहाबाद से प्रकाशित और धर्मवीर भारती द्वारा संपादित पत्रिका निकष में छपी थी। यही वही समय है, जहाँ से हिन्दी कहानी की नयी धारा के रूप में ‘नयी कहानी’ चल पड़ी। उस दौर में निर्मल वर्मा, राजेन्द्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर, रांगेय राघव, भीष्म साहनी के साथ-साथ फणीश्वरनाथ रेणु भी कहानी लिख रहे थे। एकसाथ इतनी कथा-प्रतिभा का आगमन निश्चित रूप से इस कालावधि को महत्तर बनाती हैं। इन कहानियों की अंतर्वस्तु और शिल्प में इतनी नवीनता थी कि इन्हें नयी कहानी की संज्ञा ही मिल गयी। 1965 तक नयी कहानी का विस्तार माना जाता है।
‘नयी कहानी ‘ में नगरीय बोध का प्राचुर्य है। इस दौर में ग्राम जीवन की कहानी लिखनेवाले लेखकों में रेणु और मार्कण्डेय का नाम लिया जाता है। मैला आँचल उपन्यास के बाद रेणु पर एक विशेषण आँचलिक चस्पाँ कर दिया गया। इसलिए इनकी गिनती नयी कहानियों में नहीं हो सकी। नामवर सिंह को नयी कहानी का सर्वसम्मत आलोचक माना गया है। उनकी पुस्तक कहानी : नयी कहानी में रेणु की एक कहानी रसप्रिया के नाम का उल्लेख भर है। उनकी किसी कहानी पर नामवर सिंह ने कुछ भी नहीं लिखा। काशीनाथ सिंह से अपने एक साक्षात्कार में नामवर जी ने रेणु के साहित्य को न समझ पाने की बात कहकर अफ़सोस ज़ाहिर किया था। वे जिसतरह से कथा-साहित्य पर सोच रहे थे, लिख रहे थे, उसके स्वरूप और उद्देश्य पर यदि हम ग़ौर करें, तो समझ में आयेगा कि वे रेणु के साहित्य पर लिख नहीं सकते थे, क्योंकि वे हिन्दी कहानी के लिए जिस मापदंड का निर्माण करना चाहते थे, उसमें रेणु की रचनाएँ न केवल मिसफ़िट थीं, वरन् उसमें बाधा भी खड़ी कर रही थीं। नामवर जी कहानी में नागर बोध की खोज कर रहे थे। लोक-संवेदना उनकी सोच के दायरे में नहीं था। हिन्दी आलोचना में कविता की समीक्षा के टूल्स थे। नामवर जी कहानी समीक्षा के टूल्स के निर्माण में लगे थे। उन्होंने कथा के मूल्यांकन का व्याकरण रच दिया। अब कहानियाँ उसी चौखटे में फ़िट होने लगीं। यदि किसी के पैर उस चौहद्दी से बाहर निकल गये, तो वे समीक्षा से ओझल हो गये। इसी काल-खंड में फणीश्वरनाथ रेणु कहानी-उपन्यास लिख रहे थे। स्वाभाविक रूप से हिन्दी आलोचना ने न उनकी परवाह की और न उन्होंने आलोचकों की। पाठकों ने उन्हें बहुत मान दिया। उनकी यह बेफ़िक्री न होती , तो भारत की ग्रामीण संवेदना का इतना प्रामाणिक दस्तावेज वे नहीं रख पाते। वे एक साथ प्रेमचंद और सतीनाथ भादुड़ी, ताराशंकर बंद्योपाध्याय, विभूतिभूषण बंद्योपाध्याय जैसे महान रचनाकारों के विरसे को समृद्ध करने में लगे हुए थे।
हिन्दी कथा-साहित्य में प्रेमचंद मील के पत्थर हैं। 1936 में लखनऊ के प्रगतिशील लेखक संघ के पहले सम्मेलन की उन्होंने अध्यक्षता की थी। उनकी कहानियों में ग्रामीण जीवन के यथार्थ को जिस सहजता से उठाया गया है , वह अनुपमेय है। उनके कथा-साहित्य में किसानों के कठोर जीवन की सच्चाई गहनता के साथ व्यक्त हुई है। प्रगतिशील आलोचकों ने उन्हें कहानी के मापदंड के बतौर अपना लिया। यदि प्रेमचंद के बाद ग्रामीण जीवन की बारीकियों को कथा-साहित्य में लाने का प्रयास किसी ने किया तो वह रेणु हैं। इस सच्चाई को सभी ने अब स्वीकार भी कर लिया है। प्रेमचंद के पात्र हामिद, जुम्मन, अलगू चौधरी, घीसू, माधव, सुजान भगत आदि की तरह रेणु के पात्र हिरामन, हीराबाई, पँचकौड़ी, रमपतिया, सिरचन आदि भी अब प्रतीक बन चुके हैं। हिन्दी की प्रगतिशील आलोचना को इस सत्य को स्वीकार करने में थोड़ा विलंब हुआ। राममनोहर लोहिया अपने को कुजात गांधीवादी मानते थे। रेणु भी हिन्दी के कुजात प्रगतिशील कथाकार हैं।
अगिनखोर कहानी रेणु की अन्य कहानियों से अलग है। इसके माध्यम से वे क्या कहना चाह रहे हैं ? अगिनखोर अर्थात् फ़ायर इटर । हमने सर्कस, तमाशों में अक्सर करतब दिखाने वालों को आग मुँह में निगलते देखा है। यह एक ट्रिक है। कहानी के शीर्षक से ही लगता है कि यह किसी ऐसे ही अगिनखोर की कहानी है। यह कहानी 18 वर्षों की अवधि में फैली हुई है। कहानी में मुख्य रूप से चार पात्र हैं — साहित्यिक सूर्यनाथ, उसकी पत्नी अन्नपूर्णा, आभारानी राय और उसका पुत्र । कहानी सूर्यनाथ की आँखों से देखी गयी है। यह और बात है कि सूर्यनाथ भी दिख रहे हैं । कहानी जब कही जा रही है उस समय सूर्यनाथ की उम्र लगभग 50 वर्ष है। वह फ्लेश बैक में 18 साल पहले जाता है, उसी के आसपास आभारानी राय एक पुत्र को जन्म देती है। इसतरह उसकी उम्र 17 साल के आसपास है। ज़ाहिर है वह अभी तरुण है।
सूर्यनाथ की पत्नी अन्नपूर्णा एक हेल्थ सेंटर की इंचार्ज है। वहाँ मिडवाइफ और नर्सिंग का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसी सिलसिले में आभारानी राय आती है। उसे पति ने छोड़ दिया है। अन्नपूर्णा सूर्यनाथ से उसका परिचय कराते हुए हुए पहले उसे विडो कहती, जिसे बाद में सुधार कर वह परित्यक्ता बताती है ।
सूर्यनाथ इसे ‘एक ही बात है’ मानता है । अपने आशय को स्पष्ट करते हुए वह मजाकिया लहजे में कहता है , ” अगर स्वामी इसे नहीं छोड़ता, तो बेचारा मर ही जाता और वह विधवा हो जाती। “
सूर्यनाथ को आभा के स्वभाव में ‘सखि-सखि’ भाव दिखता है।वह लावण्यवती है । वह किसी की पत्नी होकर नहीं रह सकती है, ‘सखि होकर ही रह सकती है।
अन्नपूर्णा को लगता है कि सूर्यनाथ आभा को कहीं पहले से पहचानता तो नहीं, क्योंकि वह भी सूर्यनाथ के इलाक़े पूर्णियाँ-सहरसा की ही है। आभारानी राय अन्नपूर्णा को अपने घर लाती है और उन दोनों के परस्पर संवाद को सुन कर कहती है , ” अब कितना सुनोगे बांग्ला कीर्तन ! ”
सूर्यनाथ बांगला भाषा-साहित्य से सुपरिचित है। वह पूछ लेता है, ” श्यामा संकीर्तन या … ? ”
आभा कहती है “कृष्ण कीर्तन”। सूर्यनाथ रसिक है। उसकी रसिकता चतुरा आभारानी से छिपी नहीं रहती है। वह उसकी सुरुचि की तारीफ़ करती कहती है, “आपनि कोवि मानुष… आप कवि जो ठहरे।”
अन्नपूर्णा उसकी बात काटती हुई कहती है , “वह साहित्यिक है।”
सूर्यनाथ के ही अंदाज में ‘एकई कथा’ कहकर वह अपनी दाहिनी आँख की पलकों को दबा देती है। उसकी यह अदा सूर्यनाथ को भा जाती है। आभारानी मुक्त ख्यालों की है। उसके ख्यालात के कारण ही सूर्यनाथ उसे सबके लिए सुलभ मान लेता है। सूर्यनाथ आभारानी को अपने अंदाज से अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। आभारानी भी सूर्यनाथ के नज़दीक आना चाहती है। एक दिन वह रोहू मछली लेकर आ जाती है और मलाई करी बनाती है।
सूर्यनाथ चटखारे लेकर मछली खाता है और उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा केवल “भीषोण सुंदर” और “अपूर्बो” कहकर ही नहीं संतुष्ट होता है, बल्कि आभा को मुग्ध करने के लिए वह वैष्णव संप्रदाय की भाषा में कहता है, “अहा! ए तो क्षीरसागरे स्वयं भगवान मत्स्यावतार …।”
आभारानी उसे ‘जामाय बाबू’ कह कर संबोधित करती है, लेकिन उस दिन वह उसे .’सुरसिक’ भी कहती है। सूर्यनाथ प्रसंगवश उसे संबोधित कर कहा था — ” साली को ‘केलिकुंजिका’ भी कहा जाता है।” अन्नपूर्णा भी हँसी के उसी अंदाज में आभा को आगाह भी करती है — ‘सावधान आभा !’
स्पष्ट है कि सूर्यनाथ अपने निहित आशय का अहसास आभारानी को पूरी तरह करा देना चाहता है।
सूर्यनाथ आभा के शरीर से आकृष्ट है। आभा को इसका आभास अच्छी तरह है। एक दिन जब अन्नपूर्णा वर्किंग वीमेन्स के लिए आयोजित चैरिटी शो में व्यस्त के कारण घर से बाहर है, तभी आभा बारिश में भीगती सूर्यनाथ के यहाँ पहुँच जाती है। वह सूर्यनाथ को भी बताती है कि वह जानती है कि अन्नपूर्णा घर पर नहीं है। अर्थात् वह सूर्यनाथ के लिए प्रस्तुत होकर आई है। बाथरूम से अन्नपूर्णा की साड़ी और अँगिया पहनकर वह बाहर आती है तो सूर्यनाथ उसके लिए चाय लेकर खड़ा है । वह कहता है — “चाय नहीं। गुलबनसफा का काढ़ा, अदरक और नींबू के रस के साथ। ”
आभा उसे चखकर देखती है सच में काढ़ा ही है । सूर्यनाथ कहता है, “आपको सन्देह हुआ कि चाय में कोई नशा मिला दिया है, मैंने?”
“आप लोगों का विश्वास ! आप लोग सबकुछ कर सकते हैं।” – आभा हलाल करनेवाली हँसी के साथ कहती है।
वह ‘तुम’ संबोधित करने पर ज़ोर डालती है। वह धीरे धीरे खुलती चली जाती है। वह कहती है , “यदि कुछ नहीं मिलाया है, तो देह क्यों झनझना रही है?”
सूर्यनाथ इसकी कोई सफ़ाई नहीं देता है। आभा सूर्यनाथ के कंधे पर अपना सिर रख देती है। सूर्यनाथ उसे अपनी बाँहों में जकड़ लेता है। बाहर बिजली कौंधती है, मेघों का भयानक गर्जन होता है और सूर्यनाथ का तप्त शरीर तत्काल ठंडा हो जाता है। वह छिटककर आभा से अलग हो जाता है।कामातुर आभा कहती है, “कोई नहीं है। हवा से पल्ला खुल गया है। सूर्योदा … आप कहाँ चले गये …?”
इस घटना के बाद से आभा सूर्यनाथ से बोलना बंद कर देती है ।शायद उसने स्वयं को उसने अपमानित महसूस किया हो।
समाज में आभारानी के चरित्र के बारे में तरह-तरह के क़िस्से प्रचलित होने लगते हैं। अपमान से पीड़ित होकर उसने अपना तबादला करा लेती है । वह दस-ग्यारह महीने बाद ‘छ: महीने का पेट लेकर’ अन्नपूर्णा से मिलने आती है। वह भ्रूण को ‘गिराने’ में उसकी सहायता चाहती है। अन्नपूर्णा डाँटकर उसे मना कर देती है ।
आभा रानी के गर्भस्थ शिशु के लिए सूर्यनाथ को एंबुलेंस के ड्राइवर पर शक हो रहा है, क्योंकि उसने आभा रानी को उस ड्राइवर के साथ उसे कई बार सिनेमा हॉल में देखा है। आभारानी अन्नपूर्णा को बताती है, “कपड़े की दुकान के बूढ़े मालिक ने फुसलाकर उसका सर्वनाश किया है।”
कहानी का प्रारंभ नाटकीय है। सूर्यनाथ बाहर निकलने के लिए तैयार हो रहा है । वह भूल गया है कि अन्नपूर्णा ने कल बाज़ार में अचानक आभा के बेटे से मुलाक़ात की बात कही थी और यह भी कहा था कि आज वह सूर्यनाथ से मिलकर उसे एक इन्फॉर्मेशन देने आने वाला है। उसने अन्नपूर्णा से पूछा भी था , “उसका चेहरा किससे मिलता है ? एंबुलेंस ड्राइवर से या कपड़े की दुकान के बूढ़े मालिक से ? ”
अन्नपूर्णा किसी काम से बाहर चली जाती है । आभा का बेटा आता है । वह शुरु से ही अपने औद्धत्य का परिचय देता है ।
सूर्यनाथ को आभारानी का बेटा अपने कई नाम बताता है, सूतपुत्र, शिवलिंगा और डोगलास। सभी नाम को वह अपना असली नाम मानता है। वह कहता है कि अभी वह सूतपुत्र होकर बात कर रहा है। वह कविता शिवलिंगा के नाम से लिखता है और धनबाद, झरिया, जमशेदपुर और कलकत्ते के विभिन्न गुप्त क्लबों और डिस्कोथिक में डोगलास के नाम से वह कॉमेडियन का शो देता है। वह धनबाद में रहता है। स्पष्ट है कि वह भीषण रूप से पहचान के संकट से गुज़र रहा है। यह उसके हाव-भाव से साफ़ ज़ाहिर हो रहा है। उसका रंग गेहुँआ और क़द मझौला है। उसके भूरे बाल बिखरे हुए हैं। आते ही वह सूर्यनाथ का मज़ाक़ उड़ाना शुरु कर देता है। वह कहता है कि सूर्यनाथ की पीढ़ी का सारा साहित्य कूड़ा-कचरा है। उसकी पूरी पीढ़ी मुर्दा हो चुकी है। पूरा लेखन कमर्शियल है। कमरे की दीवारों पर टँगी छाया-छवियों, अभिनंदन पत्र, उपाधि और ‘सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट’ आगंतुक को सूर्यनाथ का व्यक्तित्व तेंदुए की तरह उछलकर दबोचने के लिए ही उसने टाँग रखे हैं। सूतपुत्र की बातों से सूर्यनाथ अप्रतिभ हो जाता है। सूतपुत्र तकियालाम की तरह ‘आइक-स्ला’ बोलता रहता है। सूर्यनाथ को उसके हाव-भाव अच्छे नहीं लगते हैं। वह चिढ़ाते हुए कहता है , “आप जैसे कमर्शियल लेखकों को अपने पेशे के लिए आत्मप्रचार करना ही पड़ता है।”
सूर्यनाथ उसे सह रहा है । उसने पहचान लिया है, यह अपने को ‘फायरईटर’ — अगिनखोर समझता है। आभारानी के बारे में पूछने पर वह बहुत लापरवाही से वह कहता है , “उनकी ‘केलिकुंजिका’ आभारानी का उसे कोई पता नहीं है। ”
सूर्यनाथ ने जब कनखी से सूतपुत्र को देखा, तो उसमें उसे आभारानी की झलक दिखी। उसकी हँसी में कपड़े की दुकान के मालिक की छाया भी दिख गयी। ठीक उसी तरह जैसे रसप्रिया में पँचकौड़ी को मोहना की बड़ी-बड़ी आँखें कमलपुर के नन्दूबाबू की आँखों जैसी दिखी थीं।
सूतपुत्र सूर्यनाथ को स्वरचित एक स्क्रिप्ट के बारे में बताता है। उसे सुनकर सूर्यनाथ ने इसे दस-ग्यारह साल पहले लिखी गयी अमेरिकन कॉमेडियन लेनी ब्रूस की कृति बताता है। यह सुनते ही सूतपुत्र का चेहरा अचानक बुझ जाता है। अपनी चोरी पकड़ी जाने पर वह तुतलाने लगता है। वह सीधे अपने उद्देश्य पर आ जाता है । वह कहता है कि डायरी के मुताबिक़ वह उसके पिता हैं। सूर्यनाथ डायरी देखता है। लिखावट आभारानी की ही है । लिखा है, “आज के सूर्योदा आमार संगे जा कॅरलेन, आमार जीवने आर केउ करे नि…। ” (आज सूर्यदा ने मेरे साथ जो कुछ किया, जीवन में और किसी ने नहीं किया।
1955-56 की डायरी को उसे होली फैमिली की मदर ने दिया है । डायरी के उस अंश को पढ़ कर उसे विश्वास है कि सूर्यनाथ ही उसके पिता हैं। सूर्यनाथ ने उसे रोजनामचा की तारीख को उसके ‘डेट ऑफ बर्थ’ से मिलाकर देखने की सलाह देकर उसके भ्रम को दूर करना चाहता है।
सूतपुत्र सूर्यनाथ को पिता मानने के अपने विश्वास पर फिर भी टिका रहता है तो सूर्यनाथ उसे बताता है, “आकर्षण के बावजूद आभारानी के साथ संबंध नहीं बना था। ”
उसे जलील करने के लिए व्यंग्यात्मक लहजे में वह कहता है — “कामातुरा सुंदरी के साथ एकांत के उस क्षण में मैं मदनोन्मत अवश्य हुआ था। किंतु…किंतु…उस लावण्यमयी रमणी के मुँह में ऐसी उत्कट दुर्गंध थी कि मैं अचानक विरक्त हो गया…”।
यह सुनकर उसकी आँखें डबडबा जाती है । उसके चेहरे पर कभी-कभी आभारानी की मासूमियत झलक जाती थी। वह लड़के से पूछ लेता है — “किंतु आप असंस्कृति और अपरंपरा के इतने कट्टर हिमायती होकर अपने पिता को क्यों खोज रहे हैं ?”
वह बताता है कि उसने इतने दिनों तक उसे पिता मान लिया था। उसे लगता रहा कि वह एक प्रसिद्ध कलाकार का पुत्र है। अपने पिता को अपना शत्रु मानकर उसे अपार बल मिलता था। आज उसकी प्रेरणा का मूल स्रोत ही सूख गया। उसकी स्थिति कवच-कुंडलहीन ‘कर्ण’ की तरह हो रही थी। सूर्यनाथ को लगता है कि आभारानी के बेटे के बालों पर अपना हाथ फेर दे। लेकिन इस स्नेह से उसके ‘वॉयलेंट’ हो जाने का ख़तरा था।
सूर्यनाथ “अब आप जाइए अगिनखोर जी !” कहकर उसे विदा कर देता है। वह सूतपुत्र, शिवालिंगा, डोगलास अपने एक नये नाम को अंगीकार कर सूर्यनाथ के घर से चला जाता है — “हाँ, हाँ। आइ एम ए फायरईटर…अगिनखोर !”
अगिनखोर कहानी में सूर्यनाथ साहित्यकार हैं। आभारानी का बेटा भी कविता लिखता है। दोनों अपनी-अपनी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मज़े की बात तो यह है कि सूर्यनाथ फणीश्वरनाथ रेणु की पीढ़ी का है और कथित सूतपुत्र उनके ठीक बाद की पीढ़ी का। रेणु जी की तरह वह भी 1955-56 में प्रसिद्ध साहित्यकार माना जाने लगा था। वह भी पूर्णिया-सहरसा की तरफ़ का है। रेणु के बाद के साहित्य में अकविता, अकहानी, भूखी पीढ़ी, श्मशानी पीढ़ी आदि की विस्फोटक और चौंकानेवाली रचनाएँ लिखी जा रही थीं। सूतपुत्र इसी पीढ़ी का है। दोनों ही पीढ़ी एक दूसरे के प्रति अविश्वास से भरी हुई है।
सूर्यनाथ को लगता है कि सूतपूत्र/शिवलिंगा पाश्चात्य साहित्य की नक़ल करता है और झूठ-मूठ का अपने को अवाँगार्द मान बैठा है। वह विद्रोही बनने के लिए अपनी परंपरा और संस्कृति की अनावश्यक हँसी उड़ाता है। वहीं सूतपुत्र सूर्यनाथ की पीढ़ी के लेखकों को अनपढ़ और कूढ़मगज मानता है। कहानी में सूर्यनाथ के कमरे में टँगी तस्वीरों, उपाधियों आदि से सूर्यनाथ की पूरी पीढ़ी की छवि आत्मकेंद्रित और आत्मरति से पीड़ित की बनती दिख रही है। कथाकार सूर्यनाथ और आभारानी के बेटे ‘सूतपुत्र’ को एक दूरी से देख रहे हैं। किसी के प्रति अतिरिक्त लगाव का आग्रह नहीं। 7 दिसंबर, 1972 में जर्मनी के विद्वान लोठार लुट्से ने एक जिज्ञासा रखी थी कि साधारणतया आप कहानी गढ़ते समय केंद्र में क्या रखते हैं — कथानक या चरित्र या कोई विचार? रेणु जी ने उत्तर में जो कहा था उससे उनकी कहानी को समझने का हमें सूत्र मिल सकता है। वे कहते हैं — “साधारणतया तो समस्याएँ जो होती हैं और उनमें खुद अपने को खोजना होता है — वे समस्याएँ जो हमको किसी-न-किसी ढंग से प्रभावित करती हैं। तो यों कहानी में मेरा ही तो बहुत-सा रूप हो जाता है। और, इसलिए कभी-कभी तो ऐसा होता है कि बात किसी पात्र पर चली आती है, और कभी-कभी घटनाओं पर चली आती है। कभी यह भी पूरा नहीं होता है, और दोनों के बीच झगड़ा ही चलता रहता है।”
सूर्यनाथ और सूतपुत्र दोनों ही चरित्र में रेणु स्वयं प्रतिभाषित हो रहे हैं। एक साहित्यिक होने के नाते सूर्यनाथ से सामान्यत: जिन मूल्यों की अपेक्षा रहती है, वे वहाँ सिरे से ग़ायब हैं। आभारानी परित्यक्ता है। वह स्वतन्त्र रूप से जीना चाहती है। उसके व्यक्तित्व में एक आभा है। वह अच्छा गाती है। उसमें दूसरों को अपनी ओर खींचने की शक्ति है। लेकिन उसकी सारी विशेषताएँ इस पुरुषतांत्रिक समाज में किसी काम की नहीं हैं। पुरुष-भोग के लिए वह उन्नत पण्य भर है। दुर्भाग्य से सूर्यनाथ जैसे प्रसिद्ध साहित्यिक के लिए भी वह भोग्य सामग्री से अधिक महत्व नहीं रखती है। सूर्यनाथ बारिश के दिन आभारानी को अनेक तरह के संकेतों के माध्यम से उसके शरीर के प्रति अपनी आसक्ति को व्यक्त करता है। यह संयोग ही था कि मेघ के गरजने या हवा के तेज चलने से वह अचानक आभा के शरीर से अलग हो जाता है। इस प्रसंग का ज़िक्र कहानी में तीन जगह हुआ है। पहली बार जब यह घटित हो रहा है।
“आभा ने सफल अभिनेत्री की तरह सूर्यनाथ के कंधे पर अपना सिर ऱख दिया था। सूर्यनाथ की देह अचानक तप उठी थी। स्वचालित यंत्र की तरह उसकी भुजाओं ने आभा को जकड़ लिया। बाहर आकाश में बिजली कौंधी थी। मेघ गर्जन हुआ था और सूर्यनाथ का तप्त शरीर तत्काल ठंडा हो गया था। आभा अस्फुट स्वर में बोली थी, ‘कोई नहीं … हवा से खिड़की का पल्ला खुल गया है। सूर्योदा … जमाय बाबू … आप कहीं चले गए … ?” स्पष्ट है कि उस दिन दोनों अत्यंत आतुर होकर एक दूसरे से आबद्ध हुए थे। किसी कारणवश वे अंतिम बिंदू तक नहीं पहुँच पाये। हो सकता है अचानक होनेवाली आवाज़ से पत्नी अन्नपूर्णा के आने का डर हुआ हो या शायद ‘विवेक’ ही जग गया हो। यहाँ अन्नपूर्णा के आने का सुबहा ज्यादा दिखता है। सूर्योदा अन्नपूर्णा की कमाई पर ही निर्भर दिखते हैं। जीवन के आधार के खिसकने की आशंका से भीत होकर संभवत: वे अलग छिटक गये हों।
आभारानी इसी घटना को अपनी डायरी में इसतरह लिखती है — “आज के सूर्योदा आमार संगे जा कॅरलेन, आमार जीवने आर केउ करे नि … “ ( आज सूर्योदा ने मेरे साथ जो कुछ किया, जीवन में और किसी ने नहीं ने नहीं किया।) आभारानी के जीवन का यह विरल अनुभव है। उसने आजतक इस बिंदू से किसी पुरुष को वापस लौटते हुए नहीं देखा। यह उसके लिए अपने स्त्रीत्व का अपमान था। वह इसे भूल नहीं पाई।
कहानी के अंत में जब आभारानी का बेटा डायरी के इसी हिस्से को आधार बनाकर सूर्यनाथ को उसका पिता मानने के लिए दबाव बनाता है, तो उससे बचाव में वह उस दिन के बारे में कहता है — “सूतपुत्तर सरकार ! आप मानें या न मानें ठेंगे से। मैं जानता हूँ कि यह सच नहीं। असल में … बावजूद आकर्षण के, आभारानी के साथ मेरा सम्बन्ध हुआ ही नहीं । कामातुरा सुन्दरी के साथ एकांत के उस क्षण में मैं मदनोन्मत अवश्य हुआ था । किन्तु … किन्तु … उस लावण्यमयी रमणी के मुँह में ऐसी उत्कट दुर्गन्ध थी कि मैं अचानक विरक्त हो गया …“। सूर्यनाथ के इस कथन में बनावटीपन साफ़ ज़ाहिर हो रहा हैं। आभारानी को जलील करने का भाव है। ‘किन्तु’ शब्द के दुहराव और उनके बीच के अंतराल के प्रयोग से कथाकार सूर्यनाथ के झूठ को कह दे रहे हैं। यहाँ सूर्यनाथ का पूरा ‘साहित्यिक’ व्यक्तित्व का मुखौटा उतर जाता है। सूर्यनाथ के लिए आभारानी जैसी स्त्री सिर्फ ‘केलिकुंजिका’ है।
1962 के चीन-भारत के युद्ध के बाद देश में हताशा का भाव व्याप्त हो गया था। फिर कांग्रेस पार्टी में नवीन और प्रवीण के आधार पर विभाजन हो गया। इस माहौल का असर नयी पीढ़ी पर बहुत गहरा हुआ। वे नकारवाद के शिकार हो गये। यही वह समय भी है जब साहित्य में अकहानी और अकविता का आंदोलन चल रहा था। बांग्ला के कवि मलय राय चौधरी ने पटना के अपने निवास से 1961 में घोषणापत्र (मेनिफेस्टो) जारी करके हंगरी जेनरेशन (भूखी पीढ़ी) का सूत्रपात किया था। मलय रायचौधरी को उनकी कविता प्रचंड बैद्युतिक छुतार लिखने के जुर्म में कलकत्ता में गिरफ्तार किया गया था। उनपर मुकदमा भी चला। फणीश्वरनाथ रेणु ने दिनमान में लेख लिख कर मलय राय चौधरी की गिरफ्तारी का विरोध किया था। रेणु जी से मलय राय चौधरी का संबंध घनिष्ठ और मित्रवत था। वे भूखी पीढ़ी के प्रेरणा-स्रोत से पूरी तरह परिचित थे। वे भूखी पीढ़ी के सभी कवियों-लेखकों से व्यक्तिगत रूप से घनिष्ठ थे।
‘सूतपुत्र’ इसी समय की मानसिकता का प्रतीक है। वह समय की उपज तो है, लेकिन उसे अपने समय की पहचान नहीं है। वह सूर्यनाथ को पिता मानकर एक मिथ्या विद्रोह की मानसिकता में जी रहा है। उसे अपनी जड़ों से रत्ती भर लगाव नहीं है। भले ही वह पिता के संधान में सूर्यनाथ तक पहुँच गया हो, लेकिन वह अपनी माँ की खोज नहीं करता। वह अमेरिका के दशक पूर्व लिखे साहित्यादि की भौंड़ी नक़ल करता है।
सूर्यनाथ रेणु जी की पीढ़ी का है। वे अपनी पीढ़ी की हिप्पोक्रेसी से त्रस्त थे। ऐसे कथाकारों का वे ज़िक्र करते हैं, जो वाणी में ही केवल आधुनिक हैं। उन्हें यह भी पता नहीं है कि धान का पौधा होता है या पेड़। अपने जमाने के साहित्यकारों की प्रदर्शनप्रियता से उन्हें बड़ी चिढ़ थी। स्त्रियों के लिए बड़ी-बड़ी बात करने वाली इस पीढ़ी के रचनाकार स्त्रियों को भोग की सामग्री के सिवा और कुछ नहीं मानते । आभारानी के प्रति केवल भोग के लिए सूर्यनाथ का आकर्षण और बारिश के उस दिन लिपटने की घटना रेणु की इस मान्यता की तस्दीक़ करती है।
अगिनखोर कहानी फणीश्वरनाथ रेणु की एक महत्वपूर्ण रचना है। इस तरह की अनेक कहानियाँ हैं, जिनका पुनर्पाठ होना ज़रूरी है। किसी भी लेखक के पूनर्मूल्यांकन के लिये उसके साहित्य पर समग्रता पर विचार करना ज़रूरी है। रेणु को कुछेक कहानियों-उपन्यासों में सीमित कर देना सर्वथा अनुचित है।

आशुतोष
जन्म : 6 फरवरी 1958 , चटमा बाजार, बांका (बिहार)। शिक्षा:स्नातकोत्तर (हिंदी) एवं पी.एच.डी.। सामाजिक और राजनीतिक समूहों में प्रखर बुद्धिजीवी और सन्तुलित चिन्तक के रूप में प्रतिष्ठित। गंगा मुक्ति आन्दोलन के प्रमुख कार्यकर्ता। संवेद, वसुधा, सबलोग, अंगचंपा आदि में कविता, समीक्षा एवं आलेख प्रकाशित।
सम्प्रति – विद्यासागर कॉलेज फॉर वीमेन,कोलकाता में अध्यापन।
संपर्क : +917003093474, angashutosh@gmail.com
4 एच सोहम अपार्टमेंट, 358/1 एन.एस.सी. बोस रोड, कोलकाता – 700047