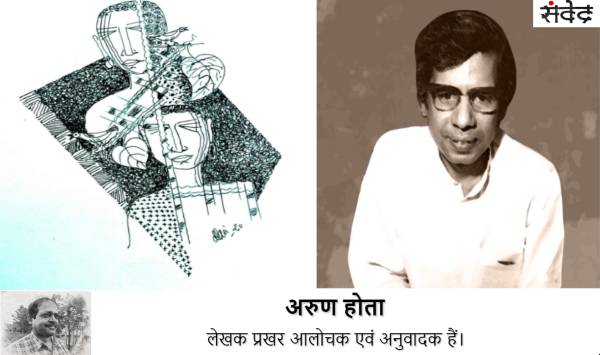प्रीत-पीड़ा-राग

रेणु की कहानियों से गुज़रते हुए मैं हर बार मिथिला के इस भूभाग, जिसको कुछ लोग ‘रेणु इलाक़े’ के तौर पर भी याद करते हैं, की बोली-वाणी और जीवन-जीविका को लेकर अनेक सवालों से घिर जाता हूँ। ऐसी दिक़्क़तें ख़ासकर तब ज़्यादा दरपेश आती हैं जब मैं इसको मिथिला से जोड़कर देखता हूँ। दरअसल मिथिला की जो पहचान मैथिल-पंडितों ने व्याख्यायित-प्रदर्शित की है उसमें यह इलाक़ा उतना फ़िट नहीं बैठता। पारंपरिक मिथिला की छवि में जो एक ख़ास तरह की कुलीनता दिखती है उससे इस इलाक़े की सांस्कृतिक समानता मुझे दूर-दूर तक नज़र नहीं आती। यह उन श्रमिकों का इलाक़ा है जिनके श्रम-कार्यों के साथ गीत-संगीत का एक अलग नाता है जो पूरी तरह लोकधर्मी है। शास्त्रीयता से ज़्यादा महत्व यहाँ लोक को मिला है। यहाँ के जीवन में प्रेम जैसे कोमल भावों का ऊँचा स्थान है, जबकि पारंपरिक मिथिला छूछे आदर्श मूल्यों के आडम्बर को लेकर शिव जी के त्रिशूल पर टिके सत्य की तरह अपनी महानता का राग अलापता रहा है। सिरचन (ठेस), पँचकौड़ी मिरदंगिया, रमपतिया (रसप्रिया), रतनी (नैना जोगिन), जनकदास (एक लोकगीत के विद्यापति!) या हीराबाई-हिरामन (तीसरी कसम) जैसे पात्रों के विचार और उनके हृदय में प्रेम के लिए जो स्थान है, इसके लिए किसी मूल्य-मानक की अपेक्षा हम इस मिथिला समाज से नहीं कर सकते।
मिथिला का जो केंद्र है, वह पंचकोसी की भाषा-संस्कृति को ही शुद्ध मानने की सवर्ण श्रेष्ठतावादी मानसिकता और ग्रन्थि का शिकार रहा है। लगभग हज़ारों साल से। बुद्ध के विचारों पर जहाँ इनके तर्क की सीमा शुरू हुई कि इन्होंने उनको ‘भगवान’ का दर्जा देकर बेअसर करने का प्रयास किया। ‘राड़’ और ‘सोलकन्ह’ जैसे शब्दों के जनक ये लोग ही हैं। ये अपने ही जैसे दक्षिण की तरफ़ के लोगों को ‘दछिनाहा’ या ‘भदेस’ कहकर हिकारत की दृष्टि से देखते रहे हैं। उत्तर के लोगों को ये मोरंगिया-मधेसी समझते रहे और पूरब वालों को ‘पूबा-नकडूबा’ या ‘कोसिकन्हा’ कहने में इन्हें आंनद आता रहा। पश्चिम के प्रति ऐसी कोई उक्ति तो सुनने में नहीं आती है लेकिन अब अपनी बेटी ब्याहने से परहेज करते हैं और वह भी अपनी सर्वश्रेष्ठ बेटी के ब्याह के बाद के परिणाम से। जाति-धर्म को लेकर यहाँ भीषण कट्टरता है। ऐंठकर बोलने और कुलीनता को पालकर रखने में जो मज़ा इन्हें आता वह तो विजया के सेवन के आंनद से भी ऊपर है। ये तमाम लक्षण सामान्य जन से प्रेम के विरुद्ध जाते हैं। इसलिए मिथिला के इस पंचकोसी केंद्र में प्रेम नहीं, व्यभिचार का बोलबाला रहा है। इसलिए प्रेम के नाम पर लुकछिप कर पारिवारिक सम्बन्धों में मुँहमारने के तमाम क़िस्से मिलते हैं। संकेतों को बहुत ग़ौर से देखें तो ज्योतिरीश्वर के ‘धुत्तसमागम’ में भी ऐसे उदाहरण मिल जाएँगे। इस मिथिला भूमि से विद्यापति पहले बड़े कवि हुए जिनकी संवेदना विशाल जनसमूह तक पहुँचती है। तभी तो बंगाल-उड़ीसा क्या, पूरे उत्तर भारत के जनकंठों तक उनकी रचना पहुँची। यहाँ प्रेम भक्ति पर भी भारी है। प्रायः इसीलिए रेणु विद्यापति को बहुत पसंद करते हैं। बारीक़ी से पड़ताल करें तो आप पाएँगे कि रेणु की कहानियाँ ही नहीं, उनके सम्पूर्ण साहित्य में विद्यापति जहाँ-तहाँ ताक-झाँक करते या आते-जाते मिल जाएँगे। रेणु का यह विद्यापति-प्रेम एकदम सहज और घुला-मिला हुआ है। प्रायः इसीलिए रेणु विद्यापति के रागबोध का एक लोकधर्मी कोसी-एडिशन रचने में भी सफल साबित हुए हैं।
मिथिला का वह भूभाग जिसको दरभंगा-मधुबनी वाले ‘पूबा-नकडूबा’ या ‘कोसिकन्हा’ कहते रहे हैं, इसके सवर्णेत्तर समाज के संघर्षशील जनसमुदाय के रागबोध के शिल्पकार रूप में रेणु अन्यतम हैं। यहाँ के जनजीवन में प्रचलित लोक गाथाओं और नाचों से गुज़रते हुए साफ़ दिखता है कि यहाँ प्रेम की समृद्ध परंपरा रही है। गाथा-कथाओं के अनुसार, महासुंदरी कोसी ने जाति बंधन तोड़कर वीर रन्नू सरदार से प्रेम किया था। कोसी के पिता गाधि राजा को यह स्वीकार नहीं हुआ। लोभी राजा ने एक हज़ार श्यामकर्ण घोड़ों के लोभ में धन-वैभव से शक्तिशाली वयोवृद्ध ऋचीक के हाथों बेटी कोसी का सौदा किया। महुआ घटवारिन के साथ भी इसी तरह से धोखा हुआ। एक सिलसिला है। यह सिलसिला रेणु के रमपतिया के बाद भी आज तक की पीढ़ी के साथ जारी है।
कहने का आशय यह कि मिथिला के परिपेक्ष्य में रेणु के समाज और उनके पात्र-परिवेश को विलगा कर देखने की ज़रूरत है। सकल मिथिला से अलग यह एक कोसी परिवेश है जो आज की तारीख़ में ‘कोसी का छाड़न’ हो गया है जिसको राजनेतागण अपनी सुविधा से ‘सीमांचल’ कहने लगे हैं। यहाँ सामान्य जन विद्यापति प्रेमी होते रहे हैं और उनका अलग महत्व भी रहा है। रेणु के ही शब्दों में, “महाकवि विद्यापति पर ‘खोज’ करते समय मैंने अनुभव किया, एक अध्याय का शीर्षक रखना पड़ेगा–‘खेतिहर-मजदूरों और गाड़ीवानों के कवि विद्यापति!’ क्योंकि पूर्णिया-सहरसा के इलाक़े में आज भी विद्यापति की पदावली गा-गाकर–भाव दिखलाकर नाचनेवालों की मंडली पायी जाती है। इन मंडलियों के नायक–भैंसवार, चरवाहे और गाड़ी हाँकनेवाले ही होते हैं, प्रायः। मैथिल पंडितों से पूछा, यह कैसे हुआ? बोले, आप किस फेर में पड़े हैं? इन्हीं मूर्खों के कारण आज विद्यापति की दुर्दशा हो रही है। ऐरे-गैरे-नत्थू-खैरे जिसके जी में जब आया–विद्यापति के नाम पर ‘चार पदावली’ जोड़ दी।… आप गुमराह हो गए हैं!…” (रेणु रचनावली, खंड-1, पृ.-303) दरअसल गुमराह मैथिल पंडित थे जो विद्यापति को भक्ति और श्रृंगार के कवि मात्र बनाए रखना चाहते। वह भी शास्त्रीय ग्रन्थों तक सीमित करते हुए। लोक में जाते ही मानो उसकी शुद्धता ख़तरे में पड़ जाएगी! जबकि रेणु विद्यापति-पदों के लोक-प्रचलन के प्रशंसक रहे हैं। उन्हें ‘विदापत’ लोकनाच वाला रूप इतना पसंद था, कि इसको बचाने के लिए उन्होंने अथक परिश्रम किया। उन्होंने अपने गाँव में इसकी एक मजबूत टीम बनाई। उस टीम के महत्वपूर्ण स्तम्भ रेणु ख़ुद थे। आज जब यह लोकनाच विलुप्ति की ओर जा रहा है तब भी मेरी जानकारी में एक महत्वपूर्ण टीम उनके ही गाँव में बची है जिसको बचाये रखने में उनके पुत्रों, ख़ासकर पद्मपुराग राय ‘वेणु’, का बड़ा योगदान है। चार-पाँच बर्ष पहले इन पंक्तियों के लेखक को भी इस टीम का एक प्रदर्शन देखने का सुअवसर मिला था। ‘रसप्रिया’ के मिरदंगिया को समझने के लिए मेरे ख़याल से उपरोक्त संदर्भ ज़रूरी है। मिरदंगिया भी विदापत गायक है, अपनी टीम का मृदंगवादक और कुछ सीमा तक मूलगैन भी।
मिरदंगिया के जीवन में इस क्षेत्र की बड़ी विडंबनाओं के कई अक्स मिलते हैं। जाति छुपाकर वह जोधन गुरुजी से मूलगैनी सीखने जाता है जहाँ गुरुजी उसको मृदंग धरा देता है। जब वह जोधन की मंडली में शामिल हुआ था तब उसकी बाल विधवा बेटी रमपतिया बारहवें साल में थी और “नव अनुरागिनी राधा, किछु नहि मानय बाधा” गुनगुनाती पर्दे का अर्थ समझने लायक़ हो गई थी। आठ वर्ष तक तालीम पाते मिरदंगिया के साथ ही रमपतिया भी जवान हुई। दोनों के बीच साफ़-साफ़ प्रेम रहा। विदाई के वक़्त जब जोधन गुरु ने स्वजात समझ कर अपनी बेटी के साथ ‘चुमौना’ की बात चलाई तो वह भाग खड़ा हुआ। गुरुद्रोही कहलाया, धोखेबाज कहलाया–लेकिन क्यों? जाति जटिल समस्या है। बीच में अर्थतंत्र है। दोनों का प्रेम खरा है, लेकिन जाति-गणित और अर्थतंत्र बाधक। न मिरदंगिया रमपतिया को भूल पाता है कभी, न रमपतिया मिरदंगिया को।
मिरदंगिया किसी बच्चे को ‘बेटा’ कहते डरता है। परमानपुर में एक बार एक ब्राह्मण के लड़के को उसने ‘बेटा’ कह दिया था। मार खाते-खाते बचा था और ‘बाप’ कहकर माफी माँगना पड़ा था, लेकिन रमपतिया-पुत्र मोहना को वह ‘बेटा’ ही कहता है। मोहना के साफ-शुद्ध पदावली गायन पर वह ताल देता है। मोहना को फारबिसगंज के डागडरबाबू को दिखाकर इलाज करवाने के लिए चालीस रुपए देता है। दवा से जो पैसे बच जाए उसका दूध पीने की नसीहत भी। मोहना से अंत में वह कहता है, “तुम्हारे-जैसा गुणवान बेटा पाकर तुम्हारी माँ ‘महारानी’ हैं, मैं महाभिखारी दसदुआरी हूँ।” मोहना की इतनी प्रशंसा!… मोहना पर मिरदंगिया को इतना प्यार क्यों उमड़ रहा है? क्या सिर्फ़ प्रेमिका-पुत्र होने के कारण? फिर मोहना की बड़ी-बड़ी आँखें उसको कमलपुर के नंदुबाबू की आँखों-जैसी क्यों लगती हैं? रमपतिया से इतना प्रेम तो फिर “नंदुबाबू का घोड़ा रात के बारह बजे को” का आरोप क्या है?….
असल में यहाँ इस समाज के साथ ही नंदुबाबू को भी समझने की ज़रूरत है। विद्वान आलोचकगण उपन्यास की तरह कहानी को समझने के लिए समाज-समीक्षा की ज़रूरत नहीं समझते, लेकिन मेरे ख़याल से रेणु की कहानियों में इसकी गुंजाइश है। इतना ही नहीं, कई बार इनकी एक कहानी का तार दूसरी कहानी से नाभि-नाल-सा जुड़ा भी प्रतीत होता है। कहानी के भीतर कुछ बहुत सूक्ष्म सूत्र हैं। एक तो कमलपुर ‘बाबू लोगों’ का गाँव है, फिर ‘कमलपुर के नंदुबाबू के घराने’ की चर्चा होती है जहाँ मिरदंगिया को ‘चार मीठी बातें’, ‘एक-दो जून भोजन’ और ‘कभी-कभी रस-चर्चा’ मिल जाती। यह नंदुबाबू कौन है?… ज़रा रुकिए, ‘तीसरी क़सम…’ में एक जगह ‘नामलगर ड्योढ़ी’ के राजा का प्रसंग आता है। इसी कहानी पर बनी फ़िल्म में ‘पान खाए सइयाँ हमरो, मलमल के कुर्ते पर छींट लाले लाल’ के दृश्य में एक जमींदार नज़र आता है, मलमल के कुर्ते में। ये राजा और जमींदार नंदुबाबू के ही अलग-अलग रूप नहीं हैं क्या? अन्न-पानी और धन-सम्पत्ति ही नहीं, दूसरे के प्रेम का भी हरण करता रहा है यह परजीवी वर्ग।
रमपतिया रोती है, मिरदंगिया रोता है। प्रेम की गहरी पीड़ा के बीच बहुत कुछ टूटता है। ‘रसप्रिया’ से गुज़रते साफ़ लगता है कि कोसी के ख़रीदार ऋचीक, महुआ घटवारिन के ख़रीदार सौदागर, रमपतिया के लिए रात के बारह बजे घोड़ा भेजने वाले नंदुबाबू से होते हुए हमारे आज के राजा (विधायक, सांसद, मंत्री) तक एक लंबी परंपरा चली आ रही है। दुख की बात कि ऐसे ही लोग फल-फूल रहे हैं और इनके भक्त लगातार बढ़ रहे हैं!…

गौरीनाथ
जन्म : मार्च, 1969, जनपद सुपौल (बिहार) के कालिकापुर गाँव में।
शिक्षा: हिन्दी साहित्य में स्नातकोत्तर।
तीन कहानी संग्रह :’नाच के बाहर’ (2002), ‘मानुस’ (2007) और’बीज-भोजी’ (2017) ‘समय की ख़राद पर’( निबंध संग्रह), ‘प्यार तुम्हारा हक़ नहीं’ और’ मिट्टी की गंध’ (नाटक), ‘दाग’ (उपन्यास- मैथिली), कथा संग्रह’खकसियाह’, ‘भाईसाहेब माने राज मोहन झा’ (संस्मरणात्मक पुस्तक), ‘हिन्दी सिनेमा में हाशिये का समाज’ , ‘भारतीय दलित साहित्य और ओमप्रकाश वाल्मीकि’ और’हिन्दी की चुनिन्दा ग़ज़लें’ (सम्पादित)। पूर्व सहायक संपादक ‘हंस’।
संप्रति : सम्पादक,प्रकाशक -हिन्दी त्रैमासिक’बया’ तथा मैथिली त्रैमासिक’अंतिका’
सम्पर्क : अंतिका प्रकाशन, सी-56/यूजीएफ-4, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन-2, गाजियाबाद-201005 (उ.प्र.)सम्पर्क: antika56@gmail.com