चटाक्…चट्..धा बनाम हड्डियों का कोरस

- अरविन्द कुमार
मई 1943 में बंगाल में भूख से मरने की पहली रिपोर्ट आयी और 1944 में रेणु ने ‘पहलवान की ढोलक’ कहानी लिखी। यह कहानी रेणु की प्रारम्भिक कहानियों में से एक है। वैसे ‘बटबाबा’ जो रेणु की पहली कहानी मानी जाती है, वह भी 1944 में ही लिखी गयी और ये दोनों कहानियां उस समय के अखबार ‘दैनिक विश्वामित्र’ में छपीं।
‘पहलवान की ढोलक’ के केन्द्र में मलेरिया और हैजे से आक्रान्त एक गाँव है। वैसे रेणु के यहाँ कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित अनेक गाँव हैं पर 1944 में मौत का एक बड़ा वाहक भूख से परास्त हो जाना भी था। इस कहानी का प्रारम्भ ही एक ऐसे वाक्य से होता है जो भय और आतंक की सृष्टि करता है। कहानीकार लिखता है – मलेरिया और हैजे से पीड़ित गाँव भयार्त शिशु की तरह थर-थर काँप रहा था। पुरानी और उजड़ी, बांस-फूस की झोपड़ियों में अन्धकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य, निस्तब्धता। सियारों का क्रन्दन और पेचक की डरावनी आवाज कभी-कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती थी। यानी किसे कब मलेरिया और हैजा उठाकर पटक देगा, उसे कोई समझ नहीं पाता था। इस कहानी के पहलवान लुट्टन सिंह को भी इसी बीमारी ने उठाकर वैसे ही पटक दिया था जैसे कभी लुट्टन सिंह ने शेर के बच्चे कहे जानेवाले चाँद सिंह को पटक दिया था। …चटाक्-चट्-धा। पर लुट्टन सिंह का यह मंत्र ‘चटाक्-चट्-धा, गिरधा’ तब काम नहीं आया जब मुकाबला मलेरिया और हैजे से हुआ। पहलवान की जो ढोलक लोगों में जीवन का संचार करती रही, जीवन का मंत्र बनी रही, औषधि बनकर काम करती रही, उसी ढोलक को पहलवान के परास्त होने के बाद जंगली सियारों ने नोंच डाला। पहलवान की जिन जंघाओं पर विजय की थाप पड़ती थी, उसे भी सियारों ने लहुलुहान कर दिया। यानी रात्रि की निस्तब्धता और सन्नाटे को ललकारने वाली ढोलक आखिरकार पराजित हो गयी। पहले अनावृष्टि, फिर मलेरिया और हैजा….पराजय तो निश्चित थी।
रेणु लिखते हैं कि पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, किन्तु गाँव के अर्धमृत औषधि-उपचार-पथ्य विहीन प्राणियों में वह संजीवनी शक्ति भरने का काम करता था। स्पंदन-शक्ति-शून्य स्नायुओं में भी बिजली दौड़ जाती थी। अवश्य ही ढोलक की आवाज में न तो बुखार हटाने का कोई गुण था और न महामारी की सर्वनाश-गति को रोकने की शक्ति ही पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आँख मूँदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी, मृत्यु से वे डरते नहीं थे। इसलिए जब पहलवान के दोनों बेटों को मलेरिया और हैजे ने पटक दिया तो असह्य पीड़़ा से छटपटाते हुए भी उन्होंने कहा था – ‘बाबा! उठा-पटक दो वाला ताल बजाओ!’ …..यानी मौत भले ही आ जाए पर मन से हारना नहीं है। और पहलवान यह जानते हुए कि उसके बेटों की यह आखिरी रात है, सारी रात ढोलक पीटता रहा… ‘चटाक्-चट्-धा चटाक्-चट्-धा ’ और उन्हें उत्साहित करता रहा – ‘मारो बहादुर!’
अकाल और महामारी की इसी 1943-44 की पृष्ठभूमि को लेकर रेणु का एक रिपोर्ताज है – ‘हड्डियों का पुल’ जो उन्होंने 1950 में लिखा था और जो ‘जनता’ के सितम्बर 1950 के अंक में छपा था। इसके केन्द्र में रेणु का अपना इलाका है जहाँ दलितों की बस्ती है और जिसे रेणु जिन्दा लाशों का गाँव कहते हैं। चारों ओर सिर्फ जिन्दा ठठरियां दिखाई पड़ती हैं जो अनाज के कुछ दानों के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। उस गाँव के दबंग और समर्थ इसका फायदा उठाकर उन दलितों पर जुल्म करते हैं। गाँव में अन्न नहीं, काम नहीं। धरती की छाती चीरकर पाताल से अन्न निकालनेवालों को अन्न नहीं मिल रहा है। भूखों की भीड़ बढ़ती जा रही है। जिसके पास अनाज है, वे मजदूरी देकर काम नहीं कराना चाहते। दो-दो फसलों का नुकसान। छोटे हल-बैल वालों और जमीनवालों की हालत खुद खराब है।
चमरू दुसाध प्रार्थना भरे शब्दों में गाँव की पुतोहू भगिया से कहता है- ‘‘बेटी! तुम सिर्फ टहलू की पुतोहू नहीं, गाँव भर की पुतोहू हो। बात यह है कि इलाके में अब न अन्न है और न काम। हम क्या करें? गाँव छोड़ दें? डीह छोड़ दें?….बोल भगवती, बोल भगवती? रास्ता बता, गाँव वालों को उबार!’
भगिया कुरसाहा से आयी है और कम उम्र की होकर भी गाँव भर में सबसे ज्यादा ‘देखी-सुनी’ और समझदार औरत है। चमकीले पीतल का कनफूल पहनती है। पूरे गाँव में उसका सम्मान है और दलितों की बस्ती यह समझती है कि जब तक भगिया है, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसलिए भगिया की झोपड़ी के बाहर गाँव भर की पंचायत बैठती है-औरत, बूढ़े, बच्चे, जवान जहाँ टहलू पागलों की तरह नाच-नाचकर भगिया से गाँव की कुशलता के लिए प्रार्थना करता है। टहलू पर अक्सर दीना भदरी (मुसहरों के देवता) सवार होते हैं।
भगिया खखासकर गला साफ करती है ..‘घर में सात दिनों के लिए ‘करमी’ और ‘सारुख’ है। घटेगा तो एकाध दिन पटुआ साग से भी काम चल जाएगा। दस दिन में अन्न लेकर गाँव लौटना है।’ रेणु लिखते हैं कि अन्न की खोज में कोखजली धरती के लाल बढ़े जा रहे हैं। जहाँ खाना मिले, मजदूरी मिले, जान बचे…। पर अन्न और काम कहीं नहीं है। भूखे थके-हारे, बेजान लोग घर लौट आए हैं। …खाली हाथ! उम्मीद की पतली डोरी भी छूट जाती है। भूख की ज्वाला और तेज हो जाती है, बारह दिनों से ‘पटुआ’ और ‘करमी’ खाकर बस उम्मीद पर जी रहे थे।…और इस उम्मीद पर भी कि भगिया उनकी रक्षा कर लेगी।
पर समझदार भगिया भी यहाँ उसी तरह हथियार डाल देती है जिस तरह लुट्टन ने अपना हथियार डाल दिया था। जब स्थितियां प्रतिकूल हों और गाँव या इलाके की निर्धारक शक्तियाँ मनमानी कर रही हों तो आम आबादी कमजोर पड़ ही जाती है। अनाज की कोई कमी नहीं है पर वह कुछ खास घरों में या कोठियों में कैद है। उन कोठियों से उस अनाज को मुक्त कराने की ताकत किसी के पास नहीं है। ऐसा कोई संगठन गाँवों में नहीं है जो अकाल पीड़ित होकर नहीं बल्कि अपने अधिकार की लड़ाई लड़ते हुए मुक्ति पा ले। पहलवान की ढोलक कम से कम बजती तो है, महामारी से युद्ध का उद्घोष तो होता है पर यहाँ तो मुट्ठी भर मकई के दानों के लिए अपने पुरुषों के सामने ही औरतें बिछ जाती हैं। रेणु के इस रिपोर्ताज में एक ऐसे घृणित समय के दृश्य हैं जो पूरी तरह अमानवीकृत हो चुका है। समर्थ घरानों के सयानों की कौन कहे, बड़े हो रहे बच्चे भी अपना रास्ता भटक चुके हैं और चार मुट्ठी मकई के दाने के सूद के एवज में मुसहर टोली की औरतों के साथ चाहे वे बूढ़ी हो, जवान या बच्ची यौनाचार कर रहे हैं। …वर्दी-पेटी, कोट-पैंट, सुफेद कपड़ों के नीचे का इंसान! कितना बेदर्द, कितना वहशी! …करमी के झुरमुट में भगिया ऐंठ रही है। लोग एक-एक कर ऐंठ रहे हैं। भगिया की आँखें फूलों को देखती है…करमी के फूल, खूबसूरत फूल पर किसके लिए। उन्हें तो बस भूख के डरावने साये दिख रहे हैं। कुरसाहा से आयी पंद्रह साल की बच्ची भगिया के सपने तो मर ही चुके हैं, अब उसका शरीर भी साथ छोड़ रहा है।
देवदूतों की टोली सुफेद टोपी और लाल फीतावाली फाइलों के साथ तैयार है। मोटर बोट, बाढ़ से फैली हुई कोशी की छाती पर, अस्थायी समुद्र की अगम धारा में भड़भड़ाती हुई निकल पड़ती है। सारा भू-भाग पानी में डूबा हुआ, हरियाली का कहीं चिह्न नहीं, फसलों का एक तिनका भी कहीं नजर नहीं आता। भदई धान, मकई, बाजरा कोशी के जल-प्लावन में नष्ट हो चुके हैं तथा हवा के झोंके में जंगलों, फसलों, घोंघों और कीचड़ की सड़ांध मिली हुई है। और ‘देवता’ खोज रहे हैं…कहाँ है अकाल? ‘देवता’ नाव से उतरते हैं। पीछे-पीछे सत्यान्वेषकों का दल!
….‘अगहनू मुसहर कैसे मरा?’
बुढ़िया कांपने लगती है। हाकिम, पुलिस, बाप रे! – ‘हजूर, बेराम रहै।’
सत्यान्वेषकों का दल फिर पूछता है- ‘रामफल कैसे मरा?’
…जवाब मिलता है – ‘हजूर, हमरा कुछ नै मालूम।’
भूख से बेहाल गाँव में भगदड़ मच जाती है। मलेटरी….पुलिस…गोर्रा…बंदूक! ‘देवता’ नाराज हैं। चेहरा तमतमाया हुआ है। बड़बड़ाते हुए कह रहे हैं- ‘हुं, हल्ला मचा दिया…अकाल का तांडव-नृत्य….लोग मर रहे हैं। अकाल की बात करने वाले गद्दार हैं।’ …सब गलत…एक गद्दारी सत्य। …सत्य, अहिंसा, गाँधी जी और रामराज की छाती को कुचलती हुई गश्ती चिट्ठी चक्कर मारती है।…अकाल की बातें मत करो। मौतें हुईं हैं मत बोलो। यानी सत्य, अहिंसा, गाँधी और रामराज्य जैसे शब्द अपना अर्थ खो चुके हैं।
रेणु लिखते हैं – पत्रकारों की टोली मुँह फाड़कर देखती है, कान खोलकर सुनती है और अवाक् रह जाती है। केन्द्रीय खाद्य मन्त्री धीरे-धीरे अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं….चेहरे पर कहीं शर्म की कोई रेखा नहीं। आश्चर्य! इतना भीषण झूठ बोलकर भी आदमी निगाहें उठाकर देख सकता है!…केन्द्रीय संसद में, इंद्रप्रस्थ में, प्रजातन्त्र के पवित्र पाए पर टिकी हुई इमारत में भी – ‘नरो वा कुँजरो’ की पुनरावृत्ति होती है, और ताज्जुब, वह इमारत जरा भी न हिली, न डुली…। दूसरी ओर चौथे खंभे का गोदी मीडिया भी सरकार के समर्थन में खड़ा है। देवदूतों की बोलियाँ बदल गयी हैं। पवित्र राष्ट्रीय पूँजी प्राप्त पत्रों की वाणी मूक हो गयी है। पुछल्ले पत्रों के हेड लाइन बदल जाते हैं और केन्द्रीय मन्त्री की वाणी सामने आती है – ‘अकाल की सारी बातें निराधार हैं।’ ….बिल्कुल वही गोदी मीडिया आज उसी रूप में दिखाई दे रहा है जहाँ वह दिन-रात सत्ता का गुणगान कर पूँजी बटोरने में लगा है।
कोशी की प्रलयंकारी बाढ़ में आखिर कौन मरता है? कोशी के धूसर अन्नविहीन अंचल में किसकी मौत होती है? वही जिसे सत्ता या राजनीति किनारे कर देती है। उसे उसकी परवाह नहीं होती। सत्ता को यह भी पता होता है कि उस आबादी को अपने वश में करना बहुत आसान होता है। यदि वह हाशिए पर और उसमें भी बहुत नीचे है तो उसे थोड़ी सी सुविधा देकर कभी भी अपनी तरफ किया जा सकता है। रेणु के पात्रों की दुनिया बहुत ही सरल है। जिन्होंने सबकुछ पहली बार देखा है, उनके लिए वहाँ किसी विशेष संकल्पना का सवाल ही पैदा नहीं होता। जिसे कोई भी परिवर्तन उसकी जिन्दगी का बाधक तत्व लगता है वह तो वैसा ही कहेगा जैसा कि नौजवान गोरखू मुसहर कहता है – ‘रेलगाड़ी ! साला रेल नहीं होता तो अपने मुलुक का चावल, धान, मकई दूसरा मुलुक जाता!’ या वह इतना सरल होगा जैसा कि बूढ़ा तेतर जो पुल और गाड़ी की बंदगी करते हुए कहता है – ‘काली माई है।… जय गाड़ी जी! जय पुल जी! जय सरकार बहादुर! सरकार के आग-पानी का खेल है यह गाड़ी।’…गाँव के सामंतों और पूँजीपतियों के सहारे संसद या विधान सभाओं में पहुँचनेवाले प्रतिनिधि जनता की ऐसी ही सरलता और नादानी का फायदा उठाते हैं और अपनी कोठियां भरते हैं। एक आजाद देश में यदि अकाल, भुखमरी और रोग से लोगों की अकाल मृत्यु होती है तो यह बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। लेकिन रेणु के यहाँ यह आम बात है। उनके इलाके हमेशा अकाल, भुखमरी और रोग की गिरफ्त में होते हैं और इनसे मुक्ति का कोई भी साधन कभी भी सामने नहीं आता। इसीलिए रेणु की कथा-भूमि में एक नैराश्य भाव भी दिखाई देता है। भले ही सेठ कुन्दनमल की थुलथुल देह का रोम-रोम पुलकित हो रहा हो और कह रहा हो- ‘आ रही है, लक्ष्मी आ रही है। ये एक बोरो चावल नहीं, मोती के दानो हैं दानो!’ हमारा देश आजाद तो हो गया पर अन्न उत्पादन को लेकर नीतियाँ नहीं बन पायीं। सूखे, बाढ़ और महामारी से लड़ने का कोई तरीका विकसित नहीं किया जा सका। देश को राजनीतिक आजादी दिलाने में सारी-शक्ति लगी पर आन्तरिक विपत्तियों का मुकाबला कैसे करना होगा इस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया।
अब जब सब कुछ प्रतिकूल है तो पुराने काँग्रेसी और सोशलिस्ट शोभित बाबू भी क्या कर सकते हैं। यह करना आसान भी नहीं है क्योंकि जब किसुनपुर के गंभीर बाबू अपनी हवेली बन्द कर लें तो भूख से दम तोड़ रहे ये लोग कहाँ जाएं। रेणु लिखते हैं – ‘किसुनपुर कोठी! पूर्णिया के सबसे बड़े काश्तकार…गंभीर बाबू की हवेली….राजदरबार…अनाज के बखारों की कतार…लक्ष्मी यहाँ बिराजती हैं।’ जिनके पास पचास से भी ज्यादा कामत हों और हरेक कामत पर औसतन बीस हजार मन से भी ज्यादे धान होता हो…वहाँ अन्न नहीं? तो फिर कहाँ होगा अन्न? जिले के विशाल भू-भाग पर जिनके पुराने ‘हल’ से लेकर ट्रैक्टर तक चलते हों…वहाँ अन्न नहीं? तो आगे बढ़ना बेकार है।
कोशी की फैली हुई गंदली जलराशि पर डूबते सूरज की रोशनी पड़ती है…लहू का समुंदर! दिशाएं धुंधली हो रही हैं। कुरसाहा से चार मील उत्तर चन्ननपट्टी दियारा पर अर्धमृतकों की टुकड़ी खड़ी है। ….भोर और शाम, दिन और रात, भूख और अन्न से परे मुसाफिरों के जीवन में कभी भोर हुआ ही नहीं। …प्रांत पर अकाल का काला पंजा, पूर्णिया और सहरसा में अन्न के बिना रोज मौतें हो रही हैं।
भगिया अपने ‘पुरुख’ को देखती है जो हड्डियों का ढाँचा लेकर लौटा है। कुछ ही दिन पहले इसकी बाहों की मांसपेशियां कैसी उभरी हुई थीं। राक्षस की तरह ताकत थी बाहों में पर उन बाहों ने अब हथियार डाल दिये हैं। कभी इसी पुरुख पर उसे बहुत नाज था। जाहिर है, उसके भीतर बहुत सारी इच्छाएँ भी होंगी। सपने भी होंगे जो उसने इस पुरुख को लेकर देख रखे होंगे। पर अब चार माह की गर्भवती भगिया सोचती है, यह उसका ‘पुरुख’ नहीं, पुरुख का पिशाच भले ही हो।
‘पहलवान की ढोलक’ का लुट्टन भी तो अब ‘पुरुख’ से ठठरी बन गया है। उसके भीतर भी अब इतनी ताकत नहीं थी कि वह मरते समय भूखे सियारों को अपनी जंघाओं से हटा सके। लुट्टन जाति का दुसाध है। हड्डियों का पुल’ का चमरू भी दुसाध है जबकि टहलू, अगहनू मुसहर हैं। ये जातियाँ जीवन-संग्राम में हारना नहीं जानतीं। धरती की छाती को चीरकर पाताल से भी अन्न निकाल सकती हैं। पर पाताल में भी अन्न नहीं है। ये रोग और भूख से लड़़ना भी जानती हैं पर कब तक? चटाक्…चट्…धा जीवन जीतने का एक मंत्र तो हो सकता है पर जब हाथ ही कमजोर पड़ जाए तो थाप कौन देगा? जब तक अन्न था और रोग नहीं था तब तक तो ढोलक बजती रही पर जब अन्न छिन गया और रोग ने आक्रमण कर दिया तो मंत्र पराजित हो गया। राजा साहब के दरबार में पंद्रह वर्षों तक पहलवान की हुकूमत रही पर समय बदला तो राजा साहब के पुत्र ने एक पहलवान को पालना बेवकूफी समझा और उसे छुट्टी दे दी। दिन अकाल और रोग के थे ही, जैसे ही राजदरबार से अपने दोनों बेटों के साथ निकलकर लुट्टन बाहर आया, समय की जकड़न में उलझ गया। राजपंडित जिसने मुँह बिचकाया था कि एक दुसाध को ‘सिंह’ की उपाधि कैसे दी जा सकती है, वह तो राजदरबार में बना रह गया पर लुट्टन ने अपनी जाति का दंश झेला। जैसे चमरू, टहलू, अगहनू, गोरखू, तेतर, रामफल और भगिया ने झेला।
….रहिकपुर और चन्ननपट्टी के बाबू लोग तो चाँदनी रात में उस काले जल में भी नौका-विहार करते रहे और संगीत का आनन्द लेते रहे। हारमोनियम, तबला और बाँसुरी से जीवन में राग भरते रहे पर बाकियों के जीवन में राग कहाँ था? बाकी के लिए तो अकाल था, रोग था और मौत थी। यह मौत 1944 से 19़50 के बीच रेणु द्वारा लिखी दो अन्य कहानियों में भी है जहाँ जीवन हारता हुआ दिखता है। 1945 में लिखी गयी कहानी ‘प्राणों में घुले रंग’ में भी भूख और हैजा है और लोगों को बचाने के साधनों की कमी है। उस समय तक गाँवों या सुदूर अंचलों में स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है, न ही कोई डाॅक्टर सामन्यतः अपना दवाखाना स्वतन्त्र रूप से चलाने की बात सोचता है। यदि सोचता भी है तो उसे चलाना एक चुनौती की तरह है। जैसे ‘प्राणों में घुले रंग’ में जब एक डाक्टर अपनी माँ की स्मृति में अपने गाँव में एक स्वास्थ्य केन्द्र या दवाखाना खोलता है और गाँव में रुकना चाहता है तो उसे गरीबों का पक्षधर होने के कारण वहाँ के जमींदार द्वारा लांछित कर भगा दिया जाता है। इसी तरह 1947 की कहानी ‘इतिहास, मजहब और आदमी’ का गाँव भी हैजे और मलेरिया से आक्रांत है जहाँ जमींदार का बेटा मनमोहन बहुत मुश्किल से एक मेडिकल कैम्प स्थापित करवा पाने में सफल होता है। हालाँकि वह काफी नहीं है और उसके होते हुए भी रुकिया का परिवार काल का शिकार हो जाता है।
इसलिए ‘हड्डियों का पुल’ के अन्त में रेणु अपने को एक पात्र राजेन के बहाने कुछ कहने से रोक नहीं पाते। यह छोटे किसान का बेटा राजेन भी उन्हीं की तरह प्रगतिशील मानवतावादी है, जिसे पूर्णिया के अकाल ने कमजोर कर रख दिया है। वह पिछले कई वर्षों से अकाल और महामारी को झेल रहे अपने क्षेत्र की पीड़ा से दुखी है और चाहता है कि राजसत्ता इसका कोई स्थायी निदान खोजे। जाहिर है कि इसके लिए शासन के पास एक संवेदनशील मन चाहिए। हालाँकि रेणु का मन इसकी ओर से आश्वस्त नहीं है। इसीलिए राजेन अपने एक मित्र शशांक से जो जनता अखबार में कॉलम लिखता है, पत्र के बहाने कहता है – ‘शशांक, तुम्हारे नृत्य के विशेषज्ञों ने मृत्यु का नंगा नाच नहीं देखा है। तुम्हारे कवि ने भूख से दम तोड़ते हुए इंसान के बेजान और पुरदर्द नगमें को नहीं सुना। तुम्हारे चित्रकार, मुर्झाए हुए चेहरे पर बुझती हुई आँखों को नहीं आंक सकते। तुमने मृत्यु-संगीत के कोरस को नहीं सुना है।….तुम्हारे रंगमंच पर हड्डियां बिखर रही हैं – यह तुम्हें नहीं मालूम। हाँ, मैं देख रहा हूँ। इन बिखरी हुई हड्डियों को बटोरकर कोषी डैम नहीं, कम-से-कम कोशी पर एक विशाल पुल तैयार किया जा सकता है। पूँजीवादी समाज के इंजीनियरिंग विभाग का नया नमूना।
…चंद महीनों के बाद ही सारे जिले में बंगाल से भी भीषण अकाल का महातांडव-नृत्य शुरु हो जाएगा। और उस महानृत्य की पृष्ठभूमि से- मैं आशा की चमक-क्रांति की चिनगारी को निकलते देखता हूँ। इस बार नरमेध यज्ञ के कुंड से महा-बवण्डर फूटेगा।’ ….यहाँ अकाल के महातांडव से क्रांति की चिनगारी प्रकट होने की जो बात रेणु कह रहे हैं वह शायद इसलिए कि 1950 में 26 जनवरी को भारत का अपना संविधान बना और भारत गणतन्त्र हो गया। और इस स्वतन्त्र गणतन्त्र भारत में इतनी अपेक्षाएं तो होनी ही थीं कि वह संप्रभुता की देखभाल के साथ-साथ देश की जो हाशिए की आबादी है, उसकी भी रक्षा करेगा। और जब ऐसा कुछ होता नहीं दिखा तो रेणु ने वहाँ क्रांति के बीज बोने की बात रख दी। जाहिर है कि संविधान बनने के बाद भारत को अपनी सारी पुरानी नीतियाँ बदलनी थीं और थके जनमानस में आशा का संचार करना था। शायद इसीलिए रेणु क्रोधित थे और नछत्तर मालाकार को अपने भीतर जीवित रखना चाहते थे। आखिरकार उन्होंने उसे आगे चलकर चरित्तर कर्मकार के रूप में सृजित भी किया ताकि बुझते अँधेरे जीवन में फिर से रोशनी का संचार हो सके।

लेखक तिलका माँझी भागलपुर विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष हैं।
सम्पर्क- +919934665938, arvind.kr.bgp@gmail.com
502, महेश अपार्टमेंट, बड़ी खंजरपुर, भागलपुर- 812001



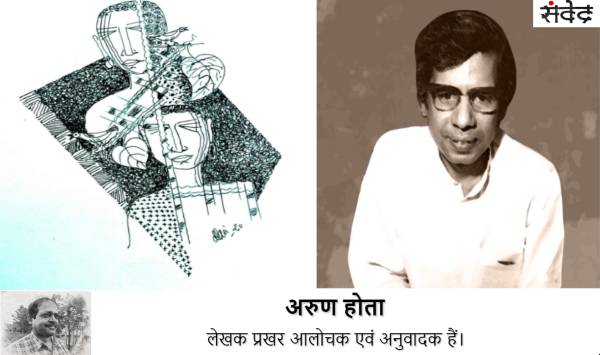






[…] […]