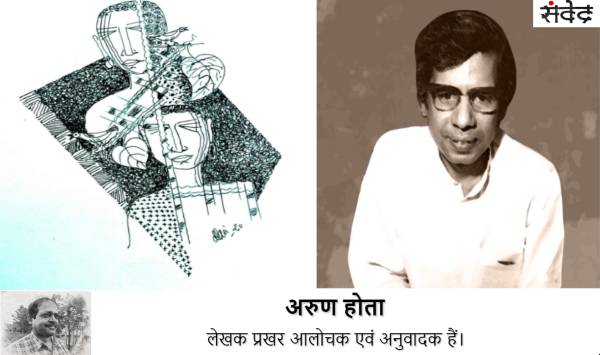प्रेम की चाह और व्यवस्था का शास्त्र

(तीसरी कसम अर्थात मारे गये गुलफाम)
‘तीसरी कसम उर्फ मारे गये गुलफाम’ कहानी का हिरामन रह-रह कर मन के द्वार पर दस्तक दे रहा है।
‘क्या हीराबाई से मिलीं तुम कभी? मैं तो अपनी कसम की जकड़न में इतना बंध गया कि स्त्री क्या, उसके साए से भी दूर रहा जिन्दगी भर। अब उम्र की आखिरी बेला में … जी चाहता है एक बार उसका सुमरन करूँ। दरस-परस तो बीते जुगों की बात हो गयी है शायद।’
मैं 21वीं सदी के कोरोनावायरस मुक्त भारत की सन्तान! हड़बड़ी और बदहवासी में आसपास बिखरे सौन्दर्य और नियामतों से नजरें चुराकर पता नहीं किन अ-दीखते गन्तव्य की ओर भागते रहने की फिराक में। मितभाषी के संकोच को समझने की संवेदना और धीरज कहाँ हम इलेक्ट्रॉनिक युग के बाशिन्दों में? चाहा, थोड़ा रुक कर पूछ लूँ – कौन सी हीराबाई भाई? फिल्म वाली या कहानी वाली? लेकिन चुप लगा गयी। अब कौन इससे मत्था मारे कि फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी को उनकी सजग चौकन्नी देखभाल में बनी फिल्म ‘तीसरी कसम उर्फ मारे गये गुलफाम’ ही खा गयी है। या शायद कौन जाने हिरामन फिल्म वाली हीराबाई को ही खोज रहा हो – प्यार-व्यार की दो तरफा सुगबुगाहटें तो वहीं शुरू हुईं थीं न?
‘ सुनो भाई!’ मैंने पलट कर हिरामन को आवाज देकर करीब बुलाना चाहा तो देखा, गुमसुम सा वह लम्बा फासला तय कर आवाज़ की जद से बाहर चला गया है।
चौंक कर कलम परे रख देती हूँ, रेणु की क्लासिक कहानी ‘तीसरी कसम उर्फ मारे गये गुलफाम’ पर संजीदगी से लिखने की बजाए यह मैं किन फन्तासियों के बचकाने सफर पर निकल आयी हूँ? एलिस बन्ना आसान है, लेकिन हर बार किसी वंडरलैंड में जाकर दुनियवी विद्रूपताओं को समझना आसान नहीं। लेकिन मेरी उलझन अपनी जगह अडिग-अडोल है। लाख हड़काने पर भी वही एक सवाल बार-बार – कौन सी हीराबाई को तलाश रहा है हिरामन? मैं सिर झटक कर सवाल का सिरा ही उलट देना चाहती हूँ – कहानी का नायक तो हिरामन है। फिर हीराबाई के इस या उस रूप में होने से उसकी कहानी पर क्या असर पड़ता है? लेकिन फर्क तो पड़ता ही है – हिरामन की नियति पर भी; और उससे ज्यादा लेखक की मंशा पर भी कि क्या कहानी उन्हें अधूरी लगी जो फिल्म में ज्यादा मानीखेज, ज्यादा प्रत्यक्ष, ज्यादा व्यापक कर वे हिरामन के बरक्स हीराबाई को नहीं, अभागी स्त्रियों की समूची जमात को ले आए?
फणीश्वर नाथ रेणु प्रेमचंद की तरह जमीन और मिट्टी से जुड़े हुए रचनाकार जरूर हैं, लेकिन प्रेमचंद की तरह समसामयिक मुद्दों और समस्याओं से जूझ कर उन पर अपनी निश्चित राय/ समाधान देने की हड़बड़ी उनमें बिल्कुल नहीं। वे कलम के मजदूर नहीं, रंगरसिया हैं। कलम को होठों से लगाकर उसमें रस-प्राण फूंक देते हैं – इतना कि मिट्टी का कण-कण अपनी तमाम भूख-प्यास, अमृत-खजाना लेकर उस में घुल-मिल जाता है; और मानुष के अंतर का राग अपनी हूकों और ख्वाहिशों के संग फूट आता है। इसलिए रेणु के यहां ‘पल‘ महत्वपूर्ण है। पल वक्त की कोख से छिटक लय-भंग का कतरा नहीं होता, वक्त की निरंतरता में किसी एक अनुभूति के सघन होकर स्वत: ही अभिव्यक्त हो जाने की मुखरता है। फलत: उनके साहित्य में समाज के पुनर्सृजन के बड़े-बड़े दावे और वादे नहीं हैं, अपनी स्वत:स्फूर्तता में अनायास बहता अकृत्रिम जीवन है – पहाड़ी दरिया में बहती किसी स्फटिक जलधार सा। रेणु अपने पात्रों को उंगली पकड़कर किसी महायात्रा की ओर नहीं ले जाते। उनके अनिर्दिष्ट सफर में कुछ पल संग चल कर अलग हो जाते हैं। इसलिए उनकी कहानियां व्यक्ति के अंतर्मन की मनोरम मार्मिक झांकियां प्रस्तुत करती हैं, अपने निश्चित काल-खंड का ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं बनतीं। न ही उम्मीद से बंधे किसी बुद्धिजीवी पाठक को उम्मीद बंधाती हैं कि आगे बढ़ कर अपने अंतिम पाठ में वे समय का विधान रचने वाली अमूर्त सुगबुगाहटों को मूर्तिमान करेंगी। मनुष्य की सोच और गतिविधियां, क्रियाकलाप और प्रतिक्रियाएं जितनी नैसर्गिक दिखती हैं, उतनी ही वे दरअसल सामाजिक-सांस्कृतिक, राजनीतिक-आर्थिक विधि-विधानों से बँधी होती हैं रस-लोलुप पाठक को रेणु आनंदमग्न होने की प्रतीति देते हैं तो बुद्धिजीवी के सामने उच्छ्वास में एक सवाल बाँध कर धर देते हैं – सोचो, विश्लेषण करो, और देखो कि सभ्यता-संस्कृति को हम सब किस राह की ओर ठेल रहे हैं? कि अपने सम्भावित गन्तव्य की ओर जाती इस महायात्रा से क्या हम संतुष्ट हैं?
जाहिर है अपनी ऊपरी परत में ‘तीसरी कसम’ भी भावप्रवण कहानी है, किसी बौद्धिक आडंबर या बहस का आयोजन नहीं। लेकिन मैं देर तक इस सवाल से जूझती रहती हूँ कि संवेदनाओं पर ठंडा फाहा रखने के बाद क्या साहित्य का लक्ष्य उन छोटे-छोटे जख्मों को कुरेद देना नहीं है जिन पर मलहम लगाने की बाध्यता आन पड़ी? रेणु अक्सर यही करते हैं। मुखर भाव से नहीं। चुपचाप! वह भावोच्छ्वास में गूंध कर अपने चरित्रों को गढ़ते जरूर हैं, लेकिन उनके भीतर अनुभव और बेबसी से तीक्ष्णतर हुए सवालों को भी पिरोते चलते हैं। सवाल हर हाल में व्यक्ति (लेखक) की अपनी वैचारिक प्रतिबद्धताओं के खूंटे ही हुआ करते हैं। जैसे ‘ठेस’ कहानी सिरचन के आत्मसम्मान और वत्सल हृदय की कहानी न रहकर अपनी प्रस्थान-यात्रा में भारतीय समाज की हायरार्कीकल संरचना का परिचय देने लगती है जहां जाति और व्यवसाय के साथ पैसा और प्रतिष्ठा जोड़कर पावर पॉलिटिक्स के दुर्ग खड़े किए जाते हैं। तब सिरचन का होना क्रूर व्यवस्था का प्रतिलोम रचते स्वप्न को धरती पर उतार देने का आह्वान बनकर आता है।
इसलिए ‘तीसरी कसम उर्फ मारे गये गुलफाम’ कहानी पर दो दृष्टियों से विचार करना चाहूँगी। एक, क्या यह सचमुच प्रेम-कहानी है, जैसा कि परंपरागत आलोचना मानती रही है? दूसरे, यदि हां, तो प्रेम में मिलन की बजाए वियोग को इतनी तरजीह क्यों दी जाती है? इन सवालों के उगने का कारण बहुत स्पष्ट है। मेरी पुरानी ऑब्जर्वेशन है कि प्रेम कहानी में और जो भी हो, प्रेम नहीं होता … कि बंजर भारतीय समाज में प्रेमांकुरण की स्थितियां बेशक बन जाएं, आबोहवा में नमी और ताप के सही मिकदार की कमी उसे पल्लवित-पुष्पित होने से पहले ही मुरझा डालती है।
1
मैं अपनी नजर हिरामन पर केंद्रित करती हूँ। दरअसल कहानी कही भी उसी के जरिए गयी है, और कही भी उसी के लिए गयी है। उसके मन में पलती अबूझ गांठों, सपनों, स्वर-लहरियों को निगूढ़ खामोशी के साथ सुनने के लिए। ख्याल रहे कि रेणु के यहां खामोशी सन्नाटे की मांग नहीं करती। वह बातचीत की चपल तरंगों के बीच चुपचाप अपनी अंतर्यात्रा तय करती चलती है – समानांतर भाव से। ठीक वैसे, जैसे ‘लाल पान की बेगम’ कहानी में तमाम रूठने-अबोले-उलाहने और मंगलकामना के बीच जंगी की पतोहू को गहरे सख्य भाव के साथ मेला ले चलने का औचक निमंत्रण!
बेखबरी में जीता है हिरामन। हीराबाई और लेखक दोनों की नजर में वह सचमुच हीरा है। ‘चालीस साल का हट्टा-कट्टा, काला कलूटा देहाती नौजवान …। अपनी गाड़ी और बैलों के सिवाय दुनिया की किसी बात में विशेष दिलचस्पी नहीं लेता।’ शिशु सुलभ निश्छलता और वैसी ही निष्कपट चपलता …। होरी सरीखा यह संतोषी जीव भारत की ग्रामीण संस्कृति का जीता जागता प्रतिरूप है जिसके लिए पाप पुण्य, सत-असत का मामला जितना गंभीर है, उतना ही सरल है आड़े वक्त में झूठ बोल कर खाल बचाना। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाय, ना मैं भूखा आप रहूँ साधु न भूखा जाए – कबीर दर्शन ग्रामीण संस्कृति की फक्कड़मिजाजी है। हिरामन गांव-देहात के युवकों जैसा है जो अपने बंद दायरों में जीते हुए न दुनिया को जानने की लालसा रखता है, न दुनिया को पलटने की महत्वाकांक्षा। लीक ही उसकी मर्यादा है, और लीक ही उसका गन्तव्य।
रेणु जब ऐसे हिरामन को कहानी का नायक बनाते हैं तो एक साथ दो स्तरों पर उसके विशिष्टता को बनाए रखते हैं। हिरामन संवेदनशील, दिलेर और कर्मठ युवक के रूप में अपनी निजता अंत तक बनाए रखता है, और औसत भारतीय युवक का प्रतिनिधित्व करता हुआ प्रेम के संदर्भ में भारतीय दृष्टि के वैशिष्ट्य को समझने का आग्रह भी करता है।
भारतीय संस्कृति में भले ही कितनी प्रेम-कथाएं हों, भारतीय समाज में प्रेम वर्जित फल है। ऐसा फल जो ऋतु आने पर फूलता है, गमकता है, अपनी गंध से युवा हृदय को मदोन्मत्त करता है, लेकिन अपेक्षा की जाती है कि आत्म संयम की लगाम कसकर वह निष्काम बना रहे। स्त्री के लिए यदि प्रेम पाप है तो पुरुष के लिए प्रिय से दूरी बरतकर ब्रह्मचर्य को बनाए रखना जीवन का सबसे बड़ा तप- पुण्य। प्रेम की जितनी भी स्वीकृति है, वह स्वकीय प्रेम के रूप में है, अथवा उसका उदात्तीकरण कर उसे अशरीरी प्लैटोनिक रूप दे दिया जाता है। परकीय प्रेम आज भी वर्जना के इलाके में पलने वाली कोई छुईमुई सी पोशीदा अनुभूति है।
“ उसकी गाड़ी में फिर चंपा का फूल खिला उस फूल में एक परी बैठी है हिरामन के मन में कोई अजानी रागिनी बज उठी। सारी देह सिरसिरा रही है।”
क्यों हिरामन? तुमने तो गाड़ी में बैठी जनाना सवारी को देखा तक नहीं, फिर क्यों सारी देह सिरसिराने लगी? प्रेम क्या ऐसी एकल एकांतिक अनुभूति है कि दूसरे की जीवंतता और साहचर्य का अनुभव किए बिना मन-प्राण में काम का ज्वार बनकर छा जाती है। न, हिरामन! यह प्रेम नहीं, देह में दमित सेक्सुअलिटी का जोर मारना है। प्रेम में काम अंतर्भूत रहता है, लेकिन काम का ज्वार ही प्रेम नहीं है।
हिरामन के लिए गरब करने की सबसे बड़ी पूंजी यही ब्रह्मचर्य है जो एक ओर लंगोट कस कर दंड पेलने में अपनी अतिरिक्त ऊर्जा की निकासी पाता है तो दूसरी ओर स्त्री की छाया से भी दूर रहने की जुगत में स्त्री को मनुष्य न मान मायाविनी (देह, पत्थर, चुड़ैल, परी) समझने का दुराग्रह पाल लेता है। इसलिए अचरज नहीं कि सात साल से नियमपूर्वक मेले की लदनी ढोने वाले हिरामन और उसके मित्रों ने न कभी बाइस्कोप देखा है, न बाईजी का नाच। उल्लेखनीय है कि भारतीय परंपरा ब्रह्मचर्य को इतना महिमामंडित करती रही है और उसी परिमाण में स्त्री-जीव को नरक का द्वार कहकर इतना दुरदुराती रही है कि इन भोले-भाले युवकों को पता ही नहीं चलता, वे कब परंपरा-पोषित मिथ्या छवियों के शिकार होकर जिन्दगी के प्रवाह और यथार्थ से दूर होते गये हैं। जिन्दगी के ताप को स्वयं अपनी त्वचा पर महसूस किए बिना उन्हीं बोली-बनियों को दोहराते चलते हैं जो शास्त्र-विधानों ने उन्हें दी हैं, और इस प्रकार परंपरा के विकास को ऊर्ध्वाकार रेखा का रूप देने की बजाय वर्तुलाकार परिधि में घूमते रहने की नियति को विकास का मानदंड बताते चलते हैं। प्रश्नाकुलता रूढ़िवादी सोच का प्रतिकार करने का सबसे प्रभावी औरजार है, लेकिन हिरामन और उसका सजातीय वर्ग अपनी वैचारिक जड़ता में इतना निमग्न है कि स्थिति को जस का तस स्वीकार करता चलता है। प्रश्नाकुलता के लिए जरूरी है खुली चौकस दृष्टि; यथार्थ/स्थिति का संज्ञान; उसका विश्लेषण; उसकी भीतरी जड़ता और सड़ांध को दूर करने की व्याकुलता; यथार्थ का अतिक्रमण करने की दृढ़ इच्छाशक्ति। हिरामन की बाल-सरलता युवा-शक्ति की प्रश्नाकुल ऊर्जा को स्याही-सोख्ता के समान चूस डालने को अभिशप्त है। वह स्त्री ‘पदार्थ‘ को कुल पांचरूपों में जानता है। एक, मां के रूप में, जहां भाभी-बहन-बेटी और नाते रिश्ते की स्त्रियां अपनी निजता खोकर मातृरूपा पहचान के साथ उसकी कल्याणमयी देखभाल में उपस्थित रहती हैं। दूसरे, पत्नी जिसके साथ गृहस्थी चलाने का संयुक्त दायित्वपूर्ण अभाव भार संभालना वह नहीं जानता। अलबत्ता स्वामित्व के चाबुक से गाड़ी हांकने का अधिकार जरूर विरासत से आता है। स्त्री इस रूप में उसकी निजी संपत्ति है और उसके पौरुष के अहम को सहलाने का जरिया भी। तीसरे, देवी के रूप में जिसे उसने साक्षात देखा नहीं है, लेकिन परंपरा ने काल्पनिक मूर्ति गढ़ कर उसे विश्वास दिलाया है कि वह सर्वशक्तिमान है, वरदायिनी है। अतः उसका कृपाकांक्षी होकर जीवन के सुखों को पाया जा सकता है। इस मूर्ति के समक्ष वह नतमस्तक हैं, निरीह है, याचक है। चूंकि यह स्त्री समाज में है ही नहीं, अतः इसके समक्ष अपने करबद्ध उपस्थिति को लेकर उसे शर्मसार होना नहीं पड़ता। चौथे, वेश्या के रूप में, जिसके साथ उसके संबंध खासे चुनौतीपूर्ण है। दरअसल यही एकमात्र स्त्री है जिसे वह पा भी लेना चाहता है, और समर्पित भी हो जाना चाहता है। यह स्त्री उसके भीतर प्रेम की दबी हुई आग को भड़काती है, उस आग को शांत करने का अवसर सुलभ कराती है, और काम-पिपासा शांत हो जाने के बाद खरीदी हुई चीज के रूप में उसकी घृणा और हिंसा का शिकार बनती है। पांचवें, डायन के रूप में, जिसे समाज-विरोधी आचरण के कारण दंडित करने का पुण्य कार्य उसे करना है। वह कभी सवाल नहीं उठाता कि परंपरा द्वारा उपलब्ध कराई गयी आचार-संहिताएं किसी की जीवंतता के मूल्यांकन का आधारभूत मानदंड क्यों बनें? कि क्यों बस्ती के बाहर चुपचाप अपने कर्मयोग में लीन उस डायन को मार दिया जाए जो गाहे-बगाहे दवा या ज्ञान के सहारे आपदा में फंसे बस्ती वालों की मदद कर रही है? या क्यों वेश्या को भोग कर दुत्कारा जाए जो कभी गृहस्थी की चारदीवारी के भीतर बेटी-बहन-पत्नी भूमिकाओं में जीवन जीती रही है? वह सवाल करने लायक संवेदनशील व्याकुलता अपने भीतर नहीं पाता कि कौन स्त्री को वेश्यालय तक लाता है? कि कौन वेश्यालय तक आ गयी स्त्री के लौटने के सारे द्वारों को कील देता है? अपनी सरलता में देह की ताकत मिलाकर वह दो ही काम कर सकता है – अपनी ‘बाई जी‘ की ‘पवित्रता‘ के प्रति निश्चयात्मक होना (यानी यौन शुचिता की अवधारणा को मजबूत करना), और दूसरे प्रोटेक्टिव होकर उसकी सेक्सुएलिटी की ओर टकटकी लगाने वाले पुरुष समाज से भिड़ जाना ( यानी पुरुष की श्रेष्ठ रक्षक स्थिति का स्वीकार)।
‘तीसरी कसम उर्फ मारे गये गुलफाम‘ प्रेम की नहीं, प्रेम के प्रति उद्दाम आकर्षण की कहानी है जो अपनी गूढ़ संरचना में पुरुष मानस के भीतर सेक्सुअलिटी की गांठों को खोलने/समझने की तमन्ना रखती है। जाहिर है यह पड़ताल पितृसत्तात्मक व्यवस्था की संरचना और स्त्री-पुरुष संबंध के ताने-बाने को समझने की संवेदना पाठक तक संप्रेषित करना चाहती है।
मैं एक-एक कर कहानी से तीन दृश्य सामने रखना चाहती हूँ। पहला दृश्य उस समय का है जब घाट पर स्नान के लिए हिरामन गाड़ी रोकता है और हीराबाई की अनुपस्थिति में उसके बिछावन को छूता है। छूने की यह क्रिया ऐसी मानो स्वयं हीराबाई को छू रहा हो।
“हीरामन टिकटी पर टिकी गाड़ी पर बैठ गया। उसने टप्पर में झांक कर देखा। एक बार इधर-उधर देख कर हीराबाई के तकिये पर हाथ रख दिया। फिर तकिये पर केहुनी डाल कर झुक गया, झुकता गया। खुशबू उसकी देह में समा गयी। तकिये के ख़िलाफ़ पर कढ़े फूलों को उंगलियों से छूकर उसने सूंघा। हाय रे हाय! इतनी सुगंध! हिरामन को लगा, एक साथ पाँच चिलम गांजा फूंक कर वह उठा है। हीराबाई के छोटे आयीने में उसने अपना मुँह देखा। आंखें उसकी इतनी लाल क्यों हैं?”
दूसरा दृश्य : मीना बाजार यानी पतुरिया पट्टी की हीराबाई की आवक का समाचार जानते ही लहसुनवा का कामार्त्त होकर तमतमा जाना … और फिर कंपनी में नौकरी करने के बाद हीराबाई के संसर्ग की कामना में सिहरते चलना :
“हीराबाई की साड़ी धोने के बाद कठौते का पानी अत्तरगुलाब जाता है। उसमें अपनी गमछी डुबाकर छोड़ देता हूँ। लो, सूंघोगे?”
तीसरा दृश्य भक्त पलटदास का है जिसकी भक्ति में छुपी वासना की पतली सी लकीर हीराबाई को भीतर तक क्रोधित कर देती है :
“पलटदास चुपचाप गाड़ी की आसनी पर जाकर बैठ गया, हिरामन की जगह पर। हीराबाई ने पूछा, तुम भी हिरामन के साथ हो? पलटदास ने गरदन हिलाकर हामी भरी। हीराबाई फिर लेट गयी। ।।। चेहरा-मोहरा और बोली-बानी देख-सुन कार पलटदास का कलेजा कांपने लगा। न जाने क्यों। हाँ, राम लीला में सिया सुकुमारी इसी तरह थकी लेटी हुई थी। जै! सियावर रामचंद्र की जै! ।।। पलटदास के मन में जै-जैकार होने लगा। वह दास बैस्नव है। कीर्तनिया है। थकी हुई सीता महारानी के चरण टीपने की इच्छा प्रकट की उसने, हाथ की उंगलियों के इशारे से, मानो हारमोनियम की पटरियों पर नचा रहा हो। हीराबाई तमक कर बैठ गयी – अरे, पागल है क्या? जाओ, भागो…”
ब्याह की परिधि से बाहर खड़े इन तीनों युवकों के लिए स्त्री न निरी देह है, न वर्जना। वह उन्हें देह के भीतर अंगड़ाई लेती कामनाओं के ज्वार से लुभाती भी है; और डराती भी है। मजेदार बात यह है कि लोभ और भय की इस प्रक्रिया में यह स्त्री न उनकी राजदार है, न साझीदार। स्त्री की देह एक भौतिक सच्चाई की तरह उनके सामने है, लेकिन भीतर ही भीतर उसे लेकर उनके मनोभावों की दृश्यावलियां उन्हें आपत्तिजनक स्थितियों और उत्तेजक मुद्राओं से भरती चलती हैं। अपने आप को इस नए उत्तप्त रूप में देखना उसे विस्मित भी करता है और अपने पौरुष के प्रति आत्मीयतापूर्ण अभिमान भी जगाता है। दुर्भाग्यवश वह अपनी देह में होने वाले परिवर्तनों और हार्मोन के संचरण को न बायलॉजी की भाषा में समझता है, न स्त्री की दैहिक संरचना को जानता है। नैतिक वर्जनाओं और पर्देदारी के बीच उसका अज्ञान और कौतूहल स्त्री को पाने पालतू बनाने की दमित अभिलाषा में ढल जाता है। स्त्री के साथ मित्रवत व्यवहार की उन्मुक्तता बंद भारतीय समाज नहीं देता। यह बात हिरामन के लिए जितनी सही है, आज के 21वीं सदी के महानगरीय किशोर के लिए भी उतनी ही सटीक है। वैज्ञानिक दृष्टि और सह शिक्षा के बावजूद भारतीय समाज की नैतिक अवधारणाएं अभी वैचारिक जड़ता के उसी बिंदु पर खड़ी हैं। फर्क यह है कि हिरामन सरीखे ग्रामीण युवकों की ताक-झांक जैसी मासूम हरकतें आज बॉयस लॉकर रूम की चैट में सुनियोजित यौन अपराध का रूप लेती दिखाई पड़ती हैं।
“ एक तो पीठ में गुदगुदी लग रही है। दूसरे रह-रहकर चंपा का फूल खिल जाता है उसकी गाड़ी में। बैलों को डांटो तो ‘इस-बिस करने लगती है उसकी सवारी उसकी सवारी। औरत अकेली! तंबाकू बेचने वाली बूढ़ी नहीं!”
जब से हिरामन की गाड़ी में हीराबाई सवार हुई है, हिरामन की पीठ में गुदगुदी लगती रहती है। ठीक वैसे जैसे ‘अनामदास का पोथा‘ उपन्यास (हजारी प्रसाद द्विवेदी) में रैक्व की पीठ में खुजली। हिरामन के भीतर श्रुत परंपरा के जरिए भारतीय संस्कृति घर कर चुकी है,जहां प्रेम का अर्थ है स्त्री को पा लेना – चाहे युद्ध में जीत अपहरण कर, या साधना करके। भारतीय पौराणिक साहित्य में पुरुष की दृष्टि से प्रेम का इतना एकांगी एवं खंडित चित्रण किया गया है प्रेमांकुरण के लिए प्रिया की सदेह उपस्थिति, सहमति और भागीदारी जरूरी ही नहीं समझी जाती। मान लिया जाता है कि पुरुष जिसे अपने काम-विलास के लिए चुनता है, वह अनुगृहीत सी उसकी अंकशायिनी बनने को तैयार है। रूप-गुण श्रवण, चित्र/ स्वप्न दर्शन प्रेम में बावरा होने के लिए काफी हैं। दरअसल पुरुष-देह में काम के संचार को ही प्रेम की निशानी समझने की अपरिपक्व मानसिकता समाज में प्रेम का दर्शन रचती रही है। इसलिए तीस घंटे के गाड़ी के सफर के दौरान हिरामन का भोला विश्वास बार-बार अपने को दिलासा देना चाहता है कि उसकी सवारी भी उससे प्रेम कर रही है। न, सवारी कहकर वह अपमान नहीं करना चाहता क्योंकि सवारी ने ही उसे ‘मीता‘ नाम दिया है। गाड़ीवानों को पुकारने वाला औपचारिक संबोधन ‘भैया‘ नहीं। हिरामन जानता है मीता शब्द का अर्थ, इसकी कोर कोर में बुना नेह का रस। वह तो ‘अरे बाप! ई तो परी है!‘ कहकर उसके सौन्दर्य को छक कर पीना चाहता था। या चुड़ैल समझकर मारे डर के घिग्घी बंधी रही थी देर तक उसकी, जब तक जतन करके उसके पैर नहीं देख लिए कि सीधे हैं या टेढ़े। हीराबाई ने मीता क्या कहा, हिरामन का मन ‘सतरंगा छाता‘ खोलकर धीरे-धीरे खिलने लगा। कितने दिनों का हौसला पूरा हुआ है हिरामन का। ऐसे कितने सपने देखे हैं उसने। वह अपनी दुल्हन को लेकर लौट रहा है। हर गांव के बच्चे तालियां बजाकर गा रहे हैं। हर आंगन से झांक कर देख रही हैं औरतें। मर्द लोग पूछते हैं, कहाँ की गाड़ी है, कहाँ जाएगी? उसकी दुल्हन डोली का पर्दा थोड़ा सरका कर देखती है। और भी कितने सपने …!”
मैं हिरामन को आगाह कर देना चाहती हूँ कि प्यार की आकांक्षा का इंद्रधनुष दूर आसमान में ही सोहता है। जमीन पर उतारने के प्रयास में वह रंगों का नूर बेशक बरकरार रखे, धनुष की तरह खूंटी पर टंगा नहीं रह सकता। वह मुझे निरुत्तर करने के लिए अपनी पोटली से एक दृश्य निकालता है जब पास के गांव से भोजन लेकर लौटा तो कैसे हीराबाई ने अपने हाथ से उसका पत्तल बिछा दिया। पानी छींट दिया। चूड़ा निकाल कर दिया।”
हिरामन, इसमें मन का जुड़ाव कहाँ? यह तो सफर के दौरान सहयात्री के संग मिल-बैठकर वक्त काटने की जुडगते हैं।
मैं आसमान में उड़ते हिरामन को जमीन पर ले आना चाहती हूँ। जानती हूँ, उसका अगला तर्क होगा, फिर हीराबाई ने नौटंकी देखने आने का इसरार क्यों किया? इसरार किया सो किया, क्यों उसके कहने पर एक नहीं, दो नहीं, पांच-पांच अठनिया पास दे दिए।
ये सब औपचारिकताएं हैं हिरामन! यूं समझो, अपनी भलमनसाहत दर्शाने की तरकीबें! तीस घंटे के सफर में किसी की नेकनीयती और निष्कपटता दिल में खुभ जाए तो उसे असीसने का मन होता है। हिसाब-किताब और दुनियादारी से परे का व्यवहार प्रेम नहीं होता।
जानती हूँ, मेरे इस जवाब से पाठक हिरामन की तरह मायूस भर नहीं होगा। कुपित होकर आरोपों की झड़ी लगा देगा और मेरा वध करने हेतु ब्रह्मास्त्र निकाल लेगा कि कहानी के पुनर्सृजन की आड़ में मैं कहानी का कुपाठ कर रही हूँ। हिरामन और हीराबाई को अधबीच छोड़ फिलहाल यही सवाल ज्यादा मानीखेज हो गया है कि रचना का कुपाठ दरअसल है क्या बला? कि कौन फैसला करेगा, किसका पाठ कुपाठ की श्रेणी में आता है? और क्यों? क्या परंपरागत मान्यताओं के विरोध में जाकर अपनी अपेक्षाओं, मन:वृत्तियों, विश्लेषण और दृष्टिकोण के हिसाब से तर्क देते हुए भिन्न पाठ करना कुपाठ है? या वह संवेदना और विचार के नए गवाक्षों के खुलने का संकेत है जो संक्रमणशील परिस्थितियों में समय के दबाव में खुद ब खुद खुल जाते हैं?
कुपाठ के फतवे परंपरा की सुगम पगडंडियों पर आंख मूंदकर चलने के सुभीते हैं।
मैं हरचंद कोशिश कर रही हू कि ‘तीसरी कसम उर्फ मारे गये गुलफाम‘ को प्रेम-कहानी मानकर प्रेम की गहराइयों में डूब जाऊं। देखती हूँ हिरामन को कि “शाम होते ही नौटंकी का नगाड़ा बजने लगता। नगाड़े की आवाज सुनते ही हीराबाई की पुकार कानों के पास मंडराने लगती – भैया, मीता, हिरामन, उस्ताद, गुरुजी … हमेशा कोई न कोई बाजा उसके मन के कोने में बजता रहता, दिनभर। कभी हारमोनियम, कभी नगाड़ा, कभी ढोलक और कभी हीराबाई की पैंजनी। उन्हीं साजों की गत पर हिरामन उठता-बैठता, चलता-फिरता। नौटंकी कंपनी के मैनेजर से लेकर पर्दा खींचने वाले तक उस को पहचानते हैं। ।।।हीराबाई का आदमी है।”
तत्क्षण दूसरा दृश्य प्रेम के रंग को गाढ़ा करने चला आता है, जब रात के समय मेला-स्थल पर पहुंचने पर हीराबाई कहती है – सुबह होते ही रौता नाटक कंपनी में भर्ती हो जाएगी वह। “बस, एक रात! आज रात भर हिरामन की गाड़ी में रहेगी वह।” और हिरामन के ब्रह्मचर्य व्रत की गर्दन मरोड़ जिन्न की तरह हावी होता सपना गृहस्थी की बेल-बूटियों में पनाह लेने लगता है, मानो हीराबाई कह रही हो ‘आज रात भर हिरामन की गाड़ी में नहीं,घर में रहेगी वह।‘
लेकिन प्रेम का सपना प्रेम नहीं होता। प्रेम दो हृदयों के एकाकार हो जाने का गहन सम्मोहन है। यह भीतर के सूनेपन को पूरने की कोशिश है। लेकिन इस कोशिश में इतना ध्यान अवश्य रहता है कि दूसरे के भीतर का सूनापन भी उसके मिलन के चमकीले उजास में नया लिबास पहन ले। प्रेम अपनी ढपली पर अपना राग अलापने की अपरिपक्वता नहीं है। हिरामन औसत भारतीय युवक की तरह प्रेम की तासीर नहीं जानता। वह अपने हृदय की किन्ही निगूढ़ गहराइयों में गुमप्राय हो गयी प्रेम की भावना से प्रेम करता आया है। चूंकि वह स्वयं नहीं जानता कि प्रेम की कस्तूरी उसकी अपनी नाभि में कहीं गढ़ी हुई है, इसलिए उसका एहसास कराने वाली स्त्री (हीराबाई) को इसका श्रेय देकर वह उससे प्रेम करने का सपना पालता है। ‘तीसरी कसम उर्फ मारे गये गुलफाम‘ कहानी हर व्यक्ति के हृदय में पलती प्रेम की आकांक्षा से प्रेम करने की कहानी है। बेहद मासूम और निर्दोष कहानी! स्त्री तो मात्र आलंबन के रूप में उपस्थित हुई है।
रेणु जानते हैं, राजदरबार में परकीय प्रेम के कवित्त। छंद, दोहे सुनने वाले राजा-अमीर-उमरा भले ही कवियों पर सोने की अशर्फियां लुटाते हों, समाज में प्रेम की अंतिम परिणति स्वकीय प्रेम के शास्त्र में ही होती है। स्वकीय प्रेम चूंकि दांपत्य संबंध की नित्यक्रमिकता में बासी हो जाने के लिए अभिशप्त है, इसलिए परकीय प्रेम की अपेक्षा जहां वह अधिक अनुदार, बंधनयुक्त और अपेक्षापूर्ण हो जाता है, वहीं परकीय प्रेम संबंधों के भीतर लोकतांत्रिक ढांचे का हिमायती है। मुक्ति के द्वारों को खोलकर उन्मुक्त, उदार और व्यापक हो जाने का अपरिसीम साहस! स्वकीय प्रेम पितृसत्तात्मक व्यवस्था के बंधनों को साथ लिए चलता है जिसे स्त्री पर पुरुष के स्वामित्व भाव (पजेसिवनेस) और स्त्री की रक्षा के भाव में देखा जा सकता है। हिरामन का जमाने भर की नजर से बचा कर हीराबाई को बेदाग रखना और हीराबाई की मर्यादा की रक्षा के लिए नौटंकी देखने आए आगंतुकों से मारपीट करना उसके भीतर पैठी इसी ग्रंथि का उदाहरण है जो प्रेम की फेनिल फुहार के भीतर मर्दानगी की नुकीली खरोचों को भर देते हैं।
2
यदि मैं ‘तीसरी कसम उर्फ मारे गये गुलफाम‘ कहानी के लिखित पाठ तक अपने को सीमित करूँ तो देखती हूँ, हीराबाई व्यक्ति के रूप में कथा के पन्नों में नहीं झलकती। वह मुसाफिर है या नौटंकी की बाई जी। उसके समूचे व्यक्तित्व में एक पेशेवर स्त्री की सजगता है। अपने सुख-दुख को बांटने की विकलता नहीं। उसका घर-परिवार, नौटंकी पेशे में क्यों आयी, कब आयी, घर बसाने की इच्छा, पेशे में उसके खट्टे-तीते अनुभव – कहीं कोई उल्लेख नहीं। तीस घंटे के सफर में वह हिरामन से खूब बतियाती है। नाटक की रिहर्सल भी करती है। हिरामन को पसंद करती है। लेकिन उसकी ओर से हिरामन से मिलने, मिलते रहने, प्रेम (यानी ब्याह) के न संकेत हैं, न सपने। लौटते हुए हिरामन से मिलने को परेशान है तो इसलिए उसकी धरोहर (हिरामन की रुपयों की थैली) लौटाने की नैतिक जिम्मेदारी उसे विकल बनाए हुए है। कहानी में उसका होना हिरामन के भीतर प्रेम (ब्याह) की आग लहकाने के लिए है। हिरामन से प्रेम करके एक मुकम्मल प्रेम कथा बुनने के लिए नहीं।
सच्चाई यह है कि साहित्यिक हलकों में जब-जब भी ‘तीसरी कसम उर्फ मारे गये गुलफाम‘ कहानी की बात होती है, उसमें अनिवार्य रूप से ‘तीसरी कसम‘ फिल्म का उत्तरार्ध जुड़ जाता है जो कहानी में नहीं है। साथ ही फिल्म में पिरोए गये गीत, स्थिति, चरित्र, भाव और विद्रूप की व्यंजकता को बढ़ाने का काम करते हैं। कहानी का केंद्रीय पात्र यदि हिरामन है तो फिल्म हीराबाई को केंद्र में लाकर स्त्री का दैहिक शोषण करके सच्चरित्र बनी रहने वाली भारतीय संस्कृति के पाखंड को चुपके से उघाड़ जाती है।
हीराबाई और हिरामन की दुनिया में कहीं कोई समानता नहीं। हिरामन अपनी बाल-सरलता की मेंड पर उगी चालाकियों की छोटी-मोटी झरबेरी की झाड़ियों में इतना मगन है कि तिकड़म और सज्जनता की पर्देदारी में चल रहे दुनियावी व्यापार को नहीं समझता। वह तो भीतर तक निर्मल जल है। जब भी झांकता है, सबको अपने जैसा समझ अपना ही उज्जवल अक्स उसमें देख लेता है। हीराबाई ने तीस घंटे के इस सफर में इस निष्कपट युवक के अंतस का राई-रत्ती हाल ले लिया है। गप रिसाने का भेद खूब जानता है हिरामन, लेकिन यह नहीं जान पाता कि गप रिसाते-रिसाते अपने सपनों और विचारों को, मान्यताओं और शंकाओं को एक-एक कर हीराबाई के सामने खोलता चला गया है। हीराबाई दुनिया की नजर में ‘खेली खाई‘ स्त्री है। मगरमच्छों से घिरी दुनिया उसकी शरण स्थली भी है, कर्म-स्थली भी, और उसका नर्क भी। इस दुनिया से मर्मांतक जख्म लेकर जख्म देना, और अपने जख्मों पर मल्हम लगाकर अगले दिन के आहार-शिकार के लिए तैयार रहने की मजबूरियों ने उसे जितना सबल और आत्मनिर्भर बनाया है, उतना ही भीतर से दरका कर एकाकी और असुरक्षित भी किया है। हिरामन के लिए हीराबाई अजूबा है। एक ऐसी स्त्री जो फिरंगी कंपनी की मेम की तरह बाघ को वश में नहीं करती, लेकिन मेम की तरह रात-घाट में अकेले सफर कर सकती है, ‘शास्तरों‘ की बात कर सकती है, तेज-जहीन इतनी है कि एक बार सुन कर पूरा का पूरा गीत गुनगुना सकती है। तिस पर परी! भारतीय मानस के लिए परी हमेशा कामना की चीज रही है। वह सौन्दर्य का आधार और उनमुक्तता का पर्याय तो है ही, साथ ही अपनी तमाम कमनीयता में रक्षणीया (चिड़िया) होने का भाव भी जगाती है, जिसे जब-तब राक्षस पकड़ लेता है, और धरती का राजकुमार उसकी रक्षा के लिए पहुंचता है। हीराबाई उसकी भौजाई का विलोम है। उसने स्त्री को मित्र के रूप में संवाद करते कभी नहीं देखा। न ही वर्जनाओं की पोटली कहीं परे फेंक उन्मुक्त आचरण करते हुए गाड़ी का झटका लगने पर किसी पराए मर्द के कंधों पर हाथ रखते देखा है। उसने मर्यादा के नाम पर सहमी-सिकुड़ी दड़बे में बंद स्त्री को देखा है। हीराबाई का सख्य भाव उसके भीतर परिणय की गुलाबी छटा जगाता है, और राजकुमार बनकर उसकी रक्षा करने का कर्तव्यनिष्ठ भाव पैदा करता है। दुनिया भर की निगाह से बचाकर हीराबाई को नौटंकी कंपनी तक पहुंचा आना मानो उसकी अग्निपरीक्षा है। हीराबाई हिरामन का हौसला भी जानती है, और बूता भी। हिरामन उसके थके अरक्षित मन को भावनात्मक सुरक्षा की छांह देता है। वह न समंदर की लहरों की सवारी करना चाहती है, न आसमान की बुलंदियां नापना चाहती है। घर की देहरी के भीतर किसी की दुल्हन बन कर जिन्दगी जी लेने का सपना किसी भी किशोरी कुमारी की तरह आज भी अंदर धड़कता है। हिरामन उसका कूल किनारा है, भटकते जहाज का लंगर!
मैं फिल्म देखती जा रही हूँ और प्रेम की रिमझिम में भीगते हुए महसूस कर रही हूँ कि हां, प्रेम अपने-अपने अभाव को पूरने की कोशिश ही तो है। दरअसल साहित्य भी अपने पहले चरण में पाठक के लिए अभावपूर्ति का स्वप्न बनकर आता है। साहित्य उसे उसके कुत्सित यथार्थ से साक्षात्कार भी कराता है, और उससे उबरने के संघर्ष में कथा-चरित्रों के जरिए विरेचन का सुख भी देता है। लेकिन साहित्य की अपील स्थिति के प्रथम दर्शन तक जाकर ही समाप्त नहीं होती, वरन् वहीं से शुरू होती है। इस बार लेखक और कथा-पात्रों के हस्तक्षेप से अलग बिल्कुल अकेले! गुपचुप! अपने ही अंतर में वह नहीं जान पाता कि कथा के प्रभाव ने उसे अपने परिवेश के प्रति इतना संवेदनशील बनाया है या अपने परिवेश के प्रति उसकी सतत संवेदनशील दृष्टि ने कहानी के प्रभाव को गहराया है। लेकिन इतना सच है कि एक-दूसरे की संगति में अपनी संवेदना और वैचारिकता को तीक्ष्ण करते हुए वह कथागत पात्र पर नहीं, कथागत पात्र का निर्माण करने वाली सामाजिक-सांस्कृतिक मान्यताओं, अवधारणाओं, सच्चाइयों पर विचार करने लगता है। रसलोभी पाठक कथा को सूंघता भर है। रसविश्लेषक पाठक कथा के समय में अपने समय के सच को मिलाकर अपनी अंतर्वृत्तियों और विजन के सहारे बेहतर समय के सच तक पहुंचने की पगडंडियां बनाने की जुगत करता है। ठीक कथाकार की तरह। पगडंडियं बनाने की बेचैनी पैदा होना संवेदनशील पाठक को मननशील नागरिक (चेतना) में तब्दील करती है। साहित्य से क्रांति की अपेक्षा करना गुजरे जमाने की ओवररेटेड अपेक्षा है। अलबत्ता आज उसका लक्ष्य यही है कि वह नागरिक चेतना का विकास कर जिम्मेदार पीढ़ी पैदा कर सके।
बहस तलब बात यह भी हो सकती हैं कि कहानी का प्रभाव क्या कहानी में ही कहीं निहित है? यदि हां, तो कहाँ? और क्यों सभी पाठक उस प्रभाव को समान भाव से ग्रहण नहीं कर पाते? क्या पाठक का प्रभाव पाठक के अपने बोध के स्तर में होता है? जाहिर है बोध को बनाने में परिवेश, संवेदना, वैचारिकता, विश्लेषण क्षमता और सृजनात्मकता की भूमिका अहम रहती है। यदि सारा मामला पाठक के बोध पर ही निर्भर करता है, तो कहानी/साहित्य की क्या अहमियत है? सवाल यह भी है कि क्या प्रभाव कहानीकार की दृष्टि में निहित है? उसके संवेदनात्मक वैचारिक दर्शन का कुल निचोड़? अच्छी कहानी सतह पर चहती-महकती भले ही दिखती हो, उस की बुनियादी संरचना सतह से नीचे चलती पनडुब्बी की तरह है जो समय के अध्ययन-चिंतन-मनन की गहराइयों में जाकर भीतरी दरारों में छिपे अमूर्त से वायरस को पकड़ लाती है। मैं रसलोभी पाठक की तरह कहानी का पाठ करती हूँ तो हिरामन की सादगी और सपनों पर लट्टू हो जाती हूँ। आसपास के आपाधापी भरे बेईमान माहौल में हिरामन का होना मुझे यूटोपिया में विचरने का सुख देता है। सब हिरामन जैसे हों – मेरे अंतस् से आह फूटती है, और अपने पैरों पर पानी डाले बगैर मैं आह्लाद के समंदर में दूर तक तैर आती हूँ। साहित्य सुख (मनोरंजन) नहीं है। वह संस्कार है। अतः मैं अपने आपको दूसरी भूमिका – रसविश्लेषक – के लिए तैयार करती हूँ। पाठ के साथ बहती हूँ, चरित्रों के भीतर उतरती हूँ और हीराबाई की अव्यक्त व्यथा को उसके सारे पारिवारिक-सामाजिक संदर्भों के साथ अपने मस्तिष्क में बुनने लगती हूँ।
हीराबाई यानी ‘पिंजरे वाली मुनिया‘! फिल्म में गीत (‘चलत चलत मुसाफिर मोह लियो रे पिंजरे वाली मुनिया‘) का उपयोग खासा प्रतीकात्मक है। पुरुष के संदर्भ में स्त्री की सेक्सुएलिटी पर कटाक्ष करने के बहाने अपनी मर्दानगी और बेचारगी का दंभ भरा ऐलान! स्त्री के संदर्भ में कुलीनता की चौहद्दिओं में घिरी स्त्री की माल की तरह सरेबाजार बिकने की बेबसी। कोठे पर बैठी अपने हुनर से महफिलें सजाती या नौटंकी में नाचती-गाती स्त्री स्वतंत्र दिखती है; स्वतंत्र है नहीं। अदृश्य पिंजरा उसे चारों ओर से घेरकर संग-संग चलता है। कहानी की तरह फिल्म भी लाउड नहीं है। मंथर गति से बहती नदी की अविराम कलकल में शांत-स्तब्ध प्रकृति की अंदरूनी हलचलों को सुनने की धीर संवेदना से पकी हुई। हीराबाई घर से हाट-बाजार तक पहुंचने की कथा स्वयं नहीं कहती, लेकिन ‘सजनवा बैरी हो गये हमार! चिठिया हो तो हर कोई बांचे, भाग न बांचे कोई। करमवा बैरी हो गये हमार!‘ गीत के दौरान जिस प्रकार बतरस में डूबी हीराबाई धीरे-धीरे गीत के बोलों के साथ आत्मस्थ होती चलती है, और आंखों की भीगी कोर के जरिए आत्मा की अंदरूनी तहों तक पैठ गये दुख की छाया में घिरती है, उससे सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि प्यार में प्रवंचना या किसी परिवार जन के देह-शोषण या गरीबी की गहरी मार ने उसे यहां तक पहुंचाया होगा। नौटंकी में नाचना उसकी चुनी हुई जिन्दगी नहीं है। थोपे हुए अभिशाप की काली छाया है। हीराबाई जैसी स्त्रियों को रेड लाइट एरिया में लाकर बैठाना पितृसत्तात्मक व्यवस्था की मजबूरी है क्योंकि पुरुष-वासना की गंदगी बहाने के लिए उसे नालियों की जरूरत है। रेणु की कलम की ताकत यह है कि सतह पर वे हीराबाई-हिरामन प्रेम-कथा को रसिक-भाव से सुनाते हैं, (गप रिसाने की कला हिरामन ने उन्हीं से पाई है) और सतह के नीचे सजग समाजशास्त्री की तरह सामाजिक यथार्थ की चीर-फाड़ करते दिखाई देते हैं। कहानी से अलग फिल्म में जमींदार की नए चरित्र के रूप में उपस्थिति इसका प्रमाण है। सादगी रेणु की खासियत है। वे रूढ़ छवियों को छोड़ते नहीं। उन्हें ठीक उसी रूप में प्रयुक्त कर स्थितियों को ऐसा अप्रत्याशित मोड़ देते हैं कि पाठक स्वयं बिलबिला उठता है। जमींदार अन्य जमीदारों जैसा ही है – रंगीला, दंभी, क्रूर! साम दाम दंड भेद उसके व्यक्तित्व का कुल सार! स्त्री क्या, मनुष्य की गरिमा भी उसके अहंकार के सामने बौनी-बेमानी! पैसे और ताकत के बल पर क्या नहीं पाया जा सकता? फिर बाई जी का शरीर!! राग, प्रेम, संवेदन, इच्छा, सहमति जैसी शब्दावली कमजोरों का शास्त्र गढ़ती है। इसलिए गाड़ीवान की सुधि में सुध-बुध खोई हीराबाई को होश में लाने का एक ही उपाय है – गाड़ीवान को रास्ते से हटा देना! पहले धमकी देकर। फिर जरूरत पड़े तो अमलीजामा पहनाकर। देखा जाए तो जमीदार की एंट्री कहानी की गंभीरता को मसाला फिल्म के प्रिडिक्टेबल सतहीपन में रिड्यूस कर देती है। और प्रेम-कथा को वियोग के अंतिम बिंदु पर लाकर कुलीन बनाम बाजारू स्त्री की बायनरी को यथावत् बनाए रखती है, जिस की तासीर तेल-पानी की तरह अपनी-अपनी हदों में रहने की है, घुल-मिलकर एक हो जाने की नहीं।
हीराबाई के संवाद – ‘हम हमेशा लैला का पार्ट अदा करेंगे। लैला बन नहीं सकेंगे‘ – को मैं फिल्म की स्क्रिप्ट से अपने कथन की पुष्टि में उठाती हूँ, लेकिन रस विश्लेषक पाठक की भूमिका में स्थितियों को जस का तस स्वीकारने को बाध्य नहीं होती। मैं स्थितियों के साथ गुफ्तगू करते हुए उनकी स्वाभाविक चाल को थोड़ा सा मोड़ दे देती हूँ। तब मेरे सामने यह स्थिति दो भिन्न-भिन्न रूपों में सवाल बनकर आती है। एक, यदि लैला का पार्ट करने वाली हीराबाई असल जिन्दगी में हिरामन की लैला ( पत्नी) बन कर उसी में समा जाती, तो? दूसरे, यदि हीराबाई नौटंकी की बाई जी न होकर किसी सद्गृहस्थ परिवार की एक सामान्य लड़की होती, तो?
सबसे पहले पहला सवाल। लेकिन इस पर बात करने से पहले यह रेखांकित करना जरूरी है कि फिल्म के उत्तरार्ध में हिरामन की क्रमश: कम होती उपस्थिति हीराबाई को केंद्र में लाने के लिए इतनी नहीं है, जिसने उसे (हिरामन को) कुछ सुविधाजनक सवालों से दूर रखने के लिए है। रेणु की नीयत पर शक करने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन हिरामन की निश्छलता के प्रति लेखक की अतिरिक्त सहानुभूति पूरी कहानी में पक्षपातपूर्ण गंध की तरह मौजूद है। यही नहीं, प्रेम-प्रवंचित दिखाकर रेणु ने पाठकीय सहानुभूति भी उसकी झोली में डालने की कोशिश की है। स्त्री को ‘ठगिनी‘ और बाईजी को ‘प्यार की व्यापारी‘ मानने वाली संस्कृति की अपेक्षाओं के अनुरूप ही है यह निष्कर्ष। स्टेशन से लौटते हुए हिरामन चोट खाए विक्षिप्त से भिन्न नहीं है। क्रोध और प्रवंचना, मोह और अविश्वास की उस नि:संज्ञ अवस्था में वह स्त्री सवारी की लदनी न करने की भावाकुल कसम खाकर स्वयं को ऊंचे दर्जे का प्रेमी सिद्ध कर सकता है; लेकिन अपने से कभी सवाल पूछने की नैतिक हिम्मत और परिपक्व समझदारी नहीं पा सकता की कहीं हीराबाई के पलायन में उसके (हिरामन) दब्बू व्यक्तित्व की भूमिका तो नहीं थी?
हिरामन हीराबाई के साथ घर बसाने के सपने देखता है; हीराबाई को उन सपनों का साझीदार बनाकर विवाह का प्रस्ताव नहीं रखता, यद्यपि संभावित वधू को लेकर परंपरागत भारतीय पुरुष की प्राथमिकता – कुमारी कन्या/यौन शुचिता – को वह अपनी अल्प बुद्धि से पहले ही जान चुका है। हीराबाई हिरामन की दुविधा और कायरता दोनों को अच्छी तरह से जानती है। वह जानती है कि स्त्री को देवी कहकर पूजने वाला पुरुष ही उसे वेश्या बना कर दुत्कारने में कोर-कसर नहीं छोड़ता। हिरामन अपने समय का अक्स है। समय का विद्रोही रचयिता नहीं। वेश्या और देवी यानी देह और देहातीत हो जाने के बीच स्त्री हाड-मांस की इंसान के रूप में उसके सामने कभी नहीं आती। यदि हिरामन दुर्बल न होकर विद्रोही होता, तो भी हीराबाई का उस पर भरोसा करना कठिन था क्योंकि समाज जितनी सहजता से घर की चौखट से स्त्री को बाहर निकाल देता है, उतनी तत्परता से उसे वापस चौखट में दाखिल होने नहीं देता। पत्नी की मर्यादा की रक्षा के लिए सर्वशक्तिमान राम ही जब लोकापवाद से टक्कर नहीं ले पाए तो एक मामूली युवक की क्या बिसात! पौराणिक कथाएं भारतीय-मानस को जिस अनुपात में नियतिवादी बनाती हैं, उसी अनुपात में उसकी निष्क्रियता को बढ़ाते हुए कूप मंडूक भी बना देती हैं।
लेकिन यहीं एक और संभावना सिर उठाने लगती है। मान लें कि घर-समाज के विरोध के बावजूद हिरामन हीराबाई से ब्याह कर लेता है, तब उनके संबंध का स्वरूप क्या रहेगा? हीराबाई से यह अपेक्षा करना वृथा होगा कि भौजाई की तरह मुँह सी कर, आंख पर पट्टी बांधकर वह सिर्फ़ काम और काम करती रहे। एक नई ज़िंदगी के उछाह में भले ही शुरु-शुरु में अपने प्रवाह के विरुद्ध तैरना भला लगता हो, लेकिन धीरे-धीरे जब नशा उतरता है तो बरसों पुरानी दिनचर्या आदत की तरह मान-प्राण पर हावी हो जाती है। नृत्य हीराबाई का पेशा है, लेकिन हर पेशेवर स्त्री का पैशन भी होती है कला। पारंपरिक भारतीय समाज स्त्रियों को हॉबी और पैशन के लिए स्पेस देना नहीं जानता। ऐसे में क्या संभावना नहीं कि ‘आँधी’ फ़िल्म की नायिका की तरह हीराबाई भी प्रोफैशनल ज़िंदगी की उन्मुक्तता, निजता और आत्मसम्मान को तरजीह देने लगे। मैं यहाँ अभिनेत्री हंसा वाडेकर की ज़िंदगी पर बनी फ़िल्म ‘भूमिका’ का भी स्मरण कर लेना चाहती हूँ जहाँ गृहस्थी और प्रोफ़ेशन मृगतृष्णा बन कर एकबारगी घर की चौखट के बाहर खड़ा कर दी गयी इस स्त्रियों को छलती रहती है।
अब दूसरा विकल्प! पारंपरिक भारतीय समाज में युवक-युवती के बीच वर्जनामुक्त मैत्री संबंध की स्वीकृति नहीं है। अलबत्ता समाज की नज़र बचाकर भांडा फूटने तक गुपचुप प्रेम और यौन संबंध पनप सकते हैं। प्रेम को अक्सर चरित्रहीनता का लक्षण समझा जाता है। इसलिए प्रेम में ‘पकड़ी’ गयी युवती आनन-फ़ानन में ब्याह भी जाती है – सामाजिक शर्म को छुपाने के लिए। पुरुष के लिए तो खैर वह अतिरिक्त योग्यता है। यानी संबंध विच्छेद/ विरह दोनों स्थितियों में अनिवार्य है क्योंकि यह व्यवस्था के वर्चस्व को अनंतिम बनाए रखने का मुफ़ीद इलाज है।
प्रेम को स्त्री के संदर्भ में आज भी ग्रामीण समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता है क्योंकि यह सशक्त स्त्री की अवधारणा को ख़तरे की तरह समाज के पटल पर रखता है। प्रेम करने, प्रेम का ऐलान करने, प्रेम को विवाह तक पहुँचाने के लिए संघर्ष करने वाली स्त्री ‘गाय’ (मूक) स्त्री के बिंब को तोड़ कर आत्मनिर्णय संपन्न गतिशील स्त्री की छवि को गढ़ती है जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था और सामंती ढांचे दोनों के लिए घातक है।
लेकिन कहानी के पाठ से इतनी दूर चलकर विचार करने की परंपरा हिंदी जगत में नहीं है। मान लिया जाता है कि कहानी में उतरना ही देखें, जितना लेखक दिखा रहा है; उतनी ही अपेक्षा करें जितना लेखक का युग-समाज उससे बोध और दृष्टि के नाम पर दे रहा है। अपने वक्त की अपेक्षाओं और ज़मीन पर खड़ा हो कर पाठक कहानी की गूंज से बाहर छूट गयी घुटी आवाजों को ना सुने। साहित्य अपनी दीर्घायु के लिए सजग कलाकार और आलोचक के विश्लेषणात्मक विवेक की जुगलबंदी पर निर्भर करता है। कहानीकार का जगत के प्रति विश्लेषण अनुभूति और प्रभाव की शक्ल में रचना में आता है। आलोचक उस प्रभाव के जरिए अपनी दृष्टि से विश्लेषण की जमीन पर पैर टिका कर समय के मनोविज्ञान को पकड़ने की कोशिश करता है। आलोचक की दृष्टिगत भिन्नता रचना के पाठ को विश्लेषण और पुनर्सृजन के नए आयाम तक ले जाती है। इसलिए मूल रचना आलोचक के जरिए न केवल नवा होती है, बल्कि अपनी प्रारंभिक स्थापनाओं से दूर आकर स्वयं को नए अर्थों (सज्जा) में देखने का रोमांचक सुख भी पाती है। उदाहरण के लिए ‘ईदगाह’ कहानी को वात्सल्य एवं कर्तव्यपरायणता की कहानी न मानकर उपभोक्ता संस्कृति के प्रतिरोध की कहानी मानना; या ‘पुरस्कार’ कहानी को प्रेम कहानी न मानकर भूमि अधिग्रहण कानून के विरोध में उठी आवाज मानना। यदि कहानी पात्र और घटनाओं के मकड़जाल से मुक्त कर पाठक को अपने समय और व्यवस्था की खुर्दबीनी जांच के लिए विकल करती है तो यह कहानी से पाठक का भटकाव नहीं, कहानी की ताकत है और लेखक की आंतरिक इच्छा भी। यह मानकर चलना होगा लेखक गृहिणी/हलवाई नहीं कि रिमझिम होते ही कड़ाही चढ़ाकर समोसे-जलेबी छानने लगे। वह उर्वर होते रहने की आकांक्षा में सदा नमी ग्रहण करने को आतुर जमीन है जो बूंद-बूंद पानी सोख कर उसे दूर-दूर तक अपने गर्भ में फैली जड़ों के जाल तक पहुँचा देती है। ‘तीसरी क़सम उर्फ मारे गये गुलफ़ाम’ दरअसल प्रेम के बहाने समाज-व्यवस्था के विधि-विधानों को समझने की कॉमन सेंस है। प्रेम अपनी मूल प्रकृति में मनुष्य के भीतर बंद पड़ी नालियों को खोलकर समंदर के उमड़ने का आह्वान करता है। ऐसे में मनुष्य की गरिमा की रक्षा की अपेक्षा सामाजिक मर्यादाओं की रक्षा का क्या औचित्य?
पुनश्च : गाड़ी हांकते हिरामन की मद्धम बड़बड़ाहट तमाम दूरियां लांघकर मेरे कानों में घुली जा रही हैं। ‘बहुत भरमाया प्यार ने, पर समझ नहीं पाया इसका मरम! कभी लगता है, प्यार के एक महीन धागे में छुपे हैं कई-कई रेशे सूत – गुस्सा भी, नफरत भी; उम्मीद भी, चाहत भी; रूठना भी, मनाना भी; सांस भी, सांसत भी।’
‘कभी लगता है, शायद कोई अनछुई आस है प्यार!! अपनी ही हदबंदियों को तोड़ने की अतृप्त अधूरी छलांग!’
‘कभी लगता है, अपरंपार है प्यार! जिन खोजा तिन पाइयां!’ और अचानक कपाल पर हाथ मार वह ठठा कर हंस पड़ा – ‘और मैं ।।। अपने मान के अहंकार में किसी के दरद को न बूझ सका। बस, इतना कहना चाहता हूँ कि आज मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष है प्रेम और विश्वास के तंतुओं से रची दुनिया को बचाना।’

रोहिणी अग्रवाल
हिंदी उपन्यास में कामकाजी महिला,एक नज़र कृष्णा सोबती पर, इतिवृत्त की संरचना और संरूप,
समकालीन कथा साहित्य : सरहदें और सरोकार, स्त्री लेखन : स्वप्न और संकल्प,साहित्य की ज़मीन और स्त्री मन के उच्छ्वास,हिंदी कहानी : वक़्त की शिनाख्त और सृजन का राग,हिंदी उपन्यास का स्त्री पाठ,साहित्य का स्त्री स्वर,हिंदी उपन्यास : समय से संवाद,कथालोचना के प्रतिमान (आलोचना);घने बरगद तले,आओ माँ हम परी हो जाएं (कहानी संग्रह) प्रकाशित।
हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा कहानी एवं आलोचना पर तीन बार स्पंदन आलोचना सम्मान,
वनमाली कथा आलोचना सम्मान,रेवांत मुक्तिबोध सम्मान,डॉक्टर शिव कुमार मिश्र स्मृति सम्मान,डॉक्टर रामविलास शर्मा स्मृति सम्मान,नारी शक्ति सम्मान।
सम्प्रति:रिटायर्ड प्रोफेसर, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक।
सम्पर्क: rohini1959@gmail.com +919416053847
.